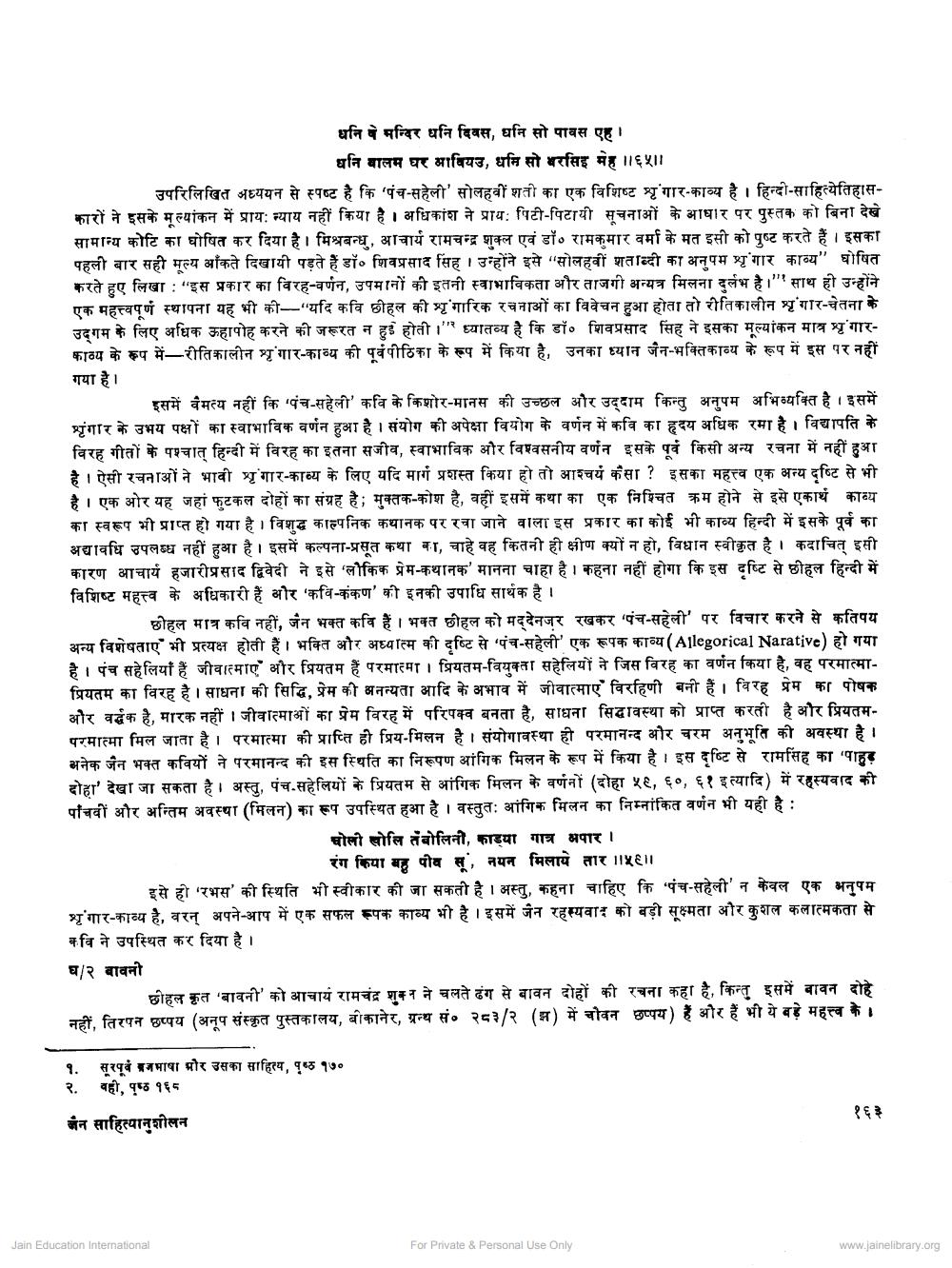________________
धनि वे मन्दिर धनि दिवस, धनि सो पावस एह।
धनि बालम घर आवियउ, धमि सो बरसिइ मेह ॥६५॥ उपरिलिखित अध्ययन से स्पष्ट है कि 'पंच-सहेली' सोलहवीं शती का एक विशिष्ट शृगार-काव्य है । हिन्दी-साहित्येतिहासकारों ने इसके मूल्यांकन में प्राय: न्याय नहीं किया है। अधिकांश ने प्राय: पिटी-पिटायी सूचनाओं के आधार पर पुस्तक को बिना देखे सामान्य कोटि का घोषित कर दिया है। मिश्रबन्धु, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं डॉ. रामकुमार वर्मा के मत इसी को पुष्ट करते हैं । इसका पहली बार सही मूल्य आँकते दिखायी पड़ते हैं डॉ. शिवप्रसाद सिंह । उन्होंने इसे “सोलहवीं शताब्दी का अनुपम शृगार काव्य" घोषित करते हुए लिखा : “इस प्रकार का विरह-वर्णन, उपमानों की इतनी स्वाभाविकता और ताजगी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। साथ ही उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण स्थापना यह भी की-“यदि कवि छीहल की शृगारिक रचनाओं का विवेचन हुआ होता तो रीतिकालीन शृगार-चेतना के उद्गम के लिए अधिक ऊहापोह करने की जरूरत न हुई होती।" ध्यातव्य है कि डॉ. शिवप्रसाद सिंह ने इसका मूल्यांकन मात्र शृगारकाव्य के रूप में-रीतिकालीन शृगार-काव्य की पूर्वपीठिका के रूप में किया है, उनका ध्यान जैन-भक्तिकाव्य के रूप में इस पर नहीं गया है।
इसमें वैमत्य नहीं कि 'पंच-सहेली' कवि के किशोर-मानस की उच्छल और उद्दाम किन्तु अनुपम अभिव्यक्ति है । इसमें श्रृंगार के उभय पक्षों का स्वाभाविक वर्णन हुआ है । संयोग की अपेक्षा वियोग के वर्णन में कवि का हृदय अधिक रमा है। विद्यापति के विरह गीतों के पश्चात् हिन्दी में विरह का इतना सजीव, स्वाभाविक और विश्वसनीय वर्णन इसके पूर्व किसी अन्य रचना में नहीं हुआ है । ऐसी रचनाओं ने भावी शृगार-काव्य के लिए यदि मार्ग प्रशस्त किया हो तो आश्चर्य कैसा? इसका महत्त्व एक अन्य दृष्टि से भी है । एक ओर यह जहां फुटकल दोहों का संग्रह है ; मुक्तक-कोश है, वहीं इसमें कथा का एक निश्चित कम होने से इसे एकार्थ काव्य का स्वरूप भी प्राप्त हो गया है। विशुद्ध काल्पनिक कथानक पर रचा जाने वाला इस प्रकार का कोई भी काव्य हिन्दी में इसके पूर्व का अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है। इसमें कल्पना-प्रसूत कथा का, चाहे वह कितनी ही क्षीण क्यों न हो, विधान स्वीकृत है। कदाचित् इसी कारण आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे 'लौकिक प्रेम-कथानक' मानना चाहा है । कहना नहीं होगा कि इस दृष्टि से छीहल हिन्दी में विशिष्ट महत्त्व के अधिकारी हैं और 'कवि-कंकण' की इनकी उपाधि सार्थक है।
छोहल मात्र कवि नहीं, जैन भक्त कवि हैं । भक्त छोहल को मद्देनजर रखकर 'पंच-सहेली' पर विचार करने से कतिपय अन्य विशेषताएं भी प्रत्यक्ष होती हैं। भक्ति और अध्यात्म की दृष्टि से 'पंच-सहेली' एक रूपक काव्य (Allegorical Narative) हो गया है। पंच सहेलियाँ हैं जीवात्माएं और प्रियतम हैं परमात्मा। प्रियतम-वियुक्ता सहेलियों ने जिस विरह का वर्णन किया है, वह परमात्माप्रियतम का विरह है। साधना की सिद्धि, प्रेम की अनन्यता आदि के अभाव में जीवात्माएं विरहिणी बनी हैं। विरह प्रेम का पोषक
और वर्द्धक है, मारक नहीं । जीवात्माओं का प्रेम विरह में परिपक्व बनता है, साधना सिद्धावस्था को प्राप्त करती है और प्रियतमपरमात्मा मिल जाता है। परमात्मा की प्राप्ति ही प्रिय-मिलन है। संयोगावस्था ही परमानन्द और चरम अनुभूति की अवस्था है । अनेक जैन भक्त कवियों ने परमानन्द की इस स्थिति का निरूपण आंगिक मिलन के रूप में किया है । इस दृष्टि से रामसिंह का 'पाहुड दोहा' देखा जा सकता है। अस्तु, पंच.सहेलियों के प्रियतम से आंगिक मिलन के वर्णनों (दोहा ५६, ६०, ६१ इत्यादि) में रहस्यवाद की पाँचवीं और अन्तिम अवस्था (मिलन) का रूप उपस्थित हआ है । वस्तुत: आंगिक मिलन का निम्नांकित वर्णन भी यही है :
घोली खोलि तंबोलिनी, काड्या गात्र अपार ।
रंग किया बड्ड पीव सू, नयन मिलाये तार |५६।। इसे ही 'रभस' की स्थिति भी स्वीकार की जा सकती है । अस्तु, कहना चाहिए कि “पंच-सहेली' न केवल एक अनुपम शृंगार-काव्य है, वरन् अपने-आप में एक सफल रूपक काव्य भी है। इसमें जैन रहस्यवाद को बड़ी सूक्ष्मता और कुशल कलात्मकता से कवि ने उपस्थित कर दिया है। घ/२ बावनी
छोहल कृत 'बावनी' को आचार्य रामचंद्र शुक्न ने चलते ढंग से बावन दोहों की रचना कहा है, किन्तु इसमें बावन दोहे नहीं, तिरपन छप्पय (अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, ग्रन्थ सं० २८३/२ (झ) में चौवन छप्पय) हैं और हैं भी ये बड़े महत्त्व के।
१. सरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, पृष्ठ १७० २. वही, पृष्ठ १६८ जैन साहित्यानुशीलन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org