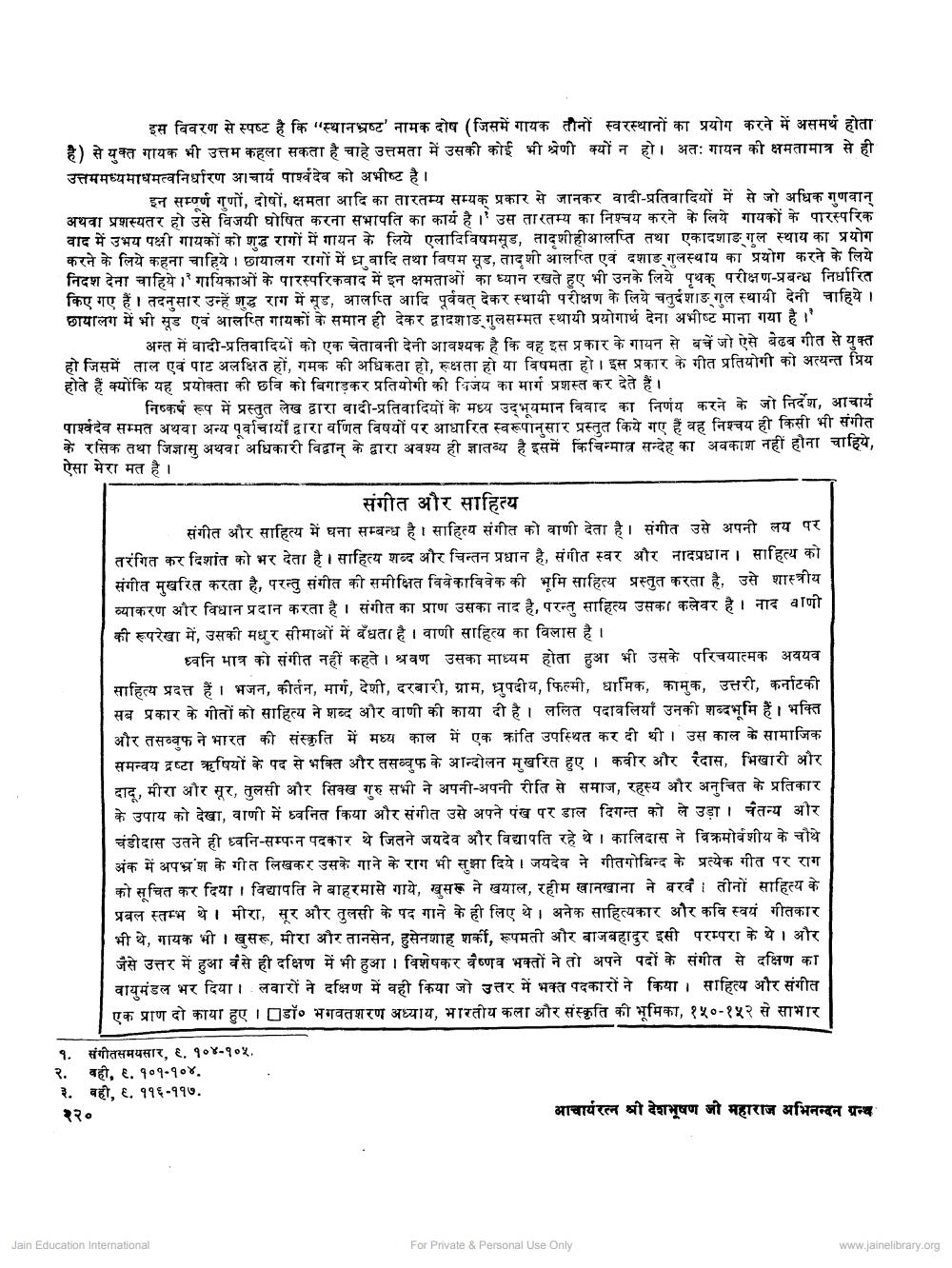________________
इस विवरण से स्पष्ट है कि "स्थानभ्रष्ट' नामक दोष (जिसमें गायक तीनों स्वरस्थानों का प्रयोग करने में असमर्थ होता है) से युक्त गायक भी उत्तम कहला सकता है चाहे उत्तमता में उसकी कोई भी श्रेणी क्यों न हो। अतः गायन की क्षमतामात्र से ही उत्तममध्यमाधमत्वनिर्धारण आचार्य पार्श्वदेव को अभीष्ट है।
इन सम्पूर्ण गणों, दोषों, क्षमता आदि का तारतम्य सम्यक प्रकार से जानकर वादी-प्रतिवादियों में से जो अधिक गुणवान् अथवा प्रशस्यतर हो उसे विजयी घोषित करना सभापति का कार्य है। उस तारतम्य का निश्चय करने के लिये गायकों के पारस्परिक वाद में उभय पक्षी गायकों को शुद्ध रागों में गायन के लिये एलादिविषमसूड, तादृशीहीआलप्ति तथा एकादशाङ्गुल स्थाय का प्रयोग करने के लिये कहना चाहिये। छायालग रागों में ध्र वादि तथा विषम सूड, तादृशी आलप्ति एवं दशाङ गलस्थाय का प्रयोग करने के लिये निदश देना चाहिये। गायिकाओं के पारस्परिकवाद में इन क्षमताओं का ध्यान रखते हुए भी उनके लिये पृथक् परीक्षण-प्रबन्ध निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार उन्हें शुद्ध राग में सूड, आलप्ति आदि पूर्ववत् देकर स्थायी परीक्षण के लिये चतुर्दशाङ्गुल स्थायी देनी चाहिये। छायालग में भी सूड एवं आलप्ति गायकों के समान ही देकर द्वादशाङ्गुलसम्मत स्थायी प्रयोगार्थ देना अभीष्ट माना गया है।
अन्त में वादी-प्रतिवादियों को एक चेतावनी देनी आवश्यक है कि वह इस प्रकार के गायन से बचें जो ऐसे बेढब गीत से युक्त हो जिसमें ताल एवं पाट अलक्षित हों, गमक की अधिकता हो, रूक्षता हो या विषमता हो। इस प्रकार के गीत प्रतियोगी को अत्यन्त प्रिय होते हैं क्योंकि यह प्रयोक्ता की छवि को बिगाड़कर प्रतियोगी की विजय का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।
निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत लेख द्वारा वादी-प्रतिवादियों के मध्य उदभयमान विवाद का निर्णय करने के जो निदंश, आचार्य पार्श्वदेव सम्मत अथवा अन्य पूर्वाचार्यों द्वारा वणित विषयों पर आधारित स्वरूपानुसार प्रस्तुत किये गए हैं वह निश्चय ही किसी भी संगीत के रसिक तथा जिज्ञासु अथवा अधिकारी विद्वान् के द्वारा अवश्य ही ज्ञातव्य है इसमें किचिन्मात्र सन्देह का अवकाश नहीं होना चाहिये, ऐसा मेरा मत है।
संगीत और साहित्य संगीत और साहित्य में घना सम्बन्ध है। साहित्य संगीत को वाणी देता है। संगीत उसे अपनी लय पर तरंगित कर दिशांत को भर देता है। साहित्य शब्द और चिन्तन प्रधान है, संगीत स्वर और नादप्रधान । साहित्य को संगीत मुखरित करता है, परन्तु संगीत की समीक्षित विवेकाविवेक की भूमि साहित्य प्रस्तुत करता है, उसे शास्त्रीय व्याकरण और विधान प्रदान करता है। संगीत का प्राण उसका नाद है, परन्तु साहित्य उसका कलेवर है। नाद वाणी की रूपरेखा में, उसकी मधुर सीमाओं में बँधता है । वाणी साहित्य का विलास है ।
ध्वनि मात्र को संगीत नहीं कहते । श्रवण उसका माध्यम होता हुआ भी उसके परिचयात्मक अवयव साहित्य प्रदत्त हैं। भजन, कीर्तन, मार्ग, देशी, दरबारी, ग्राम, ध्रुपदीय, फिल्मी, धार्मिक, कामुक, उत्तरी, कर्नाटकी सब प्रकार के गीतों को साहित्य ने शब्द और वाणी की काया दी है। ललित पदावलियाँ उनको शब्दभूमि हैं। भक्ति और तसव्वुफ ने भारत की संस्कृति में मध्य काल में एक क्रांति उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामाजिक समन्वय द्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति और तसव्वुफ के आन्दोलन मुखरित हुए। कवीर और रैदास, भिखारी और दादू, मीरा और सूर, तुलसी और सिक्ख गुरु सभी ने अपनी-अपनी रीति से समाज, रहस्य और अनुचित के प्रतिकार के उपाय को देखा, वाणी में ध्वनित किया और संगीत उसे अपने पंख पर डाल दिगन्त को ले उड़ा। चैतन्य और चंडीदास उतने ही ध्वनि-सम्पन्न पदकार थे जितने जयदेव और विद्यापति रहे थे। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय के चौथे अंक में अपभ्रंश के गीत लिखकर उसके गाने के राग भी सुझा दिये । जयदेव ने गीतगोबिन्द के प्रत्येक गीत पर राग को सूचित कर दिया। विद्यापति ने बाहरमासे गाये, खुसरू ने खयाल, रहीम खानखाना ने बरवं। तीनों साहित्य के प्रबल स्तम्भ थे। मीरा, सूर और तुलसी के पद गाने के ही लिए थे। अनेक साहित्यकार और कवि स्वयं गीतकार भी थे, गायक भी । खुसरू, मीरा और तानसेन, हुसेनशाह शर्की, रूपमती और बाजबहादुर इसी परम्परा के थे। और जैसे उत्तर में हुआ वैसे ही दक्षिण में भी हुआ। विशेषकर वैष्णव भक्तों ने तो अपने पदों के संगीत से दक्षिण का वायुमंडल भर दिया। लवारों ने दक्षिण में वही किया जो उत्तर में भक्त पदकारों ने किया। साहित्य और संगीत एक प्राण दो काया हुए। डॉ. भगवतशरण अध्याय, भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, १५०-१५२ से साभार
१. संगीतसमयसार, ६. १०४-१०५. २. वही, ६.१०१-१०४. ३. वही, ६. ११६-११७.
१२०
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org