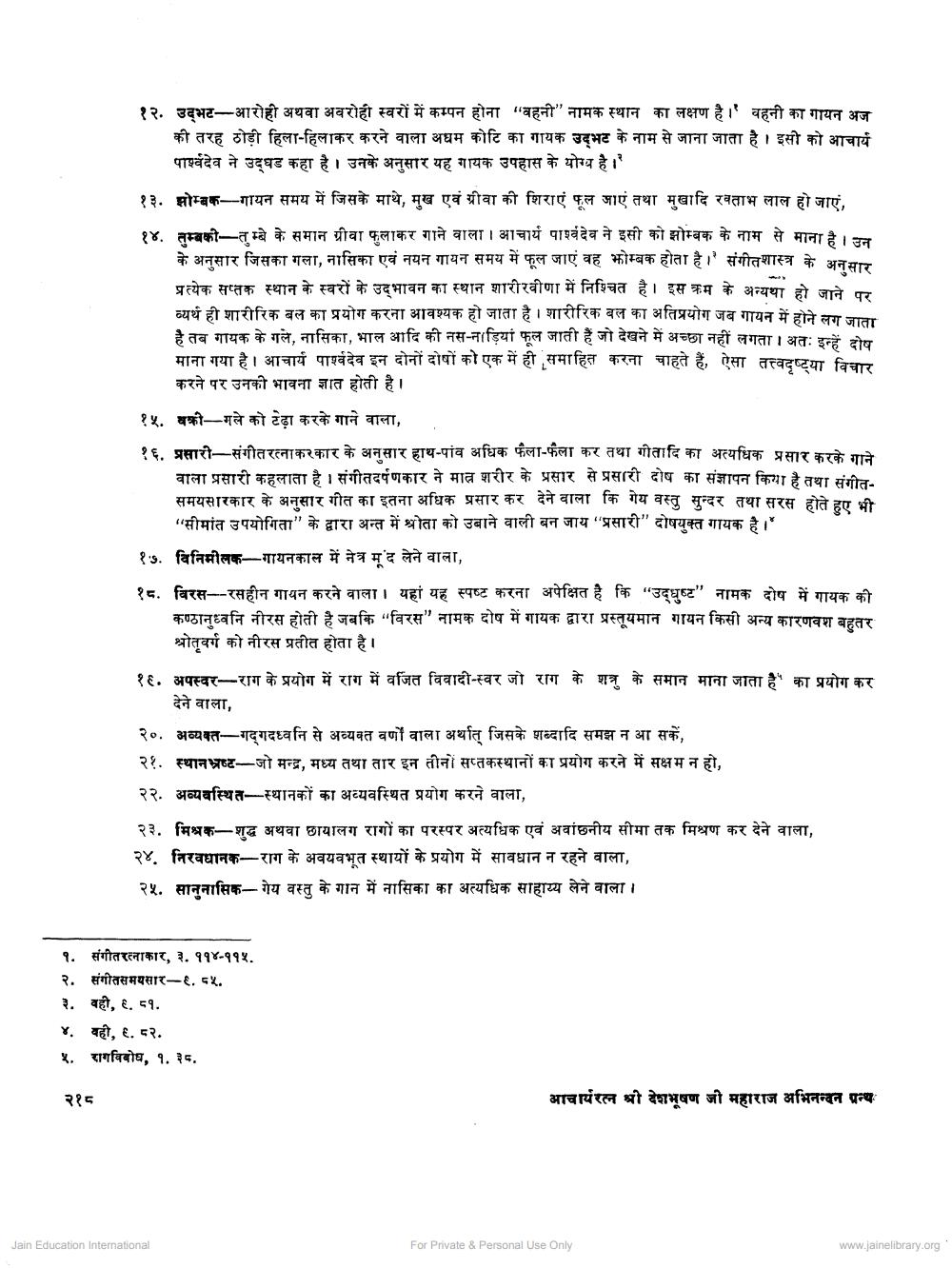________________
१२. उद्भट-आरोही अथवा अवरोही स्वरों में कम्पन होना "वहनी” नामक स्थान का लक्षण है।' वहनी का गायन अज
की तरह ठोड़ी हिला-हिलाकर करने वाला अधम कोटि का गायक उद्भट के नाम से जाना जाता है। इसी को आचार्य पार्श्वदेव ने उद्घड कहा है। उनके अनुसार यह गायक उपहास के योग्य है।
१३. झोम्बक-गायन समय में जिसके माथे, मुख एवं ग्रीवा की शिराएं फूल जाएं तथा मुखादि रक्ताभ लाल हो जाएं, १४. तुम्बको-तुम्बे के समान ग्रीवा फुलाकर गाने वाला। आचार्य पार्श्वदेव ने इसी को झोम्बक के नाम से माना है।
के अनुसार जिसका गला, नासिका एवं नयन गायन समय में फूल जाएं वह झोम्बक होता है। संगीतशास्त्र के अनम प्रत्येक सप्तक स्थान के स्वरों के उद्भावन का स्थान शारीरवीणा में निश्चित है। इस क्रम के अन्यथा हो जाने व्यर्थ ही शारीरिक बल का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। शारीरिक बल का अतिप्रयोग जब गायन में होने लगा है तब गायक के गले, नासिका, भाल आदि की नस-नाड़ियां फूल जाती हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता। अतः इन्हें हो माना गया है। आचार्य पार्श्वदेव इन दोनों दोषों को एक में ही समाहित करना चाहते हैं, ऐसा तत्त्वदष्ट्या विचार करने पर उनकी भावना ज्ञात होती है।
१५. वक्री-मले को टेढ़ा करके गाने वाला, १६. प्रसारी-संगीतरत्नाकर कार के अनुसार हाथ-पांव अधिक फैला-फैला कर तथा गीतादि का अत्यधिक प्रसार करना
वाला प्रसारी कहलाता है । संगीतदर्पणकार ने मात्र शरीर के प्रसार से प्रसारी दोष का संज्ञापन किया है तथा संगीत समयसारकार के अनुसार गीत का इतना अधिक प्रसार कर देने वाला कि गेय वस्तु सुन्दर तथा सरस होतेची "सीमांत उपयोगिता" के द्वारा अन्त में श्रोता को उबाने वाली बन जाय "प्रसारी" दोषयुक्त गायक है।
१७. विनिमीलक-गायनकाल में नेत्र मूद लेने वाला, १८. विरस--रसहीन गायन करने वाला। यहां यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि "उद्धृष्ट" नामक दोष में गायक की
कण्ठानध्वनि नीरस होती है जबकि "विरस" नामक दोष में गायक द्वारा प्रस्तूयमान गायन किसी अन्य कारणवश बहतर श्रोतृवर्ग को नीरस प्रतीत होता है।
१६. अपस्वर-राग के प्रयोग में राग में वजित विवादी-स्वर जो राग के शत्रु के समान माना जाता है। का प्रयोग कर
देने वाला, २०. अव्यक्त-गद्गदध्वनि से अव्यक्त वर्णों वाला अर्थात् जिसके शब्दादि समझ न आ सकें, २१. स्थानभ्रष्ट-जो मन्द्र, मध्य तथा तार इन तीनों सप्तकस्थानों का प्रयोग करने में सक्षम न हो, २२. अव्यवस्थित-स्थानकों का अव्यवस्थित प्रयोग करने वाला, २३. मिश्रक-शुद्ध अथवा छायालग रागों का परस्पर अत्यधिक एवं अवांछनीय सीमा तक मिश्रण कर देने वाला, २४. निरवधानक-राग के अवयवभूत स्थायों के प्रयोग में सावधान न रहने वाला, २५. सानुनासिक- गेय वस्तु के गान में नासिका का अत्यधिक साहाय्य लेने वाला।
१. संगीतरत्नाकार, ३. ११४-११५. २. संगीतसमयसार-६.६५. ३. वही, ६.८१. ४. वही, ६. ८२. ५. रागविबोध, १. ३८.
२१८
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रन्या
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org