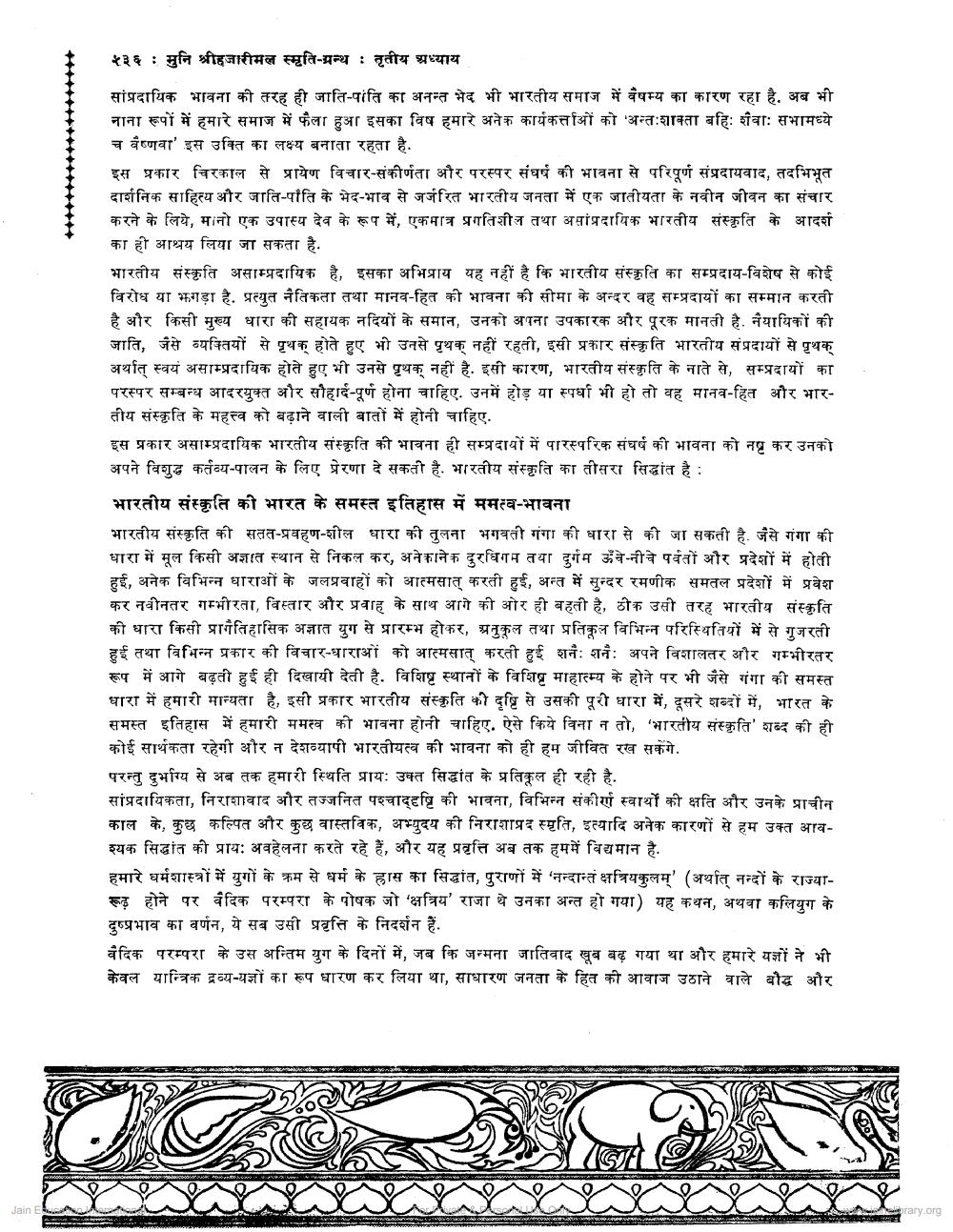________________
+
+
+
++++++++++++++++
१३६ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : तृतीय अध्याय सांप्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पांति का अनन्त भेद भी भारतीय समाज में वैषम्य का कारण रहा है. अब भी नाना रूपों में हमारे समाज में फैला हुआ इसका विष हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को 'अन्तःशाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवा' इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है. इस प्रकार चिरकाल से प्रायेण विचार-संकीर्णता और परस्पर संघर्ष की भावना से परिपूर्ण संप्रदायवाद, तदभिभूत दार्शनिक साहित्य और जाति-पाति के भेद-भाव से जर्जरित भारतीय जनता में एक जातीयता के नवीन जीवन का संचार करने के लिये, मानो एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र प्रगतिशील तथा असांप्रदायिक भारतीय संस्कृति के आदर्श का ही आश्रय लिया जा सकता है. भारतीय संस्कृति असाम्प्रदायिक है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय संस्कृति का सम्प्रदाय-विशेष से कोई विरोध या झगड़ा है. प्रत्युत नैतिकता तथा मानव-हित की भावना की सीमा के अन्दर वह सम्प्रदायों का सम्मान करती है और किसी मुख्य धारा की सहायक नदियों के समान, उनको अपना उपकारक और पूरक मानती है. नैयायिकों की जाति, जैसे व्यक्तियों से पृथक् होते हुए भी उनसे पृथक् नहीं रहती, इसी प्रकार संस्कृति भारतीय संप्रदायों से पृथक अर्थात् स्वयं असाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथक् नहीं है. इसी कारण, भारतीय संस्कृति के नाते से, सम्प्रदायों का परस्पर सम्बन्ध आदरयुक्त और सौहार्द-पूर्ण होना चाहिए. उनमें होड़ या स्पर्धा भी हो तो वह मानव-हित और भारतीय संस्कृति के महत्त्व को बढ़ाने वाली बातों में होनी चाहिए. इस प्रकार असाम्प्रदायिक भारतीय संस्कृति की भावना ही सम्प्रदायों में पारस्परिक संघर्ष की भावना को नष्ट कर उनको अपने विशुद्ध कर्तव्य-पालन के लिए प्रेरणा दे सकती है. भारतीय संस्कृति का तीसरा सिद्धांत है : भारतीय संस्कृति की भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना भारतीय संस्कृति की सतत-प्रवहण-शील धारा की तुलना भगवती गंगा की धारा से की जा सकती है. जैसे गंगा की धारा में मूल किसी अज्ञात स्थान से निकल कर, अनेकानेक दुरधिगम तथा दुर्गम ऊँचे-नीचे पर्वतों और प्रदेशों में होती हुई, अनेक विभिन्न धाराओं के जलप्रवाहों को आत्मसात् करती हुई, अन्त में सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशों में प्रवेश कर नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और प्रवाह के साथ आगे की ओर ही बहती है, ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति की धारा किसी प्रागैतिहासिक अज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकुल तथा प्रतिकूल विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराओं को आत्मसात् करती हुई शनैः शनैः अपने विशालतर और गम्भीरतर रूप में आगे बढ़ती हुई ही दिखायी देती है. विशिष्ट स्थानों के विशिष्ट माहात्म्य के होने पर भी जैसे गंगा की समस्त धारा में हमारी मान्यता है, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उसकी पूरी धारा में, दूसरे शब्दों में, भारत के समस्त इतिहास में हमारी ममत्व की भावना होनी चाहिए. ऐसे किये विना न तो, 'भारतीय संस्कृति' शब्द की ही कोई सार्थकता रहेगी और न देशव्यापी भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवित रख सकेंगे. परन्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्रायः उक्त सिद्धांत के प्रतिकूल ही रही है. सांप्रदायिकता, निराशावाद और तज्जनित पश्चादृष्टि की भावना, विभिन्न संकीर्ण स्वार्थों की क्षति और उनके प्राचीन काल के, कुछ कल्पित और कुछ वास्तविक, अभ्युदय की निराशाप्रद स्मृति, इत्यादि अनेक कारणों से हम उक्त आवश्यक सिद्धांत को प्रायः अवहेलना करते रहे हैं, और यह प्रवृत्ति अब तक हममें विद्यमान है. हमारे धर्मशास्त्रों में युगों के क्रम से धर्म के ह्रास का सिद्धांत, पुराणों में 'नन्दान्तं क्षत्रियकुलम्' (अर्थात् नन्दों के राज्यारूढ़ होने पर वैदिक परम्परा के पोषक जो 'क्षत्रिय' राजा थे उनका अन्त हो गया) यह कथन, अथवा कलियुग के दुष्प्रभाव का वर्णन, ये सब उसी प्रवृत्ति के निदर्शन हैं. वैदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनों में, जब कि जन्मना जातिवाद खूब बढ़ गया था और हमारे यज्ञों ने भी केवल यान्त्रिक द्रव्य-यज्ञों का रूप धारण कर लिया था, साधारण जनता के हित की आवाज उठाने वाले बौद्ध और
MARKESARNEARNAMASHAVAT
ARATEST
कर 2-80038ARAT VERe८ -
Jain Eucati
rary.org