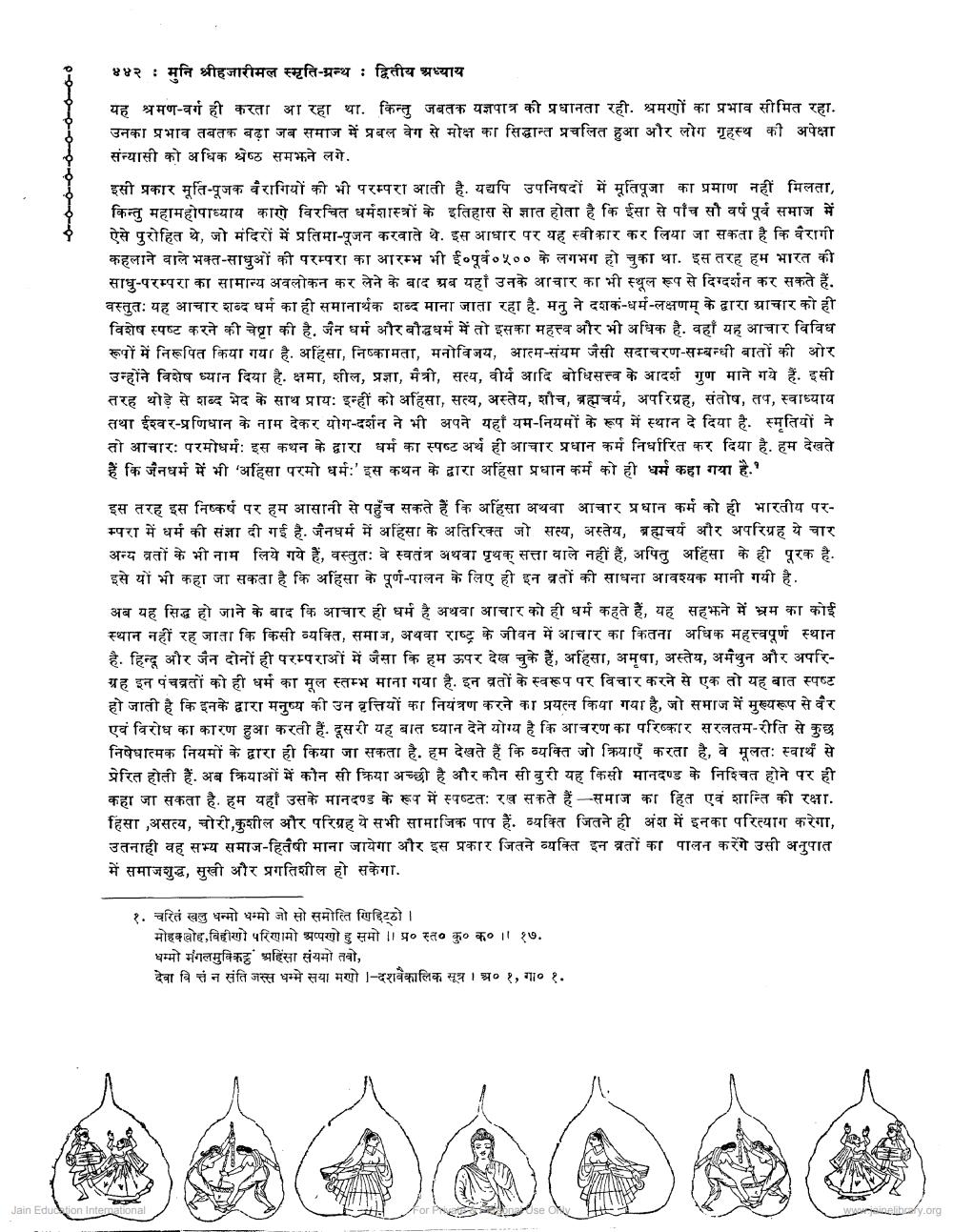________________
همهمنمنننمه
४४२ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय यह श्रमण-वर्ग ही करता आ रहा था. किन्तु जबतक यज्ञपात्र की प्रधानता रही. श्रमणों का प्रभाव सीमित रहा. उनका प्रभाव तबतक बढ़ा जब समाज में प्रबल वेग से मोक्ष का सिद्धान्त प्रचलित हुआ और लोग गृहस्थ की अपेक्षा संन्यासी को अधिक श्रेष्ठ समझने लगे. इसी प्रकार मूर्ति-पूजक वैरागियों की भी परम्परा आती है. यद्यपि उपनिषदों में मूर्तिपूजा का प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु महामहोपाध्याय काणे विरचित धर्मशास्त्रों के इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व समाज में ऐसे पुरोहित थे, जो मंदिरों में प्रतिमा-पूजन करवाते थे. इस आधार पर यह स्वीकार कर लिया जा सकता है कि वैरागी कहलाने वाले भक्त-साधुओं की परम्परा का आरम्भ भी ई०पूर्व०५०० के लगभग हो चुका था. इस तरह हम भारत की साधु-परम्परा का सामान्य अवलोकन कर लेने के बाद अब यहाँ उनके आचार का भी स्थूल रूप से दिग्दर्शन कर सकते हैं. वस्तुतः यह आचार शब्द धर्म का ही समानार्थक शब्द माना जाता रहा है. मनु ने दशकं-धर्म-लक्षणम् के द्वारा प्राचार को ही विशेष स्पष्ट करने की चेषा की है. जैन धर्म और बौद्धधर्म में तो इसका महत्त्व और भी अधिक है. वहाँ यह आचार विविध रूपों में निरूपित किया गया है. अहिंसा, निष्कामता, मनोविजय, आत्म-संयम जैसी सदाचरण-सम्बन्धी बातों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है. क्षमा, शील, प्रज्ञा, मैत्री, सत्य, वीर्य आदि बोधिसत्त्व के आदर्श गुण माने गये हैं. इसी तरह थोड़े से शब्द भेद के साथ प्रायः इन्हीं को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान के नाम देकर योग-दर्शन ने भी अपने यहाँ यम-नियमों के रूप में स्थान दे दिया है. स्मृतियों ने तो आचारः परमोधर्मः इस कथन के द्वारा धर्म का स्पष्ट अर्थ ही आचार प्रधान कर्म निर्धारित कर दिया है. हम देखते हैं कि जैनधर्म में भी 'अहिंसा परमो धर्मः' इस कथन के द्वारा अहिंसा प्रधान कर्म को ही धर्म कहा गया है.'
इस तरह इस निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं कि अहिंसा अथवा आचार प्रधान कर्म को ही भारतीय परम्परा में धर्म की संज्ञा दी गई है. जैनधर्म में अहिंसा के अतिरिक्त जो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये चार अन्य व्रतों के भी नाम लिये गये हैं, वस्तुतः वे स्वतंत्र अथवा पृथक् सत्ता वाले नहीं हैं, अपितु अहिंसा के ही पूरक है. इसे यों भी कहा जा सकता है कि अहिंसा के पूर्ण-पालन के लिए ही इन व्रतों की साधना आवश्यक मानी गयी है. अब यह सिद्ध हो जाने के बाद कि आचार ही धर्म है अथवा आचार को ही धर्म कहते हैं, यह सहझने में भ्रम का कोई स्थान नहीं रह जाता कि किसी व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र के जीवन में आचार का कितना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है. हिन्दू और जैन दोनों ही परम्पराओं में जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अमैथुन और अपरिग्रह इन पंचव्रतों को ही धर्म का मूल स्तम्भ माना गया है. इन व्रतों के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है, जो समाज में मुख्यरूप से वैर एवं विरोध का कारण हुआ करती हैं. दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार सरलतम-रीति से कुछ निषेधात्मक नियमों के द्वारा ही किया जा सकता है. हम देखते हैं कि व्यक्ति जो क्रियाएँ करता है, वे मूलतः स्वार्थं से प्रेरित होती हैं. अब क्रियाओं में कोन सी क्रिया अच्छी है और कौन सी बुरी यह किसी मानदण्ड के निश्चित होने पर ही कहा जा सकता है. हम यहाँ उसके मानदण्ड के रूप में स्पष्टतः रख सकते हैं -समाज का हित एवं शान्ति की रक्षा. हिंसा असत्य, चोरी,कुशील और परिग्रह ये सभी सामाजिक पाप हैं. व्यक्ति जितने ही अंश में इनका परित्याग करेगा, उतनाही वह सभ्य समाज-हितैषी माना जायेगा और इस प्रकार जितने व्यक्ति इन व्रतों का पालन करेंगे उसी अनुपात में समाजशुद्ध, सुखी और प्रगतिशील हो सकेगा.
१. चरितं खलु धन्मो धम्मो जो सो समोति णिहिट्ठो ।
मोहकबोह,विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो || प्र० स्त० कु० क० ।। १७. धम्मो मंगलमुक्किट्ठ अहिंसा संयमो तवो, देवा वितं न संति जस्स धम्मे सया मणो |-दशवकालिक सूत्र । अ०१, गा०१.
Jain Eduion International
wapinsineliboly.org