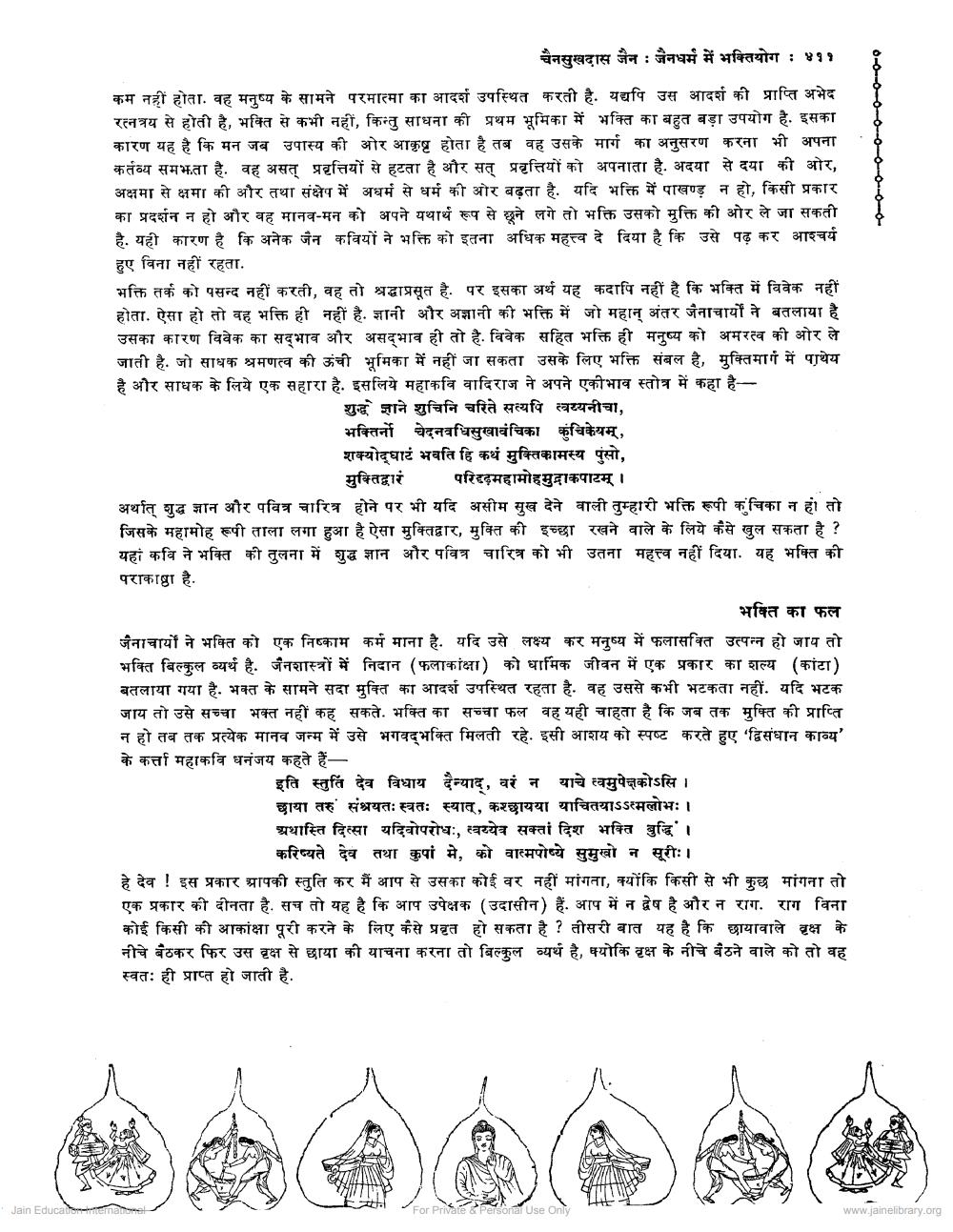________________
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
चैनसुखदास जैन : जैनधर्म में भक्तियोग : ४११ कम नहीं होता. वह मनुष्य के सामने परमात्मा का आदर्श उपस्थित करती है. यद्यपि उस आदर्श की प्राप्ति अभेद रत्नत्रय से होती है, भक्ति से कभी नहीं, किन्तु साधना की प्रथम भूमिका में भक्ति का बहुत बड़ा उपयोग है. इसका कारण यह है कि मन जब उपास्य की ओर आकृष्ट होता है तब वह उसके मार्ग का अनुसरण करना भी अपना कर्तव्य समझता है. वह असत् प्रवृत्तियों से हटता है और सत् प्रवृत्तियों को अपनाता है. अदया से दया की ओर, अक्षमा से क्षमा की और तथा संक्षेप में अधर्म से धर्म की ओर बढ़ता है. यदि भक्ति में पाखण्ड न हो, किसी प्रकार का प्रदर्शन न हो और वह मानव-मन को अपने यथार्थ रूप से छूने लगे तो भक्ति उसको मुक्ति की ओर ले जा सकती है. यही कारण है कि अनेक जैन कवियों ने भक्ति को इतना अधिक महत्त्व दे दिया है कि उसे पढ़ कर आश्चर्य हुए विना नहीं रहता. भक्ति तर्क को पसन्द नहीं करती, वह तो श्रद्धाप्रसूत है. पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भक्ति में विवेक नहीं होता. ऐसा हो तो वह भक्ति ही नहीं है. ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति में जो महान् अंतर जैनाचार्यों ने बतलाया है उसका कारण विवेक का सद्भाव और असद्भाव ही तो है. विवेक सहित भक्ति ही मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है. जो साधक श्रमणत्व की ऊंची भूमिका में नहीं जा सकता उसके लिए भक्ति संबल है, मुक्तिमार्ग में पाथेय है और साधक के लिये एक सहारा है. इसलिये महाकवि वादिराज ने अपने एकीभाव स्तोत्र में कहा है
शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा, भक्ति! चेदनवधिसुखावंचिका कुंचिकेयम् , शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो,
मुक्तिद्वारं परिदृढ़महामोहमुद्राकपाटम् । अर्थात् शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र होने पर भी यदि असीम सुख देने वाली तुम्हारी भक्ति रूपी कुंचिका न हो तो जिसके महामोह रूपी ताला लगा हुआ है ऐसा मुक्तिद्वार, मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिये कैसे खुल सकता है ? यहां कवि ने भक्ति की तुलना में शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र को भी उतना महत्त्व नहीं दिया. यह भक्ति की पराकाष्ठा है.
भक्ति का फल जैनाचार्यों ने भक्ति को एक निष्काम कर्म माना है. यदि उसे लक्ष्य कर मनुष्य में फलासक्ति उत्पन्न हो जाय तो भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है. जैनशास्त्रों में निदान (फलाकांक्षा) को धार्मिक जीवन में एक प्रकार का शल्य (कांटा) बतलाया गया है. भक्त के सामने सदा मुक्ति का आदर्श उपस्थित रहता है. वह उससे कभी भटकता नहीं. यदि भटक जाय तो उसे सच्चा भक्त नहीं कह सकते. भक्ति का सच्चा फल वह यही चाहता है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक मानव जन्म में उसे भगवद्भक्ति मिलती रहे. इसी आशय को स्पष्ट करते हुए "द्विसंधान काव्य' के कर्ता महाकवि धनंजय कहते हैं
इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद, वरं न याचे स्वमुपेक्षकोऽसि । छाया तरु संश्रयतः स्वतः स्यात्, कश्छायया याचितयाऽऽस्मलोभः । अथास्ति दित्सा यदिवोपरोधः, स्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धि।
करिष्यते देव तथा कुपां मे, को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरीः। हे देव ! इस प्रकार आपकी स्तुति कर मैं आप से उसका कोई वर नहीं मांगता, क्योंकि किसी से भी कुछ मांगना तो एक प्रकार की दीनता है. सच तो यह है कि आप उपेक्षक (उदासीन) हैं. आप में न द्वेष है और न राग. राग विना कोई किसी की आकांक्षा पूरी करने के लिए कैसे प्रवृत हो सकता है ? तीसरी बात यह है कि छायावाले वृक्ष के नीचे बैठकर फिर उस वृक्ष से छाया की याचना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योकि वृक्ष के नीचे बैठने वाले को तो वह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है.
Jain Educa
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org