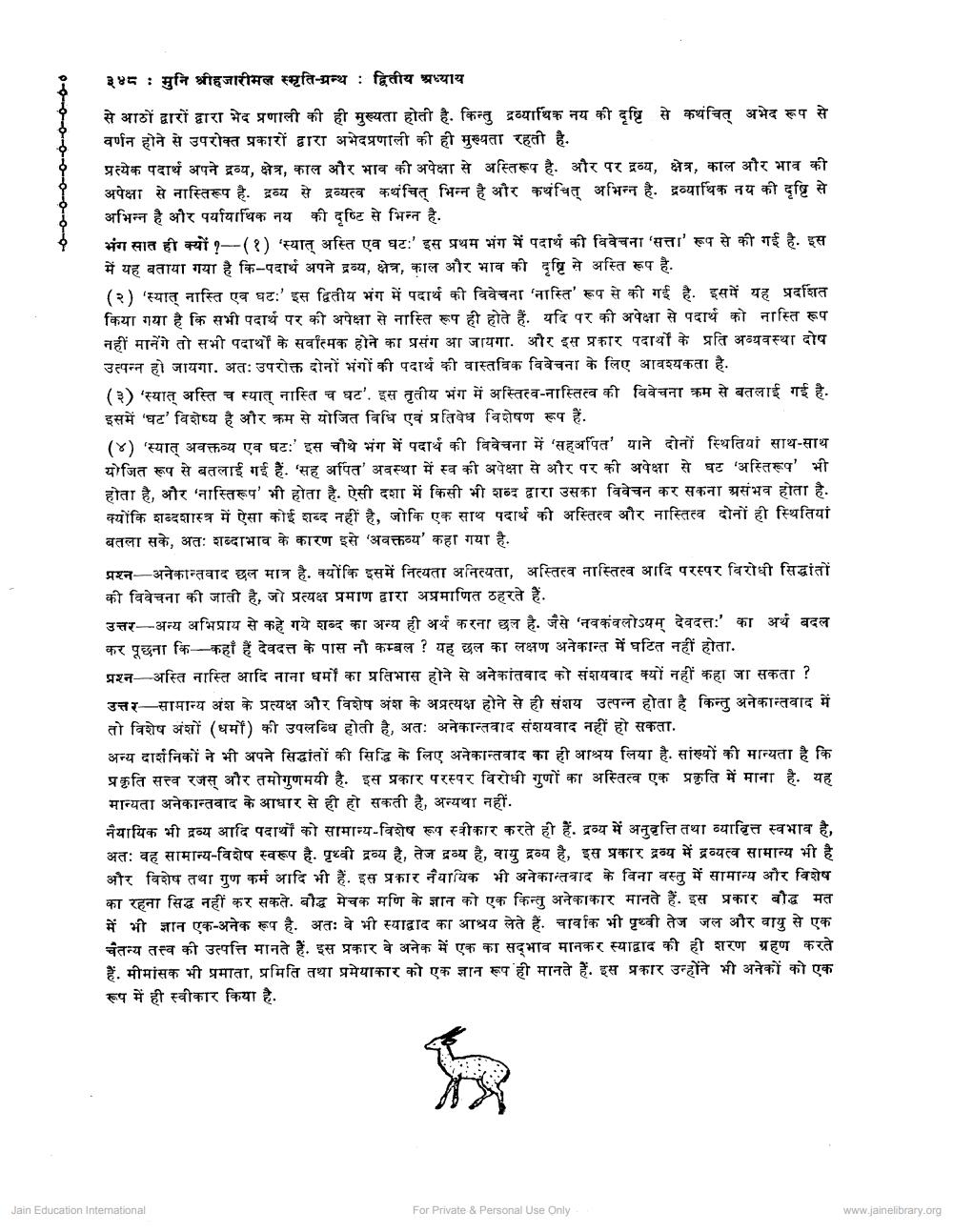________________
३४८ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय
------0-0--0--0--0--0-0-0
से आठों द्वारों द्वारा भेद प्रणाली की ही मुख्यता होती है. किन्तु द्रव्याथिक नय की दृष्टि से कथंचित् अभेद रूप से वर्णन होने से उपरोक्त प्रकारों द्वारा अभेदप्रणाली की ही मुख्यता रहती है. प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अस्तिरूप है. और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से नास्तिरूप है. द्रव्य से द्रव्यत्व कथंचित् भिन्न है और कथंचित् अभिन्न है. द्रव्याथिक नय की दृष्टि से अभिन्न है और पर्यायाथिक नय की दृष्टि से भिन्न है. भंग सात ही क्यों?-(१) 'स्यात् अस्ति एव घट:' इस प्रथम भंग में पदार्थ की विवेचना 'सत्ता' रूप से की गई है. इस में यह बताया गया है कि-पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से अस्ति रूप है. (२) 'स्यात् नास्ति एव घटः' इस द्वितीय भंग में पदार्थ की विवेचना 'नास्ति' रूप से की गई है. इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि सभी पदार्थ पर की अपेक्षा से नास्ति रूप ही होते हैं. यदि पर की अपेक्षा से पदार्थ को नास्ति रूप नहीं मानेंगे तो सभी पदार्थों के सर्वात्मक होने का प्रसंग आ जायगा. और इस प्रकार पदार्थों के प्रति अव्यवस्था दोष उत्पन्न हो जायगा. अतः उपरोक्त दोनों भंगों की पदार्थ की वास्तविक विवेचना के लिए आवश्यकता है. (३) 'स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च घट'. इस तृतीय भंग में अस्तित्व-नास्तित्व की विवेचना क्रम से बतलाई गई है. इसमें 'घट' विशेष्य है और क्रम से योजित विधि एवं प्रतिषेध विशेषण रूप हैं. (४) 'स्यात् अवक्तव्य एव घट:' इस चौथे भंग में पदार्थ की विवेचना में 'सहअपित' याने दोनों स्थितियां साथ-साथ योजित रूप से बतलाई गई हैं. 'सह अपित' अवस्था में स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से घट 'अस्तिरूप' भी होता है, और 'नास्तिरूप' भी होता है. ऐसी दशा में किसी भी शब्द द्वारा उसका विवेचन कर सकना असंभव होता है. क्योंकि शब्दशास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जोकि एक साथ पदार्थ की अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही स्थितियां बतला सके, अतः शब्दाभाव के कारण इसे 'अवक्तव्य' कहा गया है. प्रश्न–अनेकान्तवाद छल मात्र है. क्योंकि इसमें नित्यता अनित्यता, अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी सिद्धांतों की विवेचना की जाती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अप्रमाणित ठहरते हैं. उत्तर-अन्य अभिप्राय से कहे गये शब्द का अन्य ही अर्थ करना छल है. जैसे 'नवकंवलोऽयम् देवदत्तः' का अर्थ बदल कर पूछना कि-कहाँ हैं देवदत्त के पास नौ कम्बल ? यह छल का लक्षण अनेकान्त में घटित नहीं होता. प्रश्न-अस्ति नास्ति आदि नाना धर्मों का प्रतिभास होने से अनेकांतवाद को संशयवाद क्यों नहीं कहा जा सकता? उत्तर–सामान्य अंश के प्रत्यक्ष और विशेष अंश के अप्रत्यक्ष होने से ही संशय उत्पन्न होता है किन्तु अनेकान्तवाद में तो विशेष अंशों (धर्मों) की उपलब्धि होती है, अत: अनेकान्तवाद संशयवाद नहीं हो सकता. अन्य दार्शनिकों ने भी अपने सिद्धांतों की सिद्धि के लिए अनेकान्तवाद का ही आश्रय लिया है. सांख्यों की मान्यता है कि प्रकृति सत्त्व रजस् और तमोगुणमयी है. इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणों का अस्तित्व एक प्रकृति में माना है. यह मान्यता अनेकान्तवाद के आधार से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं. नैयायिक भी द्रव्य आदि पदार्थों को सामान्य-विशेष रूप स्वीकार करते ही हैं. द्रव्य में अनुवृत्ति तथा व्यावृित्त स्वभाव है, अत: वह सामान्य-विशेष स्वरूप है. पृथ्वी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, वायु द्रव्य है, इस प्रकार द्रव्य में द्रव्यत्व सामान्य भी है और विशेष तथा गुण कर्म आदि भी हैं. इस प्रकार नैयायिक भी अनेकान्तवाद के विना वस्तु में सामान्य और विशेष का रहना सिद्ध नहीं कर सकते. बौद्ध मेचक मणि के ज्ञान को एक किन्तु अनेकाकार मानते हैं. इस प्रकार बौद्ध मत में भी ज्ञान एक-अनेक रूप है. अतः वे भी स्याद्वाद का आश्रय लेते हैं. चार्वाक भी पृथ्वी तेज जल और वायु से एक चैतन्य तत्व की उत्पत्ति मानते हैं. इस प्रकार वे अनेक में एक का सद्भाव मानकर स्याद्वाद की ही शरण ग्रहण करते हैं. मीमांसक भी प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमेयाकार को एक ज्ञान रूप ही मानते हैं. इस प्रकार उन्होंने भी अनेकों को एक रूप में ही स्वीकार किया है.
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org