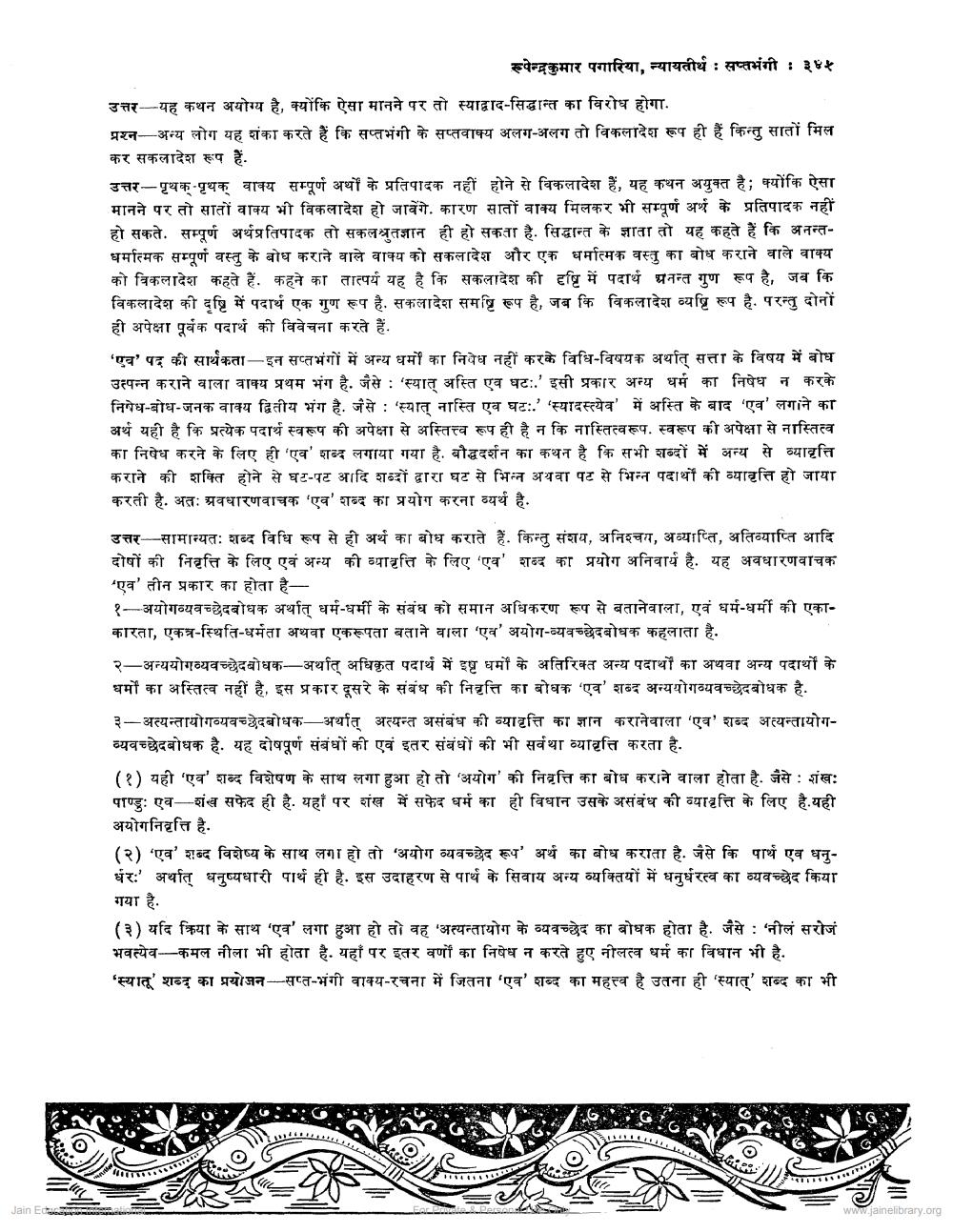________________
Jain Ed
रूपेन्द्रकुमार पगारिया, न्यायतीर्थ : सप्तभंगी : ३४५ उत्तर - यह कथन अयोग्य है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो स्याद्वाद सिद्धान्त का विरोध होगा. प्रश्न- -अन्य लोग यह शंका करते हैं कि सप्तभंगी के सप्तवाक्य अलग-अलग तो विकलादेश रूप ही हैं किन्तु सातों मिल कर सकलादेश रूप हैं.
उत्तर - पृथक्-पृथक् वाक्य सम्पूर्ण अर्थों के प्रतिपादक नहीं होने से विकलादेश हैं, यह कथन अयुक्त है; क्योंकि ऐसा मानने पर तो सातों वाक्य भी विकलादेश हो जायेंगे. कारण सातों वाक्य मिलकर भी सम्पूर्ण अर्थ के प्रतिपादक नहीं हो सकते . सम्पूर्ण अर्थप्रतिपादक तो सकलश्रुतज्ञान ही हो सकता है. सिद्धान्त के ज्ञाता तो यह कहते हैं कि अनन्तधर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तु के बोध कराने वाले वाक्य को सकलादेश और एक धर्मात्मक वस्तु का बोध कराने वाले वाक्य को विकलादेश कहते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि सकलादेश की दृष्टि में पदार्थ अनन्त गुण रूप है, जबकि विकलादेश की दृष्टि में पदार्थ एक गुण रूप है. सकलादेश समष्टि रूप है, जब कि विकलादेश व्यष्टि रूप है. परन्तु दोनों ही अपेक्षा पूर्वक पदार्थ की विवेचना करते हैं.
'एव' पद की सार्थकता – इन सप्तभंगों में अन्य धर्मों का निषेध नहीं करके विधि-विषयक अर्थात् सत्ता के विषय में बोध उत्पन्न कराने वाला वाक्य प्रथम भंग है. जैसे 'स्यात् अस्ति एव घट:.' इसी प्रकार अन्य धर्म का निषेध न करके निषेध-बोध-जनक वाक्य द्वितीय भंग है. जैसे 'स्यात् नास्ति एव घट:.' 'स्यादस्त्येव' में अस्ति के बाद 'एव' लगाने का अर्थ यही है कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्त्व रूप ही है न कि नास्तित्वरूप स्वरूप की अपेक्षा से नास्तित्व का निषेध करने के लिए ही 'एव' शब्द लगाया गया है. बौद्धदर्शन का कथन है कि सभी शब्दों में अन्य से व्यावृत्ति कराने की शक्ति होने से घट-पट आदि शब्दों द्वारा घट से भिन्न अथवा पट से भिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति हो जाया करती है. अतः अवधारणवाचक 'एव' शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है.
उत्तर- - सामान्यतः शब्द विधि रूप से ही अर्थ का बोध कराते हैं. किन्तु संशय, अनिश्चय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों की निवृत्ति के लिए एवं अन्य की व्यावृत्ति के लिए 'एव' शब्द का प्रयोग अनिवार्य है. यह अवधारणवाचक एव' तीन प्रकार का होता है—
१- अयोगव्यवच्छेदबोधक अर्थात् धर्म-धर्मी के संबंध को समान अधिकरण रूप से बतानेवाला एवं धर्म-धर्मों की एकाकारता, एकत्र स्थिति-धर्मता अथवा एकरूपता बताने वाला 'एव' अयोग-व्यवच्छेदबोधक कहलाता है.
२ – अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक - अर्थात् अधिकृत पदार्थ में इष्ट धर्मों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का अथवा अन्य पदार्थों के धर्मों का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार दूसरे के संबंध की निवृत्ति का बोधक 'एव' शब्द अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक है. द- अत्यन्तायोगव्यवच्देवबोधक अर्थात् अत्यन्त असंबंध की व्यावृत्ति का ज्ञान करानेवाला 'एव' शब्द अत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक है. यह दोषपूर्ण संबंधों की एवं इतर संबंधों की भी सर्वथा व्यावृत्ति करता है.
(१) यही 'एव' शब्द विशेषण के साथ लगा हुआ हो तो 'अयोग' की निवृत्ति का बोध कराने वाला होता है. जैसे : शंख: पाण्डुः एव — शंख सफेद ही है. यहाँ पर शंख में सफेद धर्म का ही विधान उसके असंबंध की व्यावृत्ति के लिए है. यही अयोगनिवृत्ति है.
(२) 'एव' शब्द विशेष्य के साथ लगा हो तो 'अयोग व्यवच्छेद रूप' अर्थ का बोध कराता है. जैसे कि पार्थ एव धनुधंरः' अर्थात् धनुष्यधारी पार्थ ही है. इस उदाहरण से पार्थ के सिवाय अन्य व्यक्तियों में धनुर्धरत्व का व्यवच्छेद किया गया है.
(३) यदि क्रिया के साथ 'एव' लगा हुआ हो तो वह 'अत्यन्तायोग के व्यवच्छेद का बोधक होता है. जैसे : 'नीलं सरोजं भवत्येव — कमल नीला भी होता है. यहाँ पर इतर वर्णों का निषेध न करते हुए नीलत्व धर्म का विधान भी है. 'स्यातू' शब्द का प्रयोजन - सप्तभंगी वाक्य रचना में जितना 'एव' शब्द का महत्त्व है उतना ही 'स्यात्' शब्द का भी
---
Ear Brindle &
www.jainelibrary.org