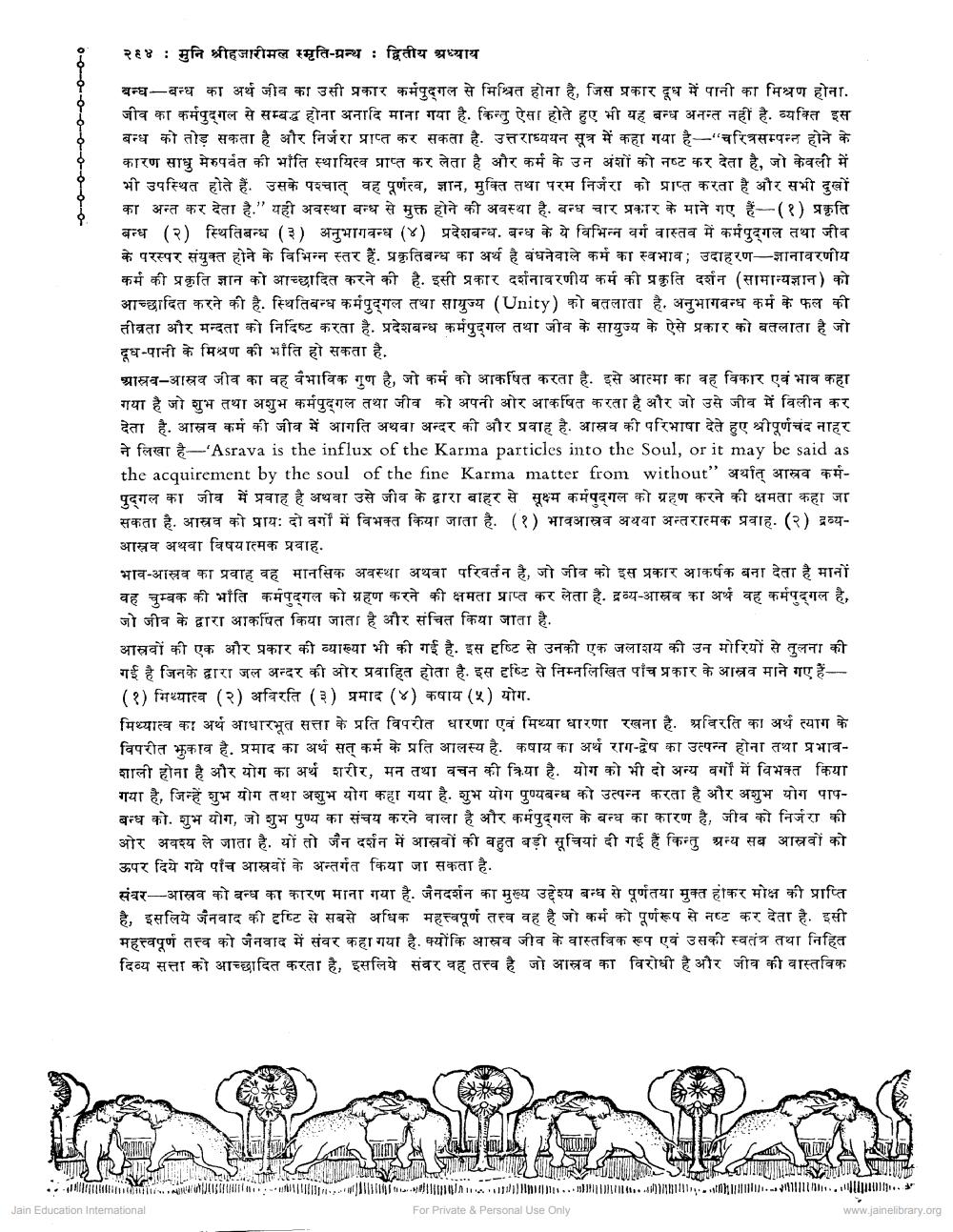________________
२६४ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय
बन्ध-बन्ध का अर्थ जीव का उसी प्रकार कर्मपुद्गल से मिश्रित होना है, जिस प्रकार दूध में पानी का मिश्रण होना. जीव का कर्मपुद्गल से सम्बद्ध होना अनादि माना गया है. किन्तु ऐसा होते हुए भी यह बन्ध अनन्त नहीं है. व्यक्ति इस बन्ध को तोड़ सकता है और निर्जरा प्राप्त कर सकता है. उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है-“चरित्रसम्पन्न होने के कारण साधु मेरुपर्वत की भाँति स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और कर्म के उन अंशों को नष्ट कर देता है, जो केवली में भी उपस्थित होते हैं. उसके पश्चात् वह पूर्णत्व, ज्ञान, मुक्ति तथा परम निर्जरा को प्राप्त करता है और सभी दुखों का अन्त कर देता है." यही अवस्था बन्ध से मुक्त होने की अवस्था है. बन्ध चार प्रकार के माने गए हैं-(१) प्रकृति बन्ध (२) स्थितिबन्ध (३) अनुभागवन्ध (४) प्रदेशबन्ध. बन्ध के ये विभिन्न वर्ग वास्तव में कर्मपुद्गल तथा जीव के परस्पर संयुक्त होने के विभिन्न स्तर हैं. प्रकृतिबन्ध का अर्थ है बंधनेवाले कर्म का स्वभाव; उदाहरण-ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति ज्ञान को आच्छादित करने की है. इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति दर्शन (सामान्यज्ञान) को आच्छादित करने की है. स्थितिबन्ध कर्मपुद्गल तथा सायुज्य (Unity) को बतलाता है. अनुभागबन्ध कर्म के फल की तीव्रता और मन्दता को निर्दिष्ट करता है. प्रदेशबन्ध कर्मपुद्गल तथा जीव के सायुज्य के ऐसे प्रकार को बतलाता है जो दूध-पानी के मिश्रण की भाँति हो सकता है. श्रास्रव-आस्रव जीव का वह वैभाविक गुण है, जो कर्म को आकर्षित करता है. इसे आत्मा का वह विकार एवं भाव कहा गया है जो शुभ तथा अशुभ कर्मपुद्गल तथा जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो उसे जीव में विलीन कर देता है. आस्रव कर्म की जीव में आगति अथवा अन्दर की और प्रवाह है. आस्रव की परिभाषा देते हुए श्रीपूर्णचंद नाहर ने लिखा है-Asrava is the influx of the Karma particles into the Soul, or it may be said as the acquirement by the soul of the fine Karma matter from without” अर्थात् आस्रव कर्मपुद्गल का जीव में प्रवाह है अथवा उसे जीव के द्वारा बाहर से सूक्ष्म कर्मपुद्गल को ग्रहण करने की क्षमता कहा जा सकता है. आस्रव को प्रायः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है. (१) भावआस्रव अथवा अन्तरात्मक प्रवाह. (२) द्रव्यआस्रव अथवा विषयात्मक प्रवाह.. भाव-आस्रव का प्रवाह वह मानसिक अवस्था अथवा परिवर्तन है, जो जीव को इस प्रकार आकर्षक बना देता है मानों वह चुम्बक की भाँति कर्मपुद्गल को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है. द्रव्य-आस्रव का अर्थ वह कर्मपुद्गल है, जो जीव के द्वारा आकर्षित किया जाता है और संचित किया जाता है. आस्रवों की एक और प्रकार की व्याख्या भी की गई है. इस दृष्टि से उनकी एक जलाशय की उन मोरियों से तुलना की गई है जिनके द्वारा जल अन्दर की ओर प्रवाहित होता है. इस दृष्टि से निम्नलिखित पाँच प्रकार के आस्रव माने गए हैं(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय (५) योग. मिथ्यात्व का अर्थ आधारभूत सत्ता के प्रति विपरीत धारणा एवं मिथ्या धारणा रखना है. अविरति का अर्थ त्याग के विपरीत झुकाव है. प्रमाद का अर्थ सत् कर्म के प्रति आलस्य है. कषाय का अर्थ राग-द्वेष का उत्पन्न होना तथा प्रभावशाली होना है और योग का अर्थ शरीर, मन तथा वचन की क्रिया है. योग को भी दो अन्य वर्गों में विभक्त किया गया है, जिन्हें शुभ योग तथा अशुभ योग कहा गया है. शुभ योग पुण्यबन्ध को उत्पन्न करता है और अशुभ योग पापबन्ध को. शुभ योग, जो शुभ पुण्य का संचय करने वाला है और कर्मपुद्गल के बन्ध का कारण है, जीव को निर्जरा की ओर अवश्य ले जाता है. यों तो जैन दर्शन में आस्रवों की बहुत बड़ी सूचियां दी गई हैं किन्तु अन्य सब आस्रवों को ऊपर दिये गये पाँच आस्रवों के अन्तर्गत किया जा सकता है. संवर–आस्रव को बन्ध का कारण माना गया है. जैनदर्शन का मुख्य उद्देश्य बन्ध से पूर्णतया मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिये जैनवाद की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व वह है जो कर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है. इसी महत्त्वपूर्ण तत्त्व को जैनवाद में संवर कहा गया है. क्योंकि आस्रव जीव के वास्तविक रूप एवं उसकी स्वतंत्र तथा निहित दिव्य सत्ता को आच्छादित करता है, इसलिये संवर वह तत्त्व है जो आस्रव का विरोधी है और जीव की वास्तविक
R
- RAMRA
P
a waim
MILIMIMPLOMATLinvest
inागात
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org