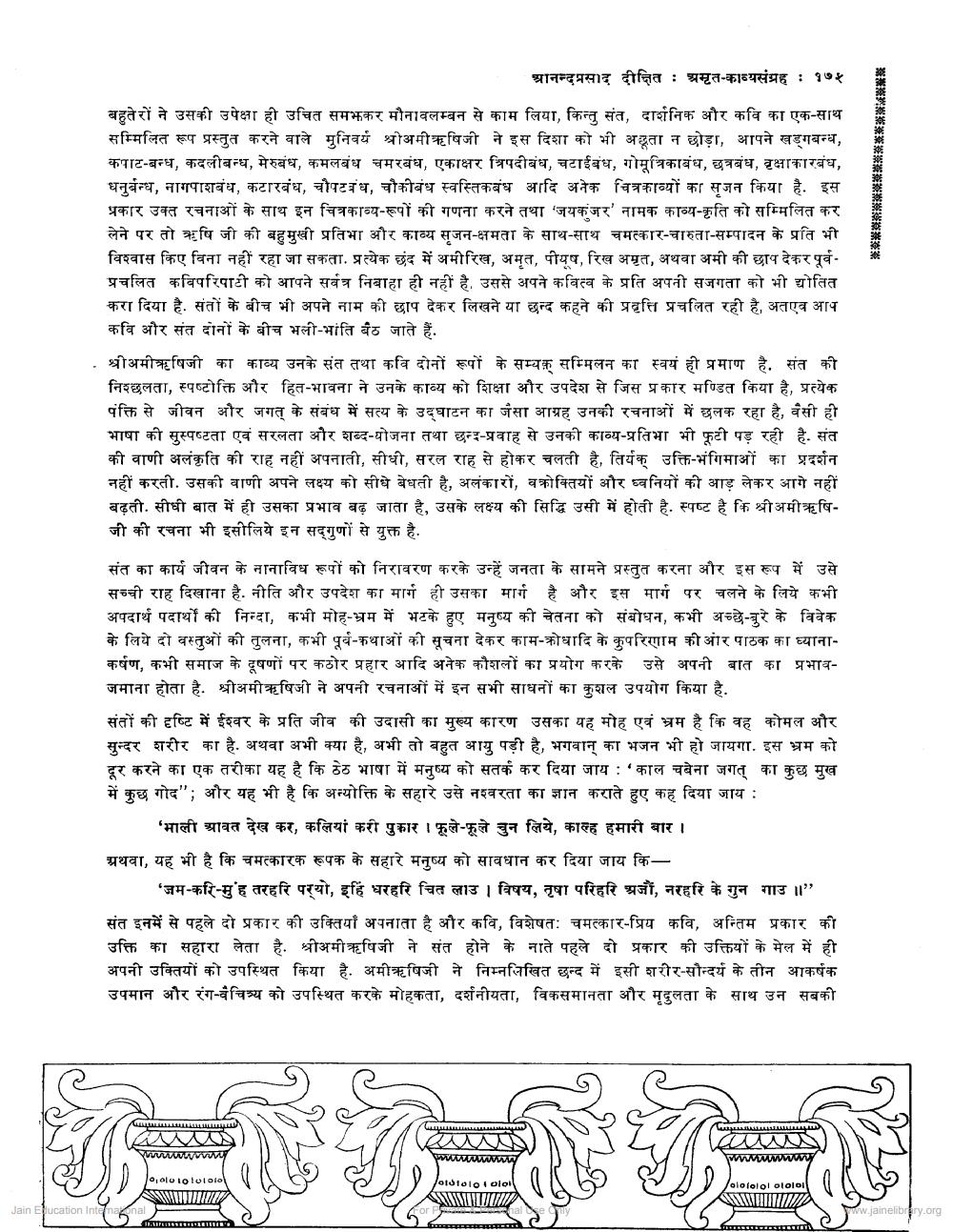________________
श्रानन्दप्रसाद दीक्षित : अमृत-काव्यसंग्रह : १७५
*EXEN94293060030038EXMRENERSE
बहुतेरों ने उसकी उपेक्षा ही उचित समझकर मौनावलम्बन से काम लिया, किन्तु संत, दार्शनिक और कवि का एक-साथ सम्मिलित रूप प्रस्तुत करने वाले मुनिवर्य श्रीअमीऋषिजी ने इस दिशा को भी अछूता न छोड़ा, आपने खड्गबन्ध, कपाट-बन्ध, कदलीबन्ध, मेरुबंध, कमलबंध चमरबंध, एकाक्षर त्रिपदीबंध, चटाईबंध, गोमूत्रिकाबंध, छत्रबंध, वृक्षाकारबंध, धनुर्बन्ध, नागपाशबंध, कटारबंध, चौपटबंध, चौकीबंध स्वस्तिकबंध आदि अनेक चित्रकाव्यों का सृजन किया है. इस प्रकार उक्त रचनाओं के साथ इन चित्रकाव्य-रूपों की गणना करने तथा 'जयकुंजर' नामक काव्य-कृति को सम्मिलित कर लेने पर तो ऋषि जी की बहुमुखी प्रतिभा और काव्य सजन-क्षमता के साथ-साथ चमत्कार-चारुता-सम्पादन के प्रति भी विश्वास किए विना नहीं रहा जा सकता. प्रत्येक छंद में अमीरिख, अमृत, पीयूष, रिख अमृत, अथवा अमी की छाप देकर पूर्वप्रचलित कविपरिपाटी को आपने सर्वत्र निबाहा ही नहीं है, उससे अपने कवित्व के प्रति अपनी सजगता को भी धोतित करा दिया है. संतों के बीच भी अपने नाम की छाप देकर लिखने या छन्द कहने की प्रवृत्ति प्रचलित रही है, अतएव आप कवि और संत दोनों के बीच भली-भांति बैठ जाते हैं. श्रीअमीऋषिजी का काव्य उनके संत तथा कवि दोनों रूपों के सम्यक् सम्मिलन का स्वयं ही प्रमाण है. संत की निश्छलता, स्पष्टोक्ति और हित-भावना ने उनके काव्य को शिक्षा और उपदेश से जिस प्रकार मण्डित किया है, प्रत्येक पंक्ति से जीवन और जगत् के संबंध में सत्य के उद्घाटन का जैसा आग्रह उनकी रचनाओं में छलक रहा है, वैसी ही भाषा की सुस्पष्टता एवं सरलता और शब्द-योजना तथा छन्द-प्रवाह से उनकी काव्य-प्रतिभा भी फूटी पड़ रही है. संत की वाणी अलंकृति की राह नहीं अपनाती, सीधी, सरल राह से होकर चलती है, तिर्यक् उक्ति-भंगिमाओं का प्रदर्शन नहीं करती. उसकी वाणी अपने लक्ष्य को सीधे बेधती है, अलंकारों, वक्रोक्तियों और ध्वनियों की आड़ लेकर आगे नहीं बढ़ती. सीधी बात में ही उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके लक्ष्य की सिद्धि उसी में होती है. स्पष्ट है कि श्रीअमीऋषिजी की रचना भी इसीलिये इन सद्गुणों से युक्त है. संत का कार्य जीवन के नानाविध रूपों को निरावरण करके उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत करना और इस रूप में उसे सच्ची राह दिखाना है. नीति और उपदेश का मार्ग ही उसका मार्ग है और इस मार्ग पर चलने के लिये कभी अपदार्थ पदार्थों की निन्दा, कभी मोह-भ्रम में भटके हुए मनुष्य की चेतना को संबोधन, कभी अच्छे-बुरे के विवेक के लिये दो वस्तुओं की तुलना, कभी पूर्व-कथाओं की सूचना देकर काम-क्रोधादि के कुपरिणाम की ओर पाठक का ध्यानाकर्षण, कभी समाज के दूषणों पर कठोर प्रहार आदि अनेक कौशलों का प्रयोग करके उसे अपनी बात का प्रभावजमाना होता है. श्रीअमीऋषिजी ने अपनी रचनाओं में इन सभी साधनों का कुशल उपयोग किया है. संतों की दृष्टि में ईश्वर के प्रति जीव की उदासी का मुख्य कारण उसका यह मोह एवं भ्रम है कि वह कोमल और सुन्दर शरीर का है. अथवा अभी क्या है, अभी तो बहुत आयु पड़ी है, भगवान् का भजन भी हो जायगा. इस भ्रम को दूर करने का एक तरीका यह है कि ठेठ भाषा में मनुष्य को सतर्क कर दिया जाय : 'काल चबेना जगत् का कुछ मुख में कुछ गोद"; और यह भी है कि अन्योक्ति के सहारे उसे नश्वरता का ज्ञान कराते हुए कह दिया जाय :
'भाली अावत देख कर, कलियां करी पुकार । फूले-फूले चुन लिये, काल्ह हमारी बार । अथवा, यह भी है कि चमत्कारक रूपक के सहारे मनुष्य को सावधान कर दिया जाय कि
'जम-करि-मुह तरहरि पर्यो, इहिं धरहरि चित लाउ । विषय, तृषा परिहरि अजौं, नरहरि के गुन गाउ॥" संत इनमें से पहले दो प्रकार की उक्तियाँ अपनाता है और कवि, विशेषतः चमत्कार-प्रिय कवि, अन्तिम प्रकार की उक्ति का सहारा लेता है. श्रीअमीऋषिजी ने संत होने के नाते पहले दो प्रकार की उक्तियों के मेल में ही अपनी उक्तियों को उपस्थित किया है. अमीऋषिजी ने निम्नलिखित छन्द में इसी शरीर-सौन्दर्य के तीन आकर्षक उपमान और रंग-वैचित्र्य को उपस्थित करके मोहकता, दर्शनीयता, विकसमानता और मृदुलता के साथ उन सबकी
AALAALAN
1COM
(wwwwwwwww
0101010 totolol
oldtoio i olol
IIIA
ololololololol
Jain Eucation Internal
www.jainelibrary.org