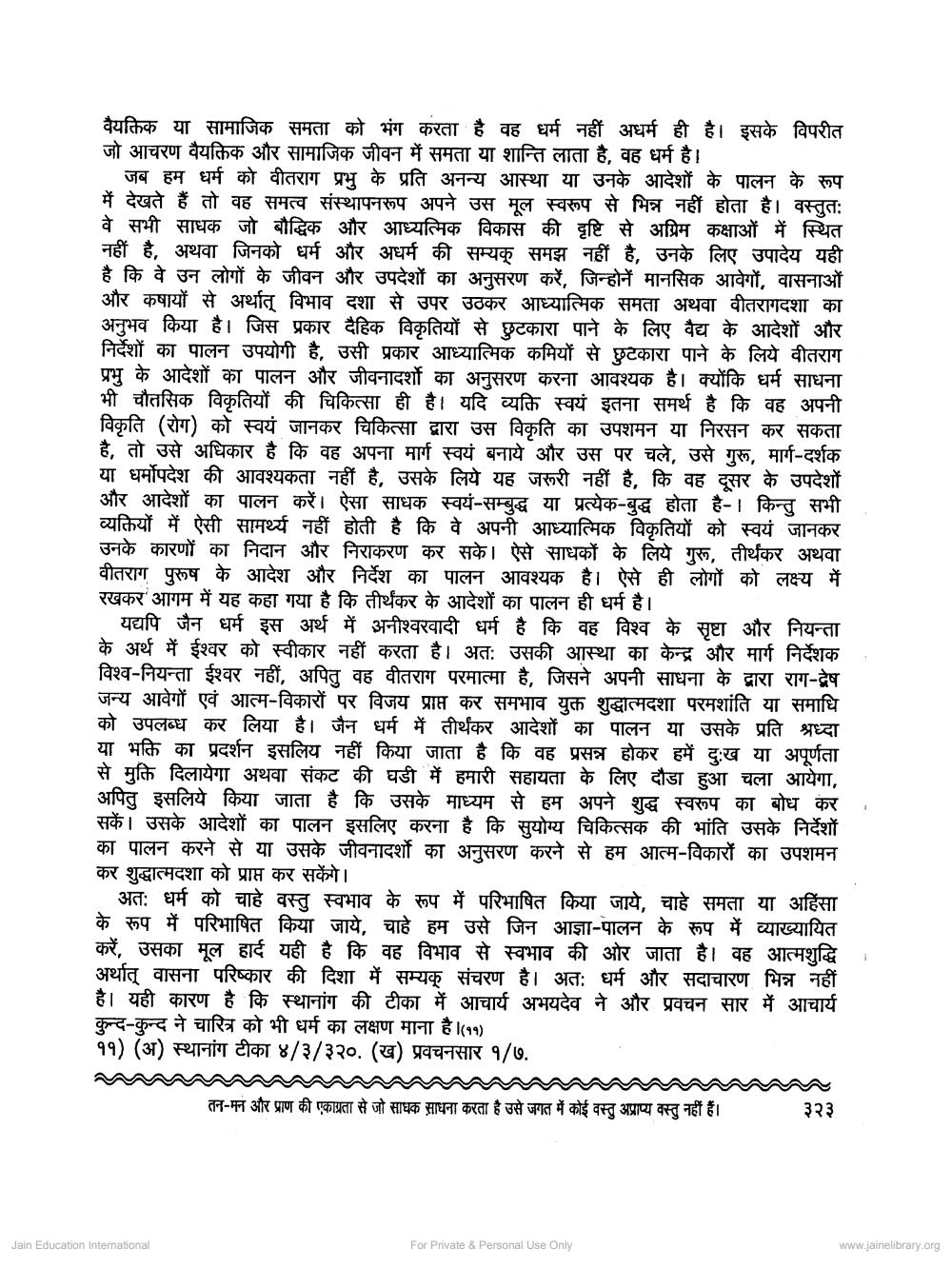________________
वैयक्तिक या सामाजिक समता को भंग करता है वह धर्म नहीं अधर्म ही है। इसके विपरीत जो आचरण वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समता या शान्ति लाता है, वह धर्म है।
जब हम धर्म को वीतराग प्रभु के प्रति अनन्य आस्था या उनके आदेशों के पालन के रूप में देखते हैं तो वह समत्व संस्थापनरूप अपने उस मूल स्वरूप से भिन्न नहीं होता है। वस्तुतः वे सभी साधक जो बौद्धिक और आध्यत्मिक विकास की दृष्टि से अग्रिम कक्षाओं में स्थित नहीं है, अथवा जिनको धर्म और अधर्म की सम्यक् समझ नहीं है, उनके लिए उपादेय यही है कि वे उन लोगों के जीवन और उपदेशों का अनुसरण करें, जिन्होनें मानसिक आवेगों, वासनाओं और कषायों से अर्थात् विभाव दशा से उपर उठकर आध्यात्मिक समता अथवा वीतरागदशा का अनुभव किया है। जिस प्रकार दैहिक विकृतियों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य के आदेशों और निर्देशों का पालन उपयोगी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक कमियों से छुटकारा पाने के लिये वीतराग प्रभु के आदेशों का पालन और जीवनादर्शो का अनुसरण करना आवश्यक है। क्योंकि धर्म साधना भी चौतसिक विकृतियों की चिकित्सा ही है। यदि व्यक्ति स्वयं इतना समर्थ है कि वह अपनी विकृति (रोग) को स्वयं जानकर चिकित्सा द्वारा उस विकृति का उपशमन या निरसन कर सकता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपना मार्ग स्वयं बनाये और उस पर चले, उसे गुरू, मार्ग-दर्शक या धर्मोपदेश की आवश्यकता नहीं है, उसके लिये यह जरूरी नहीं है, कि वह दूसर के उपदेशों और आदेशों का पालन करें। ऐसा साधक स्वयं सम्बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध होता है । किन्तु सभी व्यक्तियों में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक विकृतियों को स्वयं जानकर उनके कारणों का निदान और निराकरण कर सके। ऐसे साधकों के लिये गुरू, तीर्थंकर अथवा वीतराग पुरुष के आदेश और निर्देश का पालन आवश्यक है। ऐसे ही लोगों को लक्ष्य में रखकर आगम में यह कहा गया है कि तीर्थंकर के आदेशों का पालन ही धर्म है ।
यद्यपि जैन धर्म इस अर्थ में अनीश्वरवादी धर्म है कि वह विश्व के सृष्टा और नियन्ता के अर्थ में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। अतः उसकी आस्था का केन्द्र और मार्ग निर्देशक विश्व - नियन्ता ईश्वर नहीं, अपितु वह वीतराग परमात्मा है, जिसने अपनी साधना के द्वारा राग-द्वेष जन्य आवेगों एवं आत्म-विकारों पर विजय प्राप्त कर समभाव युक्त शुद्धात्मदशा परमशांति या समाधि को उपलब्ध कर लिया है। जैन धर्म में तीर्थंकर आदेशों का पालन या उसके प्रति श्रध्दा या भक्ति का प्रदर्शन इसलिय नहीं किया जाता है कि वह प्रसन्न होकर हमें दुःख या अपूर्णता से मुक्ति दिलायेगा अथवा संकट की घडी में हमारी सहायता के लिए दौडा हुआ चला आयेगा, अपितु इसलिये किया जाता है कि उसके माध्यम से हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध कर सकें। उसके आदेशों का पालन इसलिए करना है कि सुयोग्य चिकित्सक की भांति उसके निर्देशों का पालन करने से या उसके जीवनादर्शो का अनुसरण करने से हम आत्म-विकारों का उपशमन कर शुद्धात्मदशा को प्राप्त कर सकेंगे।
अतः धर्म को चाहे वस्तु स्वभाव के रूप में परिभाषित किया जाये, चाहे समता या अहिंसा के रूप में परिभाषित किया जाये, चाहे हम उसे जिन आज्ञा-पालन के रूप में व्याख्यायित करें, उसका मूल हार्द यही है कि वह विभाव से स्वभाव की ओर जाता है। वह आत्मशुद्धि अर्थात् वासना परिष्कार की दिशा में सम्यक् संचरण है। अतः धर्म और सदाचारण भिन्न नहीं है। यही कारण है कि स्थानांग की टीका में आचार्य अभयदेव ने और प्रवचन सार में आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र को भी धर्म का लक्षण माना है । (११)
११) (अ) स्थानांग टीका ४ / ३ / ३२० (ख) प्रवचनसार १ / ७.
Jain Education International
तन-मन और प्राण की एकाग्रता से जो साधक साधना करता है उसे जगत में कोई वस्तु अप्राप्य वस्तु नहीं हैं।
For Private Personal Use Only
३२३
1
www.jainelibrary.org