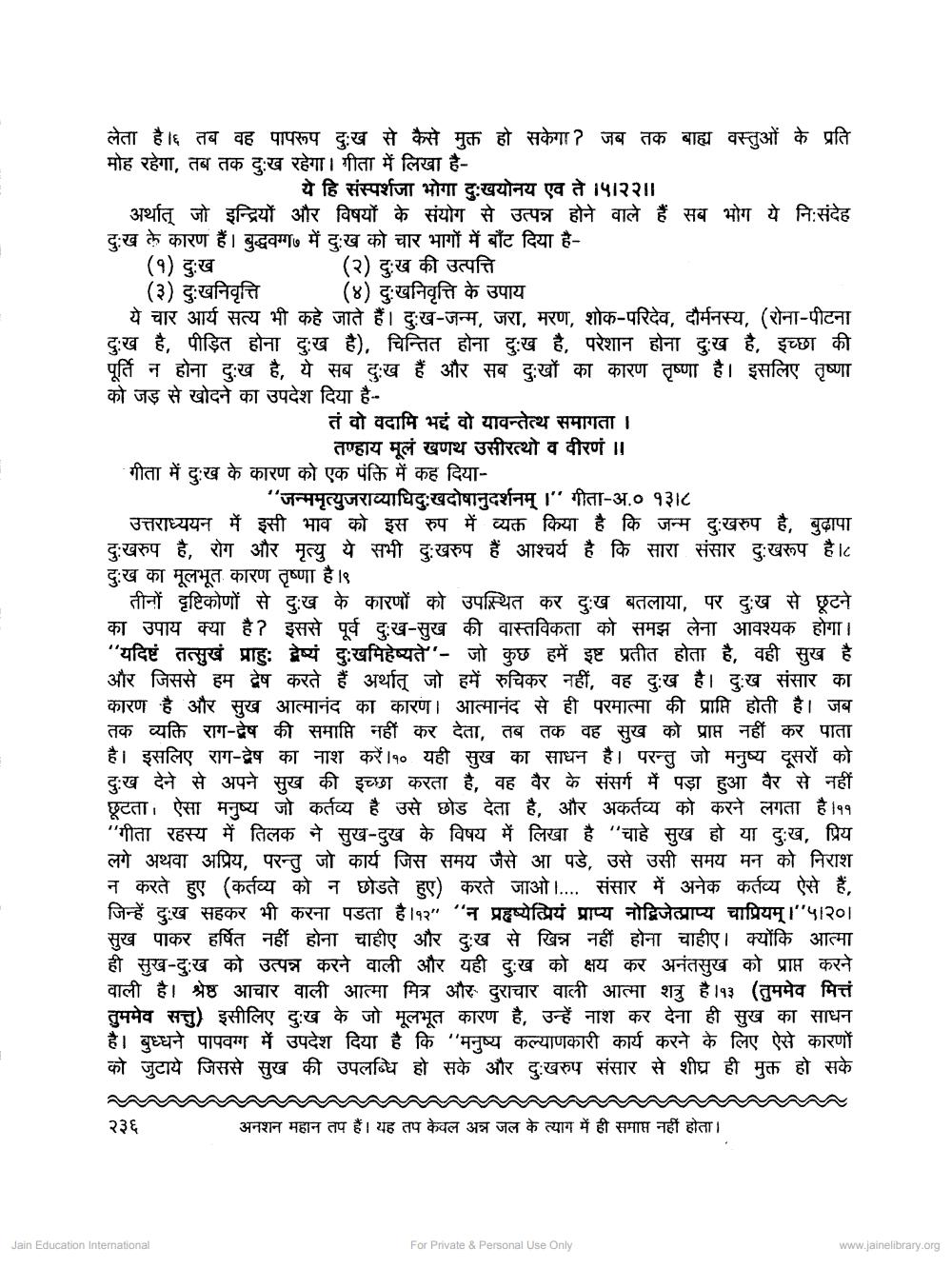________________
लेता है । ६ तब वह पापरूप दुःख से कैसे मुक्त हो सकेगा ? जब तक बाह्य वस्तुओं के प्रति मोह रहेगा, तब तक दुःख रहेगा। गीता में लिखा है
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते |५|२२||
दुःख
अर्थात् जो इन्द्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं सब भोग ये नि:संदेह के कारण हैं। बुद्धवग्ग में दुःख को चार भागों में बाँट दिया है(२) दुःख की उत्पत्ति
(४) दुःखनिवृत्ति के उपाय
(१) दु:ख
(३) दुःखनिवृत्ति
ये चार आर्य सत्य भी कहे जाते हैं। दुःख जन्म, जरा, मरण, शोक-परिदेव, दौर्मनस्य, ( रोना पीटना दुःख है, पीड़ित होना दुःख है), चिन्तित होना दुःख है, परेशान होना दुःख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुःख है, ये सब दुःख हैं और सब दुःखों का कारण तृष्णा है। इसलिए तृष्णा को जड़ से खोदने का उपदेश दिया है
गीता में दुःख के कारण को एक पंक्ति में कह दिया
तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्थ समागता । तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो व वीरणं ॥
"जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।" गीता - अ. ० १३८
उत्तराध्ययन में इसी भाव को इस रूप में व्यक्त किया है कि जन्म दुःखरूप है, बुढ़ापा दुःखरूप है, रोग और मृत्यु ये सभी दु:खरुप हैं आश्चर्य है कि सारा संसार दुःखरूप है ।८ दुःख का मूलभूत कारण तृष्णा है । ९
तीनों दृष्टिकोणों से दुःख के कारणों को उपस्थित कर दुःख बतलाया, पर दुःख से छूटने का उपाय क्या है ? इससे पूर्व दुःख-सुख की वास्तविकता को समझ लेना आवश्यक होगा। "यदिष्टं तत्सुखं प्राहुः द्वेष्यं दुःखमिहेष्यते " - जो कुछ हमें इष्ट प्रतीत होता है, वही सुख है और जिससे हम द्वेष करते हैं अर्थात् जो हमें रुचिकर नहीं, वह दुःख है । दुःख संसार का कारण है और सुख आत्मानंद का कारण । आत्मानंद से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति राग-द्वेष की समाप्ति नहीं कर देता, तब तक वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए राग-द्वेष का नाश करें | १० यही सुख का साधन है। परन्तु जो मनुष्य दूसरों को दुःख देने से अपने सुख की इच्छा करता है, वह वैर के संसर्ग में पड़ा हुआ वैर से नहीं छूटता। ऐसा मनुष्य जो कर्तव्य है उसे छोड़ देता है, और अकर्तव्य को करने लगता है ।११ "गीता रहस्य में तिलक ने सुख-दुख के विषय में लिखा है " चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय लगे अथवा अप्रिय, परन्तु जो कार्य जिस समय जैसे आ पडे, उसे उसी समय मन को निराश न करते हुए ( कर्तव्य को न छोड़ते हुए ) करते जाओ।.... संसार में अनेक कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें दुःख सहकर भी करना पडता है । १२" " न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् | ५|२०| सुख पाकर हर्षित नहीं होना चाहीए और दुःख से खिन्न नहीं होना चाहीए। क्योंकि आत्मा ही सुख-दुःख को उत्पन्न करने वाली और यही दुःख को क्षय कर अनंतसुख को प्राप्त करने वाली है। श्रेष्ठ आचार वाली आत्मा मित्र और दुराचार वाली आत्मा शत्रु है । १३ (तुममेव मित्तं तुममेव सत्तु ) इसीलिए दुःख के जो मूलभूत कारण है, उन्हें नाश कर देना ही सुख का साधन है। बुध्धने पापवग्ग में उपदेश दिया है कि "मनुष्य कल्याणकारी कार्य करने के लिए ऐसे कारणों को जुटाये जिससे सुख की उपलब्धि हो सके और दुःखरुप संसार से शीघ्र ही मुक्त हो सके
२३६
Jain Education International
अनशन महान तप हैं। यह तप केवल अन्न जल के त्याग में ही समाप्त नहीं होता।
For Private Personal Use Only
www.jainelibrary.org