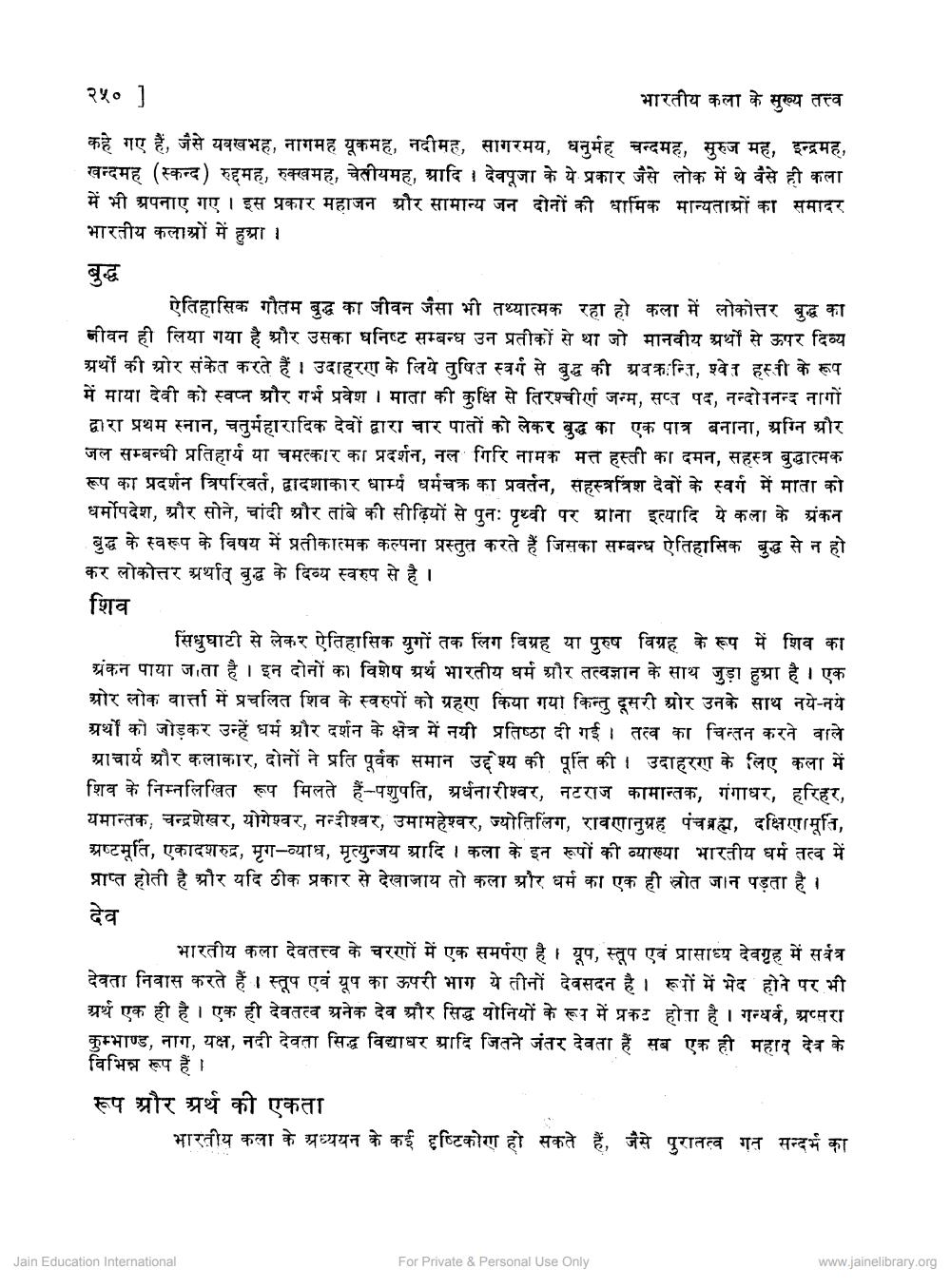________________
२५० ]
कहे गए हैं, जैसे यवखभह, नागमह यूकमह, नदीमह, सागरमय, धनुर्मह चन्दमह, सुरुज मह, इन्द्रमह, खन्दमह (स्कन्द ) रुद्दमह्, रुक्खमह, चेतीयमह, आदि । देवपूजा के ये प्रकार जैसे लोक में थे वैसे ही कला में भी अपनाए गए । इस प्रकार महाजन और सामान्य जन दोनों की धार्मिक मान्यताओं का समादर भारतीय कलाओं में हुआ ।
बुद्ध
कला में लोकोत्तर बुद्ध का मानवीय अर्थों से ऊपर दिव्य
ऐतिहासिक गौतम बुद्ध का जीवन जैसा भी तथ्यात्मक रहा हो जीवन ही लिया गया है और उसका घनिष्ट सम्बन्ध उन प्रतीकों से था जो अर्थों की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिये तुषित स्वर्ग से बुद्ध की प्रवक्रान्ति, श्वेत हस्ती के रूप में माया देवी को स्वप्न और गर्भ प्रवेश । माता की कुक्षि से तिरश्चीर्ण जन्म, सप्त पद, नन्दोपनन्द नागों द्वारा प्रथम स्नान, चतुर्महारादिक देवों द्वारा चार पातों को लेकर बुद्ध का एक पात्र बनाना, अग्नि और जल सम्बन्धी प्रतिहार्य या चमत्कार का प्रदर्शन, नल गिरि नामक मत्त हस्ती का दमन, सहस्त्र बुद्धात्मक रूप का प्रदर्शन त्रिपरिवर्त, द्वादशाकार धार्म्य धर्मचक्र का प्रवर्तन, सहस्त्रत्रिश देवों के स्वर्ग में माता को धर्मोपदेश, और सोने, चांदी और तांबे की सीढ़ियों से पुनः पृथ्वी पर आना इत्यादि ये कला के अंकन बुद्ध के स्वरूप के विषय में प्रतीकात्मक कल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसका सम्बन्ध ऐतिहासिक बुद्ध से न हो कर लोकोत्तर अर्थात् बुद्ध के दिव्य स्वरुप से है ।
शिव
भारतीय कला के
सिंधुघाटी से लेकर ऐतिहासिक युगों तक लिंग विग्रह या पुरुष विग्रह के रूप में शिव का पाया जाता है । इन दोनों का विशेष अर्थ भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है । एक ओर लोक वार्ता में प्रचलित शिव के स्वरुपों को ग्रहण किया गया किन्तु दूसरी ओर उनके साथ नये-नये अर्थों को जोड़कर उन्हें धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नयी प्रतिष्ठा दी गई। तत्व का चिन्तन करने वाले आचार्य और कलाकार, दोनों ने प्रति पूर्वक समान उद्देश्य की पूर्ति की । उदाहरण के लिए कला में शिव के निम्नलिखित रूप मिलते हैं - पशुपति, अर्धनारीश्वर, नटराज कामान्तक, गंगाधर, हरिहर, यमान्तक, चन्द्रशेखर, योगेश्वर, नन्दीश्वर, उमामहेश्वर, ज्योतिलिंग, रावणानुग्रह पंचब्रह्म, दक्षिणामूर्ति, अष्टमूर्ति एकादश रुद्र, मृग-व्याध, मृत्युन्जय आदि। कला के इन रूपों की व्याख्या भारतीय धर्म तत्व में प्राप्त होती है और यदि ठीक प्रकार से देखाजाय तो कला और धर्म का एक ही स्रोत जान पड़ता है ।
देव
रूप और अर्थ की एकता
मुख्य तत्त्व
भारतीय कला देवतत्त्व के चरणों में एक समर्पण है। यूप, स्तूप एवं प्रासाध्य देवगृह में सर्वत्र देवता निवास करते हैं । स्तूप एवं यूप का ऊपरी भाग ये तीनों देवसदन है । रूपों में भेद होने पर भी अर्थ एक ही है। एक ही देवतत्व अनेक देव और सिद्ध योनियों के रूप में प्रकट होता है । गन्धर्व, अप्सरा कुम्भाण्ड, नाग, यक्ष, नदी देवता सिद्ध विद्याधर प्रादि जितने जंतर देवता हैं सब एक ही महान देव के विभिन्न रूप हैं ।
Jain Education International
भारतीय कला के अध्ययन के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे पुरातत्व गत सन्दर्भ का
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org