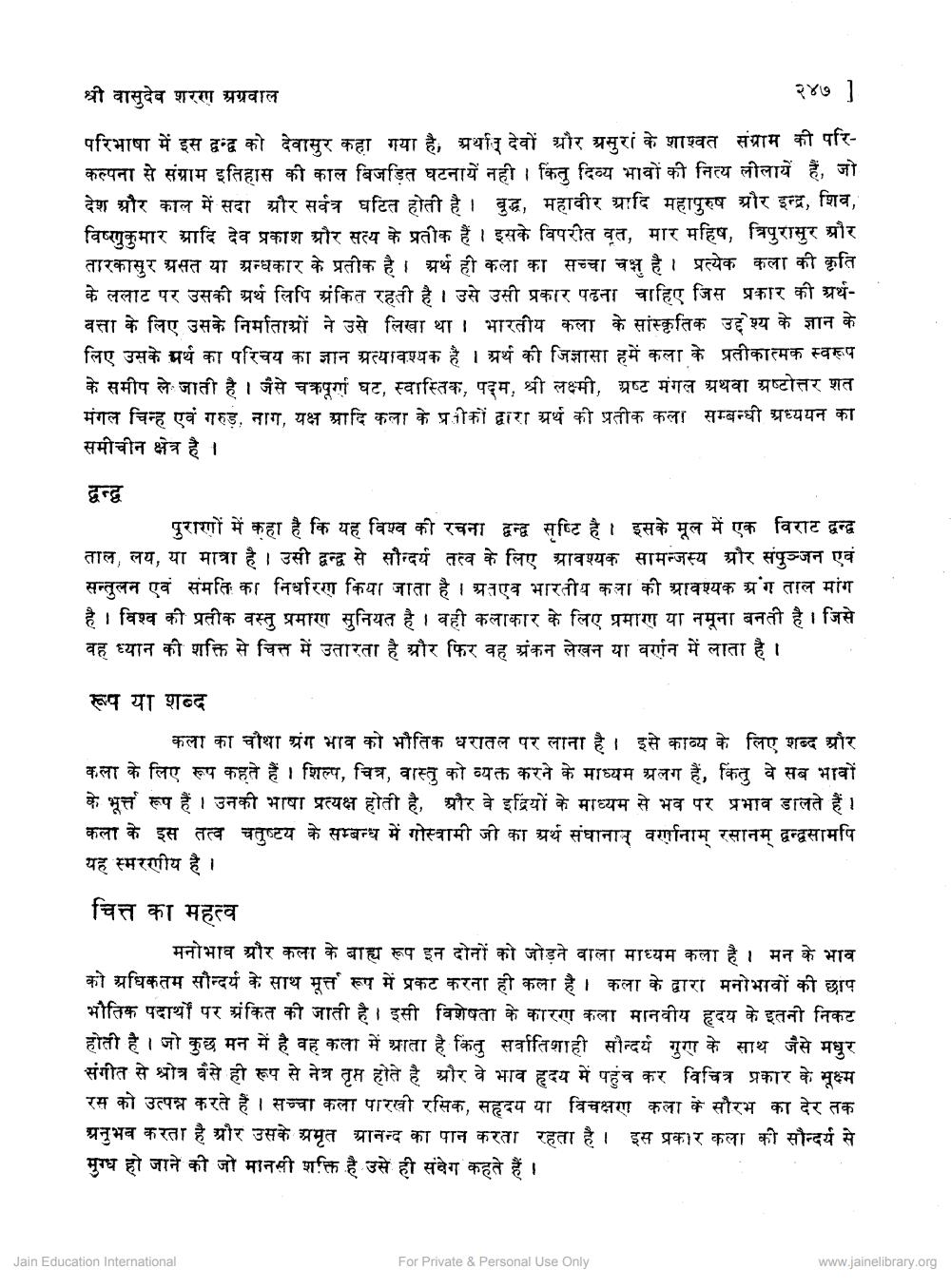________________
श्री वासुदेव शरण अग्रवाल
२४७ ] परिभाषा में इस द्वन्द्व को देवासुर कहा गया है, अर्थात् देवों और असुरां के शाश्वत संग्राम की परिकल्पना से संग्राम इतिहास की काल बिजड़ित घटनायें नही। किंतु दिव्य भावों की नित्य लीलायें हैं, जो देश और काल में सदा और सर्वत्र घटित होती है। बुद्ध, महावीर प्रादि महापुरुष और इन्द्र, शिव, विष्णुकुमार आदि देव प्रकाश और सत्य के प्रतीक हैं । इसके विपरीत वृत, मार महिष, त्रिपुरासुर और तारकासुर असत या अन्धकार के प्रतीक है। अर्थ ही कला का सच्चा चक्ष है। प्रत्येक कला की कृति के ललाट पर उसकी अर्थ लिपि अंकित रहती है। उसे उसी प्रकार पढना चाहिए जिस प्रकार की अर्थबत्ता के लिए उसके निर्माताओं ने उसे लिखा था। भारतीय कला के सांस्कृतिक उद्देश्य के ज्ञान के लिए उसके पर्थ का परिचय का ज्ञान अत्यावश्यक है । अर्थ की जिज्ञासा हमें कला के प्रतीकात्मक स्वरूप के समीप ले जाती है । जैसे चक्रपूर्ण घट, स्वास्तिक, पद्म, श्री लक्ष्मी, अष्ट मंगल अथवा अष्टोत्तर शत मंगल चिन्ह एवं गरुड़, नाग, यक्ष आदि कला के प्रतीकों द्वारा अर्थ की प्रतीक कला सम्बन्धी अध्ययन का समीचीन क्षेत्र है।
द्वन्द्व
पुराणों में कहा है कि यह विश्व की रचना द्वन्द्व सष्टि है। इसके मूल में एक विराट द्वन्द्व ताल, लय, या मात्रा है। उसी द्वन्द्व से सौन्दर्य तत्व के लिए आवश्यक सामन्जस्य और संपुजन एवं सन्तुलन एवं संमति का निर्धारण किया जाता है । अतएव भारतीय कला की आवश्यक अंग ताल मांग है । विश्व की प्रतीक वस्तु प्रमाण सुनियत है । वही कलाकार के लिए प्रमाण या नमूना बनती है । जिसे वह ध्यान की शक्ति से चित्त में उतारता है और फिर वह अंकन लेखन या वर्णन में लाता है।
रूप या शब्द
कला का चौथा अंग भाव को भौतिक धरातल पर लाना है। इसे काव्य के लिए शब्द और कला के लिए रूप कहते हैं । शिल्प, चित्र, वास्तु को व्यक्त करने के माध्यम अलग हैं, किंतु वे सब भावों के भूर्त रूप हैं । उनकी भाषा प्रत्यक्ष होती है, और वे इद्रियों के माध्यम से भव पर प्रभाव डालते हैं। कला के इस तत्व चतुष्टय के सम्बन्ध में गोस्वामी जी का अर्थ संघानान् वर्णानाम् रसानम् द्वन्द्वसामपि यह स्मरणीय है।
चित्त का महत्व
मनोभाव और कला के बाह्य रूप इन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम कला है। मन के भाव को अधिकतम सौन्दर्य के साथ मृत रूप में प्रकट करना ही कला है। कला के द्वारा मनोभावों की छाप भौतिक पदार्थों पर अंकित की जाती है। इसी विशेषता के कारण कला मानवीय हृदय के इतनी निकट होती है । जो कुछ मन में है वह कला में श्राता है किंतु सर्वातिशाही सौन्दर्य गुण के साथ जैसे मधुर संगीत से श्रोत्र वैसे ही रूप से नेत्र तृप्त होते है और वे भाव हृदय में पहुंच कर विचित्र प्रकार के मूक्ष्म रस को उत्पन्न करते हैं । सच्चा कला पारखी रसिक, सहृदय या विचक्षण कला के सौरभ का देर तक अनुभव करता है और उसके अमृत प्रानन्द का पान करता रहता है। इस प्रकार कला की सौन्दर्य से मुग्ध हो जाने की जो मानसी शक्ति है उसे ही संवेग कहते हैं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org