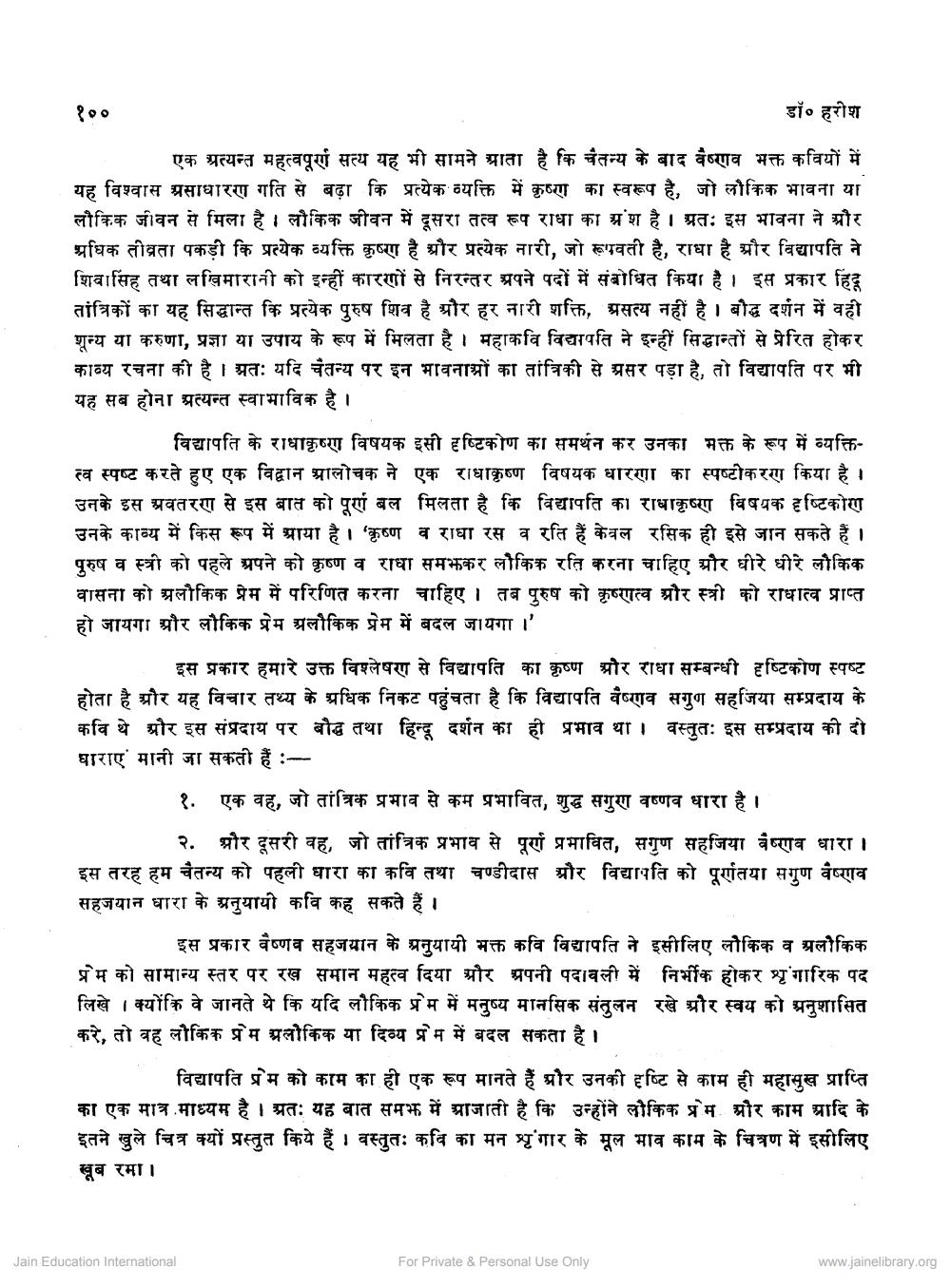________________
डॉ. हरीश
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्य यह भी सामने पाता है कि चैतन्य के बाद वैष्णव भक्त कवियों में यह विश्वास असाधारण गति से बढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण का स्वरूप है, जो लौकिक भावना या लौकिक जीवन से मिला है। लौकिक जीवन में दूसरा तत्व रूप राधा का अंश है। अतः इस भावना ने और अधिक तीव्रता पकडी कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण है और प्रत्येक नारी, जो रूपवती है, राधा है और विद्यापति ने शिवासिंह तथा लखिमारानी को इन्हीं कारणों से निरन्तर अपने पदों में संबोधित किया है। इस प्रकार हिंदू तांत्रिकों का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक पुरुष शिव है और हर नारी शक्ति, असत्य नहीं है । बौद्ध दर्शन में वही शुन्य या करुणा, प्रज्ञा या उपाय के रूप में मिलता है। महाकवि विद्यापति ने इन्हीं सिद्धान्तों से प्रेरित होकर काव्य रचना की है। अत: यदि चैतन्य पर इन भावनाओं का तांत्रिकी से असर पड़ा है, तो विद्यापति पर भी यह सब होना अत्यन्त स्वाभाविक है।
विद्यापति के राधाकृष्ण विषयक इसी दृष्टिकोण का समर्थन कर उनका भक्त के रूप में व्यक्तित्व स्पष्ट करते हुए एक विद्वान आलोचक ने एक राधाकृष्ण विषयक धारणा का स्पष्टीकरण किया है। उनके इस अवतरण से इस बात को पूर्ण बल मिलता है कि विद्यापति का राधाकृष्ण विषयक दृष्टिकोण उनके काव्य में किस रूप में पाया है। 'कृष्ण व राधा रस व रति हैं केवल रसिक ही इसे जान सकते हैं। पुरुष व स्त्री को पहले अपने को कृष्ण व राधा समझकर लौकिक रति करना चाहिए और धीरे धीरे लौकिक वासना को अलौकिक प्रेम में परिणित करना चाहिए। तब पुरुष को कृष्णत्व और स्त्री को राधात्व प्राप्त हो जायगा और लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल जायगा।'
. इस प्रकार हमारे उक्त विश्लेषण से विद्यापति का कृष्ण और राधा सम्बन्धी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और यह विचार तथ्य के अधिक निकट पहुंचता है कि विद्यापति वैष्णव सगुण सहजिया सम्प्रदाय के कवि थे और इस संप्रदाय पर बौद्ध तथा हिन्दू दर्शन का ही प्रभाव था। वस्तुतः इस सम्प्रदाय की दो धाराए मानी जा सकती हैं :
१. एक वह, जो तांत्रिक प्रभाव से कम प्रभावित, शुद्ध सगुण वष्णव धारा है ।
२. और दूसरी वह, जो तांत्रिक प्रभाव से पूर्ण प्रभावित, सगुण सहजिया वैष्णव धारा । इस तरह हम चैतन्य को पहली धारा का कवि तथा चण्डीदास और विद्यापति को पूर्णतया सगुण वैष्णव सहजयान धारा के अनुयायी कवि कह सकते हैं।
___ इस प्रकार वैष्णव सहजयान के अनुयायी भक्त कवि विद्यापति ने इसीलिए लौकिक व अलौकिक प्रेम को सामान्य स्तर पर रख समान महत्व दिया और अपनी पदावली में निर्भीक होकर शृगारिक पद लिखे । क्योंकि वे जानते थे कि यदि लौकिक प्रेम में मनुष्य मानसिक संतुलन रखे और स्वय को अनुशासित करे, तो वह लौकिक प्रेम अलौकिक या दिव्य प्रेम में बदल सकता है।
विद्यापति प्रेम को काम का ही एक रूप मानते हैं और उनकी दृष्टि से काम ही महासुख प्राप्ति का एक मात्र माध्यम है। अतः यह बात समझ में जाती है कि उन्होंने लौकिक प्रेम और काम आदि के इतने खुले चित्र क्यों प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः कवि का मन शृगार के मूल भाव काम के चित्रण में इसीलिए खूब रमा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org