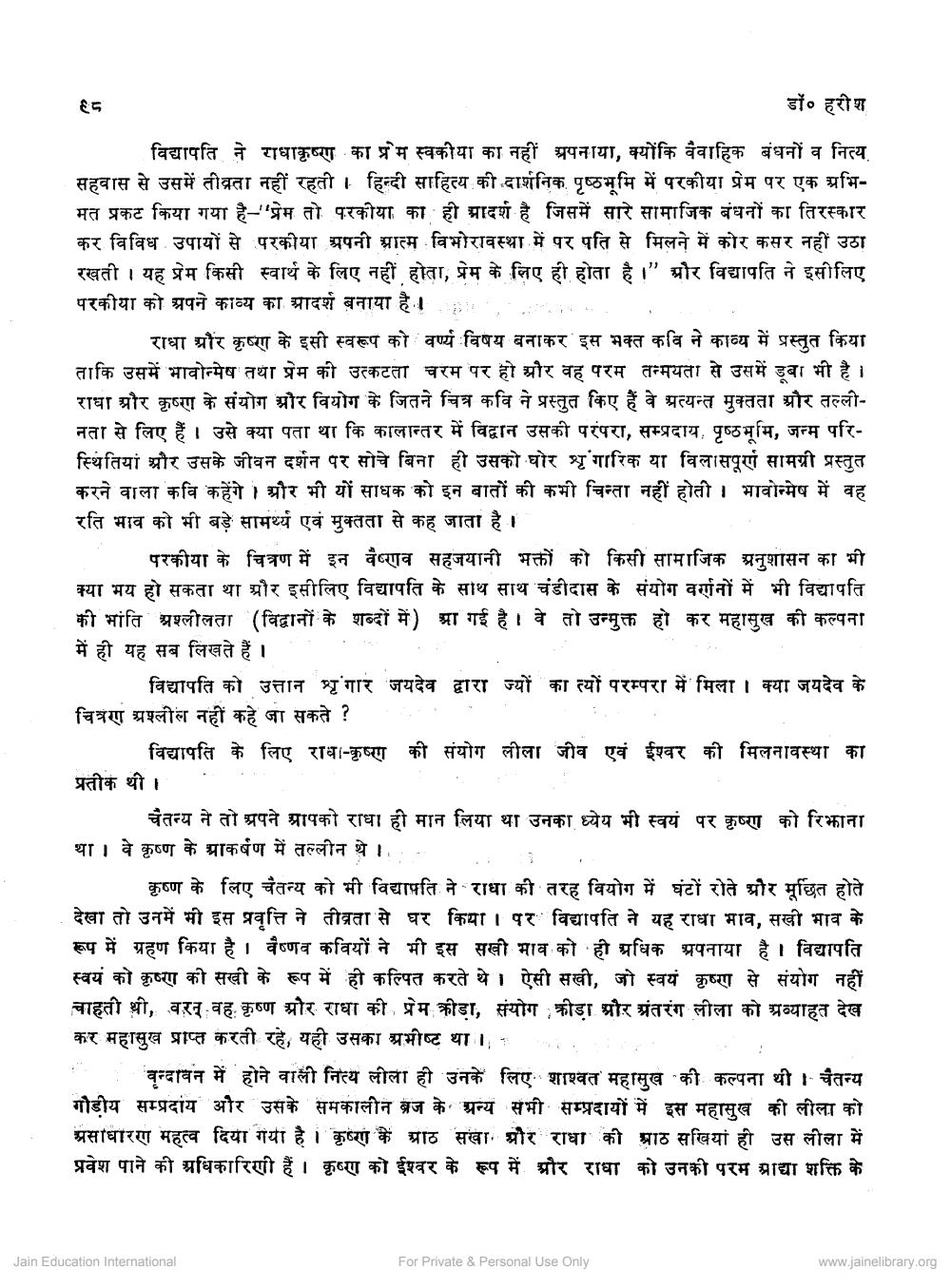________________
डॉ. हरीश
विद्यापति ने राधाकृष्ण का प्रेम स्वकीया का नहीं अपनाया, क्योंकि वैवाहिक बंधनों व नित्य सहवास से उसमें तीव्रता नहीं रहती। हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि में परकीया प्रेम पर एक अभिमत प्रकट किया गया है-"प्रेम तो परकीया का ही आदर्श है जिसमें सारे सामाजिक बंधनों का तिरस्कार कर विविध उपायों से परकीया अपनी प्रात्म विभोरावस्था में पर पति से मिलने में कोर कसर नहीं उठा रखती । यह प्रेम किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता, प्रेम के लिए ही होता है।" और विद्यापति ने इसीलिए परकीया को अपने काव्य का आदर्श बनाया है।
राधा और कृष्ण के इसी स्वरूप को वर्ण्य विषय बनाकर इस भक्त कवि ने काव्य में प्रस्तुत किया ताकि उसमें भावोन्मेष तथा प्रेम की उत्कटता चरम पर हो और वह परम तन्मयता से उसमें डुबा भी है। राधा और कृष्ण के संयोग और वियोग के जितने चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं वे अत्यन्त मुक्तता और तल्लीनता से लिए हैं। उसे क्या पता था कि कालान्तर में विद्वान उसकी परंपरा, सम्प्रदाय, पृष्ठभूमि, जन्म परिस्थितियां और उसके जीवन दर्शन पर सोचे बिना ही उसको घोर शृगारिक या विलासपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने वाला कवि कहेंगे। और भी यों साधक को इन बातों की कमी चिन्ता नहीं होती। भावोन्मेष में वह रति भाव को भी बड़े सामर्थ्य एवं मुक्तता से कह जाता है।
परकीया के चित्रण में इन वैष्णव सहजयानी भक्तों को किसी सामाजिक अनुशासन का भी क्या भय हो सकता था और इसीलिए विद्यापति के साथ साथ चंडीदास के संयोग वर्णनों में भी विद्यापति की भांति अश्लीलता (विद्वानों के शब्दों में आ गई है। वे तो उन्मुक्त हो कर महासुख की कल्पना में ही यह सब लिखते हैं।
विद्यापति को उत्तान शृगार जयदेव द्वारा ज्यों का त्यों परम्परा में मिला । क्या जयदेव के चित्रण अश्लील नहीं कहे जा सकते ?
विद्यापति के लिए राधा-कृष्ण की संयोग लीला जीव एवं ईश्वर की मिलनावस्था का प्रतीक थी।
चैतन्य ने तो अपने आपको राधा ही मान लिया था उनका ध्येय भी स्वयं पर कृष्ण को रिझाना था। वे कृष्ण के आकर्षण में तल्लीन थे।
कृष्ण के लिए चैतन्य को भी विद्यापति ने राधा की तरह वियोग में घंटों रोते और मुछित होते देखा तो उनमें भी इस प्रवृत्ति ने तीव्रता से घर किया। पर विद्यापति ने यह राधा भाव, सखी भाव के रूप में ग्रहण किया है । वैष्णव कवियों ने भी इस सखी भाव को ही अधिक अपनाया है। विद्यापति स्वयं को कृष्ण की सखी के रूप में ही कल्पित करते थे। ऐसी सखी, जो स्वयं कृष्ण से संयोग नहीं चाहती थी, वरन् वह कृष्ण और राधा की प्रेम क्रीडा, संयोग क्रीडा और अंतरंग लीला को अव्याहत देख कर महासुख प्राप्त करती रहे, यही उसका अभीष्ट था। - वृन्दावन में होने वाली नित्य लीला ही उनके लिए शाश्वत महासुख की कल्पना थी। चैतन्य गौड़ीय सम्प्रदाय और उसके समकालीन ब्रज के अन्य सभी सम्प्रदायों में इस महासुख की लीला को असाधारण महत्व दिया गया है। कृष्ण के पाठ सखा और राधा की पाठ सखियां ही उस लीला में प्रवेश पाने की अधिकारिणी हैं। कृष्ण को ईश्वर के रूप में और राधा को उनकी परम प्राद्या शक्ति के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org