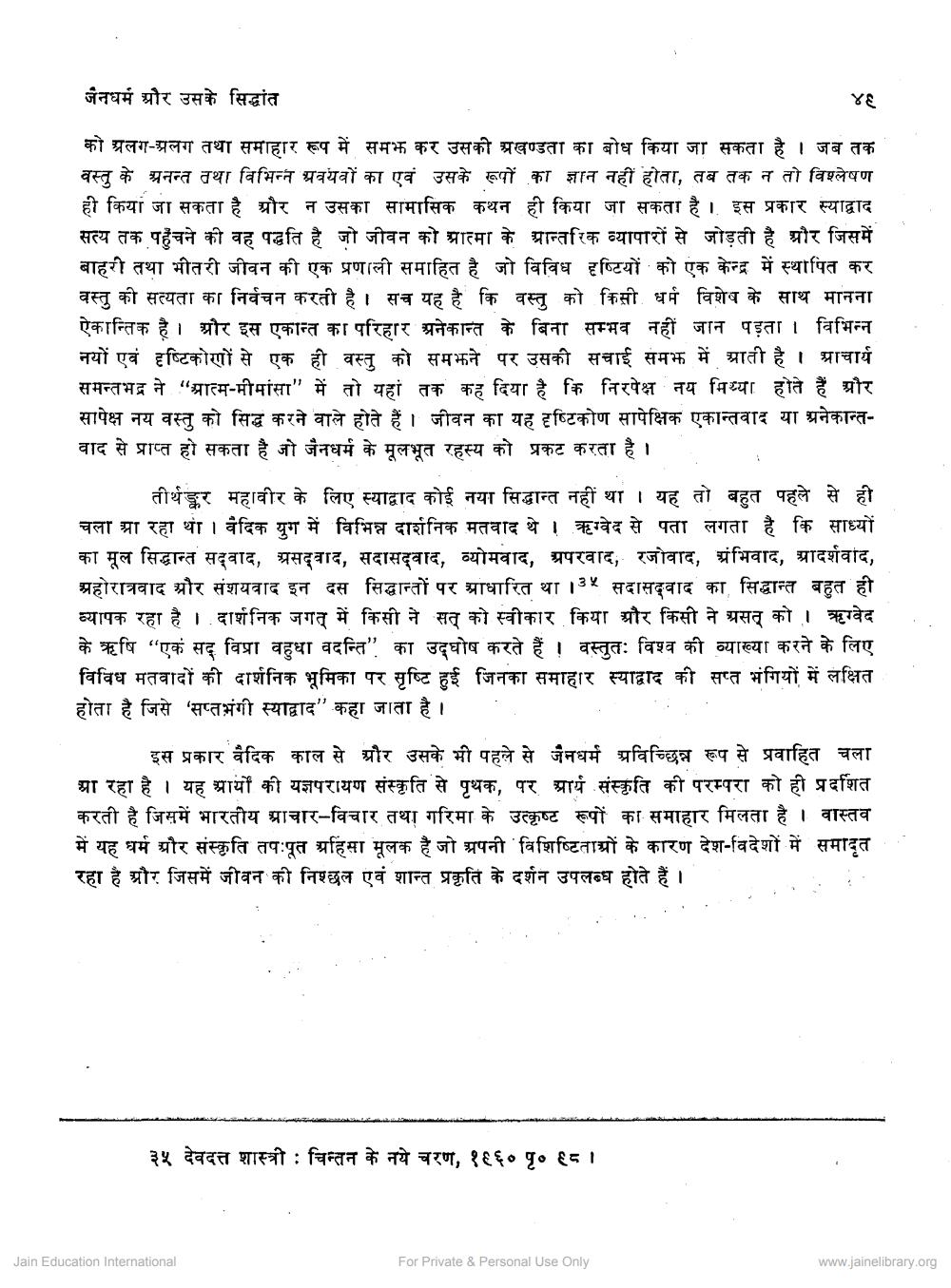________________
जैनधर्म और उसके सिद्धांत
४६
को अलग-अलग तथा समाहार रूप में समझ कर उसकी अखण्डता का बोध किया जा सकता है । जब तक वस्तु के अनन्त तथा विभिन्न अवयवों का एवं उसके रूपों का ज्ञान नहीं होता, तब तक न तो विश्लेषण ही किया जा सकता है और न उसका सामासिक कथन ही किया जा सकता है। इस प्रकार स्याद्वाद सत्य तक पहुँचने की वह पद्धति है जो जीवन को प्रात्मा के आन्तरिक व्यापारों से जोड़ती है और जिसमें बाहरी तथा भीतरी जीवन की एक प्रणाली समाहित है जो विविध दृष्टियों को एक केन्द्र में स्थापित कर वस्तु की सत्यता का निर्वचन करती है। सच यह है कि वस्तु को किसी धर्म विशेष के साथ मानना ऐकान्तिक है। और इस एकान्त का परिहार अनेकान्त के बिना सम्भव नहीं जान पड़ता । विभिन्न नयों एवं दृष्टिकोणों से एक ही वस्तु को समझने पर उसकी सचाई समझ में आती है । प्राचार्य समन्तभद्र ने "आत्म-मीमांसा" में तो यहां तक कह दिया है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय वस्तु को सिद्ध करने वाले होते हैं। जीवन का यह दृष्टिकोण सापेक्षिक एकान्तवाद या अनेकान्तवाद से प्राप्त हो सकता है जो जैनधर्म के मूलभूत रहस्य को प्रकट करता है ।
तीर्थङ्कर महावीर के लिए स्याद्वाद कोई नया सिद्धान्त नहीं था । यह तो बहुत पहले से ही चला आ रहा था। वैदिक यूग में विभिन्न दार्शनिक मतवाद थे । ऋग्वेद से पता लगता है कि साध्यों का मूल सिद्धान्त सद्वाद, असद्वाद, सदासद्वाद, व्योमवाद, अपरवाद, रजोवाद, अंभिवाद, आदर्शवाद, अहोरात्रवाद और संशयवाद इन दस सिद्धान्तों पर आधारित था । ३५ सदासद्वाद का सिद्धान्त बहुत ही व्यापक रहा है । दार्शनिक जगत् में किसी ने सत् को स्वीकार किया और किसी ने असत् को । ऋग्वेद के ऋषि “एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" का उद्घोष करते हैं । वस्तुतः विश्व की व्याख्या करने के लिए विविध मतवादों की दार्शनिक भूमिका पर सृष्टि हुई जिनका समाहार स्याद्वाद की सप्त भंगियों में लक्षित होता है जिसे 'सप्तभंगी स्याद्वाद" कहा जाता है ।
इस प्रकार वैदिक काल से और उसके भी पहले से जैनधर्म अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित चला आ रहा है । यह आर्यों की यज्ञपरायण संस्कृति से पृथक, पर आर्य संस्कृति की परम्परा को ही प्रदर्शित करती है जिसमें भारतीय प्राचार-विचार तथा गरिमा के उत्कृष्ट रूपों का समाहार मिलता है । वास्तव में यह धर्म और संस्कृति तपःपूत अहिंसा मूलक है जो अपनी विशिष्टिताओं के कारण देश-विदेशों में समादृत रहा है और जिसमें जीवन की निश्छल एवं शान्त प्रकृति के दर्शन उपलब्ध होते हैं।
३५ देवदत्त शास्त्री : चिन्तन के नये चरण, १९६० पृ०६८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org