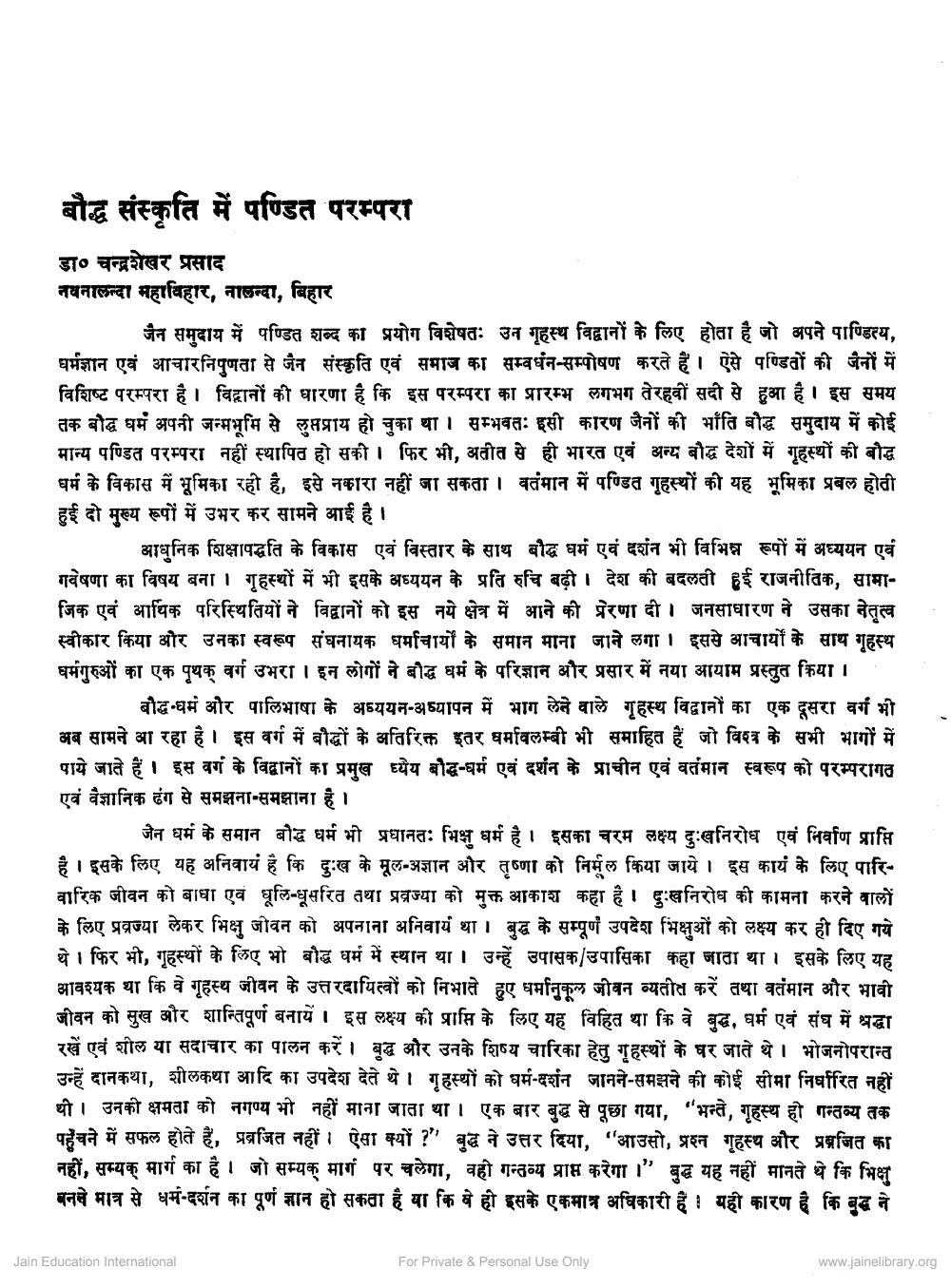________________
बौद्ध संस्कृति में पण्डित परम्परा डा० चन्द्रशेखर प्रसाद नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार
जैन समुदाय में पण्डित शब्द का प्रयोग विशेषतः उन गृहस्थ विद्वानों के लिए होता है जो अपने पाण्डित्य, धर्मज्ञान एवं आचारनिपुणता से जैन संस्कृति एवं समाज का सम्वर्धन-सम्पोषण करते हैं। ऐसे पण्डितों की जैनों में विशिष्ट परम्परा है। विद्वानों की धारणा है कि इस परम्परा का प्रारम्भ लगभग तेरहवीं सदी से हुआ है। इस समय तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लुप्तप्राय हो चुका था। सम्भवतः इसी कारण जैनों की भाँति बौद्ध समुदाय में कोई मान्य पण्डित परम्परा नहीं स्थापित हो सकी। फिर भी, अतीत से ही भारत एवं अन्य बौद्ध देशों में गृहस्थों की बौद्ध धर्म के विकास में भूमिका रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में पण्डित गृहस्थों की यह भूमिका प्रबल होती हुई दो मुख्य रूपों में उभर कर सामने आई है ।
आधुनिक शिक्षापद्धति के विकास एवं विस्तार के साथ बौद्ध धर्म एवं दर्शन भी विभिन्न रूपों में अध्ययन एवं गवेषणा का विषय बना । गृहस्थों में भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी। देश की बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने विद्वानों को इस नये क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। जनसाधारण ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया और उनका स्वरूप संघनायक धर्माचार्यों के समान माना जाने लगा। इससे आचार्यों के साथ गृहस्थ धर्मगुरुओं का एक पृथक् वर्ग उभरा । इन लोगों ने बौद्ध धर्म के परिज्ञान और प्रसार में नया आयाम प्रस्तुत किया।
बौद्ध धर्म और पालिभाषा के अध्ययन-अध्यापन में भाग लेने वाले गृहस्थ विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी अब सामने आ रहा है। इस वर्ग में बौद्धों के अतिरिक्त इतर धर्मावलम्बी भी समाहित हैं जो विश्व के सभी भागों में पाये जाते हैं। इस वर्ग के विद्वानों का प्रमख ध्येय बौद्ध-धर्म एवं दर्शन के प्राचीन एवं वर्तमान स्वरूप को परम्परागत एवं वैज्ञानिक ढंग से समझना-समझाना है।
जैन धर्म के समान बौद्ध धर्म भी प्रधानतः भिक्षु धर्म है। इसका चरम लक्ष्य दुःखनिरोध एवं निर्वाण प्राप्ति है । इसके लिए यह अनिवार्य है कि दुःख के मूल-अज्ञान और तृष्णा को निर्मूल किया जाये। इस कार्य के लिए पारिवारिक जीवन को बाधा एवं धूलि-धूसरित तथा प्रव्रज्या को मुक्त आकाश कहा है । दुःखनिरोध की कामना करने वालों के लिए प्रव्रज्या लेकर भिक्षु जीवन को अपनाना अनिवार्य था। बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेश भिक्षुओं को लक्ष्य कर ही दिए गये थे। फिर भी, गृहस्थों के लिए भो बौद्ध धर्म में स्थान था। उन्हें उपासक/उपासिका कहा जाता था। इसके लिए यह आवश्यक था कि वे गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हए धर्मानकल जीवन व्यतीत करें तथा वर्तमान और भावी जीवन को सुख और शान्तिपूर्ण बनायें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह विहित था कि वे बुद्ध, धर्म एवं संघ में श्रद्धा रखें एवं शील या सदाचार का पालन करें। बुद्ध और उनके शिष्य चारिका हेतु गृहस्थों के घर जाते थे। भोजनोपरान्त उन्हें दानकथा, शीलकथा आदि का उपदेश देते थे। गहस्थों को धर्म-दर्शन जानने-समझने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। उनकी क्षमता को नगण्य भी नहीं माना जाता था। एक बार बुद्ध से पूछा गया, "भन्ते, गृहस्थ हो गन्तव्य तक पहेंचने में सफल होते हैं, प्रबजित नहीं। ऐसा क्यों?' बुद्ध ने उत्तर दिया, "आउसो, प्रश्न गृहस्थ और प्रबजित का नहीं, सम्यक् मार्ग का है। जो सम्यक् मार्ग पर चलेगा, वही गन्तव्य प्राप्त करेगा।" बुद्ध यह नहीं मानते थे कि भिक्षु बनने मात्र से धर्म-दर्शन का पूर्ण ज्ञान हो सकता है या कि वे हो इसके एकमात्र अधिकारी हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org