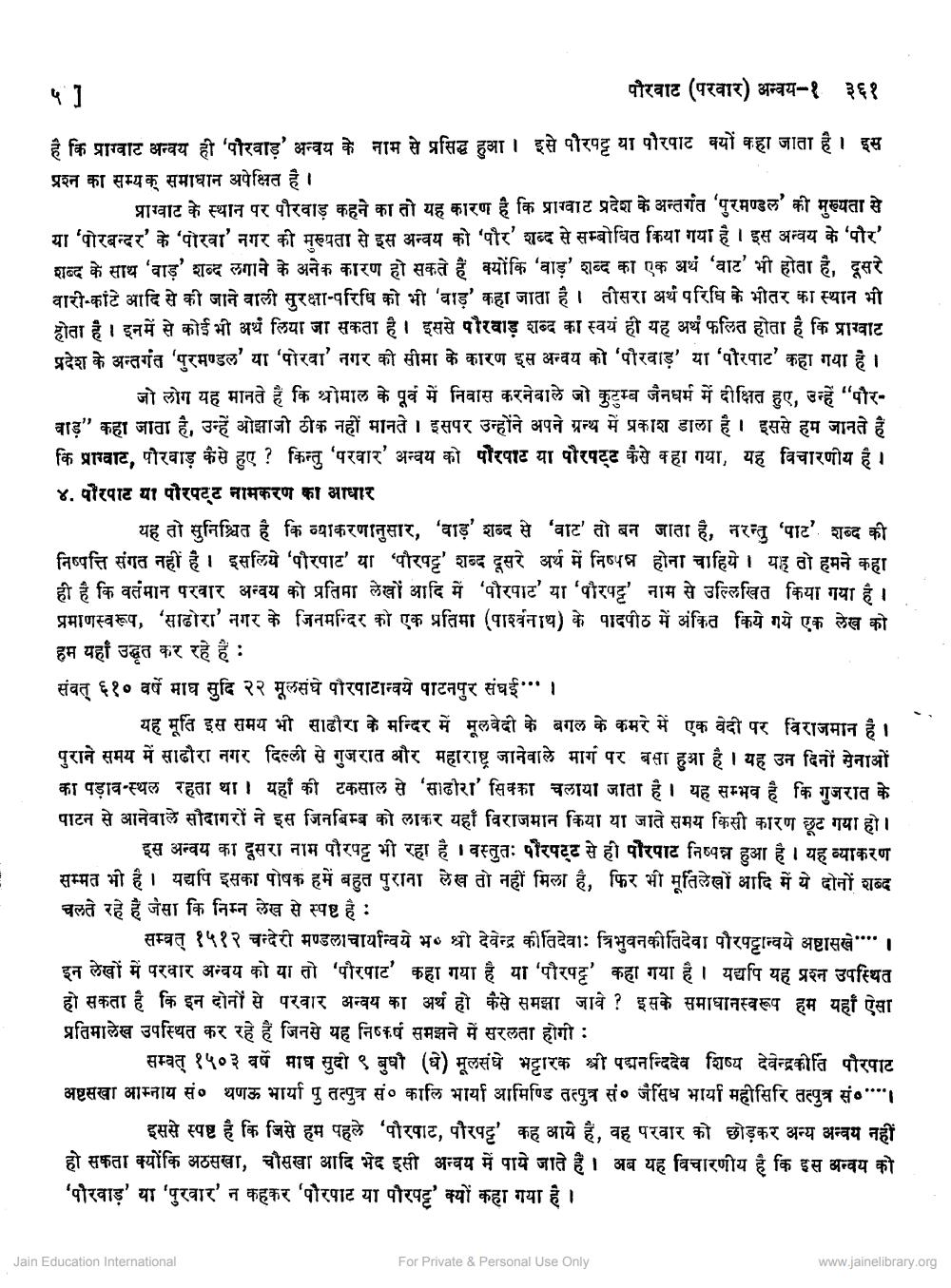________________
पौरवाट (परवार) अन्वय-१ ३६१
है कि प्राग्वाट अन्वय ही 'पौरवाड़' अन्वय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे पौरपट्ट या पौरपाट क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का सम्यक् समाधान अपेक्षित है।
प्राग्वाट के स्थान पर पौरवाड़ कहने का तो यह कारण है कि प्राग्वाट प्रदेश के अन्तर्गत 'पुरमण्डल' की मुख्यता से या 'पोरबन्दर' के 'पोरवा' नगर की मुख्यता से इस अन्वय को 'पौर' शब्द से सम्बोधित किया गया है । इस अन्वय के 'पौर' शब्द के साथ 'वाड़' शब्द लगाने के अनेक कारण हो सकते हैं क्योंकि 'वाड़' शब्द का एक अर्थ 'वाट' भी होता है, दूसरे वारी-कांटे आदि से की जाने वाली सुरक्षा-परिधि को भी 'वाड़' कहा जाता है। तीसरा अर्थ परिधि के भीतर का स्थान भी होता है। इनमें से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। इससे पौरवाड़ शब्द का स्वयं ही यह अर्थ फलित होता है कि प्राग्वाट प्रदेश के अन्तर्गत 'पुरमण्डल' या 'पोरवा' नगर की सीमा के कारण इस अन्वय को 'पौरवाड़' या 'पौरपाट' कहा गया है।
जो लोग यह मानते हैं कि श्रोमाल के पूर्व में निवास करनेवाले जो कुटुम्ब जैनधर्म में दीक्षित हुए, उन्हें "पौरवाड़" कहा जाता है, उन्हें ओझाजी ठीक नहीं मानते । इसपर उन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रकाश डाला है। इससे हम जानते हैं कि प्राग्वाट, पौरवाड़ कैसे हुए ? किन्तु 'परवार' अन्वय को पौरपाट या पौरपट्ट कैसे कहा गया, यह विचारणीय है । ४. पौरपाट या पौरपट्ट नामकरण का आधार
यह तो सुनिश्चित है कि व्याकरणानुसार, 'वाड़' शब्द से 'वाट' तो बन जाता है, नरन्तु 'पाट' शब्द की निष्पत्ति संगत नहीं है। इसलिये 'पौरपाट' या 'पौरपट्ट' शब्द दूसरे अर्थ में निष्पन्न होना चाहिये। यह तो हमने कहा ही है कि वर्तमान परवार अन्वय को प्रतिमा लेखों आदि में 'पौरपाट' या 'पौरपट' नाम से उल्लिखित किया गया है। प्रमाणस्वरूप, 'साढोरा' नगर के जिनमन्दिर को एक प्रतिमा (पार्श्वनाथ) के पादपीठ में अंकित किये गये एक लेख को हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं : संवत् ६१० वर्षे माघ सुदि २२ मूलसंघे पौरपाटान्वये पाटनपुर संघई"।
यह मूर्ति इस समय भी साढौरा के मन्दिर में मूलवेदी के बगल के कमरे में एक वेदी पर विराजमान है। पुराने समय में साढौरा नगर दिल्ली से गुजरात और महाराष्ट्र जानेवाले मार्ग पर बसा हुआ है । यह उन दिनों सेनाओं का पड़ाव-स्थल रहता था। यहां की टकसाल से 'साढोरा' सिक्का चलाया जाता है। यह सम्भव है कि गुजरात के पाटन से आनेवाले सौदागरों ने इस जिनबिम्ब को लाकर यहाँ विराजमान किया या जाते समय किसी कारण छट गया हो।
इस अन्वय का दूसरा नाम पौरपट्ट भी रहा है । वस्तुतः पौरपट्ट से ही पौरपाट निष्पन्न हुआ है । यह व्याकरण सम्मत भी है । यद्यपि इसका पोषक हमें बहुत पुराना लेख तो नहीं मिला है, फिर भी मूर्तिलेखों आदि में ये दोनों शब्द चलते रहे है जैसा कि निम्न लेख से स्पष्ट है :
सम्बत् १५१२ चन्देरी मण्डलाचार्यान्वये भ. श्री देवेन्द्र कीतिदेवाः त्रिभुवनकीतिदेवा पौरपान्वये अष्टासखे""। इन लेखों में परवार अन्वय को या तो 'पौरपाट' कहा गया है या 'पौरपट्ट' कहा गया है । यद्यपि यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इन दोनों से परवार अन्वय का अर्थ हो कैसे समझा जावे ? इसके समाधानस्वरूप हम यहाँ ऐसा प्रतिमालेख उपस्थित कर रहे हैं जिनसे यह निष्कर्ष समझने में सरलता होगी :
सम्वत् १५०३ वर्षे माघ सुदो ९ बुधौ (धे) मूलसंघे भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेव शिष्य देवेन्द्रकीर्ति पौरपाट अष्टसखा आम्नाय सं० थणऊ भार्या पु तत्पुत्र सं० कालि भार्या आमिण्डि तत्पुत्र सं० जैसिंध भार्या महीसिरि तत्पूत्र सं."।
इससे स्पष्ट है कि जिसे हम पहले 'पौरपाट, पौरपट्ट' कह आये है, वह परवार को छोड़कर अन्य अन्वय नहीं हो सकता क्योंकि अठसखा, चौसखा आदि भेद इसी अन्वय में पाये जाते है। अब यह विचारणीय है कि इस अन्वय को 'पौरवाड़' या 'पुरवार' न कहकर 'पौरपाट या पौरपट्ट' क्यों कहा गया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org