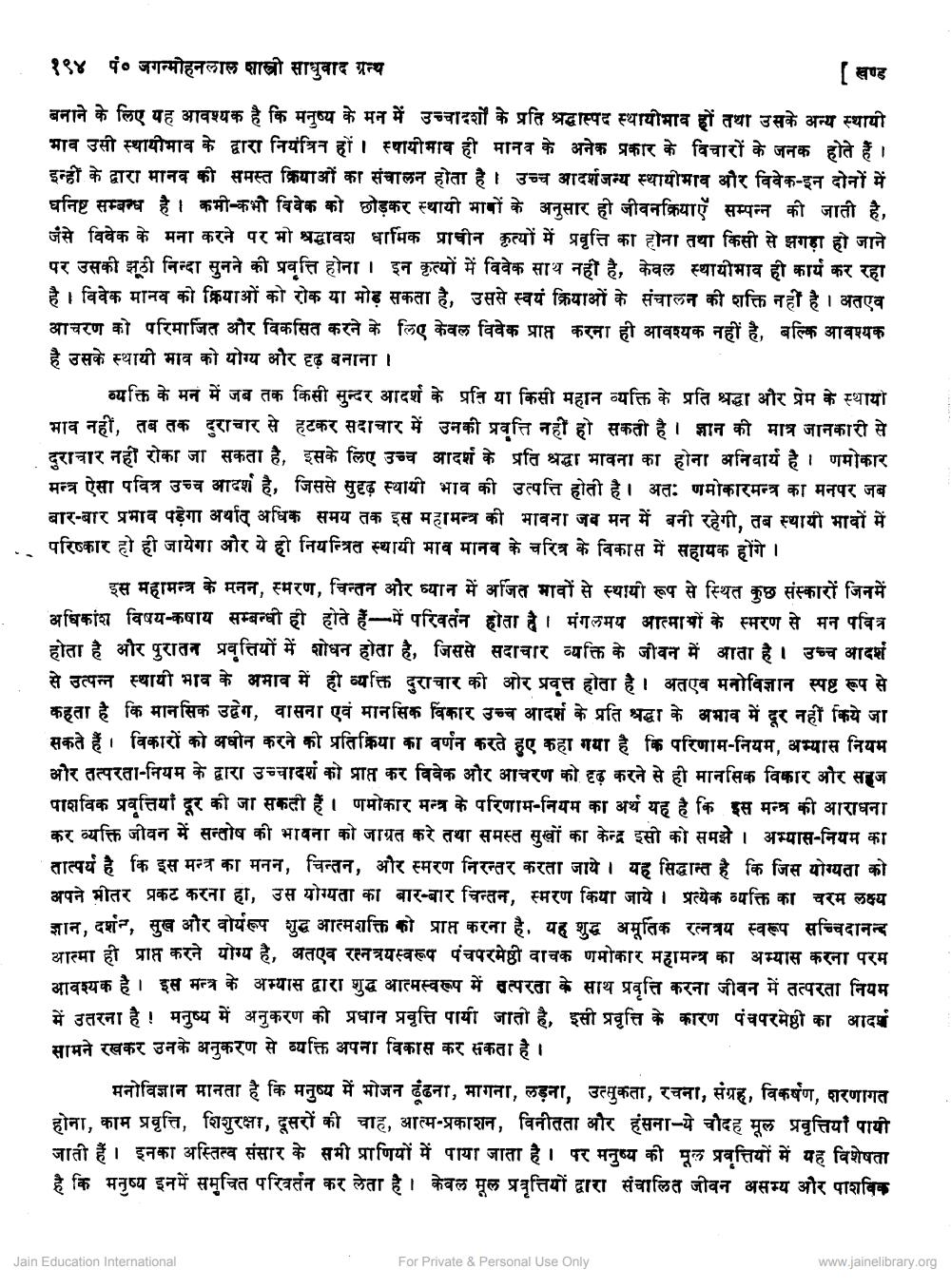________________
१९४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्य
[खण्ड
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के मन में उच्चादों के प्रति श्रद्धास्पद स्थायीभाव हों तथा उसके अन्य स्थायी भाव उसी स्थायीभाव के द्वारा नियंत्रित हों। स्थायीमाव ही मानव के अनेक प्रकार के विचारों के जनक होते हैं। इन्हीं के द्वारा मानव की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। उच्च आदर्शजन्य स्थायीमाव और विवेक-इन दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। कभी-कभी विवेक को छोड़कर स्थायी भावों के अनुसार ही जीवनक्रियाएँ सम्पन्न की जाती है, जैसे विवेक के मना करने पर भी श्रद्धावश धार्मिक प्राचीन कृत्यों में प्रवृत्ति का होना तथा किसी से झगड़ा हो जाने पर उसकी झूठी निन्दा सुनने की प्रवृत्ति होना । इन कृत्यों में विवेक साथ नहीं है, केवल स्थायीभाव ही कार्य कर रहा है। विवेक मानव को क्रियाओं को रोक या मोड़ सकता है, उससे स्वयं क्रियाओं के संचालन की शक्ति न आचरण को परिमार्जित और विकसित करने के लिए केवल विवेक प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है उसके स्थायी भाव को योग्य और दृढ़ बनाना।
व्यक्ति के मन में जब तक किसी सुन्दर आदर्श के प्रति या किसी महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रेम के स्थायो भाव नहीं, तब तक दुराचार से हटकर सदाचार में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की मात्र जानकारी से दुराचार नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए उच्च आदर्श के प्रति श्रद्धा भावना का होना अनिवार्य है । णमोकार मन्त्र ऐसा पवित्र उच्च आदर्श है, जिससे सुदृढ़ स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अतः णमोकारमन्त्र का मनपर जब बार-बार प्रभाव पड़ेगा अर्थात् अधिक समय तक इस महामन्त्र की भावना जब मन में बनी रहेगी, तब स्थायी भावों में परिष्कार हो ही जायेगा और ये ही नियन्त्रित स्थायी भाव मानव के चरित्र के विकास में सहायक होंगे ।
इस महामन्त्र के मनन, स्मरण, चिन्तन और ध्यान में अजित भावों से स्थायी रूप से स्थित कुछ संस्कारों जिनमें अधिकांश विषय-कषाय सम्बन्धी ही होते हैं में परिवर्तन होता है। मंगलमय आत्मागों के स्मरण से मन पवित्र होता है और पुरातन प्रवृत्तियों में शोधन होता है, जिससे सदाचार व्यक्ति के जीवन में आता है। उच्च आदर्श से उत्पन्न स्थायी भाव के अभाव में ही व्यक्ति दुराचार को ओर प्रवृत्त होता है। अतएव मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि मानसिक उद्वेग, वासना एवं मानसिक विकार उच्च आदर्श के प्रति श्रद्धा के अभाव में दूर नहीं किये जा सकते हैं। विकारों को अधीन करने की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परिणाम-नियम, अभ्यास नियम और तत्परता-नियम के द्वारा उच्चादर्श को प्राप्त कर विवेक और आचरण को दृढ़ करने से ही मानसिक विकार और सहज पाशविक प्रवृत्तियाँ दूर की जा सकती हैं। णमोकार मन्त्र के परिणाम-नियम का अर्थ यह है कि इस मन्त्र की आराधना कर व्यक्ति जीवन में सन्तोष की भावना को जाग्रत करे तथा समस्त सुखों का केन्द्र इसी को समझे। अभ्यास-नियम का तात्पर्य है कि इस मन्त्र का मनन, चिन्तन, और स्मरण निरन्तर करता जाये। यह सिद्धान्त है कि जिस योग्यता को अपने भीतर प्रकट करना हा, उस योग्यता का बार-बार चिन्तन, स्मरण किया जाये । प्रत्येक व्यक्ति का चरम लक्ष्य ज्ञान, दर्शन, सुख और वोर्यरूप शुद्ध आत्मशक्ति को प्राप्त करना है. यह शुद्ध अमूर्तिक रत्नत्रय स्वरूप सच्चिदानन्द आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है, अतएव रत्नत्रयस्वरूप पंचपरमेष्ठी वाचक णमोकार महामन्त्र का अभ्यास करना परम आवश्यक है। इस मन्त्र के अभ्यास द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूप में तत्परता के साथ प्रवृत्ति करना जीवन में तत्परता नियम में उतरना है। मनुष्य में अनुकरण को प्रधान प्रवृत्ति पायी जाती है, इसी प्रवृत्ति के कारण पंचपरमेष्ठी का आदर्श सामने रखकर उनके अनुकरण से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है।
मनोविज्ञान मानता है कि मनुष्य में भोजन ढूंढना, मागना, लड़ना, उत्सुकता, रचना, संग्रह, विकर्षण, शरणागत होना, काम प्रवृत्ति, शिशुरक्षा, दूसरों की चाह, आत्म-प्रकाशन, विनीतता और हंसना-ये चौदह मूल प्रवृत्तियाँ पायो जाती हैं। इनका अस्तित्व संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। पर मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में यह विशेषता है कि मनुष्य इनमें समुचित परिवर्तन कर लेता है। केवल मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित जीवन असम्य और पाशविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org