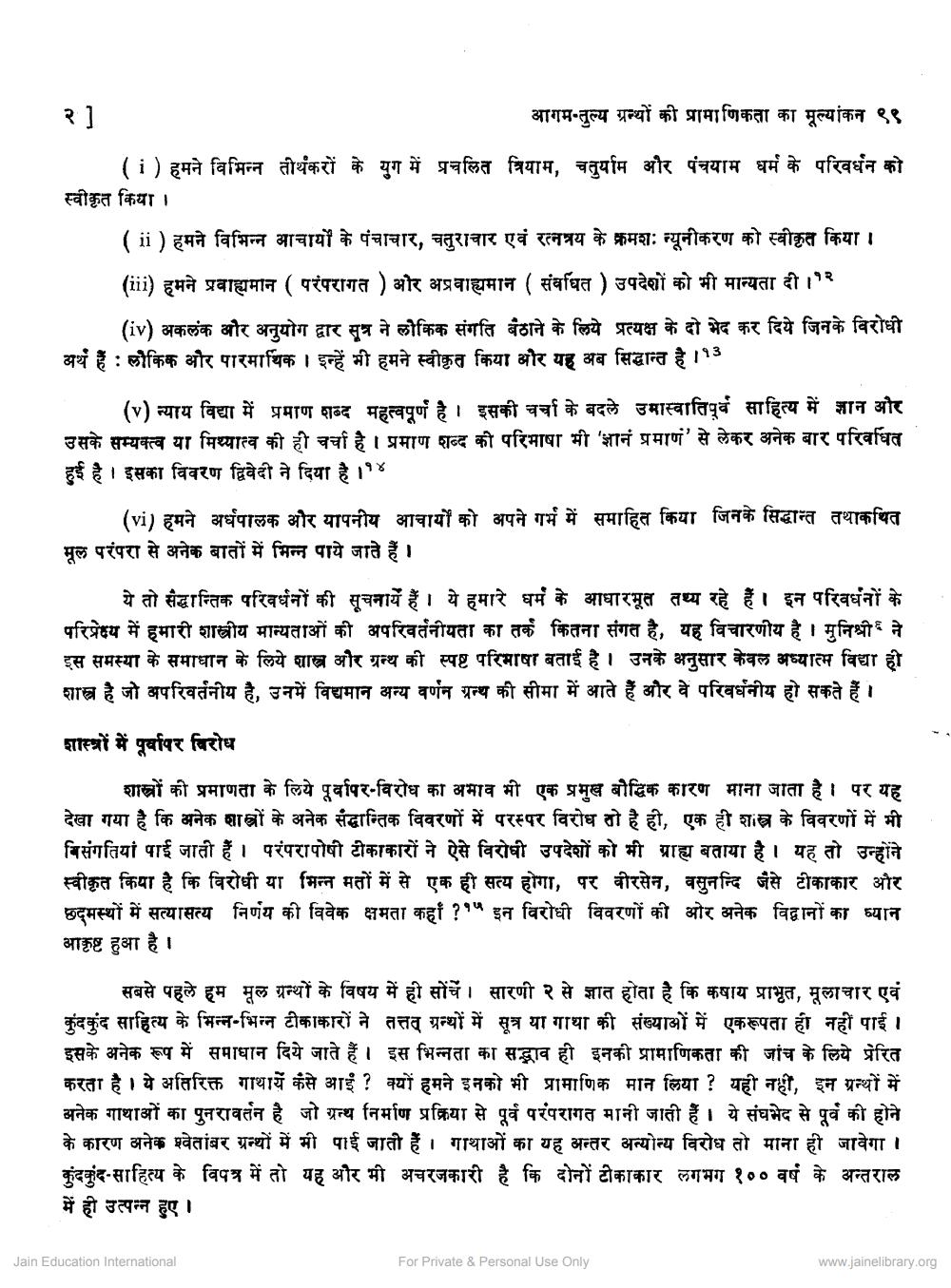________________
आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन ९९
(i) हमने विभिन्न तीर्थंकरों के युग में प्रचलित त्रियाम, चतुर्याम और पंचयाम धर्म के परिवर्धन को स्वीकृत किया।
(ii) हमने विभिन्न आचार्यों के पंचाचार, चतुराचार एवं रत्नत्रय के क्रमशः न्यूनीकरण को स्वीकृत किया । (iii) हमने प्रवाहमान ( परंपरागत ) और अप्रवाह्यमान ( संवर्धित ) उपदेशों को भी मान्यता दी।'२
(iv) अकलंक और अनुयोग द्वार सत्र ने लोकिक संगति बैठाने के लिये प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये जिनके विरोधी अर्थ हैं : लौकिक और पारमार्थिक । इन्हें भी हमने स्वीकृत किया और यह अब सिद्धान्त है । १3
(v) न्याय विद्या में प्रमाण शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा के बदले उमास्वातिपूर्व साहित्य में ज्ञान और उसके सम्यक्त्व या मिथ्यात्व की ही चर्चा है। प्रमाण शब्द की परिभाषा भी 'ज्ञानं प्रमाणं' से लेकर अनेक बार परिवधित हुई है । इसका विवरण द्विवेदी ने दिया है ।१४
(vi) हमने अर्धपालक और यापनीय आचार्यों को अपने गर्भ में समाहित किया जिनके सिद्धान्त तथाकथित मूल परंपरा से अनेक बातों में भिन्न पाये जाते हैं।
ये तो सैद्धान्तिक परिवर्धनों की सूचनायें हैं। ये हमारे धर्म के आधारभूत तथ्य रहे हैं। इन परिवर्धनों के परिप्रेक्ष्य में हमारी शास्त्रीय मान्यताओं की अपरिवर्तनीयता का तर्क कितना संगत है, यह विचारणीय है । मुनिश्री ने इस समस्या के समाधान के लिये शास्त्र और ग्रन्थ की स्पष्ट परिभाषा बताई है। उनके अनुसार केवल अध्यात्म विद्या ही शास्त्र है जो अपरिवर्तनीय है, उनमें विद्यमान अन्य वर्णन ग्रन्थ की सीमा में आते हैं और वे परिवर्धनीय हो सकते हैं।
शास्त्रों में पूर्वापर विरोध
शास्त्रों की प्रमाणता के लिये पूर्वापर-विरोध का अभाव भी एक प्रमुख बौद्धिक कारण माना जाता है। पर यह देखा गया है कि अनेक शास्त्रों के अनेक संद्धान्तिक विवरणों में परस्पर विरोध तो है ही, एक ही शास्त्र के विवरणों में भी विसंगतियां पाई जाती हैं। परंपरापोषी टीकाकारों ने ऐसे विरोधी उपदेशों को भी ग्राह्य बताया है। यह तो उन्होंने स्वीकृत किया है कि विरोधी या भिन्न मतों में से एक ही सत्य होगा, पर वीरसेन, वसुनन्दि जैसे टीकाकार और छद्मस्थों में सत्यासत्य निर्णय की विवेक क्षमता कहाँ ?१५ इन विरोधी विवरणों की ओर अनेक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।
सबसे पहले हम मूल ग्रन्थों के विषय में ही सोंचें। सारणी २ से ज्ञात होता है कि कषाय प्राभूत, मूलाचार एवं कुंदकुंद साहित्य के भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने तत्तत् ग्रन्थों में सूत्र या गाथा की संख्याओं में एकरूपता ही नहीं पाई। इसके अनेक रूप में समाधान दिये जाते हैं। इस भिन्नता का सद्भाव ही इनकी प्रामाणिकता की जांच के लिये प्रेरित करता है। ये अतिरिक्त गाथायें कैसे आई? क्यों हमने इनको भी प्रामाणिक मान लिया ? यही नहीं, इन ग्रन्थों में अनेक गाथाओं का पुनरावर्तन है जो ग्रन्थ निर्माण प्रक्रिया से पूर्व परंपरागत मानी जाती हैं। ये संघभेद से पूर्व की होने के कारण अनेक श्वेतांबर ग्रन्थों में भी पाई जाती हैं। गाथाओं का यह अन्तर अन्योन्य विरोध तो माना ही जावेगा। कूदकुंद-साहित्य के विपत्र में तो यह और भी अचरजकारी है कि दोनों टीकाकार लगभग १०० वर्ष के अन्तराल में ही उत्पन्न हुए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org