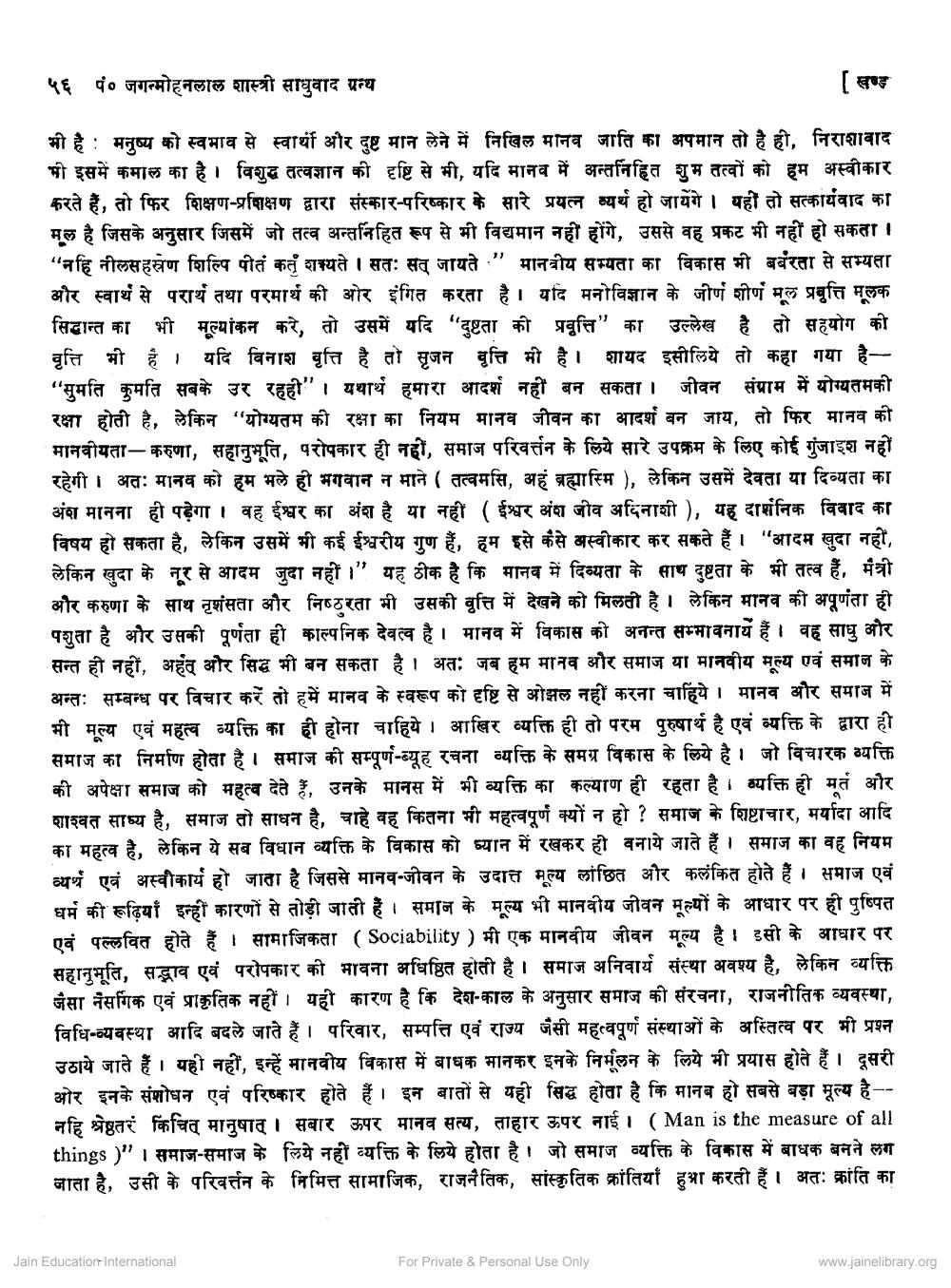________________
५६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[ खण्ड
भी है : मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी और दुष्ट मान लेने में निखिल मानव जाति का अपमान तो है ही. निराशावाद भी इसमें कमाल का है। विशुद्ध तत्वज्ञान की दृष्टि से भी, यदि मानव में अन्तनिहित शुम तत्वों को हम अस्वीकार करते हैं, तो फिर शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा संस्कार-परिष्कार के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। यही तो सत्कार्यवाद का मल है जिसके अनुसार जिसमें जो तत्व अन्तनिहित रूप से भी विद्यमान नहीं होंगे, उससे वह प्रकट भी नहीं हो सकता। "नहि नीलसहस्रेण शिल्पि पीतं कतुं शक्यते । सतः सत् जायते " मानवीय सभ्यता का विकास भी बर्बरता से सभ्यता और स्वार्थ से परार्थ तथा परमार्थ की ओर इंगित करता है। यदि मनोविज्ञान के जीर्ण शीर्ण मूल प्रवृत्ति मूलक सिद्धान्त का भी मूल्यांकन करे, तो उसमें यदि "दुष्टता की प्रवृत्ति" का उल्लेख है तो सहयोग की वृत्ति भी है । यदि विनाश वृत्ति है तो सृजन वृत्ति भी है। शायद इसीलिये तो कहा गया है"सुमति कुमति सबके उर रहही"। यथार्थ हमारा आदर्श नहीं बन सकता। जीवन संग्राम में योग्यतमकी रक्षा होती है, लेकिन "योग्यतम की रक्षा का नियम मानव जीवन का आदर्श बन जाय, तो फिर मानव की मानवीयता-करुणा, सहानुभूति, परोपकार ही नहीं, समाज परिवर्तन के लिये सारे उपक्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अतः मानव को हम भले ही भगवान न माने ( तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि ), लेकिन उसमें देवता या दिव्यता का अंश मानना ही पड़ेगा। वह ईश्वर का अंश है या नहीं ( ईश्वर अंश जीव अविनाशी ), यह दार्शनिक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसमें भी कई ईश्वरीय गुण हैं, हम इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं । "आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।" यह ठीक है कि मानव में दिव्यता के साथ दुष्टता के भी तत्व हैं, मंत्री और करुणा के साथ नृशंसता और निष्ठुरता भी उसकी वृत्ति में देखने को मिलती है । लेकिन मानव की अपूर्णता ही पशुता है और उसकी पूर्णता ही काल्पनिक देवत्व है। मानव में विकास को अनन्त सम्भावनायें हैं। वह साधु और सन्त ही नहीं, अहंत और सिद्ध भी बन सकता है। अतः जब हम मानव और समाज या मानवीय मूल्य एवं समाज के अन्तः सम्बन्ध पर विचार करें तो हमें मानव के स्वरूप को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिये । मानव और समाज में भी मूल्य एवं महत्व व्यक्ति का ही होना चाहिये । आखिर व्यक्ति ही तो परम पुरुषार्थ है एवं व्यक्ति के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। समाज की सम्पूर्ण-ब्यूह रचना व्यक्ति के समग्र विकास के लिये है। जो विचारक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देते हैं, उनके मानस में भी व्यक्ति का कल्याण ही रहता है। व्यक्ति ही मूर्त और शाश्वत साध्य है, समाज तो साधन है, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो ? समाज के शिष्टाचार, मर्यादा आदि का महत्व है, लेकिन ये सब विधान व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर ही बनाये जाते हैं। समाज का वह नियम व्यर्थ एवं अस्वीकार्य हो जाता है जिससे मानव-जीवन के उदात्त मूल्य लांछित और कलंकित होते हैं। समाज एवं धर्म की रूढ़ियाँ इन्हीं कारणों से तोड़ी जाती हैं। समाज के मूल्य भी मानवीय जीवन मूल्यों के आधार पर ही पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं । सामाजिकता ( Sociability ) मी एक मानवीय जीवन मूल्य है। इसी के आधार पर सहानुभूति, सद्भाव एवं परोपकार की भावना अधिष्ठित होती है। समाज अनिवार्य संस्था अवश्य है, लेकिन व्यक्ति जैसा नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नहीं। यही कारण है कि देश-काल के अनुसार समाज की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, विधि-व्यवस्था आदि बदले जाते हैं। परिवार, सम्पत्ति एवं राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाये जाते हैं। यही नहीं, इन्हें मानवीय विकास में बाधक मानकर इनके निर्मूलन के लिये भी प्रयास होते हैं। दूसरी ओर इनके संशोधन एवं परिष्कार होते हैं। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि मानब हो सबसे बड़ा मूल्य है-- नहि श्रेष्ठतरं किंचित् मानुषात् । सबार ऊपर मानव सत्य, ताहार ऊपर नाई। ( Man is the measure of all things )" | समाज-समाज के लिये नहीं व्यक्ति के लिये होता है। जो समाज व्यक्ति के विकास में बाधक बनने लग जाता है, उसी के परिवर्तन के निमित्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्रांतियाँ हुआ करती हैं। अतः क्रांति का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org