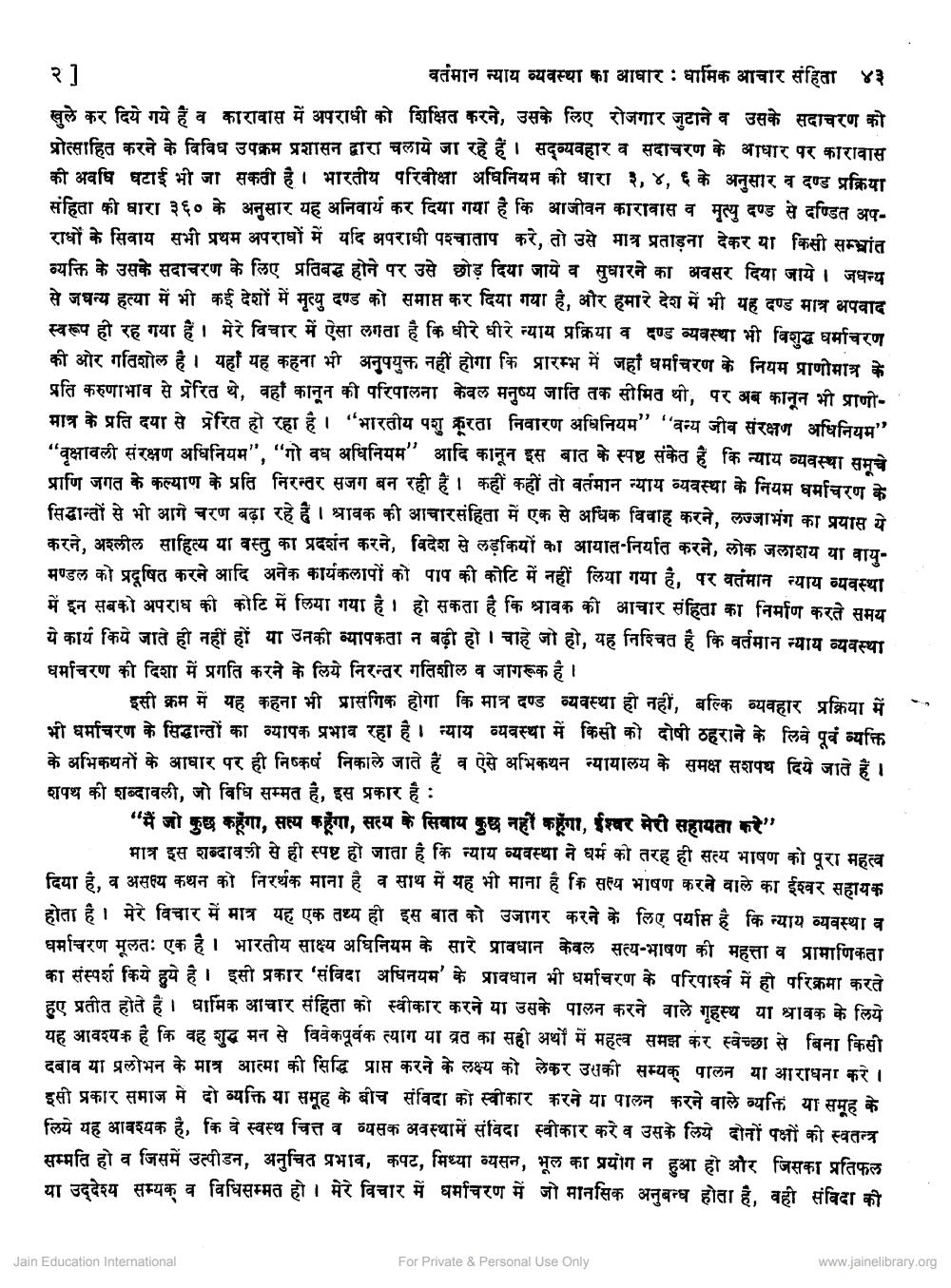________________
२]
वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार : धार्मिक आचार संहिता ४३ खुले कर दिये गये हैं व कारावास में अपराधी को शिक्षित करने, उसके लिए रोजगार जुटाने व उसके सदाचरण को प्रोत्साहित करने के विविध उपक्रम प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। सद्व्यवहार व सदाचरण के आधार पर कारावास की अवधि घटाई भी जा सकती है। भारतीय परिवीक्षा अधिनियम की धारा ३,४,६ के अनुसार व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३६० के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आजीवन कारावास व मृत्यु दण्ड से दण्डित अपराधों के सिवाय सभी प्रथम अपराधों में यदि अपराधी पश्चाताप करे, तो उसे मात्र प्रताड़ना देकर या किसी सम्भ्रांत व्यक्ति के उसके सदाचरण के लिए प्रतिबद्ध होने पर उसे छोड़ दिया जाये व सुधारने का अवसर दिया जाये। जधन्य से जघन्य हत्या में भी कई देशों में मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया गया है, और हमारे देश में भी यह दण्ड मात्र अपवाद स्वरूप ही रह गया है। मेरे विचार में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे न्याय प्रक्रिया व दण्ड व्यवस्था भी विशुद्ध धर्माचरण की ओर गतिशोल है। यहां यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि प्रारम्भ में जहाँ धर्माचरण के नियम प्राणीमात्र के प्रति करुणाभाव से प्रेरित थे, वहाँ कानून की परिपालना केवल मनुष्य जाति तक सीमित थी, पर अब कानून भी प्राणीमात्र के प्रति दया से प्रेरित हो रहा है । "भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम" "वन्य जीव संरक्षण अधिनियम" "वृक्षावली संरक्षण अधिनियम", "गो वध अधिनियम' आदि कानून इस बात के स्पष्ट संकेत है कि न्याय व्यवस्था समचे प्राणि जगत के कल्याण के प्रति निरन्तर सजग बन रही हैं। कहीं कहीं तो वर्तमान न्याय व्यवस्था के नियम धर्माचरण के सिद्धान्तों से भी आगे चरण बढ़ा रहे है । श्रावक की आचारसंहिता में एक से अधिक विवाह करने, लज्जाभंग का प्रयास ये करने, अश्लील साहित्य या वस्तु का प्रदर्शन करने, विदेश से लड़कियों का आयात-निर्यात करने, लोक जलाशय या वायमण्डल को प्रदषित करने आदि अनेक कार्यकलापों को पाप की कोटि में नहीं लिया गया है, पर वर्तमान न्याय व्यवस्था में इन सबको अपराध की कोटि में लिया गया है। हो सकता है कि श्रावक की आचार संहिता का निर्माण करते समय ये कार्य किये जाते ही नहीं हों या उनकी व्यापकता न बढ़ी हो । चाहे जो हो, यह निश्चित है कि वर्तमान न्याय व्यवस्था धर्माचरण की दिशा में प्रगति करने के लिये निरन्तर गतिशील व जागरूक है।
इसी क्रम में यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि मात्र दण्ड व्यवस्था ही नहीं, बल्कि व्यवहार प्रक्रिया में ." भी धर्माचरण के सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव रहा है। न्याय व्यवस्था में किसी को दोषी ठहराने के लिये पूर्व व्यक्ति के अभिकथनों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं व ऐसे अभिकथन न्यायालय के समक्ष सशपथ दिये जाते है। शपथ की शब्दावली, जो विधि सम्मत है, इस प्रकार है : ___ "मैं जो कुछ कहूँगा, सत्य कहूँगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी सहायता करे"
मात्र इस शब्दावली से ही स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व्यवस्था ने धर्म को तरह ही सत्य भाषण को पूरा महत्व दिया है, व असक्ष्य कथन को निरर्थक माना है व साथ में यह भी माना है कि सत्य भाषण करने वाले का ईश्वर सहायक होता है। मेरे विचार में मात्र यह एक तथ्य ही इस बात को उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि न्याय व्यवस्था व धर्माचरण मलतः एक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे प्रावधान केवल सत्य-भाषण की महत्ता व प्रामाणिकता का संस्पर्श किये हुये है। इसी प्रकार 'संविदा अधिनयम' के प्रावधान भी धर्माचरण के परिपार्श्व में हो परिक्रमा करते दा प्रतीत होते हैं। धार्मिक आचार संहिता को स्वीकार करने या उसके पालन करने वाले गृहस्थ या धावक के लिये यह आवश्यक है कि वह शुद्ध मन से विवेकपूर्वक त्याग या व्रत का सही अर्थों में महत्व समझ कर स्वेच्छा से बिना किसी दबाब या प्रलोभन के मात्र आत्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर उसकी सम्यक् पालन या आराधना करे । इसी प्रकार समाज मे दो व्यक्ति या समूह के बीच संविदा को स्वीकार करने या पालन करने वाले व्यक्ति या समूह के लिये यह आवश्यक है, कि वे स्वस्थ चित्त व व्यसक अवस्थामें संविदा स्वीकार करे व उसके लिये दोनों पक्षों को स्वतन्त्र सम्मति हो व जिसमें उत्पीडन, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या व्यसन, भूल का प्रयोग न हुआ हो और जिसका प्रतिफल या उददेश्य सम्यक व विधिसम्मत हो। मेरे विचार में धर्माचरण में जो मानसिक अनबन्ध होता है. वही संविदा की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org