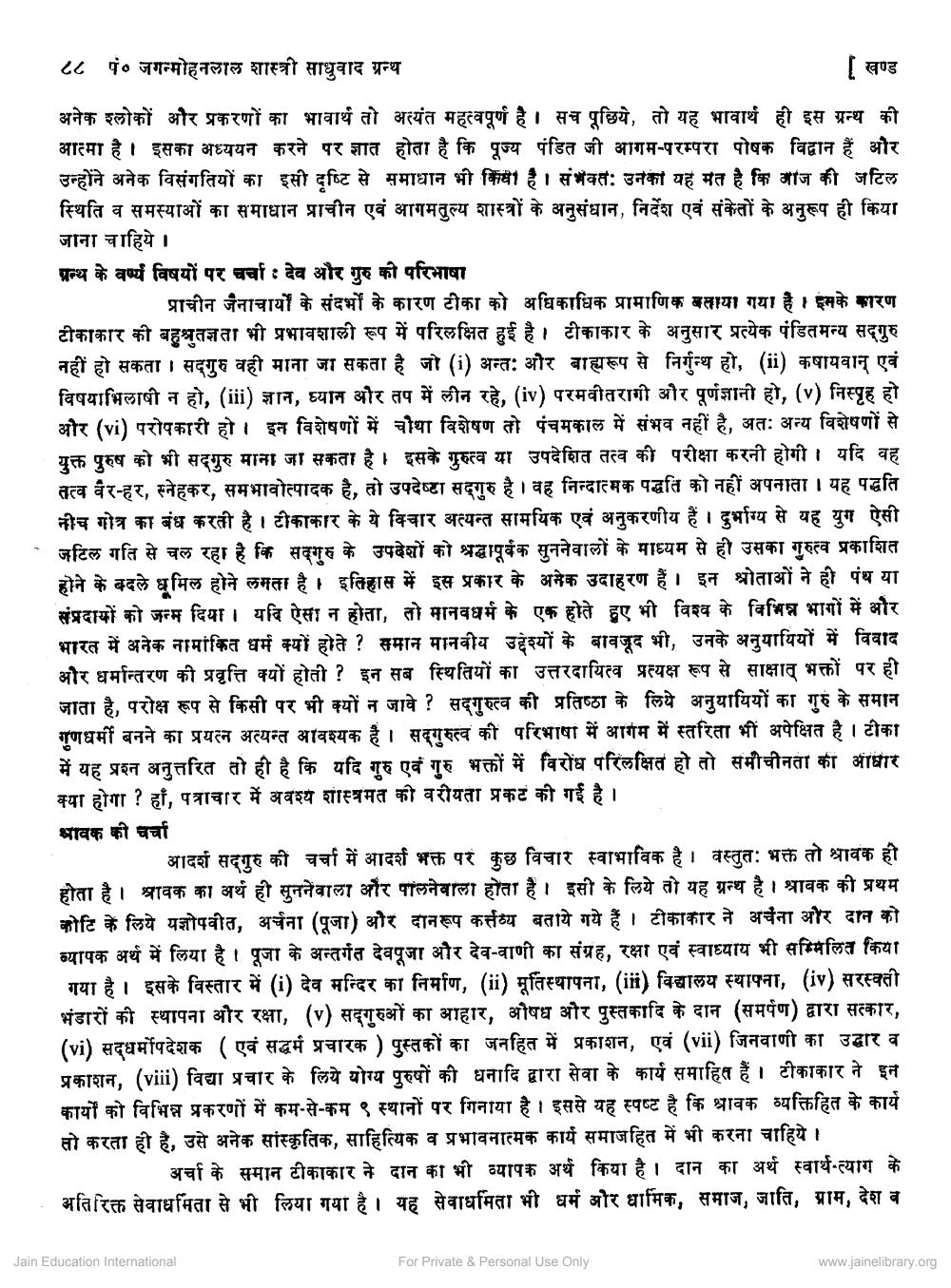________________
८८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[खण्ड अनेक श्लोकों और प्रकरणों का भावार्थ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच पूछिये, तो यह भावार्थ ही इस ग्रन्थ की आत्मा है। इसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पूज्य पंडित जी आगम-परम्परा पोषक विद्वान हैं और उन्होंने अनेक विसंगतियों का इसी दृष्टि से समाधान भी किया है। संभवत: उनका यह मत है कि आज की जटिल स्थिति व समस्याओं का समाधान प्राचीन एवं आगमतुल्य शास्त्रों के अनुसंधान, निर्देश एवं संकेतों के अनुरूप ही किया जाना चाहिये। प्रन्थ के वयं विषयों पर चर्चा : देव और गुरु को परिभाषा
प्राचीन जैनाचार्यों के संदर्भो के कारण टीका को अधिकाधिक प्रामाणिक बताया गया है। इसके कारण टीकाकार की बहुश्रुतज्ञता भी प्रभावशाली रूप में परिलक्षित हुई है। टीकाकार के अनुसार प्रत्येक पंडितमन्य सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु वही माना जा सकता है जो (i) अन्तः और बाह्यरूप से निर्गुन्थ हो, (i) कषायवान् एवं विषयाभिलाषी न हो, (iii) ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहे, (iv) परमवीतरागी और पूर्णज्ञानी हो, (v) निस्पृह हो और (vi) परोपकारी हो। इन विशेषणों में चौथा विशेषण तो पंचमकाल में संभव नहीं है, अतः अन्य विशेषणों से युक्त पुरुष को भी सद्गुरु माना जा सकता है। इसके गुरुत्व या उपदेशित तत्व की परीक्षा करनी होगी। यदि वह तत्व वर-हर, स्नेहकर, समभावोत्पादक है, तो उपदेष्टा सद्गुरु है । वह निन्दात्मक पद्धति को नहीं अपनाता । यह पद्धति नीच गोत्र का बंध करती है । टीकाकार के ये विचार अत्यन्त सामयिक एवं अनुकरणीय हैं । दुर्भाग्य से यह युग ऐसी जटिल गति से चल रहा है कि सद्गुरु के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुननेवालों के माध्यम से ही उसका गुरुत्व प्रकाशित होने के बदले धूमिल होने लगता है। इतिहास में इस प्रकार के अमेक उदाहरण हैं। इन श्रोताओं ने ही पंथ या संप्रदायों को जन्म दिया। यदि ऐसा न होता, तो मानवधर्म के एक होते हुए भी विश्व के विभिन्न भागों में और भारत में अनेक नामांकित धर्म क्यों होते ? समान मानवीय उद्देश्यों के बावजूद भी, उनके अनुयायियों में विवाद और धर्मान्तरण की प्रवृत्ति क्यों होती? इन सब स्थितियों का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से साक्षात् भक्तों पर ही जाता है, परोक्ष रूप से किसी पर भी क्यों न जावे ? सद्गुरुत्व की प्रतिष्ठा के लिये अनुया गुणधर्मी बनने का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है । सद्गुरुत्व की परिभाषा में आगम में स्तरिता भी अपेक्षित है । टीका में यह प्रश्न अनुत्तरित तो ही है कि यदि गुरु एवं गुरु भक्तों में विरोध परिलक्षित हो तो समीचीनता का आधार क्या होगा? हाँ, पत्राचार में अवश्य शास्त्रमत की वरीयता प्रकट की गई है। भावक की चर्चा
आदर्श सद्गुरु की चर्चा में आदर्श भक्त पर कुछ विचार स्वाभाविक है। वस्तुतः भक्त तो श्रावक ही होता है। श्रावक का अर्थ ही सुननेवाला और पालनेवाला होता है। इसी के लिये तो यह ग्रन्थ है। श्रावक की प्रथम कोटि के लिये यज्ञोपवीत, अर्चना (पूजा) और दानरूप कर्तव्य बताये गये हैं । टीकाकार ने अर्चना और दान को व्यापक अर्थ में लिया है। पूजा के अन्तर्गत देवपूजा और देव-वाणी का संग्रह, रक्षा एवं स्वाध्याय भी सम्मिलित किया
गया है। इसके विस्तार में (i) देव मन्दिर का निर्माण, (ii) मूर्तिस्थापना, (iii) विद्यालय स्थापना, (iv) सरस्वती भंडारों की स्थापना और रक्षा, (v) सद्गुरुओं का आहार, औषध और पुस्तकादि के दान (समर्पण) द्वारा सत्कार, (vi) सद्धर्मोपदेशक ( एवं सद्धर्म प्रचारक ) पुस्तकों का जनहित में प्रकाशन, एवं (vii) जिनवाणी का उद्धार व प्रकाशन, (viii) विद्या प्रचार के लिये योग्य पुरुषों की धनादि द्वारा सेवा के कार्य समाहित हैं। टीकाकार ने इन कार्यों को विभिन्न प्रकरणों में कम-से-कम ९ स्थानों पर गिनाया है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रावक व्यक्तिहित के कार्य तो करता ही है, उसे अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक व प्रभावनात्मक कार्य समाजहित में भी करना चाहिये ।
अर्चा के समान टीकाकार ने दान का भी व्यापक अर्थ किया है। दान का अर्थ स्वार्थ त्याग के अतिरिक्त सेवाधर्मिता से भी लिया गया है। यह सेवामिता भी धर्म और धार्मिक, समाज, जाति, ग्राम, देश व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org