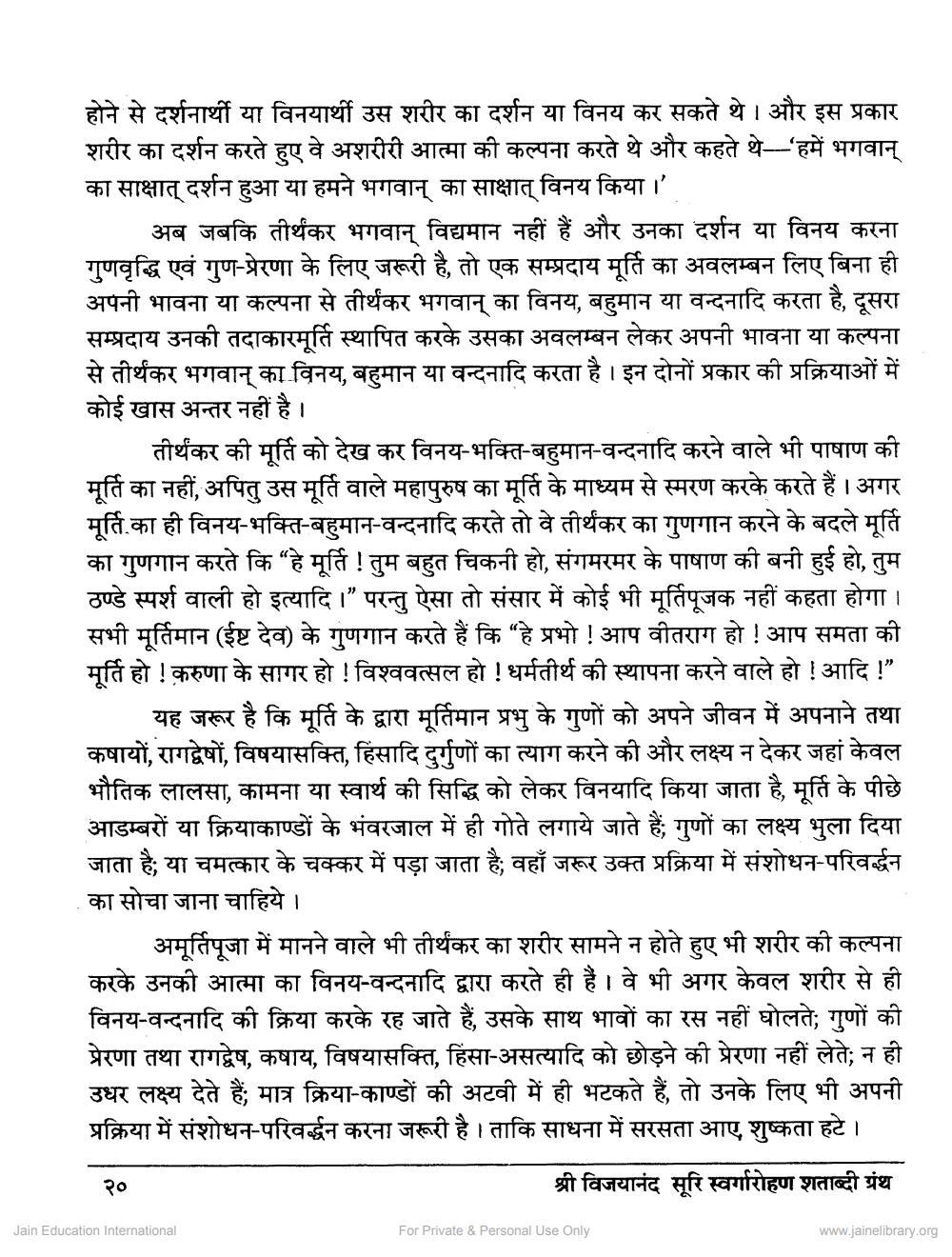________________
होने से दर्शनार्थी या विनयार्थी उस शरीर का दर्शन या विनय कर सकते थे। और इस प्रकार शरीर का दर्शन करते हुए वे अशरीरी आत्मा की कल्पना करते थे और कहते थे—'हमें भगवान् का साक्षात् दर्शन हुआ या हमने भगवान् का साक्षात् विनय किया।'
अब जबकि तीर्थंकर भगवान् विद्यमान नहीं हैं और उनका दर्शन या विनय करना गुणवृद्धि एवं गुण-प्रेरणा के लिए जरूरी है, तो एक सम्प्रदाय मूर्ति का अवलम्बन लिए बिना ही अपनी भावना या कल्पना से तीर्थंकर भगवान् का विनय, बहुमान या वन्दनादि करता है, दूसरा सम्प्रदाय उनकी तदाकारमूर्ति स्थापित करके उसका अवलम्बन लेकर अपनी भावना या कल्पना से तीर्थंकर भगवान् का विनय, बहुमान या वन्दनादि करता है । इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में कोई खास अन्तर नहीं है।
तीर्थंकर की मूर्ति को देख कर विनय-भक्ति-बहुमान-वन्दनादि करने वाले भी पाषाण की मूर्ति का नहीं, अपितु उस मूर्ति वाले महापुरुष का मूर्ति के माध्यम से स्मरण करके करते हैं। अगर मूर्ति का ही विनय-भक्ति-बहुमान-वन्दनादि करते तो वे तीर्थंकर का गुणगान करने के बदले मूर्ति का गुणगान करते कि “हे मूर्ति ! तुम बहुत चिकनी हो, संगमरमर के पाषाण की बनी हुई हो, तुम ठण्डे स्पर्श वाली हो इत्यादि ।” परन्तु ऐसा तो संसार में कोई भी मूर्तिपूजक नहीं कहता होगा। सभी मूर्तिमान (ईष्ट देव) के गुणगान करते हैं कि “हे प्रभो ! आप वीतराग हो ! आप समता की मूर्ति हो ! करुणा के सागर हो ! विश्ववत्सल हो ! धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले हो ! आदि !”
__यह जरूर है कि मूर्ति के द्वारा मूर्तिमान प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपनाने तथा कषायों, रागद्वेषों, विषयासक्ति, हिंसादि दुर्गुणों का त्याग करने की और लक्ष्य न देकर जहां केवल भौतिक लालसा, कामना या स्वार्थ की सिद्धि को लेकर विनयादि किया जाता है, मूर्ति के पीछे आडम्बरों या क्रियाकाण्डों के भंवरजाल में ही गोते लगाये जाते हैं; गुणों का लक्ष्य भुला दिया जाता है; या चमत्कार के चक्कर में पड़ा जाता है; वहाँ जरूर उक्त प्रक्रिया में संशोधन-परिवर्द्धन का सोचा जाना चाहिये।
अमूर्तिपूजा में मानने वाले भी तीर्थंकर का शरीर सामने न होते हुए भी शरीर की कल्पना करके उनकी आत्मा का विनय-वन्दनादि द्वारा करते ही है। वे भी अगर केवल शरीर से ही विनय-वन्दनादि की क्रिया करके रह जाते हैं, उसके साथ भावों का रस नहीं घोलते; गुणों की प्रेरणा तथा रागद्वेष, कषाय, विषयासक्ति, हिंसा-असत्यादि को छोड़ने की प्रेरणा नहीं लेते; न ही उधर लक्ष्य देते हैं; मात्र क्रिया-काण्डों की अटवी में ही भटकते हैं, तो उनके लिए भी अपनी प्रक्रिया में संशोधन-परिवर्द्धन करना जरूरी है। ताकि साधना में सरसता आए, शुष्कता हटे। २०
श्री विजयानंद सूरि स्वर्गारोहण शताब्दी ग्रंथ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org