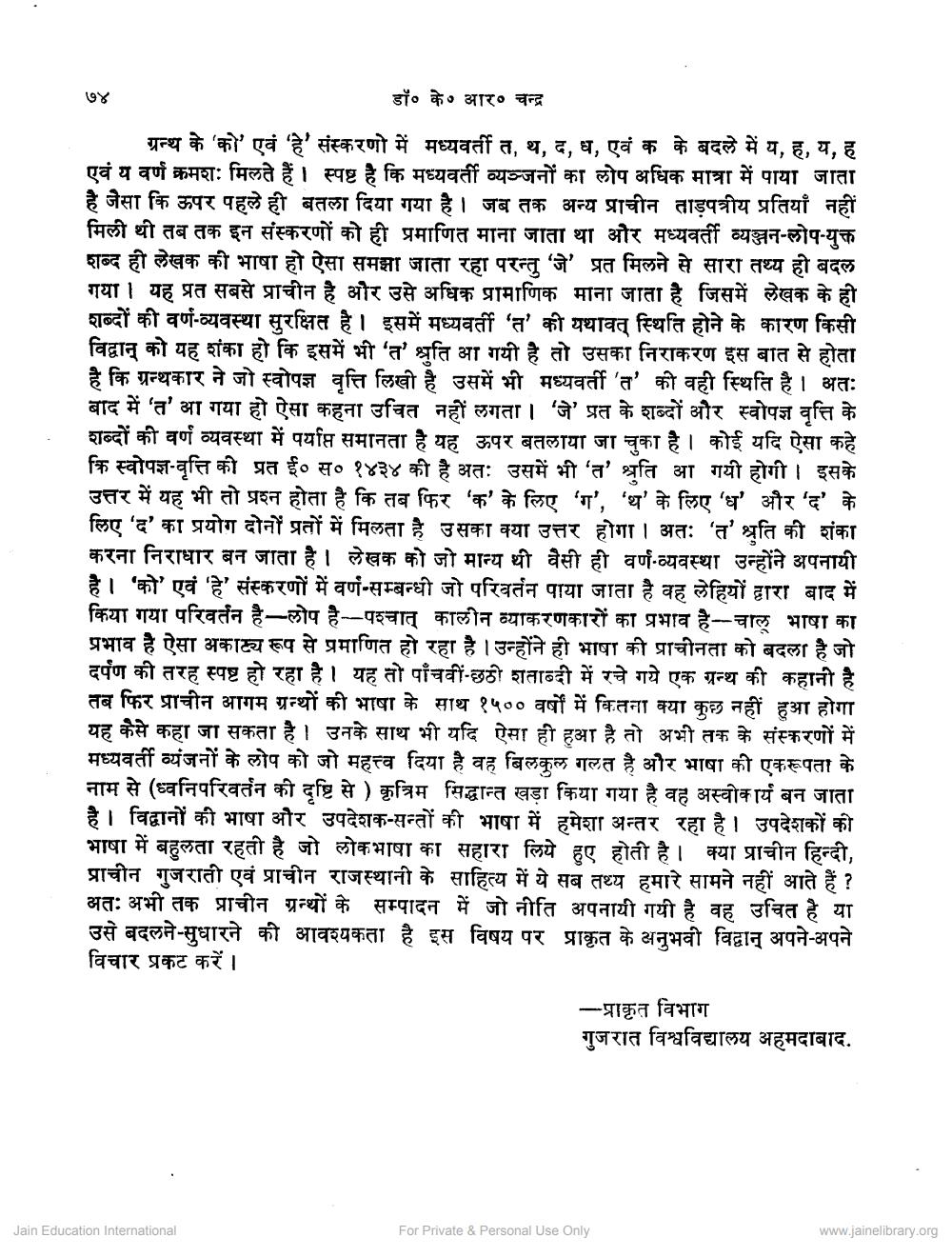________________
७४
डॉ. के. आर० चन्द्र
ग्रन्थ के 'को' एवं 'हे' संस्करणो में मध्यवर्ती त, थ, द, ध, एवं क के बदले में य, ह, य, ह एवं य वर्ण क्रमशः मिलते हैं। स्पष्ट है कि मध्यवर्ती व्यञ्जनों का लोप अधिक मात्रा में पाया जाता है जैसा कि ऊपर पहले ही बतला दिया गया है। जब तक अन्य प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियाँ नहीं मिली थी तब तक इन संस्करणों को ही प्रमाणित माना जाता था और मध्यवर्ती व्यञ्जन-लोप-युक्त शब्द ही लेखक की भाषा हो ऐसा समझा जाता रहा परन्तु 'जे' प्रत मिलने से सारा तथ्य ही बदल गया। यह प्रत सबसे प्राचीन है और उसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है जिसमें लेखक के ही शब्दों की वर्ण-व्यवस्था सुरक्षित है। इसमें मध्यवर्ती 'त' की यथावत् स्थिति होने के कारण किसी विद्वान् को यह शंका हो कि इसमें भी 'त' श्रुति आ गयी है तो उसका निराकरण इस बात से होता है कि ग्रन्थकार ने जो स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी है उसमें भी मध्यवर्ती 'त' को वही स्थिति है। अतः बाद में 'त' आ गया हो ऐसा कहना उचित नहीं लगता। 'जे' प्रत के शब्दों और स्वोपज्ञ वृत्ति के शब्दों की वर्ण व्यवस्था में पर्याप्त समानता है यह ऊपर बतलाया जा चुका है। कोई यदि ऐसा कहे कि स्वोपज्ञ-वृत्ति की प्रत ई० स० १४३४ की है अतः उसमें भी 'त' श्रुति आ गयी होगी। इसके उत्तर में यह भी तो प्रश्न होता है कि तब फिर 'क' के लिए 'ग', 'थ' के लिए 'ध' और 'द' के लिए 'द' का प्रयोग दोनों प्रतों में मिलता है उसका क्या उत्तर होगा। अतः 'त' श्रुति की शंका करना निराधार बन जाता है। लेखक को जो मान्य थी वैसी ही वर्ण व्यवस्था उन्होंने अपनायी है। 'को' एवं 'हे' संस्करणों में वर्ण-सम्बन्धी जो परिवर्तन पाया जाता है वह लेहियों द्वारा बाद में किया गया परिवर्तन है-लोप है-पश्चात् कालीन व्याकरणकारों का प्रभाव है-चालू भाषा का प्रभाव है ऐसा अकाट्य रूप से प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने ही भाषा की प्राचीनता को बदला है जो दर्पण की तरह स्पष्ट हो रहा है। यह तो पांचवीं-छठी शताब्दी में रचे गये एक ग्रन्थ की कहानी है तब फिर प्राचीन आगम ग्रन्थों की भाषा के साथ १५०० वर्षों में कितना क्या कुछ नहीं हुआ होगा यह कैसे कहा जा सकता है। उनके साथ भी यदि ऐसा ही हुआ है तो अभी तक के संस्करणों में मध्यवर्ती व्यंजनों के लोप को जो महत्त्व दिया है वह बिलकुल गलत है और भाषा की एकरूपता के नाम से (ध्वनिपरिवर्तन की दृष्टि से ) कृत्रिम सिद्धान्त खड़ा किया गया है वह अस्वीकार्य बन जाता है। विद्वानों की भाषा और उपदेशक-सन्तों की भाषा में हमेशा अन्तर रहा है। उपदेशकों की भाषा में बहुलता रहती है जो लोकभाषा का सहारा लिये हुए होती है। क्या प्राचीन हिन्दी, प्राचीन गुजराती एवं प्राचीन राजस्थानी के साहित्य में ये सब तथ्य हमारे सामने नहीं आते हैं ? अतः अभी तक प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन में जो नीति अपनायी गयी है वह उचित है या उसे बदलने-सुधारने की आवश्यकता है इस विषय पर प्राकृत के अनुभवी विद्वान् अपने-अपने विचार प्रकट करें।
-प्राकृत विभाग गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org