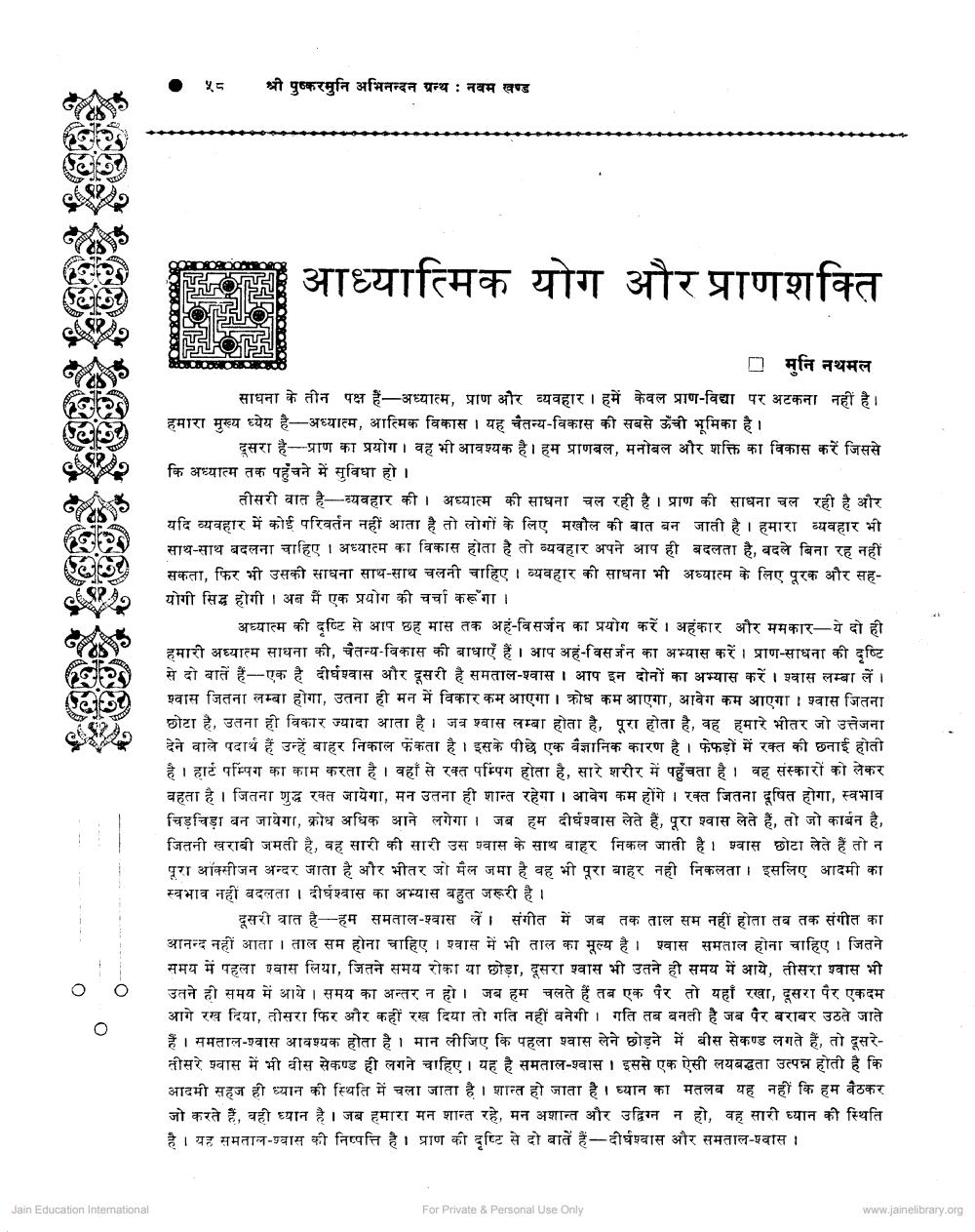________________
Jain Education International
५.८
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : नवम खण्ड
आध्यात्मिक योग और प्राणशक्ति
मुनि नथमल
साधना के तीन पक्ष हैं— अध्यात्म, प्राण और व्यवहार । हमें केवल प्राण-विद्या पर अटकना नहीं है। हमारा मुख्य ध्येय है— अध्यात्म, आत्मिक विकास । यह चैतन्य - विकास की सबसे ऊँची भूमिका है।
दूसरा है--प्राण का प्रयोग। वह भी आवश्यक है। हम प्राणबल, मनोबल और शक्ति का विकास करें जिससे कि अध्यात्म तक पहुँचने में सुविधा हो ।
तीसरी बात है—व्यवहार की
अध्यात्म की साधना चल रही है। प्राण की साधना चल रही है और यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो लोगों के लिए मखौल की बात बन साथ-साथ बदलना चाहिए । अध्यात्म का विकास होता है तो व्यवहार अपने आप ही सकता, फिर भी उसकी साधना साथ-साथ चलनी चाहिए। व्यवहार की साधना भी योगी सिद्ध होगी। अब मैं एक प्रयोग की चर्चा करूँगा ।
जाती है। हमारा व्यवहार भी बदलता है, बदले बिना रह नहीं अध्यात्म के लिए पूरक और सह
अध्यात्म की दृष्टि से आप छह मास तक अहं विसर्जन का प्रयोग करें । अहंकार और ममकार – ये दो ही हमारी अध्यात्म साधना की, चैतन्य-विकास की बाधाएँ हैं। आप अहं विसर्जन का अभ्यास करें । प्राण- साधना की दृष्टि से दो बातें हैं- एक है दीर्घश्वास और दूसरी है समताल श्वास । आप इन दोनों का अभ्यास करें। श्वास लम्बा लें । श्वास जितना लम्बा होगा, उतना ही मन में विकार कम आएगा। क्रोध कम आएगा, आवेग कम आएगा । श्वास जितना छोटा है, उतना ही विकार ज्यादा आता है। जब श्वास लम्बा होता है, पूरा होता है, वह हमारे भीतर जो उत्तेजना देने वाले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकाल फेंकता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। फेफड़ों में रक्त की छनाई होती है । हार्ट पम्पिंग का काम करता है । वहाँ से रक्त पम्पिंग होता है, सारे शरीर में पहुँचता है । वह संस्कारों को लेकर बहता है । जितना शुद्ध रक्त जायेगा, मन उतना ही शान्त रहेगा । आवेग कम होंगे । रक्त जितना दूषित होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा बन जायेगा, क्रोध अधिक आने लगेगा। जब हम दीर्घश्वास लेते हैं, पूरा श्वास लेते हैं, तो जो कार्बन है, जितनी खराबी जमती है, वह सारी की सारी उस श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। श्वास छोटा लेते हैं तो न पूरा ऑक्सीजन अन्दर जाता है और भीतर जो मैल जमा है वह भी पूरा बाहर नही निकलता। इसलिए आदमी का स्वभाव नहीं बदलता । दीर्घश्वास का अभ्यास बहुत जरूरी है ।
एकदम
दूसरी बात है हम समताल - श्वास लें। संगीत में जब तक ताल सम नहीं होता तब तक संगीत का आनन्द नहीं आता । ताल सम होना चाहिए। श्वास में भी ताल का मूल्य है । श्वास समताल होना चाहिए। जितने समय में पहला श्वास लिया, जितने समय रोका या छोड़ा, दूसरा श्वास भी उतने ही समय में आये, तीसरा श्वास भी उतने ही समय में आये । समय का अन्तर न हो। जब हम चलते हैं तब एक पैर तो यहाँ रखा, दूसरा पैर आगे रख दिया, तीसरा फिर और कहीं रख दिया तो गति नहीं बनेगी। गति तब बनती है जब पैर बराबर उठते जाते हैं । समताल श्वास आवश्यक होता है। मान लीजिए कि पहला श्वास लेने छोड़ने में बीस सेकण्ड लगते हैं, तो दूसरेतीसरे श्वास में भी बीस सेकण्ड ही लगने चाहिए। यह है समताल - श्वास । इससे एक ऐसी लयबद्धता उत्पन्न होती है कि आदमी सहज ही ध्यान की स्थिति में चला जाता है। शान्त हो जाता है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हम बैठकर जो करते हैं, वही ध्यान है । जब हमारा मन शान्त रहे, मन अशान्त और उद्विग्न न हो, वह सारी ध्यान की स्थिति है । यह समताल - श्वास की निष्पत्ति है । प्राण की दृष्टि से दो बातें हैं- दीर्घश्वास और समताल - श्वास |
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org