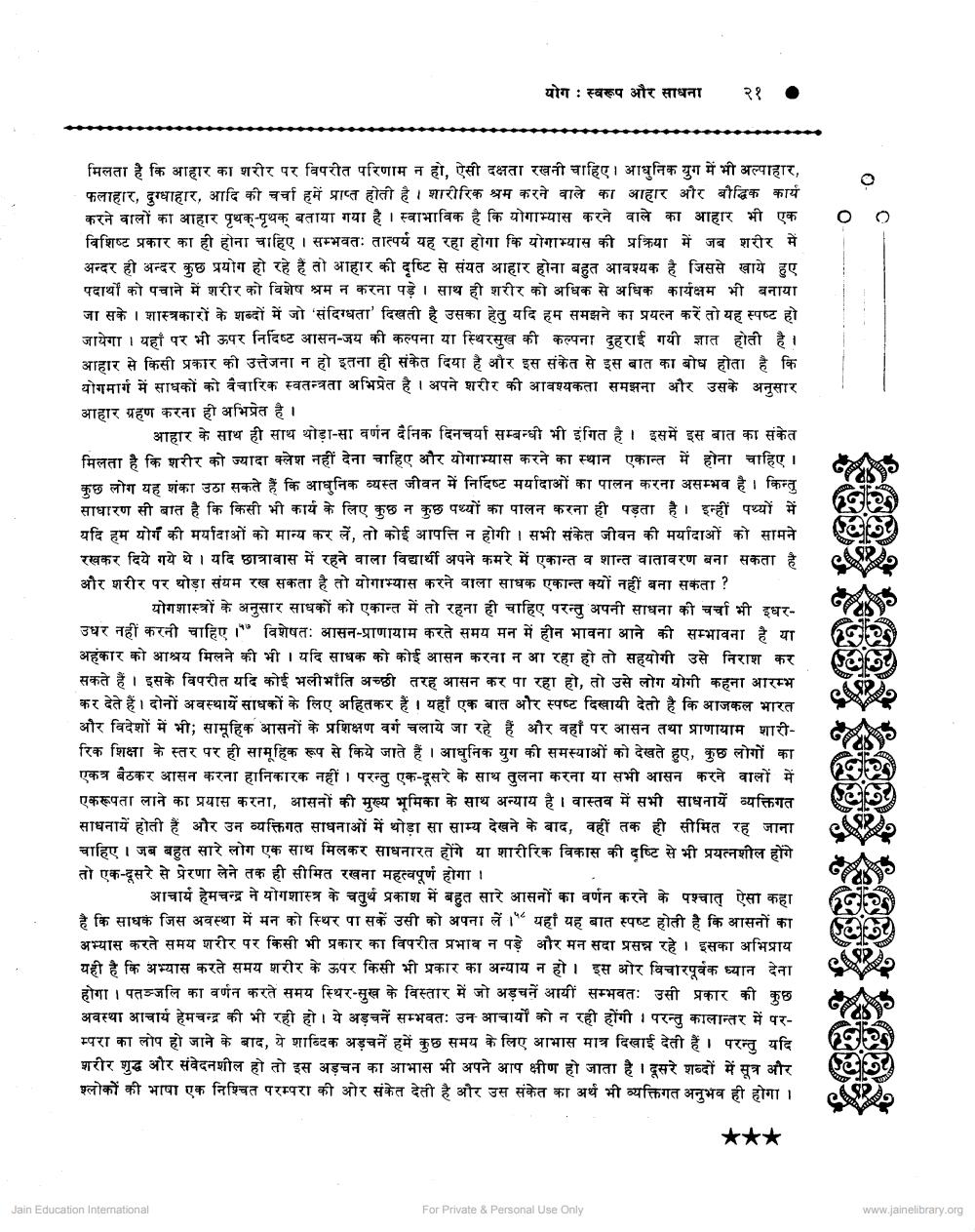________________
योग : स्वरूप और साधना
२१
.
मिलता है कि आहार का शरीर पर विपरीत परिणाम न हो, ऐसी दक्षता रखनी चाहिए। आधुनिक युग में भी अल्पाहार, फलाहार, दुग्धाहार, आदि की चर्चा हमें प्राप्त होती है। शारीरिक श्रम करने वाले का आहार और बौद्धिक कार्य करने वालों का आहार पृथक्-पृथक् बताया गया है । स्वाभाविक है कि योगाभ्यास करने वाले का आहार भी एक विशिष्ट प्रकार का ही होना चाहिए । सम्भवतः तात्पर्य यह रहा होगा कि योगाभ्यास की प्रक्रिया में जब शरीर में अन्दर ही अन्दर कुछ प्रयोग हो रहे हैं तो आहार की दृष्टि से संयत आहार होना बहुत आवश्यक है जिससे खाये हुए पदार्थों को पचाने में शरीर को विशेष श्रम न करना पड़े। साथ ही शरीर को अधिक से अधिक कार्यक्षम भी बनाया जा सके । शास्त्रकारों के शब्दों में जो 'संदिग्धता' दिखती है उसका हेतु यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा । यहाँ पर भी ऊपर निर्दिष्ट आसन-जय की कल्पना या स्थिरसुख की कल्पना दुहराई गयी ज्ञात होती है। आहार से किसी प्रकार की उत्तेजना न हो इतना ही संकेत दिया है और इस संकेत से इस बात का बोध होता है कि योगमार्ग में साधकों को वैचारिक स्वतन्त्रता अभिप्रेत है । अपने शरीर की आवश्यकता समझना और उसके अनुसार आहार ग्रहण करना ही अभिप्रेत है।
आहार के साथ ही साथ थोड़ा-सा वर्णन दैनिक दिनचर्या सम्बन्धी भी इंगित है। इसमें इस बात का संकेत मिलता है कि शरीर को ज्यादा क्लेश नहीं देना चाहिए और योगाभ्यास करने का स्थान एकान्त में होना चाहिए । कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैं कि आधुनिक व्यस्त जीवन में निर्दिष्ट मर्यादाओं का पालन करना असम्भव है। किन्त साधारण सी बात है कि किसी भी कार्य के लिए कुछ न कुछ पथ्यों का पालन करना ही पड़ता है। इन्हीं पथ्यों में यदि हम योग की मर्यादाओं को मान्य कर लें, तो कोई आपत्ति न होगी। सभी संकेत जीवन की मर्यादाओं को सामने रखकर दिये गये थे। यदि छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी अपने कमरे में एकान्त व शान्त वातावरण बना सकता है और शरीर पर थोड़ा संयम रख सकता है तो योगाभ्यास करने वाला साधक एकान्त क्यों नहीं बना सकता?
योगशास्त्रों के अनुसार साधकों को एकान्त में तो रहना ही चाहिए परन्तु अपनी साधना की चर्चा भी इधरउधर नहीं करनी चाहिए।" विशेषतः आसन-प्राणायाम करते समय मन में हीन भावना आने की सम्भावना है या अहंकार को आश्रय मिलने की भी । यदि साधक को कोई आसन करना न आ रहा हो तो सहयोगी उसे निराश कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई भलीभाँति अच्छी तरह आसन कर पा रहा हो, तो उसे लोग योगी कहना आरम्भ कर देते हैं। दोनों अवस्थायें साधकों के लिए अहितकर हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट दिखायी देतो है कि आजकल भारत और विदेशों में भी; सामूहिक आसनों के प्रशिक्षण वर्ग चलाये जा रहे हैं और वहाँ पर आसन तथा प्राणायाम शारीरिक शिक्षा के स्तर पर ही सामूहिक रूप से किये जाते हैं । आधुनिक युग की समस्याओं को देखते हुए, कुछ लोगों का एकत्र बैठकर आसन करना हानिकारक नहीं। परन्तु एक-दूसरे के साथ तुलना करना या सभी आसन करने वालों में एकरूपता लाने का प्रयास करना, आसनों की मुख्य भूमिका के साथ अन्याय है। वास्तव में सभी साधनायें व्यक्तिगत साधनायें होती हैं और उन व्यक्तिगत साधनाओं में थोड़ा सा साम्य देखने के बाद, वहीं तक ही सीमित रह जाना चाहिए । जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर साधनारत होंगे या शारीरिक विकास की दृष्टि से भी प्रयत्नशील होंगे तो एक-दूसरे से प्रेरणा लेने तक ही सीमित रखना महत्वपूर्ण होगा।
आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र के चतुर्थ प्रकाश में बहुत सारे आसनों का वर्णन करने के पश्चात् ऐसा कहा है कि साधक जिस अवस्था में मन को स्थिर पा सकें उसी को अपना लें। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि आसनों का अभ्यास करते समय शरीर पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े और मन सदा प्रसन्न रहे। इसका अभिप्राय यही है कि अभ्यास करते समय शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। इस ओर विचारपूर्वक ध्यान देना होगा । पतञ्जलि का वर्णन करते समय स्थिर-सुख के विस्तार में जो अड़चनें आयीं सम्भवतः उसी प्रकार की कुछ अवस्था आचार्य हेमचन्द्र की भी रही हो। ये अड़चनें सम्भवतः उन आचार्यों को न रही होंगी । परन्तु कालान्तर में परम्परा का लोप हो जाने के बाद, ये शाब्दिक अड़चनें हमें कुछ समय के लिए आभास मात्र दिखाई देती हैं। परन्तु यदि शरीर शुद्ध और संवेदनशील हो तो इस अड़चन का आभास भी अपने आप क्षीण हो जाता है । दूसरे शब्दों में सूत्र और श्लोकों की भाषा एक निश्चित परम्परा की ओर संकेत देती है और उस संकेत का अर्थ भी व्यक्तिगत अनुभव ही होगा।
HARINA
CSRA
RAJA
0Sda
***
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org