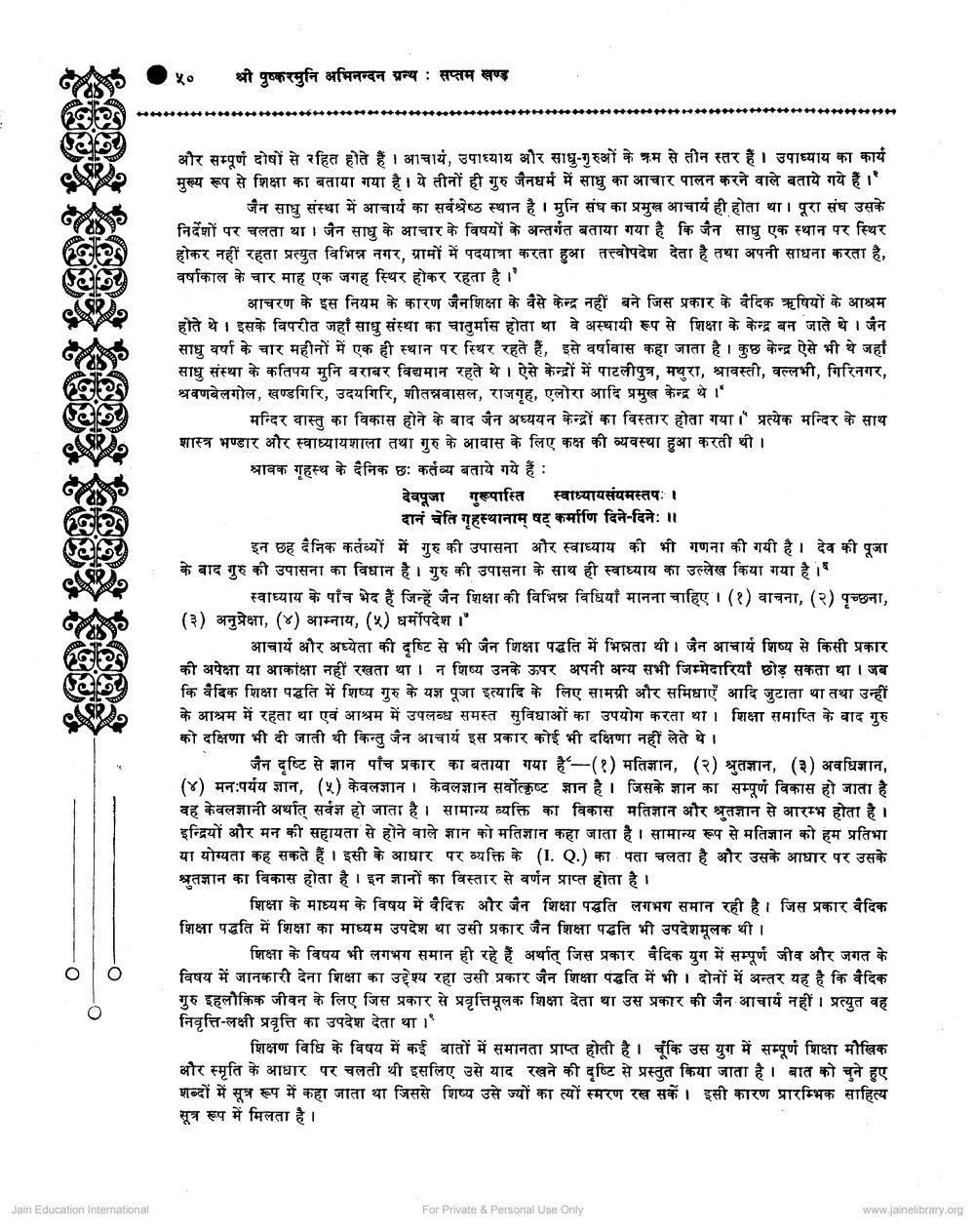________________
५०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : सप्तम खण्ड
और सम्पूर्ण दोषों से रहित होते हैं । आचार्य, उपाध्याय और साधु-गुरुओं के क्रम से तीन स्तर हैं । उपाध्याय का कार्य मुख्य रूप से शिक्षा का बताया गया है। ये तीनों ही गुरु जैनधर्म में साधु का आचार पालन करने वाले बताये गये हैं।
जैन साधु संस्था में आचार्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । मुनि संघ का प्रमुख आचार्य ही होता था। पूरा संघ उसके निर्देशों पर चलता था। जैन साधु के आचार के विषयों के अन्तर्गत बताया गया है कि जैन साधु एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता प्रत्युत विभिन्न नगर, ग्रामों में पदयात्रा करता हुआ तत्त्वोपदेश देता है तथा अपनी साधना करता है, वर्षाकाल के चार माह एक जगह स्थिर होकर रहता है।'
आचरण के इस नियम के कारण जनशिक्षा के वैसे केन्द्र नहीं बने जिस प्रकार के वैदिक ऋषियों के आश्रम होते थे। इसके विपरीत जहाँ साधु संस्था का चातुर्मास होता था वे अस्थायी रूप से शिक्षा के केन्द्र बन जाते थे । जैन साधु वर्षा के चार महीनों में एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसे वर्षावास कहा जाता है। कुछ केन्द्र ऐसे भी थे जहाँ साधु संस्था के कतिपय मुनि बराबर विद्यमान रहते थे। ऐसे केन्द्रों में पाटलीपुत्र, मथुरा, श्रावस्ती, वल्लभी, गिरिनगर, श्रवणबेलगोल, खण्डगिरि, उदयगिरि, शीतन्नवासल, राजगृह, एलोरा आदि प्रमुख केन्द्र थे ।'
मन्दिर वास्तु का विकास होने के बाद जैन अध्ययन केन्द्रों का विस्तार होता गया। प्रत्येक मन्दिर के साथ शास्त्र भण्डार और स्वाध्यायशाला तथा गुरु के आवास के लिए कक्ष की व्यवस्था हुआ करती थी। श्रावक गृहस्थ के दैनिक छः कर्तव्य बताये गये हैं :
देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्यायसंयमस्तपः ।
दानं चेति गृहस्थानाम् षट् कर्माणि दिने-दिनेः ॥ इन छह दैनिक कर्तव्यों में गुरु की उपासना और स्वाध्याय की भी गणना की गयी है। देव की पूजा के बाद गुरु की उपासना का विधान है। गुरु की उपासना के साथ ही स्वाध्याय का उल्लेख किया गया है।
__ स्वाध्याय के पाँच भेद हैं जिन्हें जैन शिक्षा की विभिन्न विधियाँ मानना चाहिए । (१) वाचना, (२) पृच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय, (५) धर्मोपदेश ।'
आचार्य और अध्येता की दृष्टि से भी जैन शिक्षा पद्धति में भिन्नता थी। जैन आचार्य शिष्य से किसी प्रकार की अपेक्षा या आकांक्षा नहीं रखता था। न शिष्य उनके ऊपर अपनी अन्य सभी जिम्मेदारियां छोड़ सकता था । जब कि वैदिक शिक्षा पद्धति में शिष्य गुरु के यज्ञ पूजा इत्यादि के लिए सामग्री और समिधाएँ आदि जुटाता था तथा उन्हीं के आश्रम में रहता था एवं आश्रम में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का उपयोग करता था। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी किन्तु जैन आचार्य इस प्रकार कोई भी दक्षिणा नहीं लेते थे।
जैन दृष्टि से ज्ञान पाँच प्रकार का बताया गया है -(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनःपर्यय ज्ञान, (५) केवलज्ञान । केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। जिसके ज्ञान का सम्पूर्ण विकास हो जाता है वह केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का विकास मतिज्ञान और श्रुतज्ञान से आरम्भ होता है। इन्द्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान कहा जाता है। सामान्य रूप से मतिज्ञान को हम प्रतिभा या योग्यता कह सकते हैं । इसी के आधार पर व्यक्ति के (I. Q.) का पता चलता है और उसके आधार पर उसके श्रुतज्ञान का विकास होता है । इन ज्ञानों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है।
शिक्षा के माध्यम के विषय में वैदिक और जैन शिक्षा पद्धति लगभग समान रही है। जिस प्रकार वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम उपदेश था उसी प्रकार जैन शिक्षा पद्धति भी उपदेशमूलक थी।
शिक्षा के विषय भी लगभग समान ही रहे हैं अर्थात् जिस प्रकार वैदिक युग में सम्पूर्ण जीव और जगत के विषय में जानकारी देना शिक्षा का उद्देश्य रहा उसी प्रकार जैन शिक्षा पद्धति में भी। दोनों में अन्तर यह है कि वैदिक गुरु इहलौकिक जीवन के लिए जिस प्रकार से प्रवृत्तिमूलक शिक्षा देता था उस प्रकार की जैन आचार्य नहीं। प्रत्युत वह निवृत्ति-लक्षी प्रवृत्ति का उपदेश देता था।
शिक्षण विधि के विषय में कई बातों में समानता प्राप्त होती है। चूंकि उस युग में सम्पूर्ण शिक्षा मौखिक और स्मृति के आधार पर चलती थी इसलिए उसे याद रखने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। बात को चुने हुए शब्दों में सूत्र रूप में कहा जाता था जिससे शिष्य उसे ज्यों का त्यों स्मरण रख सकें। इसी कारण प्रारम्भिक साहित्य सूत्र रूप में मिलता है।
००
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org