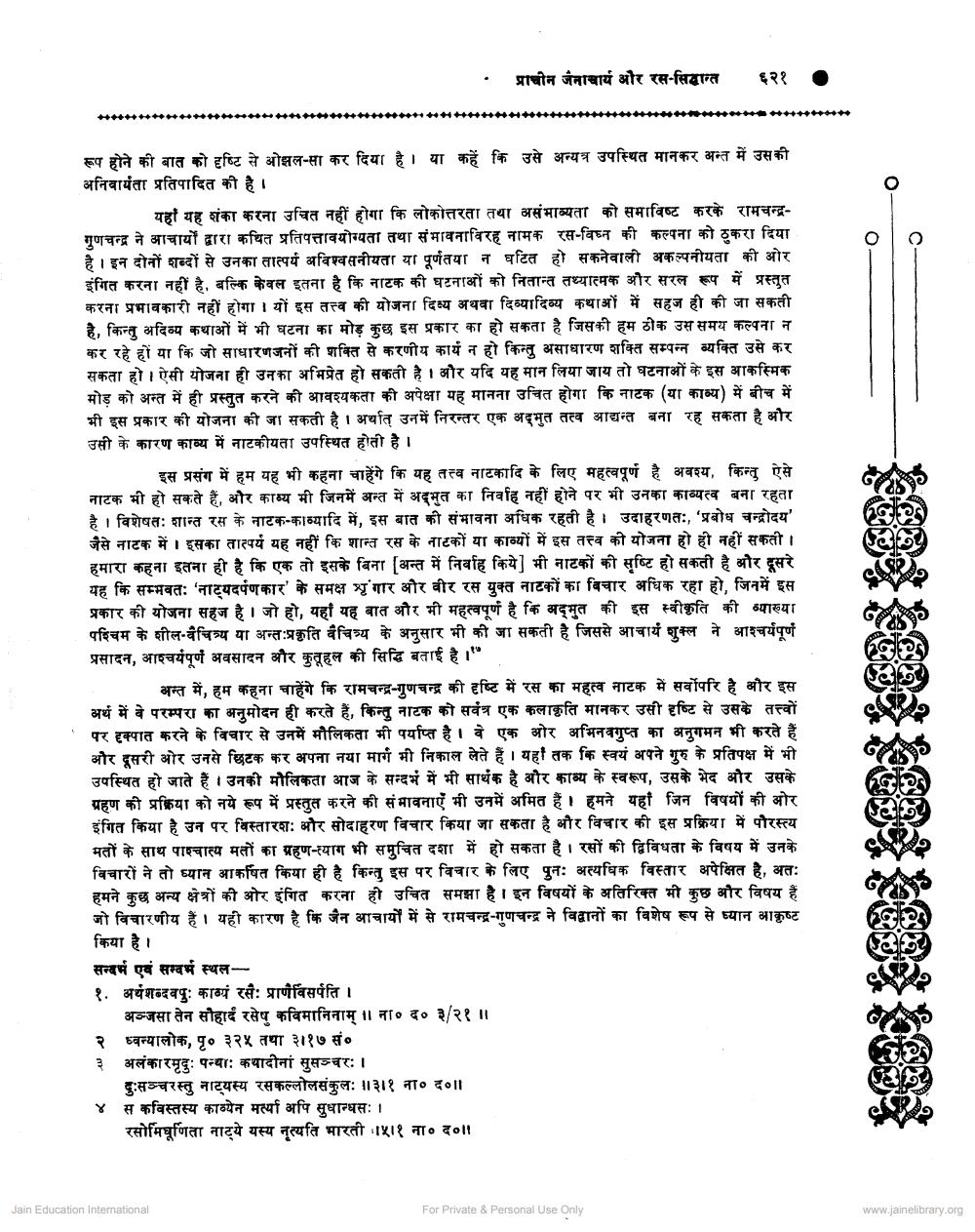________________
• प्राचीन जैनाचार्य और रस-सिद्धान्त
६२१
रूप होने की बात को दृष्टि से ओझल-सा कर दिया है। या कहें कि उसे अन्यत्र उपस्थित मानकर अन्त में उसकी अनिवार्यता प्रतिपादित की है।
यहां यह शंका करना उचित नहीं होगा कि लोकोत्तरता तथा असंभाव्यता को समाविष्ट करके रामचन्द्रगुणचन्द्र ने आचार्यों द्वारा कथित प्रतिपत्तावयोग्यता तथा समावनाविरह नामक रस-विघ्न की कल्पना को ठुकरा दिया है। इन दोनों शब्दों से उनका तात्पर्य अविश्वसनीयता या पूर्णतया न घटित हो सकनेवाली अकल्पनीयता की ओर इंगित करना नहीं है, बल्कि केवल इतना है कि नाटक की घटनाओं को नितान्त तथ्यात्मक और सरल रूप में प्रस्तुत करना प्रभावकारी नहीं होगा। यों इस तत्त्व की योजना दिव्य अथवा दिव्यादिव्य कथाओं में सहज ही की जा सकती है, किन्तु अदिव्य कथाओं में भी घटना का मोड़ कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसकी हम ठीक उस समय कल्पना न कर रहे हों या कि जो साधारणजनों की शक्ति से करणीय कार्य न हो किन्तु असाधारण शक्ति सम्पन्न व्यक्ति उसे कर सकता हो । ऐसी योजना ही उनका अभिप्रेत हो सकती है । और यदि यह मान लिया जाय तो घटनाओं के इस आकस्मिक मोड़ को अन्त में ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अपेक्षा यह मानना उचित होगा कि नाटक (या काव्य) में बीच में भी इस प्रकार की योजना की जा सकती है । अर्थात् उनमें निरन्तर एक अद्भुत तत्व आद्यन्त बना रह सकता है और उसी के कारण काव्य में नाटकीयता उपस्थित होती है।
इस प्रसंग में हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह तत्त्व नाटकादि के लिए महत्वपूर्ण है अवश्य, किन्तु ऐसे नाटक भी हो सकते हैं, और काव्य भी जिनमें अन्त में अद्भुत का निर्वाह नहीं होने पर भी उनका काव्यत्व बना रहता है । विशेषतः शान्त रस के नाटक-काव्यादि में, इस बात की संभावना अधिक रहती है। उदाहरणतः, 'प्रबोध चन्द्रोदय' जैसे नाटक में । इसका तात्पर्य यह नहीं कि शान्त रस के नाटकों या काव्यों में इस तत्त्व की योजना हो ही नहीं सकती। हमारा कहना इतना ही है कि एक तो इसके बिना [अन्त में निर्वाह किये भी नाटकों को सृष्टि हो सकती है और दूसरे यह कि सम्भवतः 'नाट्यदर्पणकार' के समक्ष शृंगार और वीर रस युक्त नाटकों का विचार अधिक रहा हो, जिनमें इस प्रकार की योजना सहज है । जो हो, यहाँ यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि अद्भुत की इस स्वीकृति की व्याख्या पश्चिम के शील-वैचित्र्य या अन्तःप्रकृति वैचित्र्य के अनुसार भी की जा सकती है जिससे आचार्य शुक्ल ने आश्चर्यपूर्ण प्रसादन, आश्चर्यपूर्ण अवसादन और कुतूहल की सिद्धि बताई है।"
अन्त में, हम कहना चाहेंगे कि रामचन्द्र-गुणचन्द्र की दृष्टि में रस का महत्व नाटक में सर्वोपरि है और इस अर्थ में वे परम्परा का अनुमोदन ही करते हैं, किन्तु नाटक को सर्वत्र एक कलाकृति मानकर उसी दृष्टि से उसके तत्त्वों पर दृक्पात करने के विचार से उनमें मौलिकता भी पर्याप्त है। वे एक ओर अभिनवगुप्त का अनुगमन भी करते हैं और दूसरी ओर उनसे छिटक कर अपना नया मार्ग भी निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि स्वयं अपने गुरु के प्रतिपक्ष में भी उपस्थित हो जाते हैं। उनकी मौलिकता आज के सन्दर्भ में भी सार्थक है और काव्य के स्वरूप, उसके भेद और उसके ग्रहण की प्रक्रिया को नये रूप में प्रस्तुत करने की संभावनाएं भी उनमें अमित हैं। हमने यहाँ जिन विषयों की ओर इंगित किया है उन पर विस्तारशः और सोदाहरण विचार किया जा सकता है और विचार की इस प्रक्रिया में पौरस्त्य मतों के साथ पाश्चात्य मतों का ग्रहण-त्याग भी समुचित दशा में हो सकता है । रसों की द्विविधता के विषय में उनके विचारों ने तो ध्यान आकर्षित किया ही है किन्तु इस पर विचार के लिए पुनः अत्यधिक विस्तार अपेक्षित है, अतः हमने कुछ अन्य क्षेत्रों की ओर इंगित करना ही उचित समझा है। इन विषयों के अतिरिक्त मी कुछ और विषय हैं जो विचारणीय हैं। यही कारण है कि जैन आचार्यों में से रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने विद्वानों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। सन्दर्भ एवं सम्वर्भ स्थल१. अर्थशब्दवपुः काव्यं रसैः प्राणविसर्पति ।
अञ्जसा तेन सौहार्द रसेषु कविमानिनाम् ॥ ना० द० ३/२१ ॥ २ ध्वन्यालोक, पृ० ३२५ तथा ३३१७ सं० ३ अलंकारमृदुः पन्थाः कयादीनां सुसञ्चरः ।
दुःसञ्चरस्तु नाट्यस्य रसकल्लोलसंकुलः ॥३१ ना० द०॥ ४ स कविस्तस्य काव्येन मा अपि सुधान्धसः ।
रसोमिघूर्णिता नाट्ये यस्य नृत्यति भारती ॥५।१ ना० द०॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org