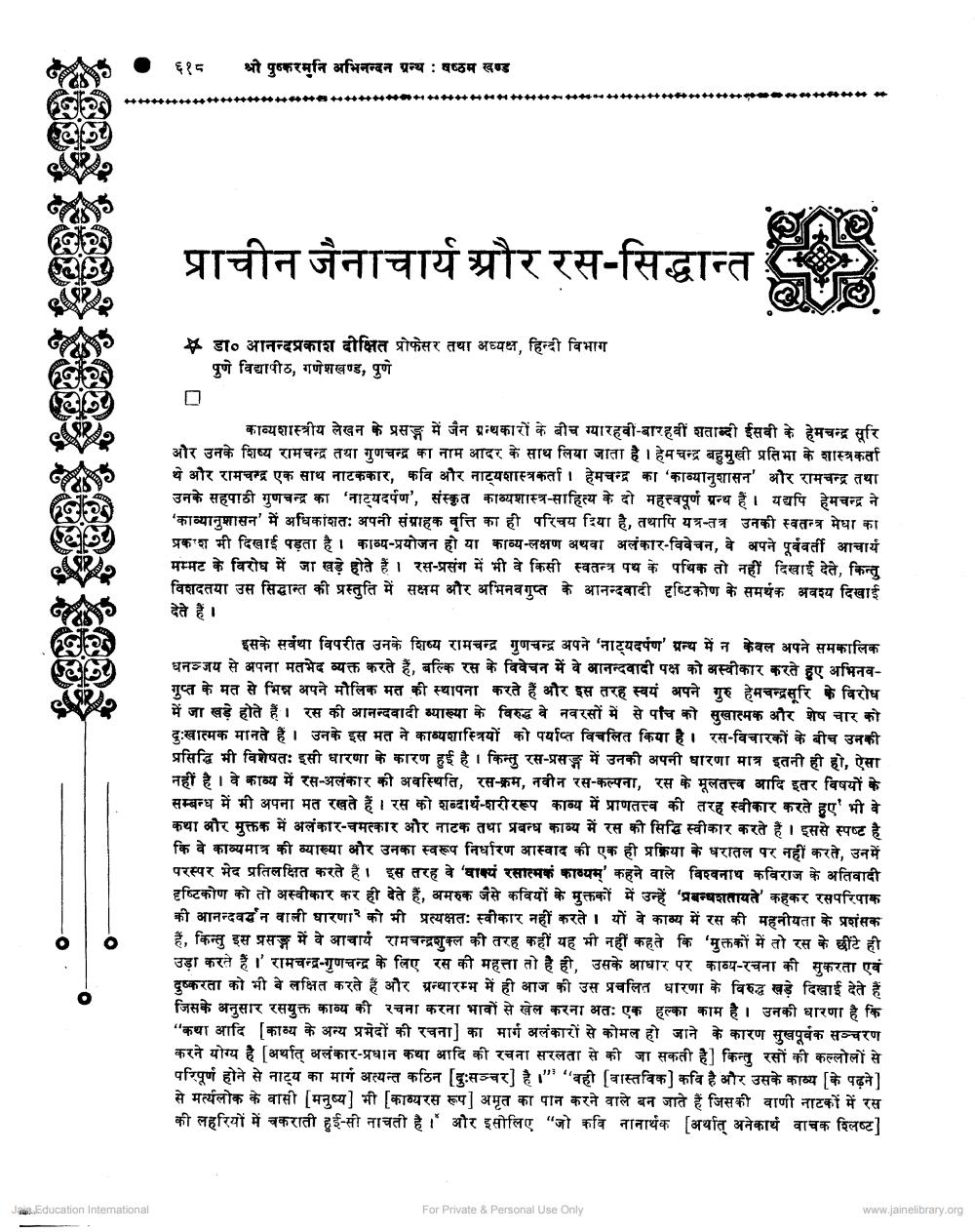________________
-O
•
-O
Jan Education International
६१८
श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठम खण्ड
►Œ++ +++++++++++++++*****
प्राचीन जैनाचार्य और रस सिद्धान्त
* डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग पुणे विद्यापीठ, गणेशखण्ड, पुणे
*********
काव्यशास्त्रीय लेखन के प्रसद्ध में जैन ग्रन्थकारों के बीच व्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ईसवी के हेमचन्द्र ि और उनके शिष्य रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र का नाम आदर के साथ लिया जाता है। हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभा के शास्त्रकर्ता थे और रामचन्द्र एक साथ नाटककार, कवि और नाट्यशास्त्रकर्ता । हेमचन्द्र का 'काव्यानुशासन' और रामचन्द्र तथा उनके सहपाठी गुणचन्द्र का 'नाट्यदर्पण', संस्कृत काव्यशास्त्र - साहित्य के दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। यद्यपि हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' में अधिकांशतः अपनी संग्राहक वृत्ति का ही परिचय दिया है, तथापि यत्र-तत्र उनकी स्वतन्त्र मेधा का प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। काव्य प्रयोजन हो या काव्य-लक्षण अथवा अलंकार-विवेचन, वे अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट के विरोध में जा खड़े होते हैं। रस-प्रसंग में भी वे किसी स्वतन्त्र पथ के पथिक तो नहीं दिखाई देते, किन्तु विशदतया उस सिद्धान्त की प्रस्तुति में सक्षम और अभिनवगुप्त के आनन्दवादी दृष्टिकोण के समर्थक अवश्य दिखाई देते हैं ।
इसके सर्वथा विपरीत उनके शिष्य रामचन्द्र गुणचन्द्र अपने 'नाट्यदर्पण' ग्रन्थ में न केवल अपने समकालिक धनञ्जय से अपना मतभेद व्यक्त करते हैं, बल्कि रस के विवेचन में वे आनन्दवादी पक्ष को अस्वीकार करते हुए अभिनवगुप्त के मत से भिन्न अपने मौलिक मत की स्थापना करते हैं और इस तरह स्वयं अपने गुरु हेमचन्द्रसूरि के विरोध में जा खड़े होते हैं । रस की आनन्दवादी व्याख्या के विरुद्ध वे नवरसों में से पांच को सुखात्मक और शेष चार को दुःखात्मक मानते हैं । उनके इस मत ने काव्यशास्त्रियों को पर्याप्त विचलित किया है। रस-विचारकों के बीच उनकी प्रसिद्धि भी विशेषतः इसी धारणा के कारण हुई है। किन्तु रस-प्रसङ्ग में उनकी अपनी धारणा मात्र इतनी ही हो, ऐसा नहीं है। वे काव्य में रस- अलंकार की अवस्थिति, रस-क्रम, नवीन रस कल्पना, रस के मूलतत्त्व आदि इतर विषयों के सम्बन्ध में भी अपना मत रखते हैं। रस को शब्दार्थ- शरीररूप काव्य में प्राणतत्त्व की तरह स्वीकार करते हुए भी वे कथा और मुक्तक में अलंकार-चमत्कार और नाटक तथा प्रबन्ध काव्य में रस की सिद्धि स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे काव्यमात्र की व्याख्या और उनका स्वरूप निर्धारण आस्वाद की एक ही प्रक्रिया के धरातल पर नहीं करते, उनमें परस्पर भेद प्रतिलक्षित करते हैं। इस तरह वे 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' कहने वाले विश्वनाथ कविराज के अतिवादी दृष्टिकोण को तो अस्वीकार कर ही देते हैं, अमरुक जैसे कवियों के मुक्तकों में उन्हें 'प्रबन्धशतायते' कहकर रसपरिपाक की आनन्दवर्द्धन वाली धारणा को भी प्रत्यक्षतः स्वीकार नहीं करते। यों वे काव्य में रस की महनीयता के प्रशंसक है, किन्तु इस यज्ञ में वे आचार्य रामचन्द्रशुक्ल की तरह कहीं यह भी नहीं कहते कि 'मुतकों में तो रस के छींटे ही उड़ा करते हैं ।' रामचन्द्र गुणचन्द्र के लिए रस की महत्ता तो है ही, उसके आधार पर काव्य रचना की सुकरता एवं दुष्करता को भी वे लक्षित करते हैं और ग्रन्थारम्भ में ही आज की उस प्रचलित धारणा के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। जिसके अनुसार रसयुक्त काव्य की रचना करना भावों से खेल करना अतः एक हल्का काम है। उनकी धारणा है कि "कथा आदि [ काव्य के अन्य प्रभेदों की रचना ] का मार्ग अलंकारों से कोमल हो जाने के कारण सुखपूर्वक सञ्चरण करने योग्य है [ अर्थात् अलंकार प्रधान कथा आदि की रचना सरलता से की जा सकती है] किन्तु रसों की कल्लोलों से परिपूर्ण होने से नाट्य का मार्ग अत्यन्त कठिन [दुःसञ्चर ] है ।" "वही [ वास्तविक ] कवि है और उसके काव्य [के पढ़ने ] से मर्त्यलोक के वासी [ मनुष्य ] भी [काव्यरस रूप] अमृत का पान करने वाले बन जाते हैं जिसकी वाणी नाटकों में रस की लहरियों में चकराती हुई-सी नाचती है और इसीलिए "जो कवि नानार्थक [अर्थात् अनेकार्थ वाचक लिष्ट ]
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org