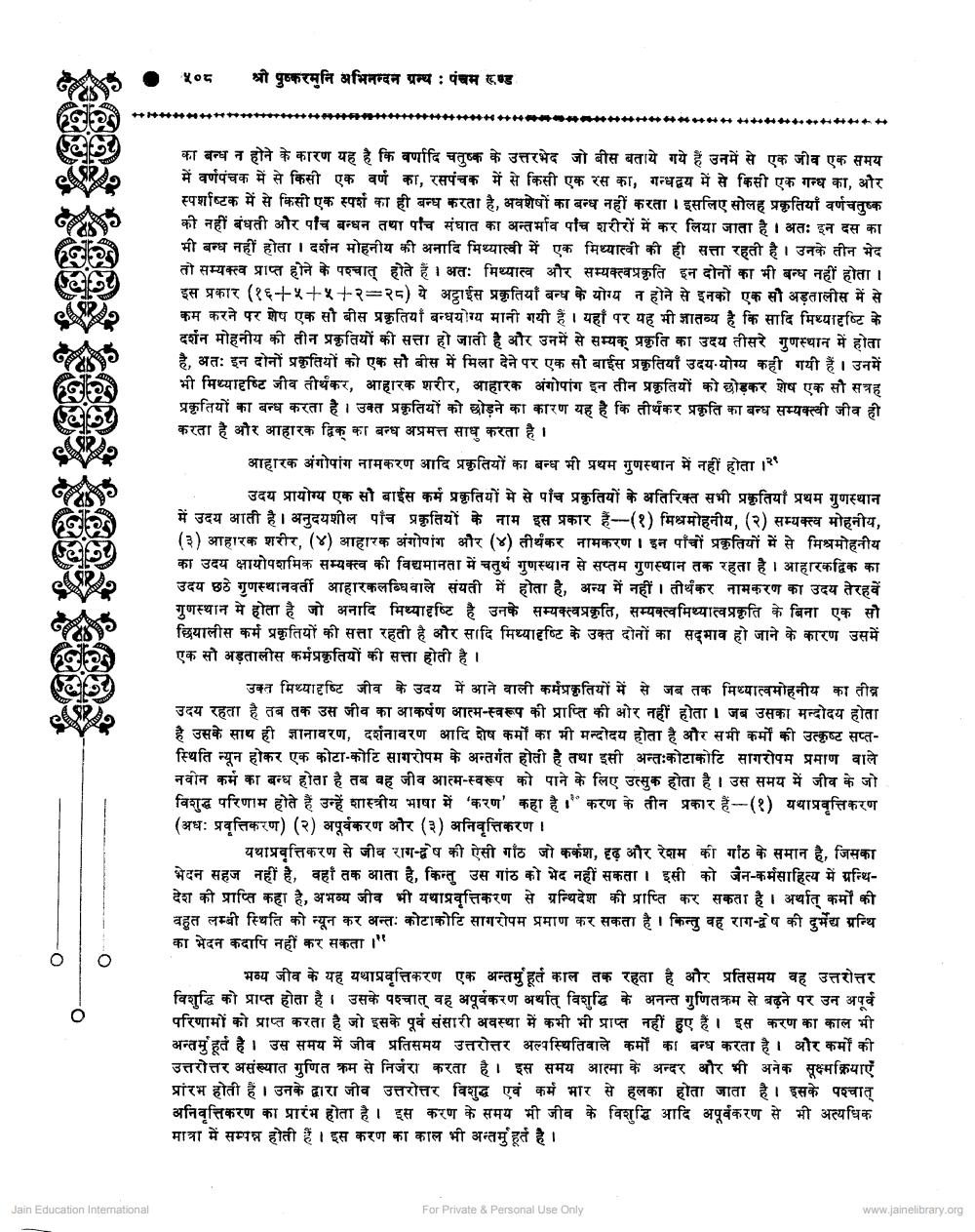________________
५०८
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम एण्ड
का बन्ध न होने के कारण यह है कि वर्णादि चतुष्क के उत्तरभेद जो बीस बताये गये हैं उनमें से एक जीव एक समय में वर्णपंचक में से किसी एक वर्ण का, रसपंचक में से किसी एक रस का, गन्धद्वय में से किसी एक गन्ध का, और स्पर्शाष्टक में से किसी एक स्पर्श का ही बन्ध करता है, अवशेषों का बन्ध नहीं करता । इसलिए सोलह प्रकृतियाँ वर्णचतुष्क की नहीं बंधती और पांच बन्धन तथा पांच संघात का अन्तर्भाव पाँच शरीरों में कर लिया जाता है। अतः इन दस का भी बन्ध नहीं होता । दर्शन मोहनीय की अनादि मिथ्यात्वी में एक मिथ्यात्वी की ही सत्ता रहती है। उनके तीन भेद तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के पश्चात् होते हैं। अतः मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन दोनों का भी बन्ध नहीं होता। इस प्रकार (१६+५+५+२=२८) ये अट्ठाईस प्रकृतियाँ बन्ध के योग्य न होने से इनको एक सौ अड़तालीस में से कम करने पर शेष एक सौ बीस प्रकृतियाँ बन्धयोग्य मानी गयी हैं। यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि सादि मिथ्यादृष्टि के दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों की सत्ता हो जाती है और उनमें से सम्यक् प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में होता है, अतः इन दोनों प्रकृतियों को एक सौ बीस में मिला देने पर एक सौ बाईस प्रकृतियाँ उदय योग्य कही गयी हैं। उनमें भी मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थकर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग इन तीन प्रकृतियों को छोड़कर शेष एक सौ सत्रह प्रकृतियों का बन्ध करता है । उक्त प्रकृतियों को छोड़ने का कारण यह है कि तीर्थकर प्रकृति का बन्ध सम्यक्त्वी जीव ही करता है और आहारक द्विक् का बन्ध अप्रमत्त साधु करता है।
आहारक अंगोपांग नामकरण आदि प्रकृतियों का बन्ध भी प्रथम गुणस्थान में नहीं होता ।
उदय प्रायोग्य एक सौ बाईस कर्म प्रकृतियों में से पांच प्रकृतियों के अतिरिक्त सभी प्रकृतियाँ प्रथम गुणस्थान में उदय आती है। अनुदयशील पाँच प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं-(१) मिश्रमोहनीय, (२) सम्यक्त्व मोहनीय, (३) आहारक शरीर, (४) आहारक अंगोपांग और (४) तीर्थंकर नामकरण । इन पाँचों प्रकृतियों में से मिश्रमोहनीय का उदय क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की विद्यमानता में चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक रहता है । आहारकद्विक का उदय छठे गुणस्थानवर्ती आहारकलब्धिवाले संयती में होता है, अन्य में नहीं । तीर्थंकर नामकरण का उदय तेरहवें गुणस्थान में होता है जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उनके सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रकृति के बिना एक सौ छियालीस कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है और सादि मिथ्यादृष्टि के उक्त दोनों का सद्भाव हो जाने के कारण उसमें एक सो अड़तालीस कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है ।
उक्त मिथ्यादृष्टि जीव के उदय में आने वाली कर्मप्रकृतियों में से जब तक मिथ्यात्वमोहनीय का तीव्र उदय रहता है तब तक उस जीव का आकर्षण आत्म-स्वरूप की प्राप्ति की ओर नहीं होता। जब उसका मन्दोदय होता है उसके साथ ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि शेष कर्मों का भी मन्दोदय होता है और सभी कर्मों की उत्कृष्ट सप्तस्थिति न्यून होकर एक कोटा-कोटि सागरोपम के अन्तर्गत होती है तथा इसी अन्तःकोटाकोटि सागरोपम प्रमाण वाले नवीन कर्म का बन्ध होता है तब वह जीव आत्म-स्वरूप को पाने के लिए उत्सुक होता है । उस समय में जीव के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उन्हें शास्त्रीय भाषा में 'करण' कहा है। करण के तीन प्रकार हैं-(१) यथाप्रवृत्तिकरण (अधः प्रवृत्तिकरण) (२) अपूर्वकरण और (३) अनिवृत्तिकरण ।
यथाप्रवृत्तिकरण से जीव राग-द्वेष की ऐसी गाँठ जो कर्कश, दृढ़ और रेशम की गांठ के समान है, जिसका भेदन सहज नहीं है, वहाँ तक आता है, किन्तु उस गांठ को भेद नहीं सकता। इसी को जैन-कर्मसाहित्य में ग्रन्थिदेश की प्राप्ति कहा है, अभव्य जीव भी यथाप्रवृत्तिकरण से ग्रन्थिदेश की प्राप्ति कर सकता है । अर्थात् कर्मों की बहुत लम्बी स्थिति को न्यून कर अन्तः कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण कर सकता है । किन्तु वह राग-द्वेष की दुर्मेद्य ग्रन्थि का भेदन कदापि नहीं कर सकता।"
भव्य जीव के यह यथाप्रवृत्तिकरण एक अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है और प्रतिसमय वह उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होता है। उसके पश्चात् वह अपूर्वकरण अर्थात् विशुद्धि के अनन्त गुणितक्रम से बढ़ने पर उन अपूर्व परिणामों को प्राप्त करता है जो इसके पूर्व संसारी अवस्था में कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस करण का काल भी अन्तर्मुहूर्त है। उस समय में जीव प्रतिसमय उत्तरोत्तर अल्पस्थितिवाले कर्मों का बन्ध करता है। और कर्मों की उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित क्रम से निर्जरा करता है। इस समय आत्मा के अन्दर और भी अनेक सूक्ष्मक्रियाएँ प्रांरभ होती हैं। उनके द्वारा जीव उत्तरोत्तर विशुद्ध एवं कर्म भार से हलका होता जाता है। इसके पश्चात् अनिवृत्तिकरण का प्रारंभ होता है। इस करण के समय भी जीव के विशुद्धि आदि अपूर्वकरण से भी अत्यधिक मात्रा में सम्पन्न होती हैं । इस करण का काल भी अन्तर्मुहूर्त है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org