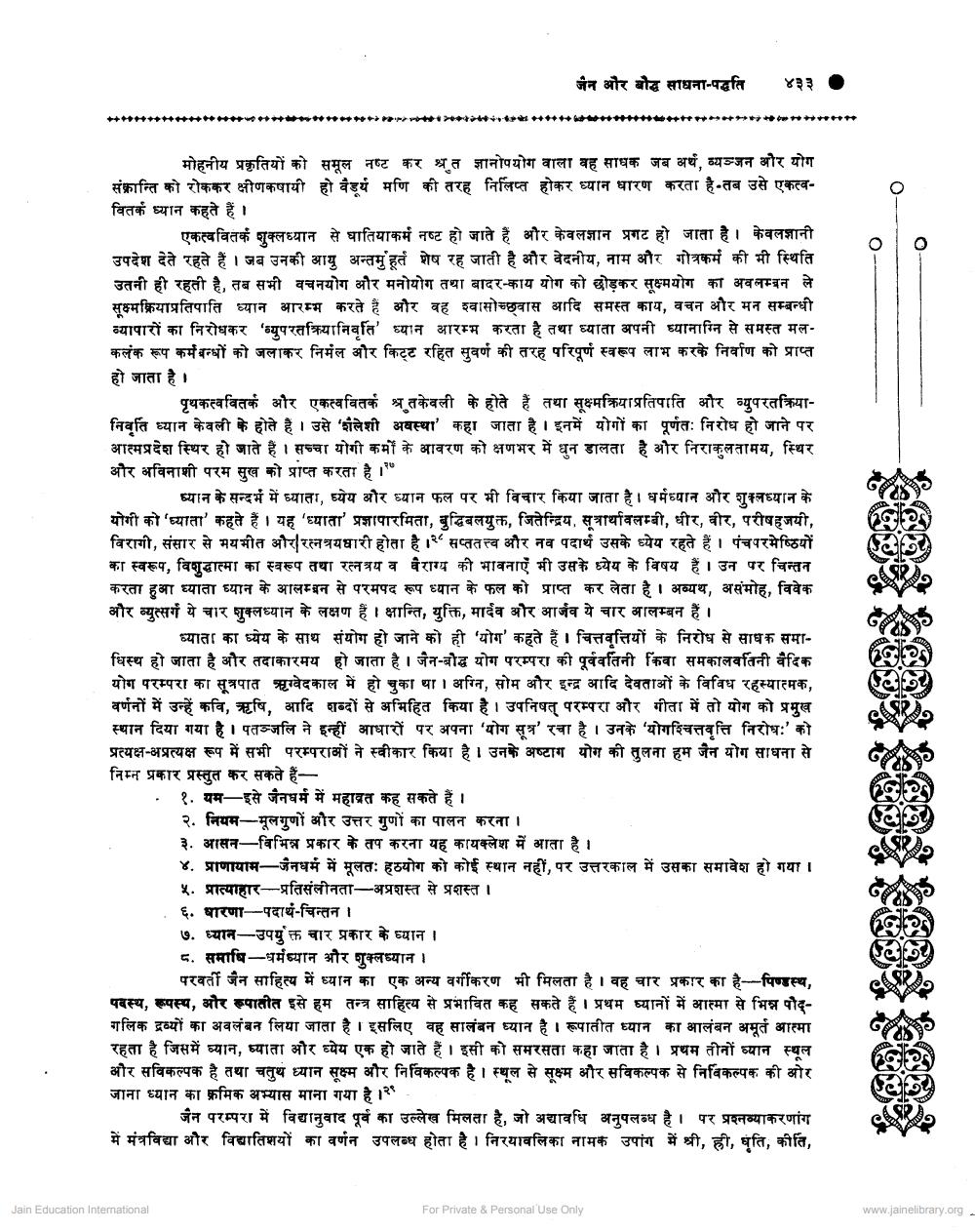________________
जैन और बौद्ध साधना-पद्धति
४३३ .
मोहनीय प्रकृतियों को समूल नष्ट कर श्रत ज्ञानोपयोग वाला वह साधक जब अर्थ, व्यञ्जन और योग संक्रान्ति को रोककर क्षीणकषायी हो वैडूर्य मणि की तरह निर्लिप्त होकर ध्यान धारण करता है तब उसे एकत्ववितर्क ध्यान कहते हैं।
एकत्ववितर्क शुक्लध्यान से घातियाकर्म नष्ट हो जाते हैं और केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। केवलज्ञानी उपदेश देते रहते हैं । जब उनकी आयु अन्तमुहूर्त शेष रह जाती है और वेदनीय, नाम और गोत्रकर्म की भी स्थिति उतनी ही रहती है, तब सभी वचनयोग और मनोयोग तथा बादर-काय योग को छोड़कर सूक्ष्मयोग का अवलम्बन ले सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान आरम्भ करते हैं और वह श्वासोच्छ्वास आदि समस्त काय, वचन और मन सम्बन्धी व्यापारों का निरोधकर 'न्यूपरतक्रियानिति' ध्यान आरम्भ करता है तथा ध्याता अपनी ध्यानाग्नि से समस्त मलकलंक रूप कर्मबन्धों को जलाकर निर्मल और किट्ट रहित सुवर्ण की तरह परिपूर्ण स्वरूप लाभ करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।
पृथकत्ववितर्क और एकत्ववितर्क श्रुतकेवली के होते हैं तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृति ध्यान केवली के होते हैं । उसे 'शैलेशी अवस्था' कहा जाता है । इनमें योगों का पूर्णतः निरोध हो जाने पर आत्मप्रदेश स्थिर हो जाते हैं । सच्चा योगी कर्मों के आवरण को क्षणभर में धुन डालता है और निराकुलतामय, स्थिर और अविनाशी परम सुख को प्राप्त करता है ।
ध्यान के सन्दर्भ में ध्याता, ध्येय और ध्यान फल पर भी विचार किया जाता है। धर्मध्यान और शुक्लध्यान के योगी को 'ध्याता' कहते हैं । यह 'ध्याता' प्रज्ञापारमिता, बुद्धिबलयुक्त, जितेन्द्रिय, सूत्रार्थावलम्बी, धीर, वीर, परीषहजयी, विरागी, संसार से भयभीत और रत्नत्रयधारी होता है। सप्ततत्त्व और नव पदार्थ उसके ध्येय रहते हैं। पंचपरमेष्ठियों का स्वरूप, विशुद्धात्मा का स्वरूप तथा रत्नत्रय व वैराग्य की भावनाएं भी उसके ध्येय के विषय हैं । उन पर चिन्तन करता हुआ ध्याता ध्यान के आलम्बन से परमपद रूप ध्यान के फल को प्राप्त कर लेता है । अव्यथ, असंमोह, विवेक और व्युत्सर्ग ये चार शुक्लध्यान के लक्षण हैं । क्षान्ति, युक्ति, मार्दव और आर्जव ये चार आलम्बन हैं।
___ध्याता का ध्येय के साथ संयोग हो जाने को ही 'योग' कहते हैं । चित्तवृत्तियों के निरोध से साधक समाधिस्थ हो जाता है और तदाकारमय हो जाता है । जैन-बौद्ध योग परम्परा की पूर्ववतिनी किंवा समकालवतिनी वैदिक योग परम्परा का सूत्रपात ऋग्वेदकाल में हो चुका था। अग्नि, सोम और इन्द्र आदि देवताओं के विविध रहस्यात्मक, वर्णनों में उन्हें कवि, ऋषि, आदि शब्दों से अभिहित किया है । उपनिषत् परम्परा और गीता में तो योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। पतञ्जलि ने इन्हीं आधारों पर अपना 'योग सूत्र' रचा है । उनके 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में सभी परम्पराओं ने स्वीकार किया है। उनके अष्टाग योग की तुलना हम जैन योग साधना से निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं. १. यम-इसे जैनधर्म में महाव्रत कह सकते हैं।
२. नियम-मूलगुणों और उत्तर गुणों का पालन करना । ३. आसन-विभिन्न प्रकार के तप करना यह कायक्लेश में आता है। ४. प्राणायाम-जैनधर्म में मूलतः हठयोग को कोई स्थान नहीं, पर उत्तरकाल में उसका समावेश हो गया । ५. प्रात्याहार-प्रतिसंलीनता-अप्रशस्त से प्रशस्त । ६. धारणा-पदार्थ-चिन्तन । ७. ध्यान-उपर्युक्त चार प्रकार के ध्यान । ८. समाधि-धर्मध्यान और शुक्लध्यान ।
परवर्ती जैन साहित्य में ध्यान का एक अन्य वर्गीकरण भी मिलता है । वह चार प्रकार का है-पिण्डस्थ, पवस्थ, रूपस्य, और रूपातीत इसे हम तन्त्र साहित्य से प्रभावित कह सकते हैं । प्रथम ध्यानों में आत्मा से भिन्न पौद्गलिक द्रव्यों का अवलंबन लिया जाता है । इसलिए वह सालंबन ध्यान है । रूपातीत ध्यान का आलंबन अमूर्त आत्मा रहता है जिसमें ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं । इसी को समरसता कहा जाता है। प्रथम तीनों ध्यान स्थूल और सविकल्पक है तथा चतुथ ध्यान सूक्ष्म और निर्विकल्पक है। स्थल से सूक्ष्म और सविकल्पक से निर्विकल्पक की ओर जाना ध्यान का क्रमिक अभ्यास माना गया है। -
जैन परम्परा में विद्यानुवाद पूर्व का उल्लेख मिलता है, जो अद्यावधि अनुपलब्ध है। पर प्रश्नव्याकरणांग में मंत्रविद्या और विद्यातिशयों का वर्णन उपलब्ध होता है । निरयावलिका नामक उपांग में श्री, ह्री, धृति, कीति,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org -