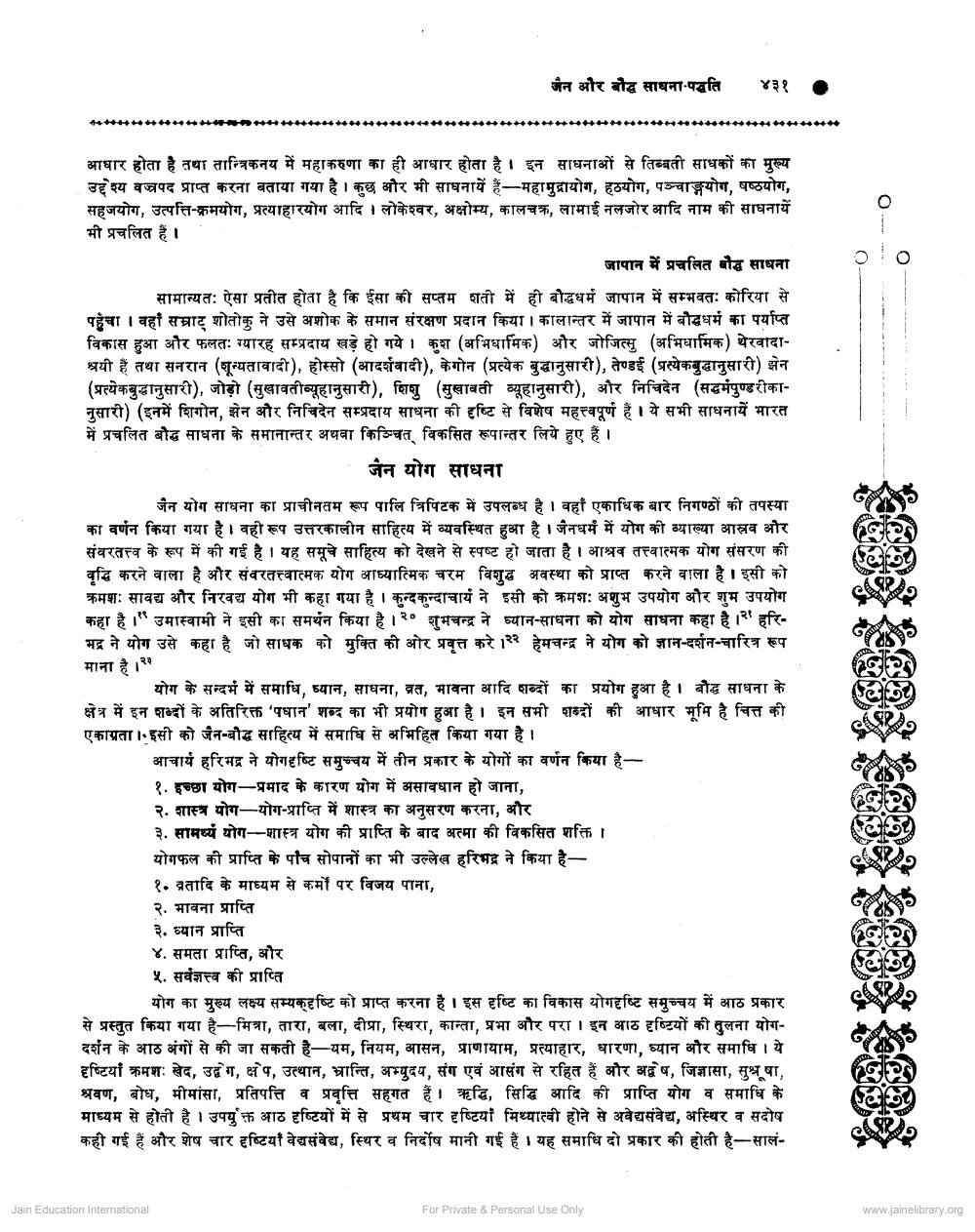________________
जैन और बौद्ध साधना पद्धति
४३१
.
आधार होता है तथा तान्त्रिकनय में महाकरुणा का ही आधार होता है। इन साधनाओं से तिब्बती साधकों का मुख्य उद्देश्य वज्रपद प्राप्त करना बताया गया है । कुछ और भी साधनायें हैं-महामुद्रायोग, हठयोग, पञ्चाङ्गयोग, षष्ठयोग, सहजयोग, उत्पत्ति-क्रमयोग, प्रत्याहारयोग आदि । लोकेश्वर, अक्षोम्य, कालचक्र, लामाई नलजोर आदि नाम की साधनायें भी प्रचलित हैं।
जापान में प्रचलित बौद्ध साधना सामान्यत: ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की सप्तम शती में ही बौद्धधर्म जापान में सम्भवतः कोरिया से पहुंचा । वहाँ सम्राट शोतोकु ने उसे अशोक के समान संरक्षण प्रदान किया। कालान्तर में जापान में बौद्धधर्म का पर्याप्त विकास हुआ और फलतः ग्यारह सम्प्रदाय खड़े हो गये। कुश (अभिधार्मिक) और जोजित्सु (अभिधार्मिक) थेरवादाश्रयी हैं तथा सनरान (शून्यतावादी), होस्सो (आदर्शवादी), केगोन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), तेण्डई (प्रत्येकबुद्धानुसारी) झेन (प्रत्येकबुद्धानुसारी), जोड़ो (सुखावतीव्यूहानुसारी), शिशु (सुखावती व्यूहानुसारी), और निचिदेन (सद्धर्मपुण्डरीकानुसारी) (इनमें शिगोन, झेन और निचिदेन सम्प्रदाय साधना की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। ये सभी साधनायें भारत में प्रचलित बौद्ध साधना के समानान्तर अथवा किञ्चित् विकसित रूपान्तर लिये हुए हैं।
- जैन योग साधना
जैन योग साधना का प्राचीनतम रूप पालि त्रिपिटक में उपलब्ध है। वहाँ एकाधिक बार निगण्ठों की तपस्या का वर्णन किया गया है। वही रूप उत्तरकालीन साहित्य में व्यवस्थित हुआ है । जैनधर्म में योग की व्याख्या आस्रव और संवरतत्त्व के रूप में की गई है। यह समूचे साहित्य को देखने से स्पष्ट हो जाता है । आश्रव तत्त्वात्मक योग संसरण की वृद्धि करने वाला है और संवरतत्त्वात्मक योग आध्यात्मिक चरम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला है। इसी को क्रमशः सावद्य और निरवद्य योग भी कहा गया है । कुन्दकुन्दाचार्य ने इसी को क्रमशः अशुभ उपयोग और शुम उपयोग कहा है।" उमास्वामी ने इसी का समर्थन किया है । २० शुभचन्द्र ने ध्यान-साधना को योग साधना कहा है । हरिभद्र ने योग उसे कहा है जो साधक को मुक्ति की ओर प्रवृत्त करे।२२ हेमचन्द्र ने योग को ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप माना है । २३
योग के सन्दर्भ में समाधि, ध्यान, साधना, व्रत, भावना आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। बौद्ध साधना के क्षेत्र में इन शब्दों के अतिरिक्त 'पधान' शब्द का भी प्रयोग हआ है। इन सभी शब्दों की आधार भूमि है चित्त की एकाग्रता। इसी को जैन-बौद्ध साहित्य में समाधि से अभिहित किया गया है।
आचार्य हरिभद्र ने योगदृष्टि समुच्चय में तीन प्रकार के योगों का वर्णन किया है१. इच्छा योग-प्रमाद के कारण योग में असावधान हो जाना, २. शास्त्र योग-योग-प्राप्ति में शास्त्र का अनुसरण करना, और ३. सामर्थ्य योग-शास्त्र योग की प्राप्ति के बाद अत्मा की विकसित शक्ति । योगफल की प्राप्ति के पांच सोपानों का भी उल्लेख हरिभद्र ने किया है१. व्रतादि के माध्यम से कर्मों पर विजय पाना, २. भावना प्राप्ति ३. ध्यान प्राप्ति ४. समता प्राप्ति, और ५. सर्वज्ञत्त्व की प्राप्ति
योग का मुख्य लक्ष्य सम्यक्दृष्टि को प्राप्त करना है । इस दृष्टि का विकास योगदृष्टि समुच्चय में आठ प्रकार से प्रस्तुत किया गया है-मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा । इन आठ दृष्टियों की तुलना योगदर्शन के आठ अंगों से की जा सकती है-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । ये दृष्टियां क्रमशः खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रान्ति, अभ्युदय, संग एवं आसंग से रहित हैं और अद्वेष, जिज्ञासा, सुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति व प्रवृत्ति सहगत हैं। ऋद्धि, सिद्धि आदि की प्राप्ति योग व समाधि के माध्यम से होती है । उपयुक्त आठ दृष्टियों में से प्रथम चार दृष्टियां मिथ्यात्वी होने से अवेद्यसंवेद्य, अस्थिर व सदोष कही गई हैं और शेष चार दृष्टियाँ वेद्यसंवेद्य, स्थिर व निर्दोष मानी गई हैं। यह समाधि दो प्रकार की होती है-साल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org