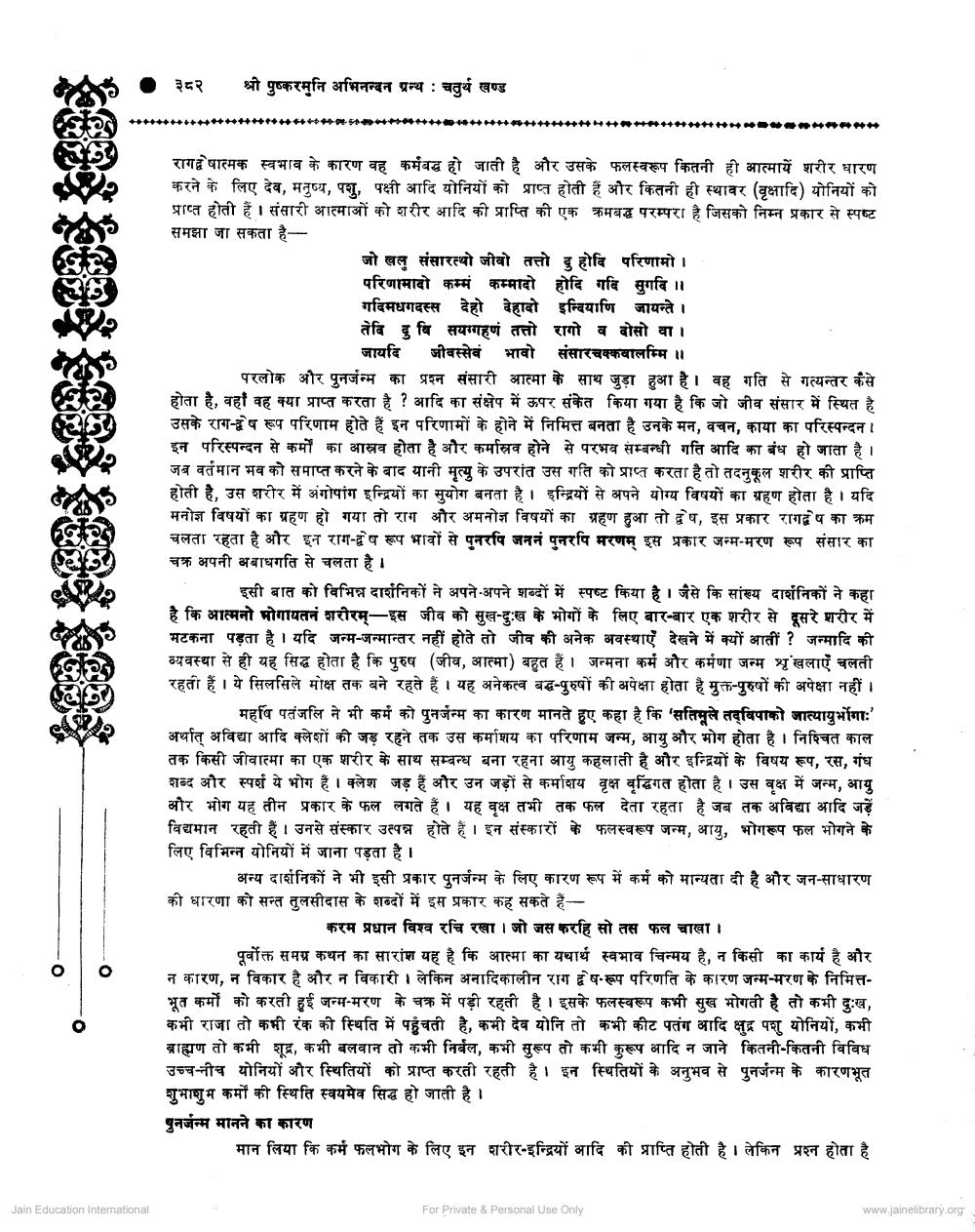________________
Jain Education International
३८२
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
-90-5000044
रागद्वेषात्मक स्वभाव के कारण वह कर्मबद्ध हो जाती है और उसके फलस्वरूप कितनी ही आत्मायें शरीर धारण करने के लिए देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होती हैं और कितनी ही स्थावर (वृक्षादि) योनियों को प्राप्त होती हैं । संसारी आत्माओं को शरीर आदि की प्राप्ति की एक क्रमबद्ध परम्परा है जिसको निम्न प्रकार से स्पष्ट समझा जा सकता है-
जो खलु संसारल्यो जीयो तत्तो दु होदि परिणामो परिणामावो कम्म कम्मादो होदि यदि सुगवि ।। गदिमधगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जायन्ते । तेवि दु वि सयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा । यदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्मि ॥
4040
परलोक और पुनर्जन्म का प्रश्न संसारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है । वह गति से गत्यन्तर कैसे होता है, वहाँ वह क्या प्राप्त करता है ? आदि का संक्षेप में ऊपर संकेत किया गया है कि जो जीव संसार में स्थित है उसके राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं इन परिणामों के होने में निमित्त बनता है उनके मन, वचन, काया का परिस्पन्दन । इन परिस्पन्दन से कर्मों का आस्रव होता है और कर्मास्रव होने से परभव सम्बन्धी गति आदि का बंध हो जाता है । जब वर्तमान भव को समाप्त करने के बाद यानी मृत्यु के उपरांत उस गति को प्राप्त करता है तो तदनुकूल शरीर की प्राप्ति होती है, उस शरीर में अंगोपांग इन्द्रियों का सुयोग बनता है । इन्द्रियों से अपने योग्य विषयों का ग्रहण होता है । यदि मनोज्ञ विषयों का ग्रहण हो गया तो राग और अमनोज्ञ विषयों का ग्रहण हुआ तो द्वेष, इस प्रकार रागद्वेष का क्रम चलता रहता है और इन राग-द्वेष रूप भावों से पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इस प्रकार जन्म-मरण रूप संसार का चक्र अपनी अबाधगति से चलता है ।
इसी बात को विभिन्न दार्शनिकों ने अपने-अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। जैसे कि सांख्य दार्शनिकों ने कहा है कि आत्मनो भोगायतनं शरीरम् — इस जीव को सुख-दुःख के भोगों के लिए बार-बार एक शरीर से दूसरे शरीर में मटकना पड़ता है । यदि जन्म-जन्मान्तर नहीं होते तो जीव की अनेक अवस्थाएं देखने में क्यों आतीं ? जन्मादि की व्यवस्था से ही यह सिद्ध होता है कि पुरुष ( जीव, आत्मा) बहुत हैं । जन्मना कर्म और कर्मणा जन्म श्रृंखलाएँ चलती रहती हैं। ये सिलसिले मोवा तक बने रहते हैं यह अनेकत्व बद्ध-पुरुषों की अपेक्षा होता है मुक्त-पुरुषों की अपेक्षा नहीं।
महाँ पतंजलि ने भी कर्म को पुनर्जन्म का कारण मानते हुए कहा है कि 'सतिमूले तद्वियाको जात्यामा अर्थात् अविद्या आदि क्लेशों की जड़ रहने तक उस कर्माशय का परिणाम जन्म, आयु और भोग होता है । निश्चित काल तक किसी जीवात्मा का एक शरीर के साथ सम्बन्ध बना रहना आयु कहलाती है और इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गंध शब्द और स्पर्श ये भोग हैं । क्लेश जड़ हैं और उन जड़ों से कर्माशय वृक्ष वृद्धिगत होता है । उस वृक्ष में जन्म, आयु और भोग यह तीन प्रकार के फल लगते हैं। यह वृक्ष तभी तक फल देता रहता है जब तक अविद्या आदि जड़ें विद्यमान रहती हैं। उनसे संस्कार उत्पन्न होते हैं । इन संस्कारों के फलस्वरूप जन्म, आयु, भोगरूप फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है ।
अन्य दार्शनिकों ने भी इसी प्रकार पुनर्जन्म के लिए कारण रूप में कर्म को मान्यता दी है और जन-साधारण की धारणा को सन्त तुलसीदास के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं
करम प्रधान विश्व रचि रखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा ।
पूर्वोक्त समग्र कथन का सारांश यह है कि आत्मा का यथार्थ स्वभाव चिन्मय है, न किसी का कार्य है और
न कारण, न विकार है और न विकारी। लेकिन अनादिकालीन राग द्वेष रूप परिणति के कारण जन्म-मरण के निमित्तभूत कर्मों को करती हुई जन्म-मरण के चक्र में पड़ी रहती है। इसके फलस्वरूप कभी सुख भोगती है तो कभी दुःख, कभी राजा तो कभी रंक की स्थिति में पहुँचती है, कभी देव योनि तो कभी कीट पतंग आदि क्षुद्र पशु योनियों, कभी ब्राह्मण तो कभी शूद्र, कभी बलवान तो कभी निर्बल, कभी सुरूप तो कभी कुरूप आदि न जाने कितनी - कितनी विविध उच्च-नीच योनियों और स्थितियों को प्राप्त करती रहती है इन स्थितियों के अनुभव से पुनर्जन्म के कारणभूत शुभाशुभ कर्मों की स्थिति स्वयमेव सिद्ध हो जाती है।
पुनर्जन्म मानने का कारण
मान लिया कि कर्म फलभोग के लिए इन शरीर इन्द्रियों आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रश्न होता है।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org