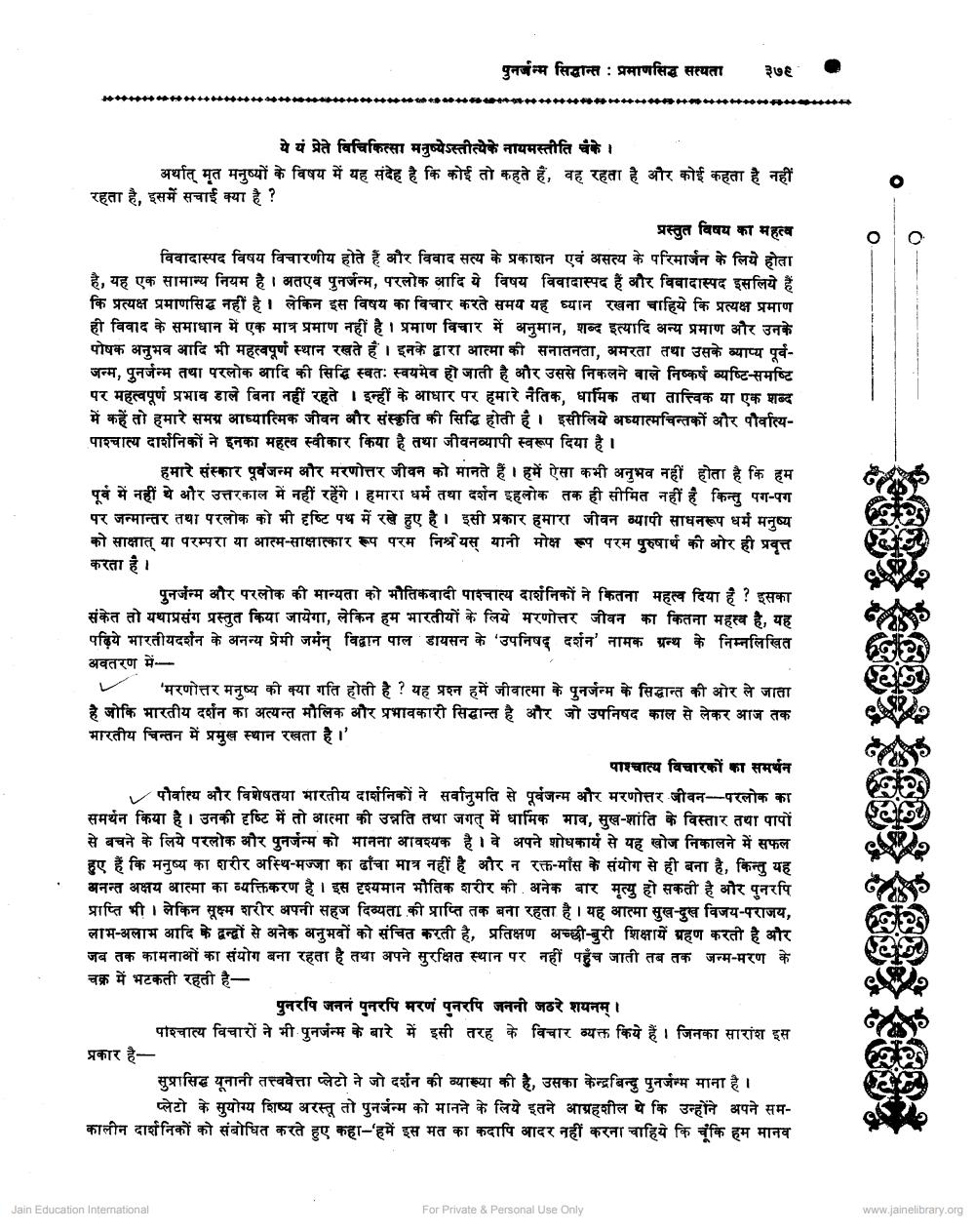________________
पुनर्जन्म सिद्धान्त : प्रमाणसिद्ध सत्यता
३७६
.
ये यं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। अर्थात् मृत मनुष्यों के विषय में यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं, वह रहता है और कोई कहता है नहीं रहता है, इसमें सचाई क्या है ?
प्रस्तुत विषय का महत्व विवादास्पद विषय विचारणीय होते हैं और विवाद सत्य के प्रकाशन एवं असत्य के परिमार्जन के लिये होता है, यह एक सामान्य नियम है । अतएव पुनर्जन्म, परलोक आदि ये विषय विवादास्पद हैं और विवादास्पद इसलिये हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध नहीं है। लेकिन इस विषय का विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही विवाद के समाधान में एक मात्र प्रमाण नहीं है । प्रमाण विचार में अनुमान, शब्द इत्यादि अन्य प्रमाण और उनके पोषक अनुभव आदि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा आत्मा की सनातनता, अमरता तथा उसके व्याप्य पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा परलोक आदि की सिद्धि स्वतः स्वयमेव हो जाती है और उससे निकलने वाले निष्कर्ष व्यष्टि-समष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले बिना नहीं रहते । इन्हीं के आधार पर हमारे नैतिक, धार्मिक तथा तात्त्विक या एक शब्द में कहें तो हमारे समग्र आध्यात्मिक जीवन और संस्कृति की सिद्धि होती है। इसीलिये अध्यात्मचिन्तकों और पौर्वात्यपाश्चात्य दार्शनिकों ने इनका महत्व स्वीकार किया है तथा जीवनव्यापी स्वरूप दिया है।
हमारे संस्कार पूर्वजन्म और मरणोत्तर जीवन को मानते हैं। हमें ऐसा कभी अनुभव नहीं होता है कि हम पूर्व में नहीं थे और उत्तरकाल में नहीं रहेंगे । हमारा धर्म तथा दर्शन इहलोक तक ही सीमित नहीं है किन्तु पग-पग पर जन्मान्तर तथा परलोक को भी दृष्टि पथ में रखे हुए है। इसी प्रकार हमारा जीवन व्यापी साधनरूप धर्म मनुष्य को साक्षात् या परम्परा या आत्म-साक्षात्कार रूप परम निश्रेयस् यानी मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की ओर ही प्रवृत्त करता है।
पुनर्जन्म और परलोक की मान्यता को भौतिकवादी पाश्चात्य दार्शनिकों ने कितना महत्व दिया है ? इसका संकेत तो यथाप्रसंग प्रस्तुत किया जायेगा, लेकिन हम भारतीयों के लिये मरणोत्तर जीवन का कितना महत्व है, यह पढ़िये भारतीयदर्शन के अनन्य प्रेमी जर्मन् विद्वान पाल डायसन के 'उपनिषद् दर्शन' नामक ग्रन्थ के निम्नलिखित अवतरण में
'मरणोत्तर मनुष्य की क्या गति होती है ? यह प्रश्न हमें जीवात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्त की ओर ले जाता है जोकि भारतीय दर्शन का अत्यन्त मौलिक और प्रभावकारी सिद्धान्त है और जो उपनिषद काल से लेकर आज तक भारतीय चिन्तन में प्रमुख स्थान रखता है।'
पाश्चात्य विचारकों का समर्थन V पौर्वात्य और विशेषतया भारतीय दार्शनिकों ने सर्वानुमति से पूर्वजन्म और मरणोत्तर जीवन-परलोक का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि में तो आत्मा की उन्नति तथा जगत् में धार्मिक भाव, सुख-शांति के विस्तार तथा पापों से बचने के लिये परलोक और पुनर्जन्म को मानना आवश्यक है। वे अपने शोधकार्य से यह खोज निकालने में सफल हुए हैं कि मनुष्य का शरीर अस्थि-मज्जा का ढाँचा मात्र नहीं है और न रक्त-माँस के संयोग से ही बना है, किन्तु यह अनन्त अक्षय आत्मा का व्यक्तिकरण है । इस दृश्यमान भौतिक शरीर की अनेक बार मृत्यु हो सकती है और पुनरपि प्राप्ति भी। लेकिन सूक्ष्म शरीर अपनी सहज दिव्यता की प्राप्ति तक बना रहता है । यह आत्मा सुख-दुख विजय-पराजय, लाम-अलाम आदि के द्वन्द्वों से अनेक अनुभवों को संचित करती है, प्रतिक्षण अच्छी-बुरी शिक्षायें ग्रहण करती है और जब तक कामनाओं का संयोग बना रहता है तथा अपने सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँच जाती तब तक जन्म-मरण के चक्र में भटकती रहती है
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् । पाश्चात्य विचारों ने भी पुनर्जन्म के बारे में इसी तरह के विचार व्यक्त किये हैं। जिनका सारांश इस प्रकार है
सुप्रासिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने जो दर्शन की व्याख्या की है, उसका केन्द्रबिन्दु पुनर्जन्म माना है ।
प्लेटो के सुयोग्य शिष्य अरस्तू तो पुनर्जन्म को मानने के लिये इतने आग्रहशील थे कि उन्होंने अपने समकालीन दार्शनिकों को संबोधित करते हुए कहा-'हमें इस मत का कदापि आदर नहीं करना चाहिये कि चूंकि हम मानव
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org