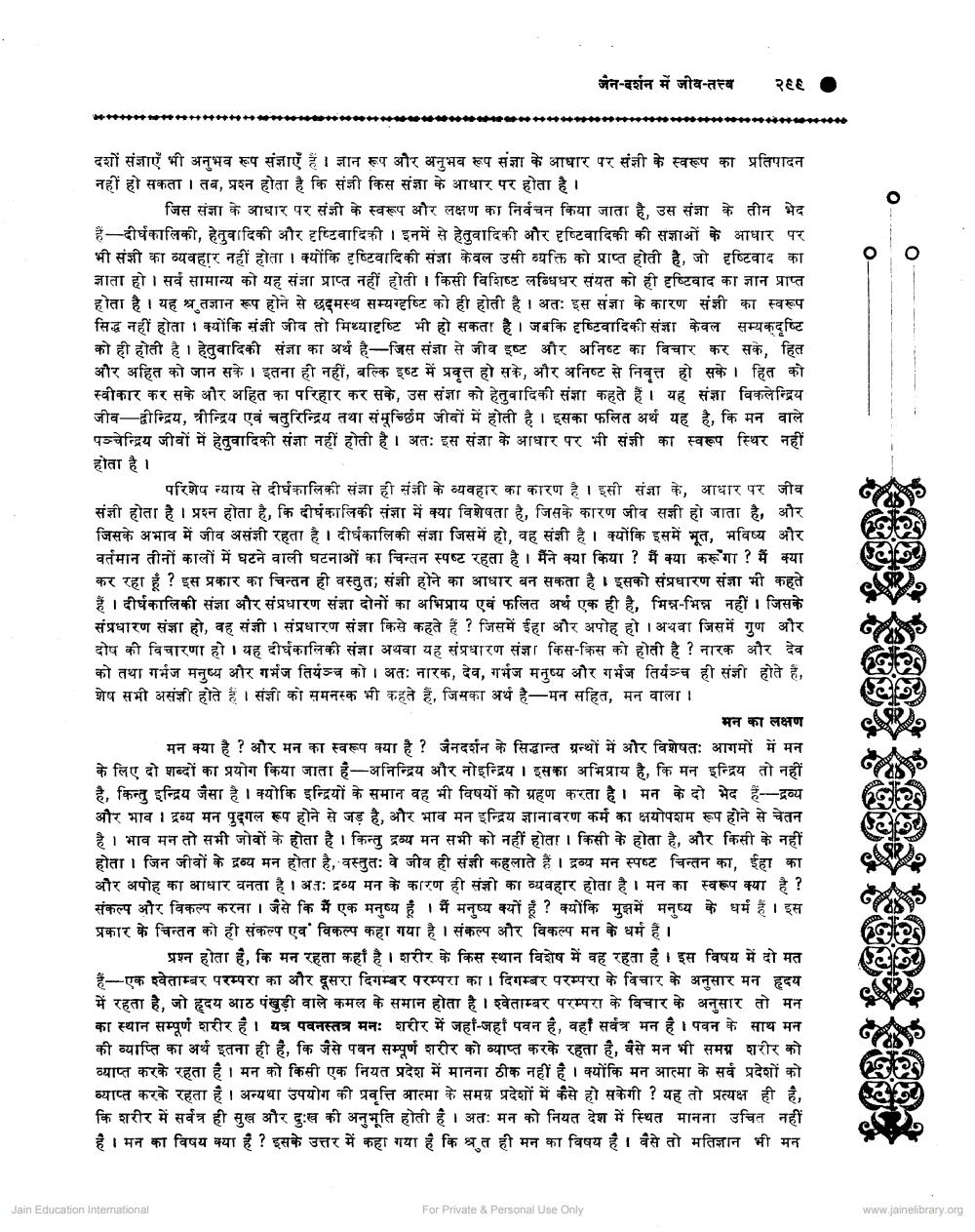________________
जैन-दर्शन में जीव-तत्त्व
२६६
.
००
दशों संज्ञाएँ भी अनुभव रूप संज्ञाएँ हैं। ज्ञान रूप और अनुभव रूप संज्ञा के आधार पर संज्ञी के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता । तब, प्रश्न होता है कि संज्ञी किस संज्ञा के आधार पर होता है।
जिस संज्ञा के आधार पर संज्ञी के स्वरूप और लक्षण का निर्वचन किया जाता है, उस संज्ञा के तीन भेद हैं-दीर्घकालिकी, हेतुवादिकी और दृष्टिवादिकी । इनमें से हेतुवादिकी और दृष्टिवादिकी की सज्ञाओं के आधार पर भी संज्ञी का व्यवहार नहीं होता। क्योंकि दृष्टिवादिकी संज्ञा केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो दृष्टिवाद का ज्ञाता हो । सर्व सामान्य को यह संज्ञा प्राप्त नहीं होती। किसी विशिष्ट लब्धिधर संयत को ही दृष्टिवाद का ज्ञान प्राप्त होता है । यह श्र तज्ञान रूप होने से छद्मस्थ सम्यग्दृष्टि को ही होती है । अतः इस संज्ञा के कारण संज्ञी का स्वरूप सिद्ध नहीं होता । क्योंकि संज्ञी जीव तो मिथ्यादृष्टि भी हो सकता है। जबकि दृष्टिवादिकी संज्ञा केवल सम्यकदृष्टि को ही होती है। हेतुवादिकी संज्ञा का अर्थ है-जिस संज्ञा से जीव इष्ट और अनिष्ट का विचार कर सके, हित और अहित को जान सके । इतना ही नहीं, बल्कि इष्ट में प्रवृत्त हो सके, और अनिष्ट से निवृत्त हो सके। हित को स्वीकार कर सके और अहित का परिहार कर सके, उस संज्ञा को हेतुवादिकी संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा विकलेन्द्रिय जीव-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं चतुरिन्द्रिय तथा संमूर्छिम जीवों में होती है। इसका फलित अर्थ यह है, कि मन वाले पञ्चेन्द्रिय जीवों में हेतुवादिकी संज्ञा नहीं होती है। अतः इस संज्ञा के आधार पर भी संज्ञी का स्वरूप स्थिर नहीं होता है।
परिशेष न्याय से दीर्घकालिकी संज्ञा ही संजी के व्यवहार का कारण है। इसी संज्ञा के, आधार पर जीव संज्ञी होता है। प्रश्न होता है, कि दीर्घकालिकी संज्ञा में क्या विशेषता है, जिसके कारण जीव सज्ञी हो जाता है, और जिसके अभाव में जीव असंज्ञी रहता है । दीर्घकालिकी संज्ञा जिसमें हो, वह संज्ञी है। क्योंकि इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में घटने वाली घटनाओं का चिन्तन स्पष्ट रहता है। मैंने क्या किया ? मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्रकार का चिन्तन ही वस्तुतः संज्ञी होने का आधार बन सकता है। इसको संप्रधारण संज्ञा भी कहते हैं । दीर्घकालिकी संज्ञा और संप्रधारण संज्ञा दोनों का अभिप्राय एवं फलित अर्थ एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं। जिसके संप्रधारण संज्ञा हो, वह संज्ञी । संप्रधारण संज्ञा किसे कहते हैं ? जिसमें ईहा और अपोह हो । अथवा जिसमें गुण और दोष की विचारणा हो । यह दीर्घकालिकी संज्ञा अथवा यह संप्रधारण संज्ञा किस-किस को होती है ? नारक और देव को तथा गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यञ्च को । अतः नारक, देव, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यञ्च ही संज्ञी होते हैं, शेष सभी असंज्ञी होते हैं । संज्ञी को समनस्क भी कहते हैं, जिसका अर्थ है-मन सहित, मन वाला।
मन का लक्षण मन क्या है ? और मन का स्वरूप क्या है ? जैनदर्शन के सिद्धान्त ग्रन्थों में और विशेषतः आगमों में मन के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है-अनिन्द्रिय और नोइन्द्रिय । इसका अभिप्राय है, कि मन इन्द्रिय तो नहीं है, किन्तु इन्द्रिय जैसा है । क्योकि इन्द्रियों के समान वह भी विषयों को ग्रहण करता है। मन के दो भेद हैं--द्रव्य और भाव । द्रव्य मन पुद्गल रूप होने से जड़ है, और भाव मन इन्द्रिय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम रूप होने से चेतन है । भाव मन तो सभी जोवों के होता है । किन्तु द्रव्य मन सभी को नहीं होता । किसी के होता है, और किसी के नहीं होता। जिन जीवों के द्रव्य मन होता है, वस्तुतः वे जीव ही संज्ञी कहलाते हैं । द्रव्य मन स्पष्ट चिन्तन का, ईहा का और अपोह का आधार बनता है । अत: द्रव्य मन के कारण ही संज्ञो का व्यवहार होता है। मन का स्वरूप क्या है ? संकल्प और विकल्प करना । जैसे कि मैं एक मनुष्य हूँ । मैं मनुष्य क्यों हूँ ? क्योंकि मुझमें मनुष्य के धर्म हैं । इस प्रकार के चिन्तन को ही संकल्प एवं विकल्प कहा गया है । संकल्प और विकल्प मन के धर्म हैं।
प्रश्न होता है, कि मन रहता कहाँ है । शरीर के किस स्थान विशेष में वह रहता है । इस विषय में दो मत हैं-एक श्वेताम्बर परम्परा का और दूसरा दिगम्बर परम्परा का। दिगम्बर परम्परा के विचार के अनुसार मन हृदय में रहता है, जो हृदय आठ पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है । श्वेताम्बर परम्परा के विचार के अनुसार तो मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर है। यत्र पवनस्तत्र मनः शरीर में जहाँ-जहाँ पवन है, वहाँ सर्वत्र मन है । पवन के साथ मन की व्याप्ति का अर्थ इतना ही है, कि जैसे पवन सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है, वैसे मन भी समग्न शरीर को व्याप्त करके रहता है। मन को किसी एक नियत प्रदेश में मानना ठीक नहीं है। क्योंकि मन आत्मा के सर्व प्रदेशों को व्याप्त करके रहता है। अन्यथा उपयोग की प्रवृत्ति आत्मा के समग्र प्रदेशों में कैसे हो सकेगी? यह तो प्रत्यक्ष ही है, कि शरीर में सर्वत्र ही सुख और दुःख की अनुभूति होती है। अतः मन को नियत देश में स्थित मानना उचित नहीं है। मन का विषय क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्रुत ही मन का विषय है। वैसे तो मतिज्ञान भी मन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org