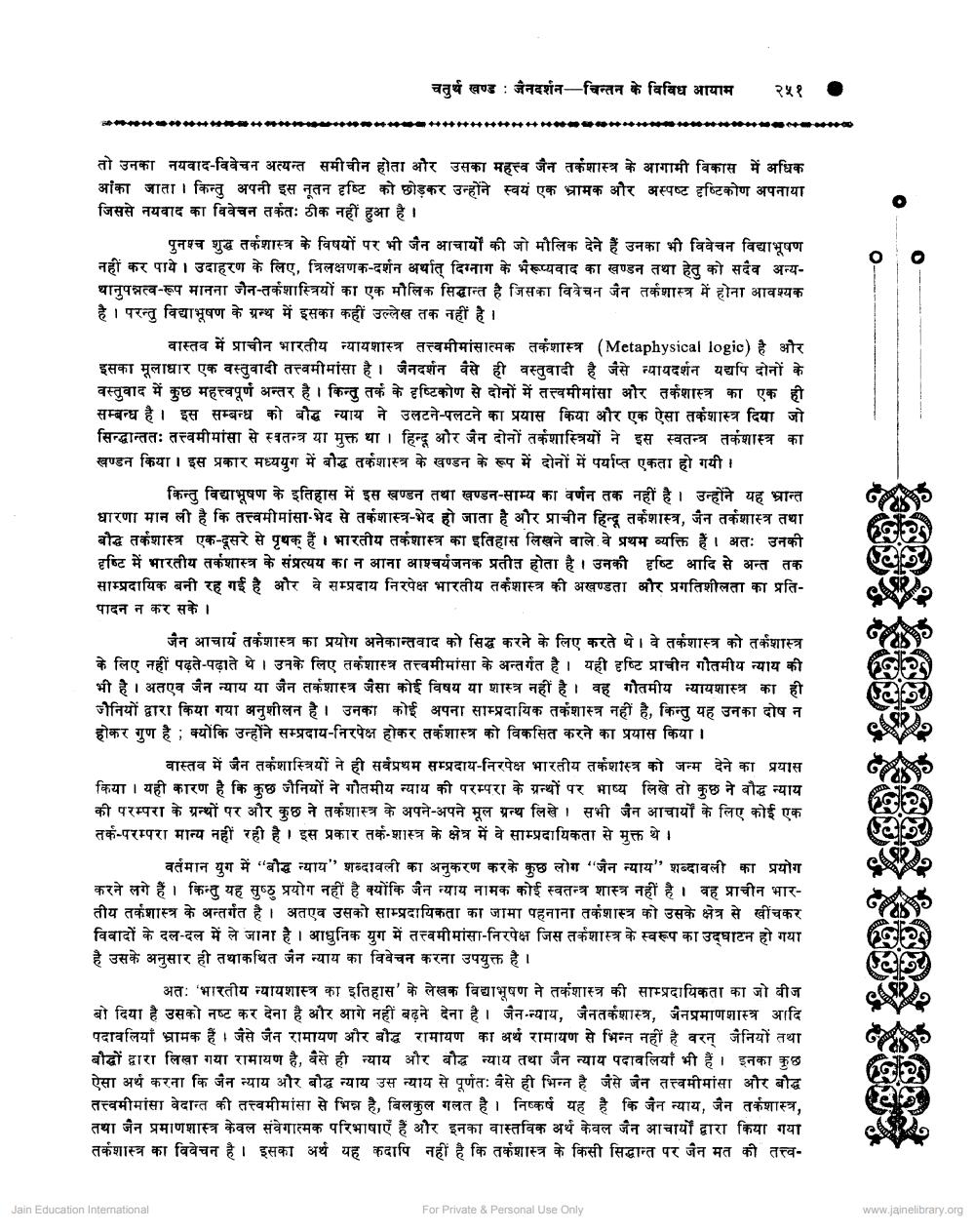________________
चतुर्थ खण्ड : जैनदर्शन–चिन्तन के विविध आयाम
२५१ .
तो उनका नयवाद-विवेचन अत्यन्त समीचीन होता और उसका महत्त्व जैन तर्कशास्त्र के आगामी विकास में अधिक आंका जाता। किन्तु अपनी इस नूतन दृष्टि को छोड़कर उन्होंने स्वयं एक भ्रामक और अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया जिससे नयवाद का विवेचन तर्कतः ठीक नहीं हुआ है।
पुनश्च शुद्ध तर्कशास्त्र के विषयों पर भी जैन आचार्यों की जो मौलिक देने हैं उनका भी विवेचन विद्याभूषण नहीं कर पाये। उदाहरण के लिए, त्रिलक्षणक-दर्शन अर्थात् दिग्नाग के भैरूप्यवाद का खण्डन तथा हेतु को सदैव अन्यथानुपन्नत्व-रूप मानना जैन-तर्कशास्त्रियों का एक मौलिक सिद्धान्त है जिसका विवेचन जैन तर्कशास्त्र में होना आवश्यक है। परन्तु विद्याभूषण के ग्रन्थ में इसका कहीं उल्लेख तक नहीं है।
वास्तव में प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र तत्त्वमीमांसात्मक तर्कशास्त्र (Metaphysical logic) है और इसका मूलाधार एक वस्तुवादी तत्त्वमीमांसा है। जैनदर्शन वैसे ही वस्तुवादी है जैसे न्यायदर्शन यद्यपि दोनों के वस्तुवाद में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर है। किन्तु तर्क के दृष्टिकोण से दोनों में तत्त्वमीमांसा और तर्कशास्त्र का एक ही सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को बौद्ध न्याय ने उलटने-पलटने का प्रयास किया और एक ऐसा तर्कशास्त्र दिया जो सिन्धान्ततः तत्त्वमीमांसा से स्वतन्त्र या मुक्त था। हिन्दू और जैन दोनों तर्कशास्त्रियों ने इस स्वतन्त्र तर्कशास्त्र का खण्डन किया। इस प्रकार मध्ययुग में बौद्ध तर्कशास्त्र के खण्डन के रूप में दोनों में पर्याप्त एकता हो गयी।
किन्तु विद्याभूषण के इतिहास में इस खण्डन तथा खण्डन-साम्य का वर्णन तक नहीं है। उन्होंने यह भ्रान्त धारणा मान ली है कि तत्त्वमीमांसा-भेद से तर्कशास्त्र-भेद हो जाता है और प्राचीन हिन्दू तर्कशास्त्र, जैन तर्कशास्त्र तथा बौद्ध तर्कशास्त्र एक-दूसरे से पृथक हैं। भारतीय तर्कशास्त्र का इतिहास लिखने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं। अतः उनकी दृष्टि में भारतीय तर्कशास्त्र के संप्रत्यय का न आना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। उनकी दृष्टि आदि से अन्त तक साम्प्रदायिक बनी रह गई है और वे सम्प्रदाय निरपेक्ष भारतीय तर्कशास्त्र की अखण्डता और प्रगतिशीलता का प्रतिपादन न कर सके।
जैन आचार्य तर्कशास्त्र का प्रयोग अनेकान्तवाद को सिद्ध करने के लिए करते थे। वे तर्कशास्त्र को तर्कशास्त्र के लिए नहीं पढ़ते-पढ़ाते थे। उनके लिए तर्कशास्त्र तत्त्वमीमांसा के अन्तर्गत है। यही दृष्टि प्राचीन गौतमीय न्याय की भी है । अतएव जैन न्याय या जैन तर्कशास्त्र जैसा कोई विषय या शास्त्र नहीं है। वह गौतमीय न्यायशास्त्र का ही जैनियों द्वारा किया गया अनुशीलन है। उनका कोई अपना साम्प्रदायिक तर्कशास्त्र नहीं है, किन्तु यह उनका दोष न होकर गुण है ; क्योंकि उन्होंने सम्प्रदाय-निरपेक्ष होकर तर्कशास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया।
वास्तव में जैन तर्कशास्त्रियों ने ही सर्वप्रथम सम्प्रदाय-निरपेक्ष भारतीय तर्कशास्त्र को जन्म देने का प्रयास किया। यही कारण है कि कुछ जैनियों ने गौतमीय न्याय की परम्परा के ग्रन्थों पर भाष्य लिखे तो कुछ ने बौद्ध न्याय की परम्परा के ग्रन्थों पर और कुछ ने तर्कशास्त्र के अपने-अपने मूल ग्रन्थ लिखे। सभी जैन आचार्यों के लिए कोई एक तर्क-परम्परा मान्य नहीं रही है। इस प्रकार तर्क-शास्त्र के क्षेत्र में वे साम्प्रदायिकता से मुक्त थे।
वर्तमान युग में "बौद्ध न्याय' शब्दावली का अनुकरण करके कुछ लोग “जैन न्याय" शब्दावली का प्रयोग करने लगे हैं। किन्तु यह सुष्ठु प्रयोग नहीं है क्योंकि जैन न्याय नामक कोई स्वतन्त्र शास्त्र नहीं है। वह प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र के अन्तर्गत है। अतएव उसको साम्प्रदायिकता का जामा पहनाना तर्कशास्त्र को उसके क्षेत्र से खींचकर विवादों के दल-दल में ले जाना है । आधुनिक युग में तत्त्वमीमांसा-निरपेक्ष जिस तर्कशास्त्र के स्वरूप का उद्घाटन हो गया है उसके अनुसार ही तथाकथित जैन न्याय का विवेचन करना उपयुक्त है।
अत: 'भारतीय न्यायशास्त्र का इतिहास' के लेखक विद्याभूषण ने तर्कशास्त्र की साम्प्रदायिकता का जो बीज बो दिया है उसको नष्ट कर देना है और आगे नहीं बढ़ने देना है। जैन-न्याय, जैनतर्कशास्त्र, जैनप्रमाणशास्त्र आदि पदावलियाँ भ्रामक हैं। जैसे जैन रामायण और बौद्ध रामायण का अर्थ रामायण से भिन्न नहीं है वरन् जैनियों तथा बौद्धों द्वारा लिखा गया रामायण है, वैसे ही न्याय और बौद्ध न्याय तथा जैन न्याय पदावलियाँ भी हैं। इनका कुछ ऐसा अर्थ करना कि जैन न्याय और बौद्ध न्याय उस न्याय से पूर्णतः वैसे ही भिन्न है जैसे जैन तत्त्वमीमांसा और बौद्ध तत्त्वमीमांसा वेदान्त की तत्त्वमीमांसा से भिन्न है, बिलकुल गलत है। निष्कर्ष यह है कि जैन न्याय, जैन तर्कशास्त्र, तथा जैन प्रमाणशास्त्र केवल संवेगात्मक परिभाषाएँ हैं और इनका वास्तविक अर्थ केवल जैन आचार्यों द्वारा किया गया तर्कशास्त्र का विवेचन है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तर्कशास्त्र के किसी सिद्धान्त पर जैन मत की तत्त्व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org