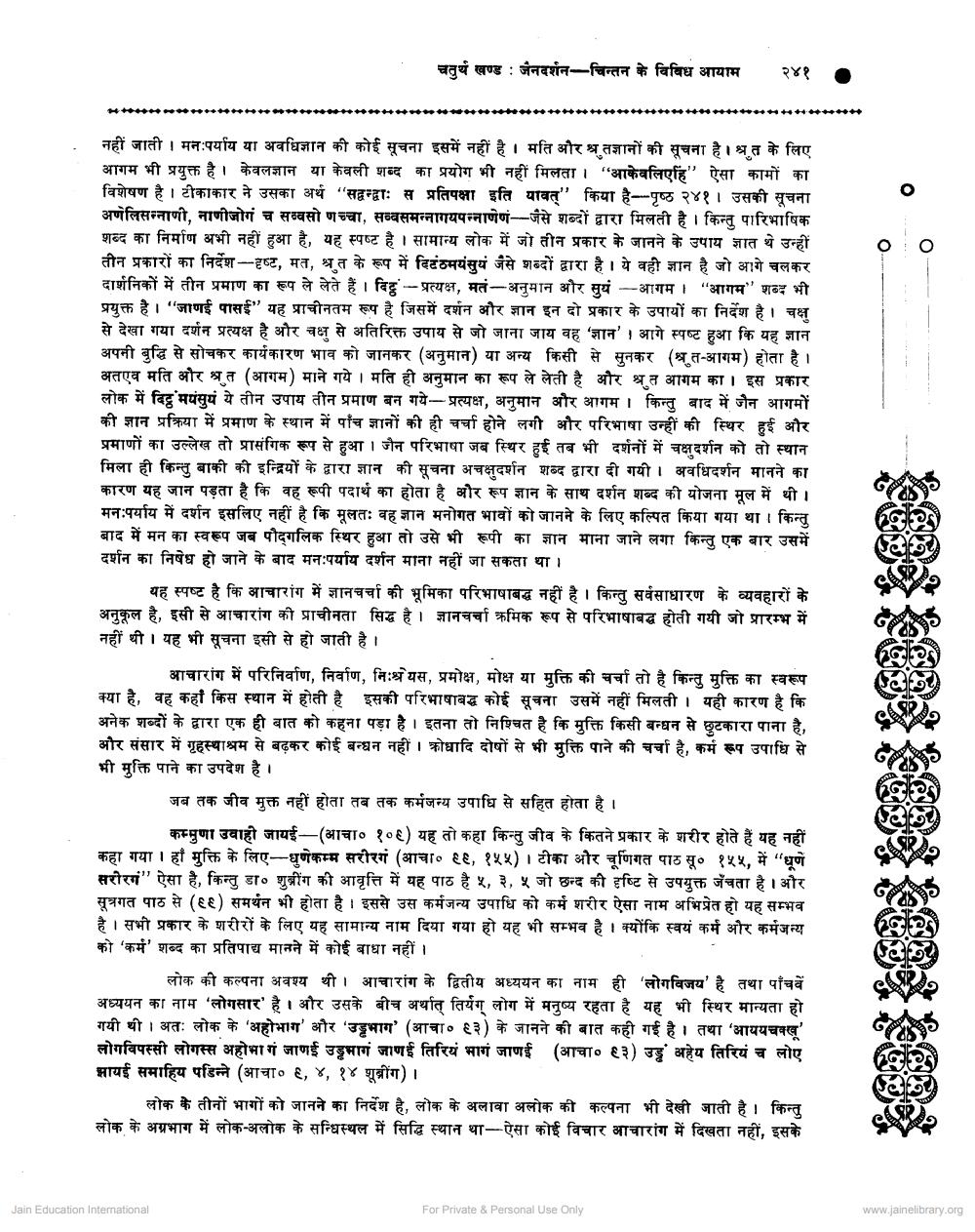________________
चतुर्थ खण्ड : जैनदर्शन - चिन्तन के विविध आयाम २४१
नहीं जाती । मनःपर्याय या अवधिज्ञान की कोई सूचना इसमें नहीं है । मति और श्रुतज्ञानों की सूचना है। श्रुत के लिए आगम भी प्रयुक्त है । केवलज्ञान या केवली शब्द का प्रयोग भी नहीं मिलता। "आकेवलिएहि" ऐसा कामों का विशेषण है। टीकाकार ने उसका अर्थ "सद्वन्द्वाः स प्रतिपक्षा इति यावत्" किया है-पृष्ठ २४१ । उसकी सूचना अणेलिसन्नाणी, नाणीजोगं च सव्वसो णच्चा, सव्वसमन्नागयपन्नाणेणं - जैसे शब्दों द्वारा मिलती है । किन्तु पारिभाषिक शब्द का निर्माण अभी नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है । सामान्य लोक में जो तीन प्रकार के जानने के उपाय ज्ञात थे उन्हीं तीन प्रकारों का निर्देश दृष्ट, मत, श्रुत के रूप में विटंठमयंसुयं जैसे शब्दों द्वारा है। ये वही ज्ञान है जो आगे चलकर दार्शनिकों में तीन प्रमाण का रूप ले लेते हैं। दिट्ठ - प्रत्यक्ष मतं - अनुमान और सुयं -आगम । " आगम" शब्द भी प्रयुक्त है। " जाणई पासई" यह प्राचीनतम रूप है जिसमें दर्शन और ज्ञान इन दो प्रकार के उपायों का निर्देश है। चक्षु से देखा गया दर्शन प्रत्यक्ष है और चक्षु से अतिरिक्त उपाय से जो जाना जाय वह 'ज्ञान' । आगे स्पष्ट हुआ कि यह ज्ञान अपनी बुद्धि से सोचकर कार्यकारण भाव को जानकर (अनुमान) या अन्य किसी से सुनकर (आगम होता है। अतएव मति और श्रुत ( आगम ) माने गये। मति ही अनुमान का रूप ले लेती है और श्रुत आगम का । इस प्रकार लोक में बिट्ठ मयंसुयं ये तीन उपाय तीन प्रमाण बन गये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम । किन्तु बाद में जैन आगमों की ज्ञान प्रक्रिया में प्रमाण के स्थान में पाँच ज्ञानों की ही चर्चा होने लगी और परिभाषा उन्हीं की स्थिर हुई और प्रमाणों का उल्लेख तो प्रासंगिक रूप से हुआ। जैन परिभाषा जब स्थिर हुई तब भी दर्शनों में चक्षुदर्शन को तो स्थान मिला ही किन्तु बाकी की इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान की सूचना अचक्षुदर्शन शब्द द्वारा दी गयी । अवधिदर्शन मानने का कारण यह जान पड़ता है कि वह रूपी पदार्थ का होता है और रूप ज्ञान के साथ दर्शन शब्द की योजना मूल में थी । मनःपर्याय में दर्शन इसलिए नहीं है कि मूलतः वह ज्ञान मनोगत भावों को जानने के लिए कल्पित किया गया था । किन्तु बाद में मन का स्वरूप जब पौद्गलिक स्थिर हुआ तो उसे भी रूपी का ज्ञान माना जाने लगा किन्तु एक बार उसमें दर्शन का निषेध हो जाने के बाद मनःपर्याय दर्शन माना नहीं जा सकता था ।
-
यह स्पष्ट है कि आचारांग में ज्ञानवर्चा की भूमिका परिभाषाबद्ध नहीं है किन्तु सर्वसाधारण के व्यवहारों के अनुकूल है, इसी से आचारांग की प्राचीनता सिद्ध है । ज्ञानचर्चा क्रमिक रूप से परिभाषाबद्ध होती गयी जो प्रारम्भ में नहीं थी । यह भी सूचना इसी से हो जाती है ।
आचारांग में परिनिर्वाण, निर्वाण, निःश्रेयस, प्रमोक्ष, मोक्ष या मुक्ति की चर्चा तो है किन्तु मुक्ति का स्वरूप क्या है, वह कहीं किस स्थान में होती है इसकी परिभाषाबद्ध कोई सूचना उसमें नहीं मिलती। यही कारण है कि अनेक शब्दों के द्वारा एक ही बात को कहना पड़ा है। इतना तो निश्चित है कि मुक्ति किसी बन्धन से छुटकारा पाना है, और संसार में गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई बन्धन नहीं । क्रोधादि दोषों से भी मुक्ति पाने की चर्चा है, कर्म रूप उपाधि से भी मुक्ति पाने का उपदेश है ।
जब तक जीव मुक्त नहीं होता तब तक कर्मजन्य उपाधि से सहित होता है ।
कम्मुणा उवाही जायई - ( आचा० १०६ ) यह तो कहा किन्तु जीव के कितने प्रकार के शरीर होते हैं यह नहीं कहा गया । हाँ मुक्ति के लिए - धुणेकम्म सरीरंगं ( आचा० ६६, १५५) । टीका और चूर्णिगत पाठ सू० १५५, में " धूणे सरोरगं" ऐसा है, किन्तु डा० शुक्रींग की आवृत्ति में यह पाठ है ५, ३, ५ जो छन्द की दृष्टि से उपयुक्त जँचता है । और सूत्रगत पाठ से (६६) समर्थन भी होता है। इससे उस कर्मजन्य उपाधि को कर्म शरीर ऐसा नाम अभिप्रेत हो यह सम्भव है । सभी प्रकार के शरीरों के लिए यह सामान्य नाम दिया गया हो यह भी सम्भव है । क्योंकि स्वयं कर्म और कर्मजन्य को 'कर्म' शब्द का प्रतिपाद्य मानने में कोई बाधा नहीं ।
लोक की कल्पना अवश्य थी। आचारांग के द्वितीय अध्ययन का नाम ही 'लोगविजय' है तथा पाँचवें अध्ययन का नाम 'लोगसार' है । और उसके बीच अर्थात् तिर्यग् लोग में मनुष्य रहता है यह भी स्थिर मान्यता हो गयी थी । अतः लोक के 'अहोभाग' और 'उड्डभाग' (आचा० ९३ ) के जानने की बात कही गई है। तथा 'आययचक्खू' लोगविपस्सी लोगस्स अहोभा गं जाई उट्टभागं जाई तिरियं भागं जाई (आचा० १३) उ अहेब तिरियं च नोए साय समाहिय पडिल्ने (आचा० ६, ४, १४ शूलींग)
Jain Education International
लोक के तीनों भागों को जानने का निर्देश है, लोक के अलावा अलोक की कल्पना भी देखी जाती है। किन्तु लोक के अग्रभाग में लोक- अलोक के सन्धिस्थल में सिद्धि स्थान था - ऐसा कोई विचार आचारांग में दिखता नहीं, इसके
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org