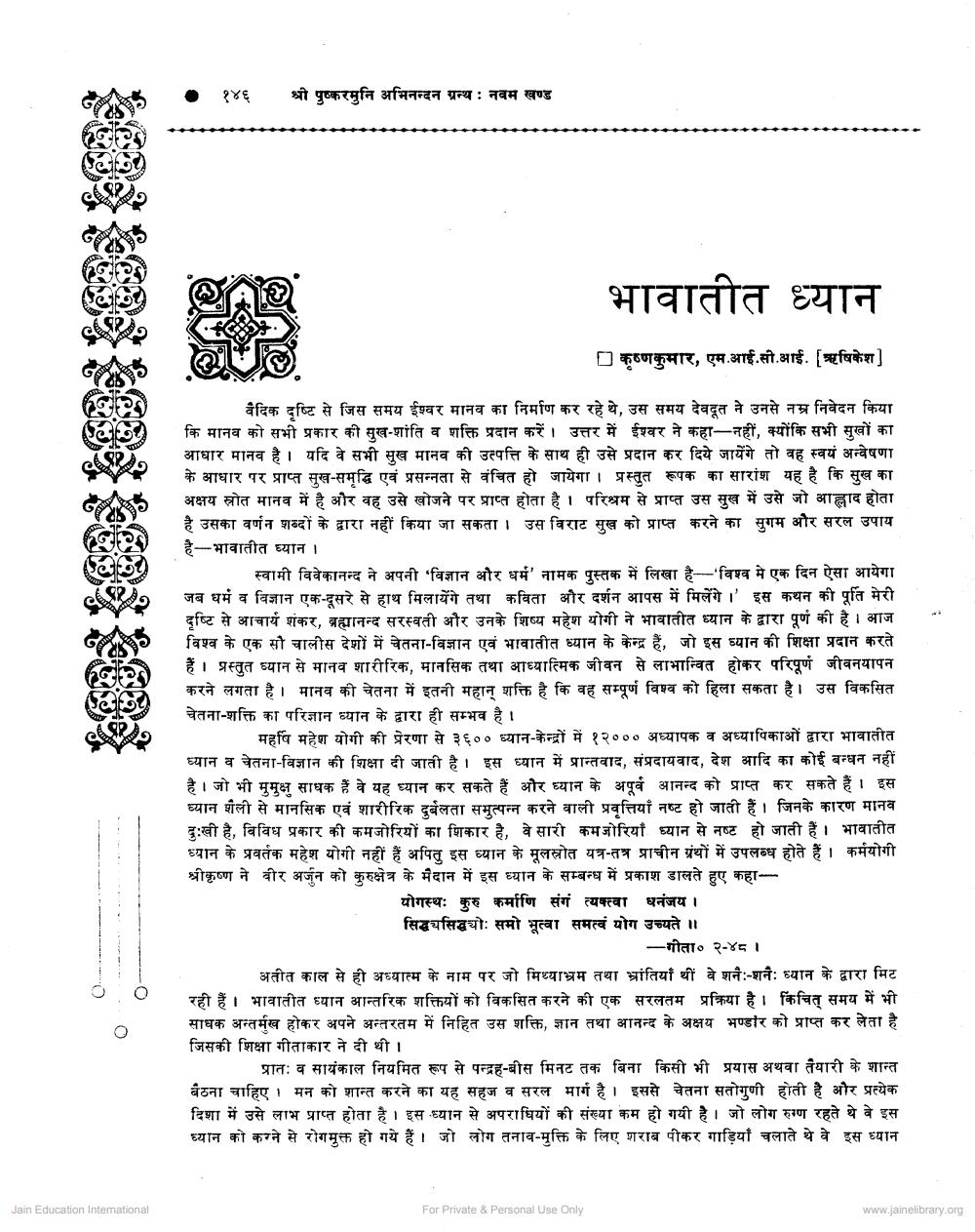________________
Jain Education International
•
१४६
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : नवम खण्ड
भावातीत ध्यान
कृष्णकुमार, एम.आई.सी.आई. [ ऋषिकेश ]
वैदिक दृष्टि से जिस समय ईश्वर मानव का निर्माण कर रहे थे, उस समय देवदूत ने उनसे नम्र निवेदन किया कि मानव को सभी प्रकार की सुख-शांति व शक्ति प्रदान करें। उत्तर में ईश्वर ने कहा- नहीं, क्योंकि सभी सुखों का आधार मानव है । यदि वे सभी सुख मानव की उत्पत्ति के साथ ही उसे प्रदान कर दिये जायेंगे तो वह स्वयं अन्वेषणा के आधार पर प्राप्त सुख-समृद्धि एवं प्रसन्नता से वंचित हो जायेगा । प्रस्तुत रूपक का सारांश यह है कि सुख का अक्षय स्रोत मानव में है और वह उसे खोजने पर प्राप्त होता है । परिश्रम से प्राप्त उस सुख में उसे जो आह्लाद होता है उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उस विराट सुख को प्राप्त करने का सुगम और सरल उपाय है - भावातीत ध्यान ।
स्वामी विवेकानन्द ने अपनी 'विज्ञान और धर्म' नामक पुस्तक में लिखा है- 'विश्व में एक दिन ऐसा आयेगा जब धर्म व विज्ञान एक-दूसरे से हाथ मिलायेंगे तथा कविता और दर्शन आपस में मिलेंगे।' इस कथन की पूर्ति मेरी दृष्टि से आचार्य शंकर, ब्रह्मानन्द सरस्वती और उनके शिष्य महेश योगी ने भावातीत ध्यान के द्वारा पूर्ण की है। आज विश्व के एक सौ चालीस देशों में चेतना-विज्ञान एवं भावातीत ध्यान के केन्द्र हैं, जो इस ध्यान की शिक्षा प्रदान करते हैं । प्रस्तुत ध्यान से मानव शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन से लाभान्वित होकर परिपूर्ण जीवनयापन करने लगता है। मानव की चेतना में इतनी महान् शक्ति है कि वह सम्पूर्ण विश्व को हिला सकता है। उस विकसित चेतना-शक्ति का परिज्ञान ध्यान के द्वारा ही सम्भव है ।
महर्षि महेश योगी की प्रेरणा से ३६०० ध्यान केन्द्रों में १२००० अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा भावातीत ध्यान व चेतना-विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इस ध्यान में प्रान्तवाद, संप्रदायवाद, देश आदि का कोई बन्धन नहीं है। जो भी मुमुक्षु साधक हैं वे यह ध्यान कर सकते हैं और ध्यान के अपूर्व आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं । इस ध्यान शैली से मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता समुत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। जिनके कारण मानव दुःखी है, विविध प्रकार की कमजोरियों का शिकार है, वे सारी कमजोरियाँ ध्यान से नष्ट हो जाती हैं। भावातीत ध्यान के प्रवर्तक महेश योगी नहीं हैं अपितु इस ध्यान के मूलस्रोत यत्र-तत्र प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने वीर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इस ध्यान के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कहा
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग
धनंजय । उच्यते ॥
- गीता० २-४८ ।
अतीत काल से ही अध्यात्म के नाम पर जो मिथ्याभ्रम तथा भ्रांतियाँ थीं वे शनैः-शनैः ध्यान के द्वारा मिट रही हैं । भावातीत ध्यान आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने की एक सरलतम प्रक्रिया है । किचित् समय में भी साधक अन्तर्मुख होकर अपने अन्तरतम में निहित उस शक्ति, ज्ञान तथा आनन्द के अक्षय भण्डोर को प्राप्त कर लेता है। जिसकी शिक्षा गीताकार ने दी थी ।
प्रातः व सायंकाल नियमित रूप से पन्द्रह-बीस मिनट तक बिना किसी भी प्रयास अथवा तैयारी के शान्त बैठना चाहिए। मन को शान्त करने का यह सहज व सरल मार्ग है। इससे चेतना सतोगुणी होती है और प्रत्येक दिशा में उसे लाभ प्राप्त होता है। इस ध्यान से अपराधियों की संख्या कम हो गयी है। जो लोग रुग्ण रहते थे वे इस ध्यान को करने से रोगमुक्त हो गये हैं। जो लोग तनाव मुक्ति के लिए शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते थे वे इस ध्यान
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org