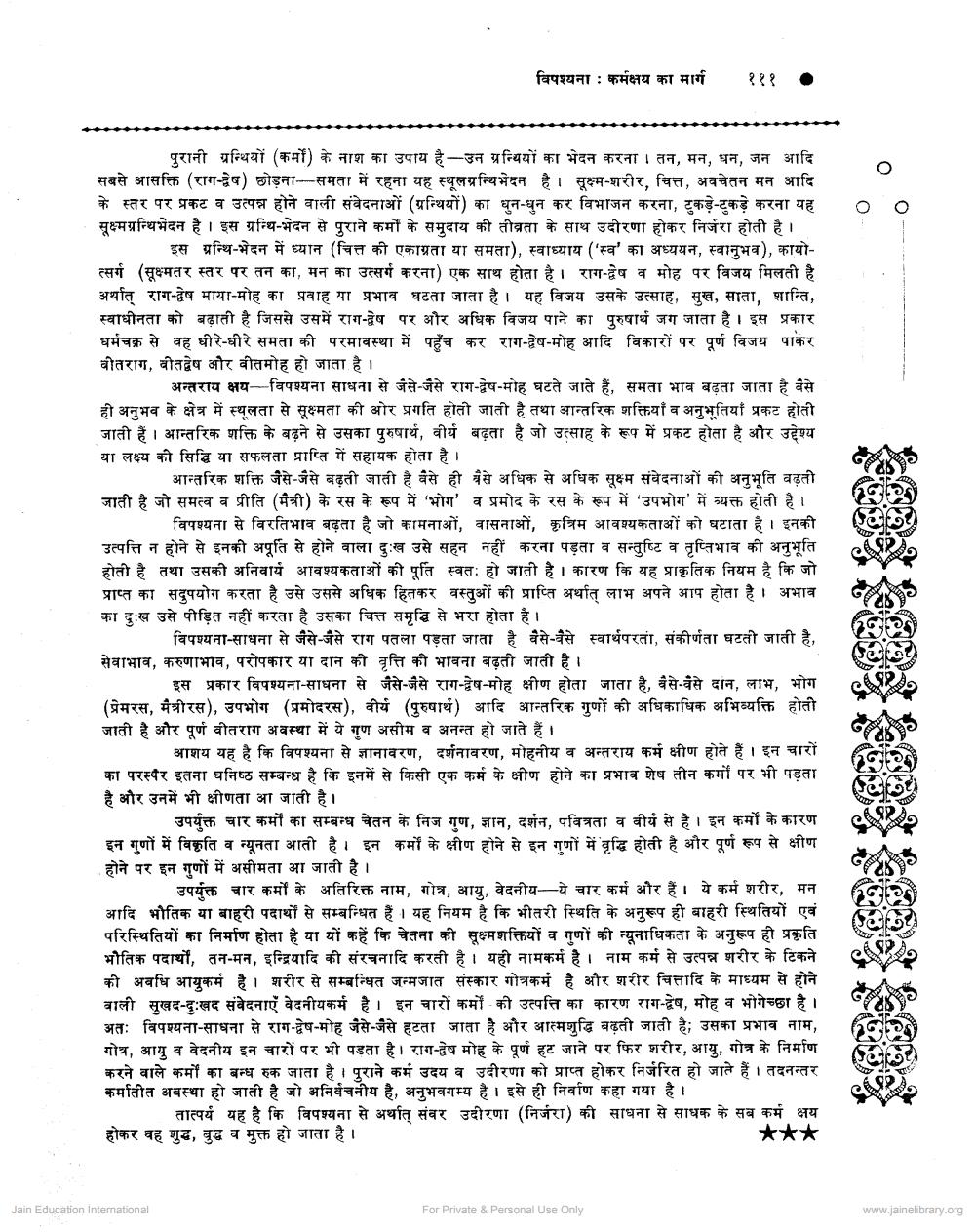________________
विपश्यना : कर्मक्षय का मार्ग
१११ .
०
पुरानी ग्रन्थियों (कर्मों) के नाश का उपाय है-उन ग्रन्थियों का भेदन करना । तन, मन, धन, जन आदि सबसे आसक्ति (राग-द्वेष) छोड़ना-समता में रहना यह स्थूल ग्रन्थिभेदन है। सूक्ष्म-शरीर, चित्त, अवचेतन मन आदि के स्तर पर प्रकट व उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं (ग्रन्थियों) का धुन-धुन कर विभाजन करना, टुकड़े-टुकड़े करना यह सूक्ष्मग्रन्थिभेदन है । इस ग्रन्थि-भेदन से पुराने कर्मों के समुदाय की तीव्रता के साथ उदीरणा होकर निर्जरा होती है।
इस ग्रन्थि-भेदन में ध्यान (चित्त की एकाग्रता या समता), स्वाध्याय ('स्व' का अध्ययन, स्वानुभव), कायोत्सर्ग (सूक्ष्मतर स्तर पर तन का, मन का उत्सर्ग करना) एक साथ होता है। राग-द्वेष व मोह पर विजय मिलती है अर्थात् राग-द्वेष माया-मोह का प्रवाह या प्रभाव घटता जाता है। यह विजय उसके उत्साह, सुख, साता, शान्ति, स्वाधीनता को बढ़ाती है जिससे उसमें राग-द्वेष पर और अधिक विजय पाने का पुरुषार्थ जग जाता है। इस प्रकार धर्मचक्र से वह धीरे-धीरे समता की परमावस्था में पहुँच कर राग-द्वेष-मोह आदि विकारों पर पूर्ण विजय पाकर वीतराग, वीतद्वेष और वीतमोह हो जाता है।
___अन्तराय क्षय-विपश्यना साधना से जैसे-जैसे राग-द्वेष-मोह घटते जाते हैं, समता भाव बढ़ता जाता है वैसे ही अनुभव के क्षेत्र में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रगति होती जाती है तथा आन्तरिक शक्तियाँ व अनुभूतियाँ प्रकट होती जाती हैं । आन्तरिक शक्ति के बढ़ने से उसका पुरुषार्थ, वीर्य बढ़ता है जो उत्साह के रूप में प्रकट होता है और उद्देश्य या लक्ष्य की सिद्धि या सफलता प्राप्ति में सहायक होता है।
आन्तरिक शक्ति जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे अधिक से अधिक सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति बढ़ती जाती है जो समत्व व प्रीति (मैत्री) के रस के रूप में 'भोग' व प्रमोद के रस के रूप में 'उपभोग' में व्यक्त होती है।
विपश्यना से विरतिभाव बढ़ता है जो कामनाओं, वासनाओं, कृत्रिम आवश्यकताओं को घटाता है । इनकी उत्पत्ति न होने से इनकी अपूर्ति से होने वाला दुःख उसे सहन नहीं करना पड़ता व सन्तुष्टि व तृप्तिभाव की अनुभूति । होती है तथा उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है। कारण कि यह प्राकृतिक नियम है कि जो प्राप्त का सदुपयोग करता है उसे उससे अधिक हितकर वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात् लाभ अपने आप होता है। अभाव का दुःख उसे पीड़ित नहीं करता है उसका चित्त समृद्धि से भरा होता है।
विपश्यना-साधना से जैसे-जैसे राग पतला पड़ता जाता है वैसे-वैसे स्वार्थपरता, संकीर्णता घटती जाती है, सेवाभाव, करुणाभाव, परोपकार या दान की वृत्ति की भावना बढ़ती जाती है।
___ इस प्रकार विपश्यना-साधना से जैसे-जैसे राग-द्वेष-मोह क्षीण होता जाता है, वैसे-वैसे दान, लाभ, भोग (प्रेमरस, मैत्रीरस), उपभोग (प्रमोदरस), वीर्य (पुरुषार्थ) आदि आन्तरिक गुणों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती जाती है और पूर्ण वीतराग अवस्था में ये गुण असीम व अनन्त हो जाते हैं।
आशय यह है कि विपश्यना से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय व अन्तराय कर्म क्षीण होते हैं। इन चारों का परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इनमें से किसी एक कर्म के क्षीण होने का प्रभाव शेष तीन कर्मों पर भी पड़ता है और उनमें भी क्षीणता आ जाती है।
उपर्युक्त चार कर्मों का सम्बन्ध चेतन के निज गण, ज्ञान, दर्शन, पवित्रता व वीर्य से है। इन कर्मों के कारण इन गुणों में विकृति व न्यूनता आती है। इन कर्मों के क्षीण होने से इन गणों में वृद्धि होती है और पूर्ण रूप से क्षीण। होने पर इन गुणों में असीमता आ जाती है।
उपर्युक्त चार कर्मों के अतिरिक्त नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय—ये चार कर्म और हैं। ये कर्म शरीर, मन आदि भौतिक या बाहरी पदार्थों से सम्बन्धित हैं । यह नियम है कि भीतरी स्थिति के अनुरूप ही बाहरी स्थितियों एवं परिस्थितियों का निर्माण होता है या यों कहें कि चेतना की सूक्ष्म शक्तियों व गुणों की न्यूनाधिकता के अनुरूप ही प्रकृति भौतिक पदार्थों, तन-मन, इन्द्रियादि की संरचनादि करती है। यही नामकर्म है। नाम कर्म से उत्पन्न शरीर के टिकने की अवधि आयुकर्म है। शरीर से सम्बन्धित जन्मजात संस्कार गोत्रकर्म है और शरीर चित्तादि के माध्यम से होने वाली सुखद-दुःखद संवेदनाएँ वेदनीयकर्म है। इन चारों कर्मों की उत्पत्ति का कारण राग-द्वेष, मोह व भोगेच्छा है। अतः विपश्यना-साधना से राग-द्वेष-मोह जैसे-जैसे हटता जाता है और आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है; उसका प्रभाव नाम, गोत्र, आयु व वेदनीय इन चारों पर भी पड़ता है। राग-द्वेष मोह के पूर्ण हट जाने पर फिर शरीर, आयु, गोत्र के निर्माण करने वाले कर्मों का बन्ध रुक जाता है। पुराने कर्म उदय व उदीरणा को प्राप्त होकर निर्जरित हो जाते हैं । तदनन्तर कर्मातीत अवस्था हो जाती है जो अनिर्वचनीय है, अनुभवगम्य है। इसे ही निर्वाण कहा गया है।
तात्पर्य यह है कि विपश्यना से अर्थात् संवर उदीरणा (निर्जरा) की साधना से साधक के सब कर्म क्षय होकर वह शुद्ध, बुद्ध व मुक्त हो जाता है ।
***
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org