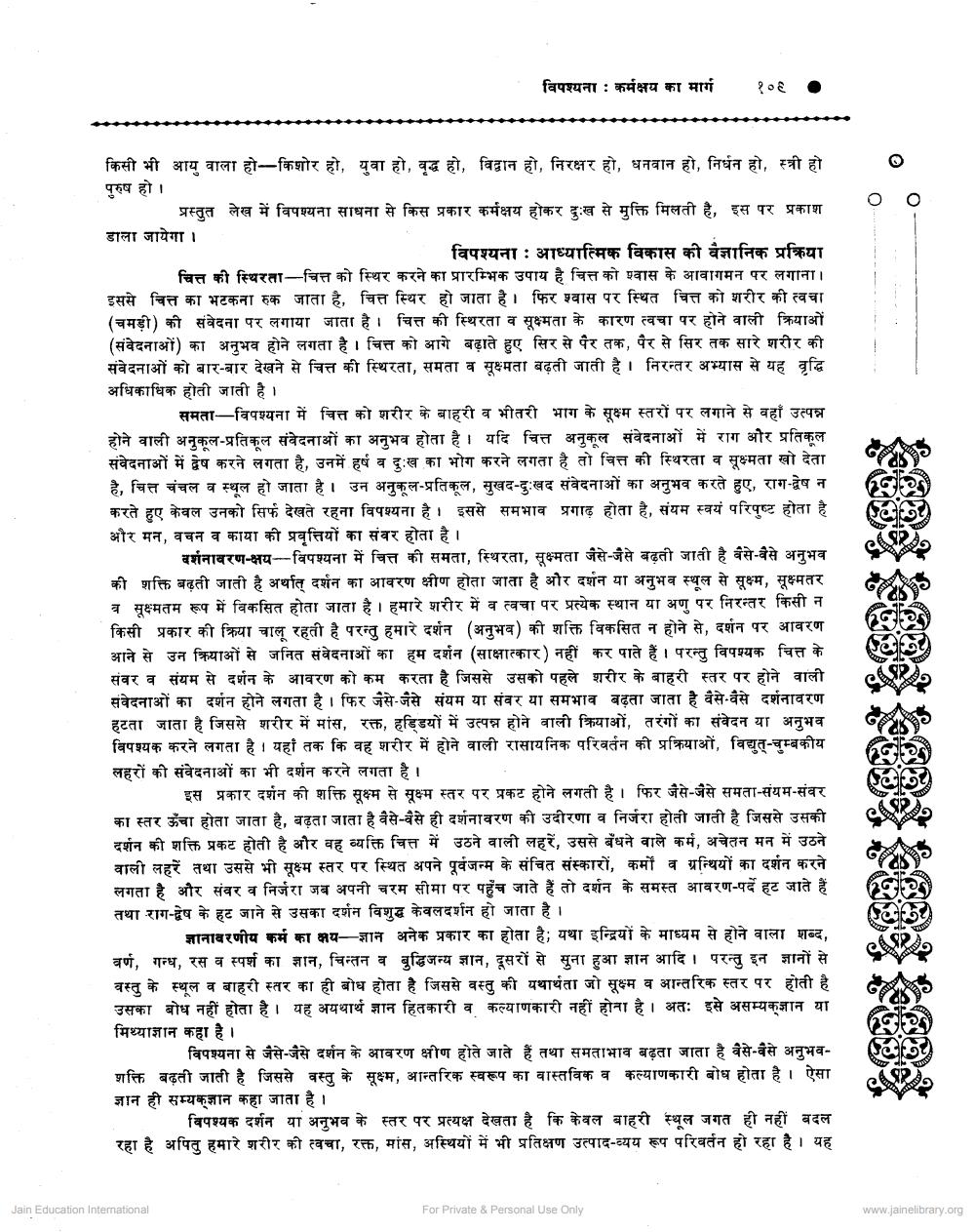________________
विपश्यना : कर्मक्षय का मार्ग
१०६
.
००
किसी भी आयु वाला हो-किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, विद्वान हो, निरक्षर हो, धनवान हो, निर्धन हो, स्त्री हो पुरुष हो।
प्रस्तुत लेख में विपश्यना साधना से किस प्रकार कर्मक्षय होकर दुःख से मुक्ति मिलती है, इस पर प्रकाश डाला जायेगा।
विपश्यना : आध्यात्मिक विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया चित्त की स्थिरता-चित्त को स्थिर करने का प्रारम्भिक उपाय है चित्त को श्वास के आवागमन पर लगाना। इससे चित्त का भटकना रुक जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। फिर श्वास पर स्थित चित्त को शरीर की त्वचा (चमड़ी) की संवेदना पर लगाया जाता है। चित्त की स्थिरता व सूक्ष्मता के कारण त्वचा पर होने वाली क्रियाओं (संवेदनाओं) का अनुभव होने लगता है। चित्त को आगे बढ़ाते हुए सिर से पैर तक, पैर से सिर तक सारे शरीर की संवेदनाओं को बार-बार देखने से चित्त की स्थिरता, समता व सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। निरन्तर अभ्यास से यह वृद्धि अधिकाधिक होती जाती है।
समता-विपश्यना में चित्त को शरीर के बाहरी व भीतरी भाग के सूक्ष्म स्तरों पर लगाने से वहाँ उत्पन्न होने वाली अनुकूल-प्रतिकूल संवेदनाओं का अनुभव होता है। यदि चित्त अनुकूल संवेदनाओं में राग और प्रतिकूल संवेदनाओं में द्वेष करने लगता है, उनमें हर्ष व दुःख का भोग करने लगता है तो चित्त की स्थिरता व सूक्ष्मता खो देता है, चित्त चंचल व स्थूल हो जाता है। उन अनुकूल-प्रतिकूल, सुखद-दुःखद संवेदनाओं का अनुभव करते हुए, राग-द्वेष न करते हुए केवल उनको सिर्फ देखते रहना विपश्यना है। इससे समभाव प्रगाढ़ होता है, संयम स्वयं परिपुष्ट होता है और मन, वचन व काया की प्रवृत्तियों का संवर होता है।
दर्शनावरण-क्षय-विपश्यना में चित्त की समता, स्थिरता, सूक्ष्मता जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे अनुभव की शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात् दर्शन का आवरण क्षीण होता जाता है और दर्शन या अनुभव स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम रूप में विकसित होता जाता है। हमारे शरीर में व त्वचा पर प्रत्येक स्थान या अणु पर निरन्तर किसी न किसी प्रकार की क्रिया चालू रहती है परन्तु हमारे दर्शन (अनुभव) की शक्ति विकसित न होने से, दर्शन पर आवरण आने से उन क्रियाओं से जनित संवेदनाओं का हम दर्शन (साक्षात्कार) नहीं कर पाते हैं । परन्तु विपश्यक चित्त के संवर व संयम से दर्शन के आवरण को कम करता है जिससे उसको पहले शरीर के बाहरी स्तर पर होने वाली संवेदनाओं का दर्शन होने लगता है। फिर जैसे-जैसे संयम या संवर या समभाव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे दर्शनावरण हटता जाता है जिससे शरीर में मांस, रक्त, हड्डियों में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं, तरंगों का संवेदन या अनुभव विपश्यक करने लगता है । यहाँ तक कि वह शरीर में होने वाली रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं, विद्युत्-चुम्बकीय लहरों की संवेदनाओं का भी दर्शन करने लगता है।
इस प्रकार दर्शन की शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रकट होने लगती है। फिर जैसे-जैसे समता-संयम-संवर का स्तर ऊँचा होता जाता है, बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ही दर्शनावरण की उदीरणा व निर्जरा होती जाती है जिससे उसकी दर्शन की शक्ति प्रकट होती है और वह व्यक्ति चित्त में उठने वाली लहरें, उससे बँधने वाले कर्म, अचेतन मन में उठने वाली लहरें तथा उससे भी सूक्ष्म स्तर पर स्थित अपने पूर्वजन्म के संचित संस्कारों, कर्मों व ग्रन्थियों का दर्शन करने लगता है और संवर व निर्जरा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो दर्शन के समस्त आवरण-पर्दे हट जाते हैं तथा राग-द्वेष के हट जाने से उसका दर्शन विशुद्ध केवलदर्शन हो जाता है ।
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय-ज्ञान अनेक प्रकार का होता है; यथा इन्द्रियों के माध्यम से होने वाला शब्द, वर्ण, गन्ध, रस व स्पर्श का ज्ञान, चिन्तन व बुद्धिजन्य ज्ञान, दूसरों से सुना हुआ ज्ञान आदि। परन्तु इन ज्ञानों से वस्तु के स्थूल व बाहरी स्तर का ही बोध होता है जिससे वस्तु की यथार्थता जो सूक्ष्म व आन्तरिक स्तर पर होती है उसका बोध नहीं होता है। यह अयथार्थ ज्ञान हितकारी व कल्याणकारी नहीं होना है। अतः इसे असम्यक्ज्ञान या मिथ्याज्ञान कहा है।
विपश्यना से जैसे-जैसे दर्शन के आवरण क्षीण होते जाते हैं तथा समताभाव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे अनुभवशक्ति बढ़ती जाती है जिससे वस्तु के सूक्ष्म, आन्तरिक स्वरूप का वास्तविक व कल्याणकारी बोध होता है। ऐसा ज्ञान ही सम्यक्ज्ञान कहा जाता है।
विपश्यक दर्शन या अनुभव के स्तर पर प्रत्यक्ष देखता है कि केवल बाहरी स्थूल जगत ही नहीं बदल रहा है अपितु हमारे शरीर की त्वचा, रक्त, मांस, अस्थियों में भी प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय रूप परिवर्तन हो रहा है। यह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org