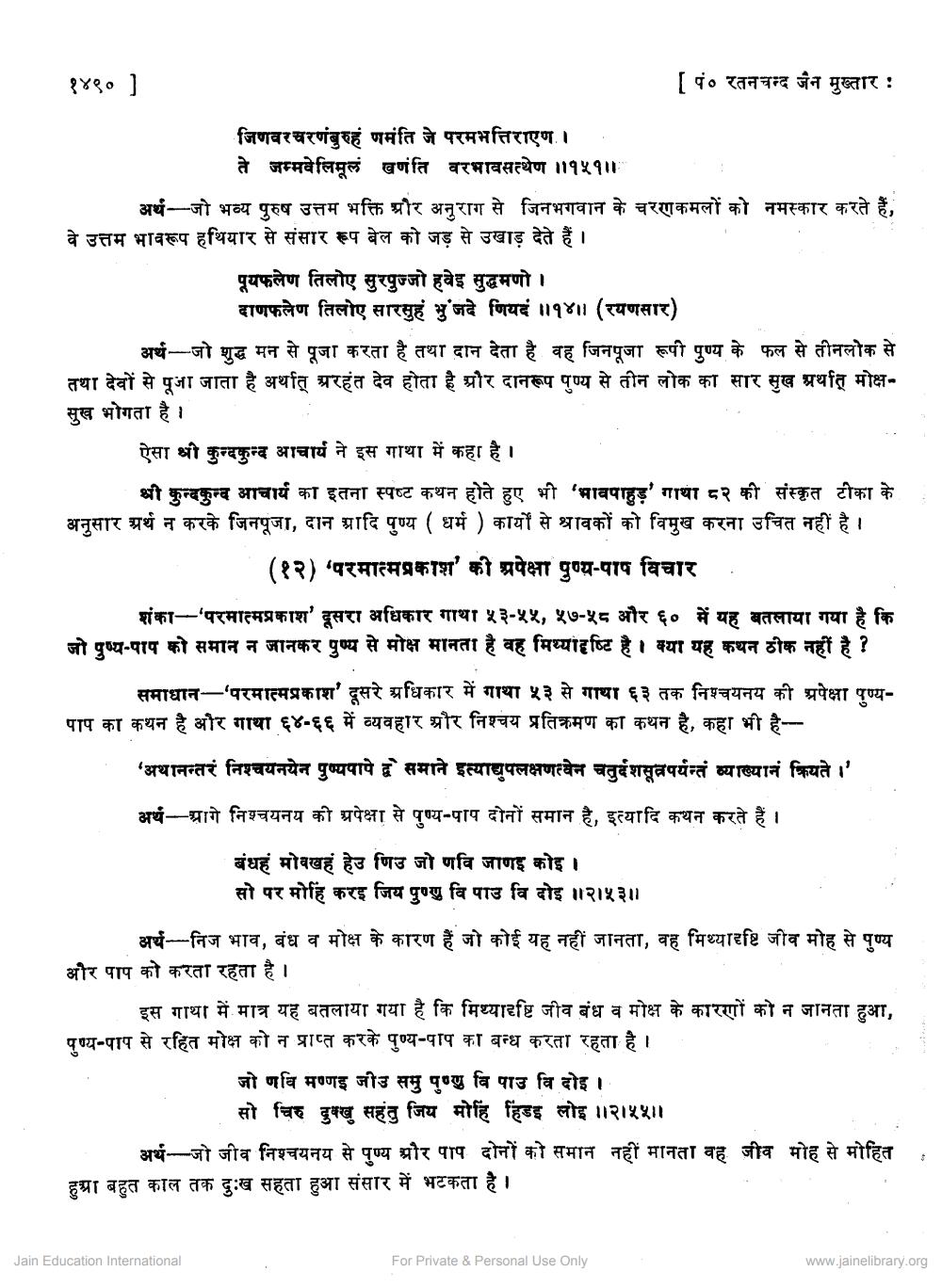________________
१४९० ]
[पं० रतनचन्द जैन मुख्तार :
जिणवरचरणंबुरुहं णमंति जे परमभत्तिराएण। ।
ते जम्मवेलिमूलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५१॥ अर्थ-जो भव्य पुरुष उत्तम भक्ति और अनुराग से जिनभगवान के चरणकमलों को नमस्कार करते हैं, वे उत्तम भावरूप हथियार से संसार रूप बेल को जड़ से उखाड़ देते हैं।
पूयफलेण तिलोए सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो।
दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुजदे णियदं ॥१४॥ (रयणसार) अर्थ-जो शुद्ध मन से पूजा करता है तथा दान देता है वह जिनपूजा रूपी पुण्य के फल से तीनलोक से तथा देवों से पूजा जाता है अर्थात् अरहंत देव होता है और दानरूप पुण्य से तीन लोक का सार सुख अर्थात् मोक्षसुख भोगता है।
ऐसा श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने इस गाथा में कहा है ।
श्री कुन्दकुन्द आचार्य का इतना स्पष्ट कथन होते हुए भी 'भावपाहुड़' गाथा ८२ की संस्कृत टीका के अनुसार अर्थ न करके जिनपूजा, दान आदि पुण्य ( धर्म ) कार्यों से श्रावकों को विमुख करना उचित नहीं है।
(१२) 'परमात्मप्रकाश' की अपेक्षा पुण्य-पाप विचार शंका-'परमात्मप्रकाश' दूसरा अधिकार गाथा ५३-५५, ५७-५८ और ६० में यह बतलाया गया है कि जो पुण्य-पाप को समान न जानकर पुण्य से मोक्ष मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। क्या यह कथन ठीक नहीं है ?
समाधान-'परमात्मप्रकाश' दूसरे अधिकार में गाथा ५३ से गाथा ६३ तक निश्चयनय की अपेक्षा पुण्यपाप का कथन है और गाथा ६४-६६ में व्यवहार और निश्चय प्रतिक्रमण का कथन है, कहा भी है
'अथानन्तरं निश्चयनयेन पुण्यपापे द्व समाने इत्याधुपलक्षणत्वेन चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियते ।' अर्थ-पागे निश्चयनय की अपेक्षा से पुण्य-पाप दोनों समान है, इत्यादि कथन करते हैं ।
बंधहं मोवखहं हेउ णिउ जो णवि जाणइ कोइ ।
सो पर मोहिं करइ जिय पुण्णु वि पाउ वि दोइ ॥२॥५३॥ अर्थ-निज भाव, बंध व मोक्ष के कारण हैं जो कोई यह नहीं जानता, वह मिथ्यादृष्टि जीव मोह से पुण्य और पाप को करता रहता है ।
इस गाथा में मात्र यह बतलाया गया है कि मिथ्याष्टि जीव बंध व मोक्ष के कारणों को न जानता हआ, पुण्य-पाप से रहित मोक्ष को न प्राप्त करके पुण्य-पाप का बन्ध करता रहता है ।
जो णवि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोइ ।
सो चिर दुक्खु सहंतु जिय मोहिं हिंडइ लोइ ॥२॥५५॥ अर्थ-जो जीव निश्चयनय से पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता वह जीव मोह से मोहित , हुआ बहुत काल तक दुःख सहता हुआ संसार में भटकता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org