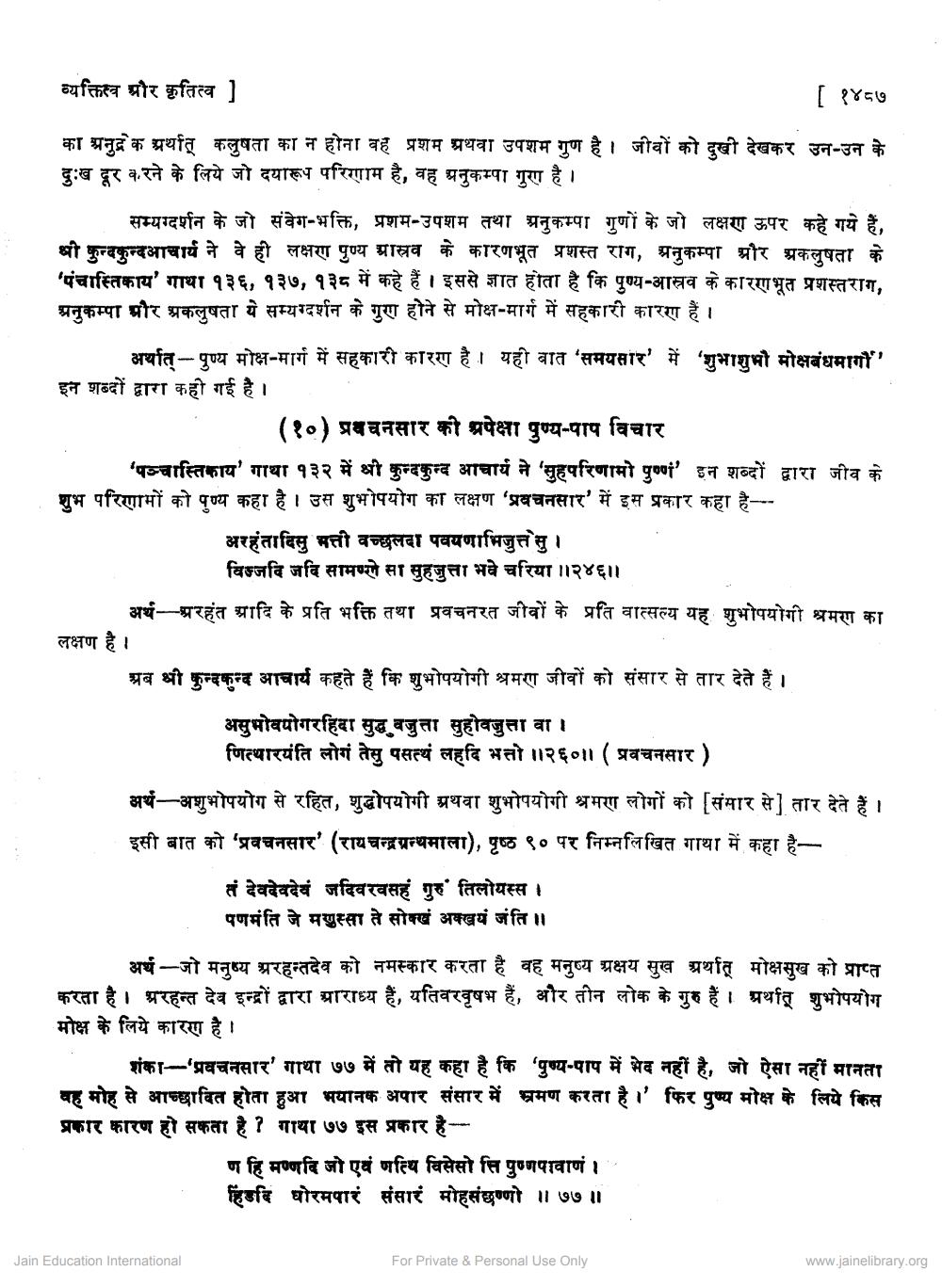________________
व्यक्तित्व और कृतित्व ]
[ १४८७ का अनुद्रेक अर्थात् कलुषता का न होना वह प्रशम अथवा उपशम गुण है। जीवों को दुखी देखकर उन-उन के दुःख दूर करने के लिये जो दयारूप परिणाम है, वह अनुकम्पा गुण है।
सम्यग्दर्शन के जो संवेग-भक्ति, प्रशम-उपशम तथा अनुकम्पा गुणों के जो लक्षण ऊपर कहे गये हैं, श्री कुन्दकुन्दआचार्य ने वे ही लक्षण पुण्य प्रास्रव के कारणभूत प्रशस्त राग, अनुकम्पा और अकलुषता के 'पंचास्तिकाय' गाथा १३६, १३७, १३८ में कहे हैं । इससे ज्ञात होता है कि पुण्य-आस्रव के कारणभूत प्रशस्तराग, अनुकम्पा और अकलुषता ये सम्यग्दर्शन के गुण होने से मोक्ष-मार्ग में सहकारी कारण हैं।
अर्थात-पुण्य मोक्ष-मार्ग में सहकारी कारण है। यही बात 'समयसार' में 'शुभाशुभौ मोक्षबंधमागौं' इन शब्दों द्वारा कही गई है।
(१०) प्रवचनसार की अपेक्षा पुण्य-पाप विचार 'पञ्चास्तिकाय' गाथा १३२ में श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने 'सुहपरिणामो पुग्ण' इन शब्दों द्वारा जीव के शुभ परिणामों को पुण्य कहा है । उस शुभोपयोग का लक्षण 'प्रवचनसार' में इस प्रकार कहा है--
अरहंतादिसु मत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्त सु ।
विज्जदि जदि सामरणे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ अर्थ-अरहंत आदि के प्रति भक्ति तथा प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य यह शुभोपयोगी श्रमण का लक्षण है। अब श्री कुन्दकुन्द आचार्य कहते हैं कि शुभोपयोगी श्रमण जीवों को संसार से तार देते हैं ।
असुभोवयोगरहिदा सुद्ध वजुत्ता सुहोवजुत्ता वा।
णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्यं लहदि भत्तो ॥२६०॥ (प्रवचनसार ) अर्थ-अशुभोपयोग से रहित, शुद्धोपयोगी अथवा शुभोपयोगी श्रमण लोगों को [संमार से] तार देते हैं । इसी बात को 'प्रवचनसार' (राय चन्द्रग्रन्थमाला), पृष्ठ ९० पर निम्नलिखित गाथा में कहा है
तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरु तिलोयस्स । पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥
अर्थ-जो मनुष्य अरहन्तदेव को नमस्कार करता है वह मनुष्य अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख को प्राप्त करता है। अरहन्त देव इन्द्रों द्वारा प्राराध्य हैं, यतिवरवृषभ हैं, और तीन लोक के गुरु हैं। अर्थात् शुभोपयोग मोक्ष के लिये कारण है।
शंका-'प्रवचनसार' गाथा ७७ में तो यह कहा है कि 'पुण्य-पाप में भेद नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता वह मोह से आच्छादित होता हुआ भयानक अपार संसार में भ्रमण करता है।' फिर पुण्य मोक्ष के लिये किस प्रकार कारण हो सकता है ? गाथा ७७ इस प्रकार है
ण हि मण्णदि जो एवं गस्थि विसेसो ति पुष्णपावाणं । हिंदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥ ७७ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org