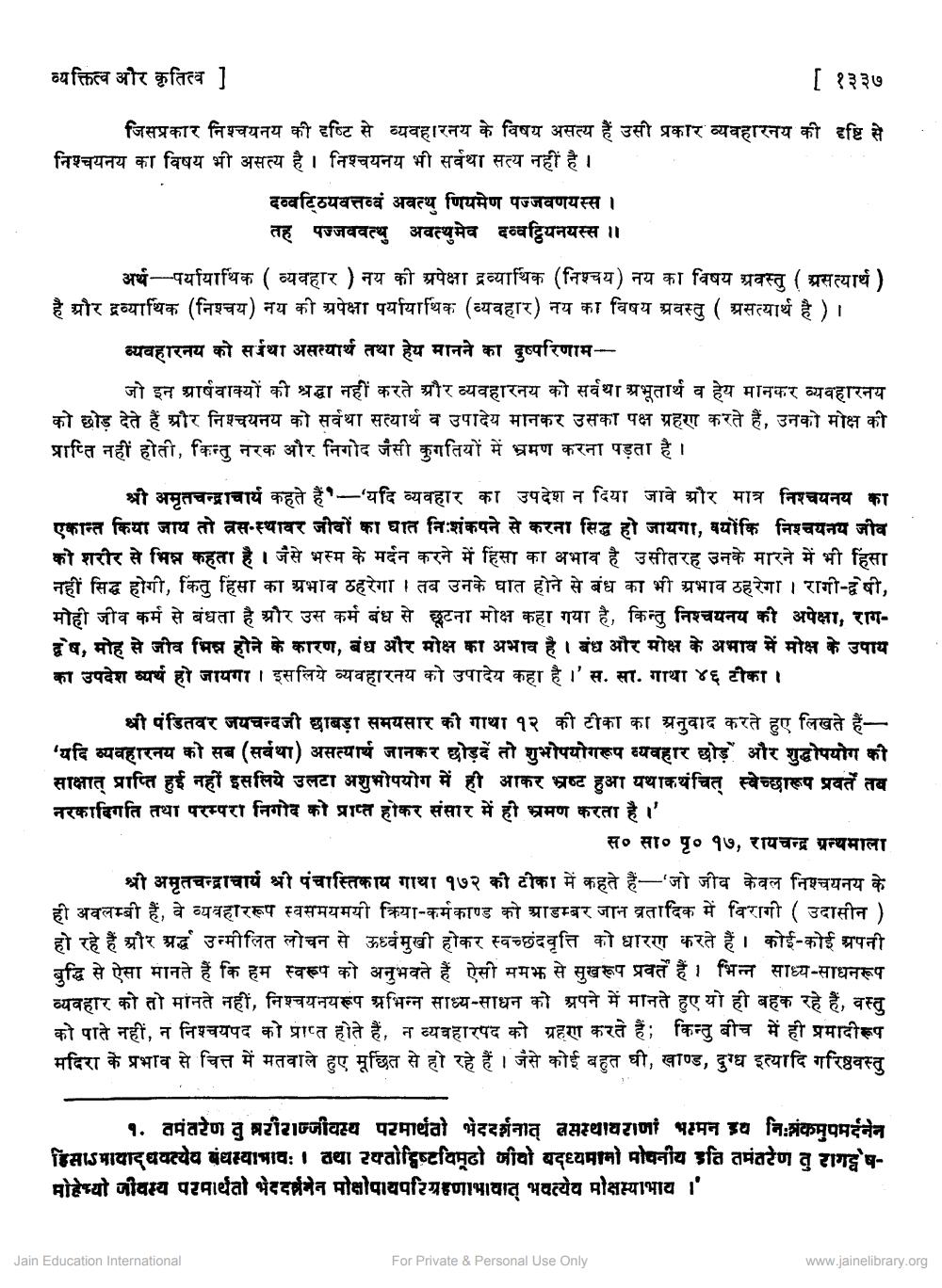________________
व्यक्तित्व और कृतित्व ]
[ १३३७
जिसप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से व्यवहारनय के विषय असत्य हैं उसी प्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से निश्चयनय का विषय भी असत्य है । निश्चयनय भी सर्वथा सत्य नहीं है ।
दवठ्ठियवत्तव्वं अवत्थु णियमेण पज्जवणयस्स ।
तह पज्जववत्थु अवत्थुमेव दम्वट्ठियनयस्स ॥ अर्थ-पर्यायाथिक ( व्यवहार ) नय की अपेक्षा द्रव्यार्थिक (निश्चय) नय का विषय अवस्तु ( असत्यार्थ) है और द्रव्याथिक (निश्चय) नय की अपेक्षा पर्यायाथिक (व्यवहार) नय का विषय अवस्तु ( असत्यार्थ है)।
व्यवहारनय को सर्वथा असत्यार्थ तथा हेय मानने का दुष्परिणाम
जो इन पार्षवाक्यों की श्रद्धा नहीं करते और व्यवहारनय को सर्वथा अभूतार्थ व हेय मानकर व्यवहारनय को छोड़ देते हैं और निश्चयनय को सर्वथा सत्यार्थ व उपादेय मानकर उसका पक्ष ग्रहण करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु नरक और निगोद जैसी कुगतियों में भ्रमण करना पड़ता है।
श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं'-'यदि व्यवहार का उपदेश न दिया जावे और मात्र निश्चयनय का एकान्त किया जाय तो बस-स्थावर जीवों का घात निःशंकपने से करना सिद्ध हो जायगा, क्योंकि निश्चयनय जीव को शरीर से भिन्न कहता है। जैसे भस्म के मर्दन करने में हिंसा का अभाव है उसीतरह उनके मारने में भी हिंसा नहीं सिद्ध होगी, किंतु हिंसा का अभाव ठहरेगा । तब उनके घात होने से बंध का भी अभाव ठहरेगा । रागी-द्वेषी, मोही जीव कर्म से बंधता है और उस कर्म बंध से छूटना मोक्ष कहा गया है, किन्तु निश्चयनय की अपेक्षा, रागद्वष, मोह से जीव भिन्न होने के कारण, बंध और मोक्ष का अभाव है। बंध और मोक्ष के अभाव में मोक्ष के उपाय का उपदेश व्यर्थ हो जायगा । इसलिये व्यवहारनय को उपादेय कहा है।' स. सा. गाथा ४६ टीका।
श्री पंडितवर जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की गाथा १२ की टीका का अनुवाद करते हुए लिखते हैं'यदि व्यवहारनय को सब (सर्वथा) असत्यार्थ जानकर छोड़दें तो शुभोपयोगरूप व्यवहार छोड़े और शुद्धोपयोग की साक्षात् प्राप्ति हुई नहीं इसलिये उलटा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट हुआ यथाकथंचित् स्वेच्छारूप प्रवर्ते तव नरकादिगति तथा परम्परा निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करता है।'
स० सा० पृ० १७, रायचन्द्र ग्रन्थमाला श्री अमृतचन्द्राचार्य श्री पंचास्तिकाय गाथा १७२ की टीका में कहते हैं-'जो जीव केवल निश्चयनय के ही अवलम्बी हैं, वे व्यवहाररूप स्वसमयमयी क्रिया-कर्मकाण्ड को आडम्बर जान व्रतादिक में विरागी ( उदासीन ) हो रहे हैं और अर्द्ध उन्मीलित लोचन से ऊर्ध्वमुखी होकर स्वच्छंदवृत्ति को धारण करते हैं। कोई-कोई अपनी बुद्धि से ऐसा मानते हैं कि हम स्वरूप को अनुभवते हैं ऐसी समझ से सुखरूप प्रवर्ते हैं । भिन्न साध्य-साधनरूप व्यवहार को तो मानते नहीं, निश्चयनयरूप अभिन्न साध्य-साधन को अपने में मानते हुए यो ही बहक रहे हैं, वस्तु को पाते नहीं, न निश्चयपद को प्राप्त होते हैं, न व्यवहारपद को ग्रहण करते हैं; किन्तु बीच में ही प्रमादीरूप मदिरा के प्रभाव से चित्त में मतवाले हुए मूर्छित से हो रहे हैं । जैसे कोई बहुत घी, खाण्ड, दुग्ध इत्यादि गरिष्ठवस्तु
१. तमंतरेण तु बरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात् बसस्थावराणां भगमन व नि:संकमुपमर्दनेन हिसाऽमायाघवत्येव बंधस्याभावः । तथा रक्तोद्विष्टविमूढो जीयो बध्यमानो मोचनीय इति तमंतरेण तु रागद्वेषमोहेज्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्भमेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवत्येव मोक्षस्याभाय ।'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org