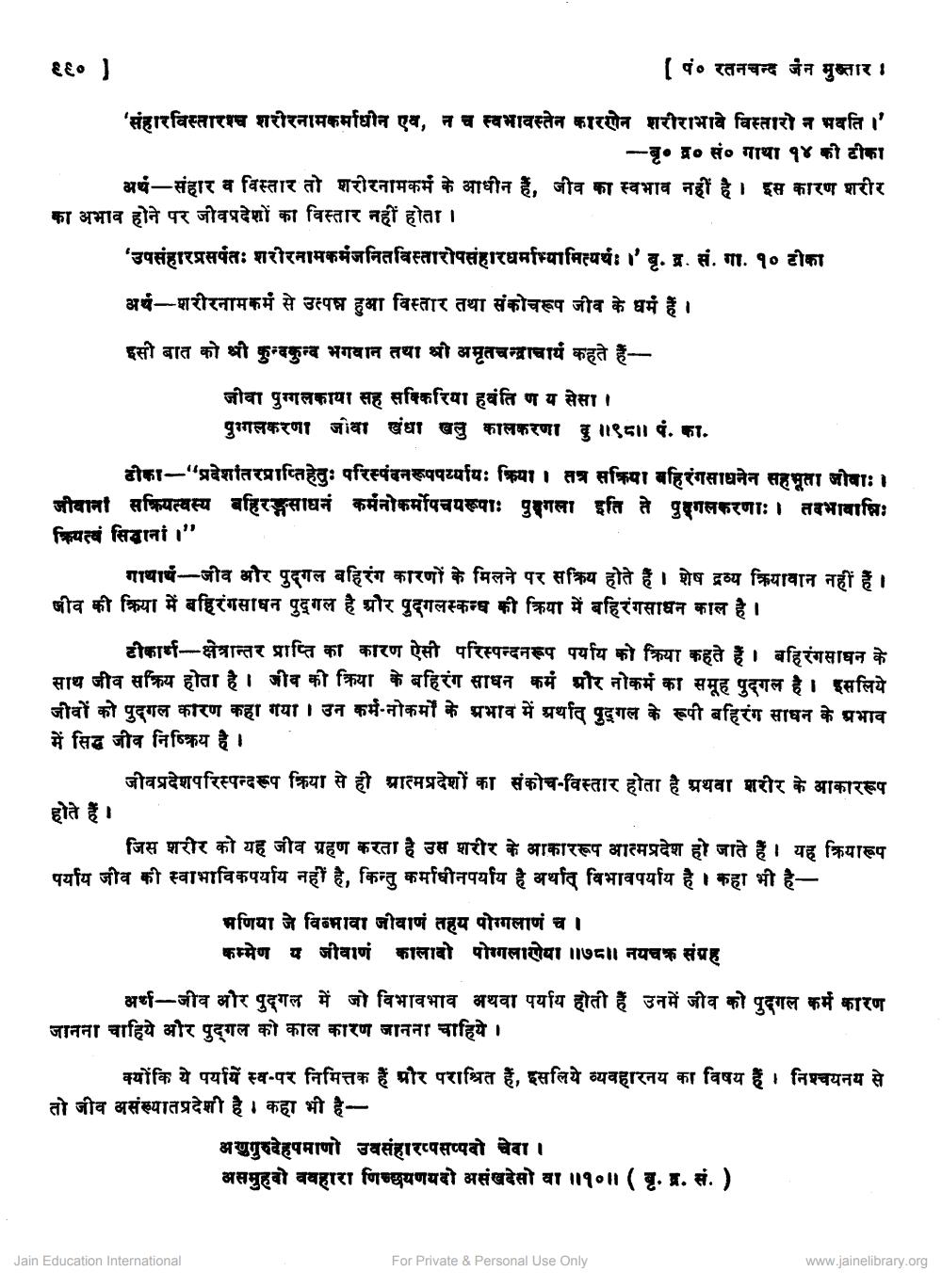________________
१६.]
[ पं. रतनचन्द जैन मुख्तार ।
'संहारविस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव, न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न भवति ।'
-बृ.द्र०सं० गाथा १४ की टीका अर्थ-संहार व विस्तार तो शरीरनामकर्म के आधीन हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। इस कारण शरीर का अभाव होने पर जीवप्रदेशों का विस्तार नहीं होता।
'उपसंहारप्रसर्पतः शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थः।' बृ.व. सं. गा. १० टोका अर्थ-शरीरनामकर्म से उत्पन्न हुआ विस्तार तथा संकोचरूप जीव के धर्म हैं । इसी बात को श्री कुन्दकुन्द भगवान तथा श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं
जीवा पुग्गलकाया सह सक्किरिया हवंति य सेसा ।
पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणा दु॥९॥.का. टीका-"प्रदेशांतरप्राप्तिहेतुः परिस्पंदनरूपपर्यायः क्रिया। तत्र सक्रिया बहिरंगसाधनेन सहभूता जोवाः । जीवानां सक्रियत्वस्य बहिरङ्गसाधनं कमनोकर्मोपचयरूपाः पुगला इति ते पुद्गलकरणाः। तवभावान्नि: क्रियत्वं सिवानां।"
गाथार्य-जीव और पुद्गल बहिरंग कारणों के मिलने पर सक्रिय होते हैं । शेष द्रव्य क्रियावान नहीं हैं। जीव की क्रिया में बहिरंगसाधन पुद्गल है और पुद्गलस्कन्ध की क्रिया में बहिरंगसाधन काल है।
टीकार्ग-क्षेत्रान्तर प्राप्ति का कारण ऐसी परिस्पन्दनरूप पर्याय को क्रिया कहते हैं । बहिरंगसाधन के साथ जीव सक्रिय होता है। जीव की क्रिया के बहिरंग साधन कम और नोकर्म का समूह पुद्गल है। इसलिये जीवों को पुद्गल कारण कहा गया। उन कर्म-नोकर्मों के प्रभाव में अर्थात् पुद्गल के रूपी बहिरंग साधन के प्रभाव में सिद्ध जीव निष्क्रिय है।
जीवप्रदेशपरिस्पन्दरूप क्रिया से ही प्रात्मप्रदेशों का संकोच-विस्तार होता है अथवा शरीर के आकाररूप होते हैं।
जिस शरीर को यह जीव ग्रहण करता है उस शरीर के आकाररूप आत्मप्रदेश हो जाते हैं। यह क्रियारूप पर्याय जीव की स्वाभाविकपर्याय नहीं है, किन्तु कर्माधीनपर्याय है अर्थात् विभावपर्याय है। कहा भी है
मणिया जे विमावा जीवाणं तहय पोग्गलाणं च ।
कम्मेण य जीवाणं कालावो पोग्गलाणेया ॥७॥ नयचक्र संग्रह अर्थ-जीव और पुद्गल में जो विभावभाव अथवा पर्याय होती हैं उनमें जीव को पुद्गल कर्म कारण जानना चाहिये और पुद्गल को काल कारण जानना चाहिये।
क्योंकि ये पर्याय स्व-पर निमित्तक हैं और पराश्रित हैं, इसलिये व्यवहारनय का विषय हैं। निश्चयनय से तो जीव असंख्यातप्रदेशी है । कहा भी है
अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेवा । असमुहवो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥ (वृ.प्र.सं.)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org