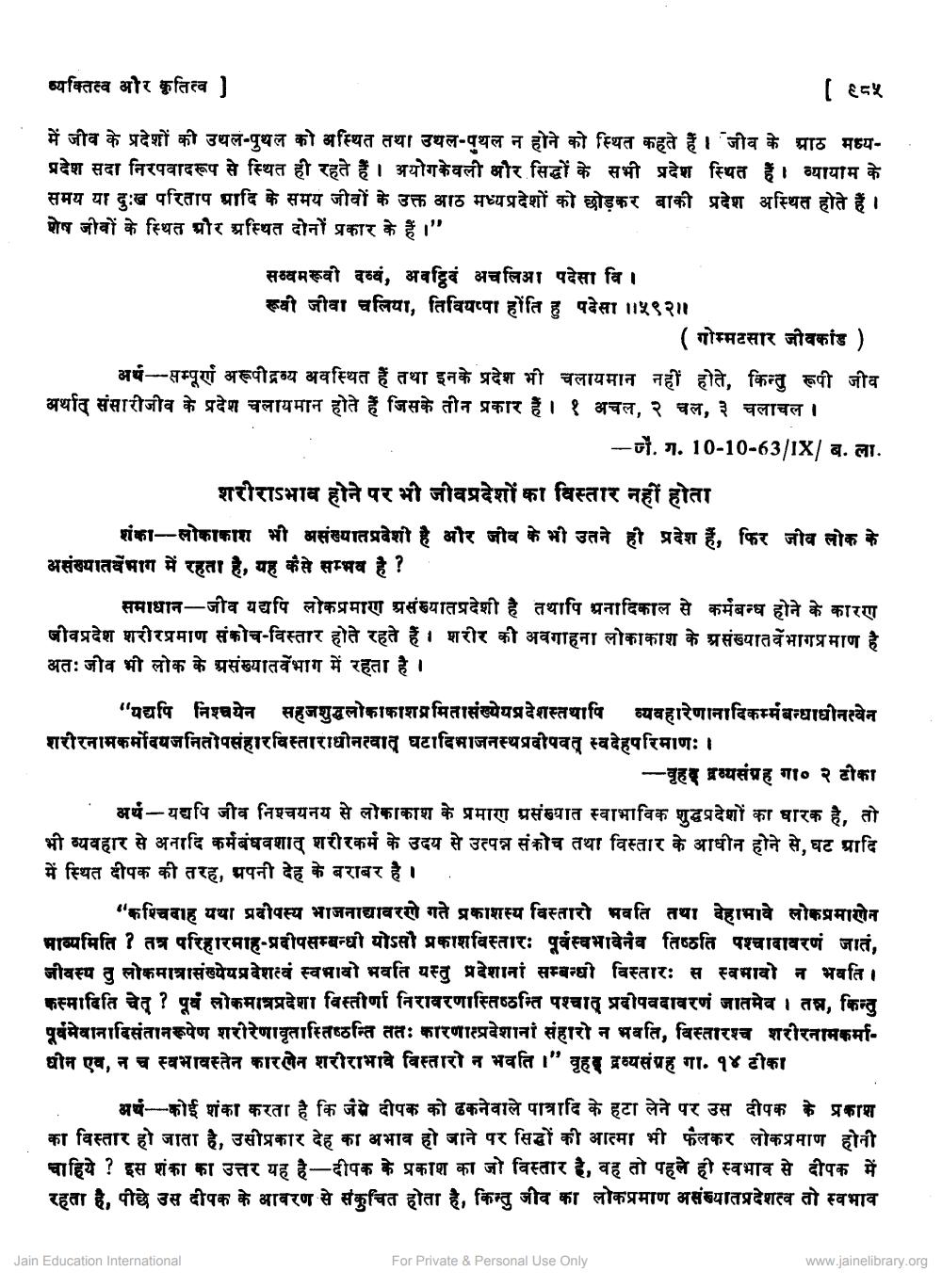________________
व्यक्तित्व और कृतित्व ]
[ ९८५
में जीव के प्रदेशों की उथल-पुथल को अस्थित तथा उथल-पथल न होने को स्थित कहते हैं। जीव के पाठ मध्यप्रदेश सदा निरपवादरूप से स्थित ही रहते हैं। अयोगकेवली और सिद्धों के सभी प्रदेश स्थित हैं। व्यायाम के समय या दुःख परिताप प्रादि के समय जीवों के उक्त आठ मध्यप्रदेशों को छोडकर बाकी प्रदेश अस्थित होते हैं। शेष जीवों के स्थित और अस्थित दोनों प्रकार के हैं।"
सव्वमरूवी दवं, अवडिवं अचलिआ पदेसा वि। ख्वी जीवा चलिया, तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥५९२॥
(गोम्मटसार जीवकांड ) अर्थ-सम्पूर्ण अरूपीद्रव्य अवस्थित हैं तथा इनके प्रदेश भी चलायमान नहीं होते, किन्तु रूपी जीव अर्थात संसारीजीव के प्रदेश चलायमान होते हैं जिसके तीन प्रकार हैं। १ अचल, २ चल,३ चलाचल ।
-णे. ग. 10-10-63/IX/ ब. ला.
शरीराऽभाव होने पर भी जीवप्रदेशों का विस्तार नहीं होता शंका-लोकाकाश भी असंख्यातप्रवेशी है और जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं, फिर जीव लोक के असंख्यातवेंभाग में रहता है, यह कैसे सम्भव है ?
समाधान-जीव यद्यपि लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है तथापि अनादिकाल से कर्मबन्ध होने के कारण जीवप्रदेश शरीरप्रमाण संकोच-विस्तार होते रहते हैं। शरीर की अवगाहना लोकाकाश के असंख्यातभागप्रमाण है अतः जीव भी लोक के असंख्यातवेंभाग में रहता है।
"यद्यपि निश्चयेन सहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशस्तथापि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धाधीनत्वेन शरीरनामकर्मोदयजनितोपसंहार विस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजनस्थप्रदीपवत स्वदेहपरिमाणः ।
-वृहद द्रव्यसंग्रह गा० २ टीका - अर्थ-यद्यपि जीव निश्चयनय से लोकाकाश के प्रमाण प्रसंख्यात स्वाभाविक शुद्धप्रदेशों का धारक है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्मबंधवशात् शरीरकर्म के उदय से उत्पन्न संकोच तथा विस्तार के आधीन होने से,घट प्रादि में स्थित दीपक की तरह, अपनी देह के बराबर है। .
"कश्चिदाह यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा वेहामावे लोकप्रमाणेन
? तत्र परिहारमाह-प्रवीपसम्बन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्वस्वभावेनैव तिष्ठति पश्चावावरणं जातं, जीवस्य लोकमात्रासंख्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्त प्रदेशानां सम्बन्धी विस्तारः स स्वमावो न भवति । कस्मादिति चेत् ? पूर्व लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात प्रदीपववावरणं जातमेव । तन्न, किन्तु पूर्वमेवानादिसंतानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रवेशानां संहारो न भवति, विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव, न च स्वभावस्तेन कारलेन शरीराभावे विस्तारो न भवति ।" वृहह द्रव्यसंग्रह गा. १४ टीका
अर्थ-कोई शंका करता है कि जैसे दीपक को ढकनेवाले पात्रादि के हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसीप्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा भी फैलकर लोकप्रमाण होनी चाहिये ? इस शंका का उत्तर यह है-दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है, किन्तु जीव का लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशत्व तो स्वभाव
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org