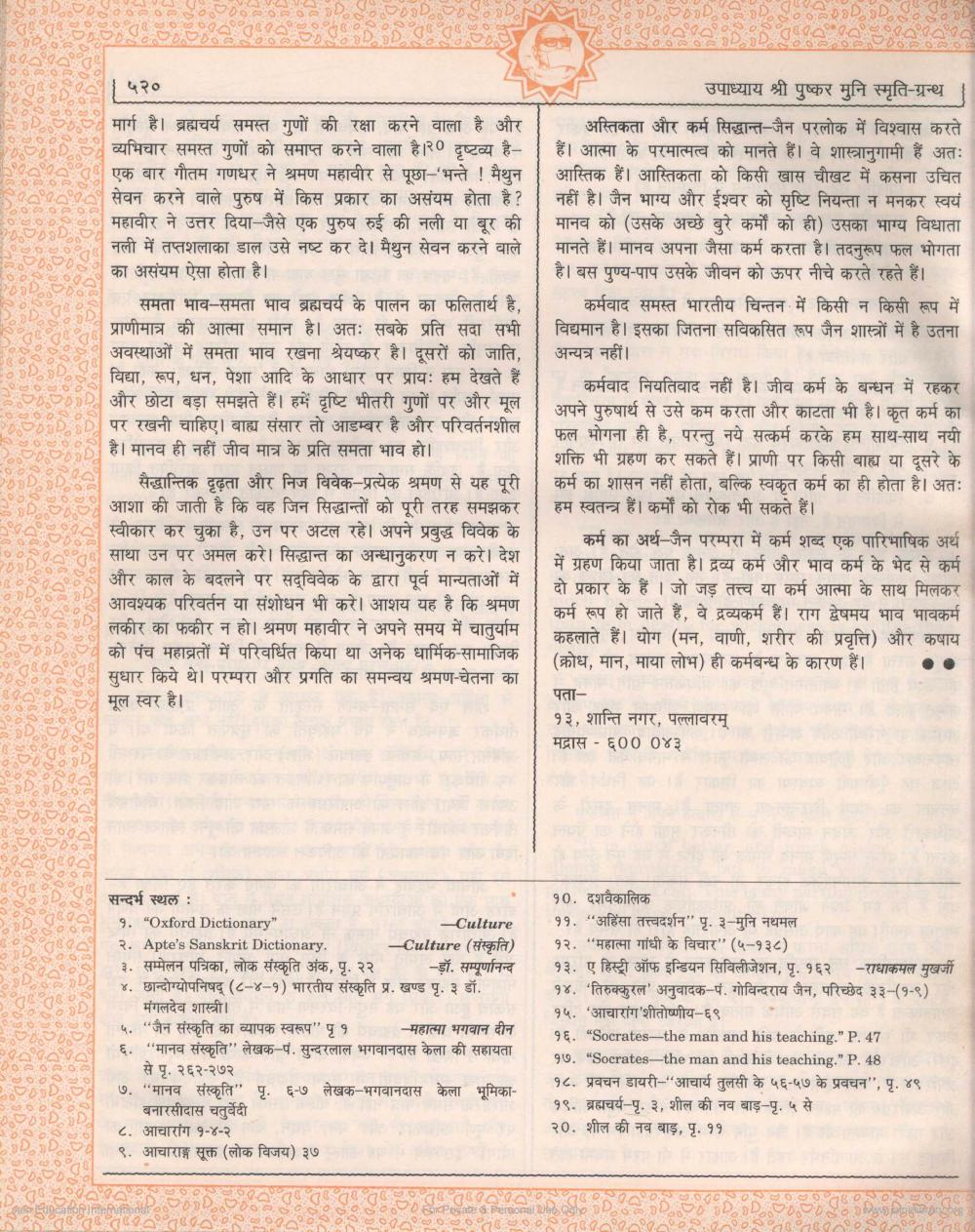________________
५२०
मार्ग है। ब्रह्मचर्य समस्त गुणों की रक्षा करने वाला है और व्यभिचार समस्त गुणों को समाप्त करने वाला है। २० दृष्टव्य हैएक बार गौतम गणधर ने श्रमण महावीर से पूछा- 'भन्ते ! मैथुन सेवन करने वाले पुरुष में किस प्रकार का असंयम होता है ? महावीर ने उत्तर दिया जैसे एक पुरुष रुई की नली या दूर की नली में तप्तशलाका डाल उसे नष्ट कर दे। मैथुन सेवन करने वाले का असंयम ऐसा होता है।
समता भाव- समता भाव ब्रह्मचर्य के पालन का फलितार्थ है, प्राणीमात्र की आत्मा समान है। अतः सबके प्रति सदा सभी अवस्थाओं में समता भाव रखना श्रेयष्कर है। दूसरों को जाति, विद्या, रूप, धन, पेशा आदि के आधार पर प्रायः हम देखते हैं और छोटा बड़ा समझते हैं। हमें दृष्टि भीतरी गुणों पर और मूल पर रखनी चाहिए। वाह्य संसार तो आडम्बर है और परिवर्तनशील है । मानव ही नहीं जीव मात्र के प्रति समता भाव हो ।
सैद्धान्तिक दृढ़ता और निज विवेक प्रत्येक श्रमण से यह पूरी आशा की जाती है कि वह जिन सिद्धान्तों को पूरी तरह समझकर स्वीकार कर चुका है, उन पर अटल रहे। अपने प्रबुद्ध विवेक के साथा उन पर अमल करे। सिद्धान्त का अन्धानुकरण न करे। देश और काल के बदलने पर सद्विवेक के द्वारा पूर्व मान्यताओं में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन भी करे। आशय यह है कि श्रमण लकीर का फकीर न हो श्रमण महावीर ने अपने समय में चातुर्याम को पंच महाव्रतों में परिवर्धित किया था अनेक धार्मिक सामाजिक सुधार किये थे। परम्परा और प्रगति का समन्वय श्रमण-चेतना का मूल स्वर है।
सन्दर्भ स्थल :
9. "Oxford Dictionary"
२. Apte's Sanskrit Dictionary.
३. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, पृ. २२
-Culture -Culture (संस्कृति) -डॉ. सम्पूर्णानन्द
४. छान्दोग्योपनिषद् (८-४-१) भारतीय संस्कृति प्र. खण्ड पृ. ३ डॉ.
मंगलदेव शास्त्री |
64
'जैन संस्कृति का व्यापक स्वरूप" पृ १
-महात्मा भगवान दीन
६. “मानव संस्कृति” लेखक- पं. सुन्दरलाल भगवानदास केला की सहायता
से पृ. २६२-२७२
७. “मानव संस्कृति" पृ. ६-७ लेखक- भगवानदास केला भूमिकाबनारसीदास चतुर्वेदी
८. आचारांग १-४-२
९. आचाराङ्ग सूक्त (लोक विजय ) ३७
International Sasala
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
अस्तिकता और कर्म सिद्धान्त-जैन परलोक में विश्वास करते हैं। आत्मा के परमात्मत्व को मानते हैं। वे शास्त्रानुगामी हैं अतः आस्तिक हैं। आस्तिकता को किसी खास चौखट में कसना उचित नहीं है। जैन भाग्य और ईश्वर को सृष्टि नियन्ता न मनकर स्वयं मानव को (उसके अच्छे बुरे कर्मों को ही उसका भाग्य विधाता मानते हैं। मानव अपना जैसा कर्म करता है। तदनुरूप फल भोगता है। बस पुण्य-पाप उसके जीवन को ऊपर नीचे करते रहते हैं।
कर्मवाद समस्त भारतीय चिन्तन में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसका जितना सविकसित रूप जैन शास्त्रों में है उतना अन्यत्र नहीं ।
कर्मवाद नियतिवाद नहीं है। जीव कर्म के बन्धन में रहकर अपने पुरुषार्थ से उसे कम करता और काटता भी है। कृत कर्म का फल भोगना ही है, परन्तु नये सत्कर्म करके हम साथ-साथ नयी शक्ति भी ग्रहण कर सकते हैं। प्राणी पर किसी बाह्य या दूसरे के कर्म का शासन नहीं होता, बल्कि स्वकृत कर्म का ही होता है। अतः हम स्वतन्त्र हैं। कर्मों को रोक भी सकते हैं।
कर्म का अर्थ-जैन परम्परा में कर्म शब्द एक पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण किया जाता है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के भेद से कर्म दो प्रकार के हैं । जो जड़ तत्त्व या कर्म आत्मा के साथ मिलकर कर्म रूप हो जाते हैं, वे द्रव्यकर्म है। राग द्वेषमय भाव भावकर्म कहलाते हैं। योग (मन, वाणी, शरीर की प्रवृत्ति) और कषाय (क्रोध, मान, माया लोभ) ही कर्मबन्ध के कारण है।
पता
१३, शान्ति नगर, पल्लावरम् मद्रास ६०००४३
१०. दशवैकालिक
११. " अहिंसा तत्त्वदर्शन" पृ. ३-मुनि नथमल १२. “महात्मा गांधी के विचार" (५-१३८)
१३. ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन सिविलीजेशन, पृ. १६२
-राधाकमल मुखर्जी
१४. 'तिरुक्कुरल' अनुवादक- पं. गोविन्दराय जैन, परिच्छेद ३३ (१-९) १५. 'आचारांग 'शीतोष्णीय-६९
१६. “Socrates the man and his teaching." P. 47 99. "Socrates-the man and his teaching." P. 48
१८. प्रवचन डायरी - "आचार्य तुलसी के ५६-५७ के प्रवचन, पृ. ४९ १९. ब्रह्मचर्य - पृ. ३, शील की नव बाड़-पृ. ५ से
२०. शील की नव बाड़, पृ. ११
Pevate & Personal Whe
0/180
ronger