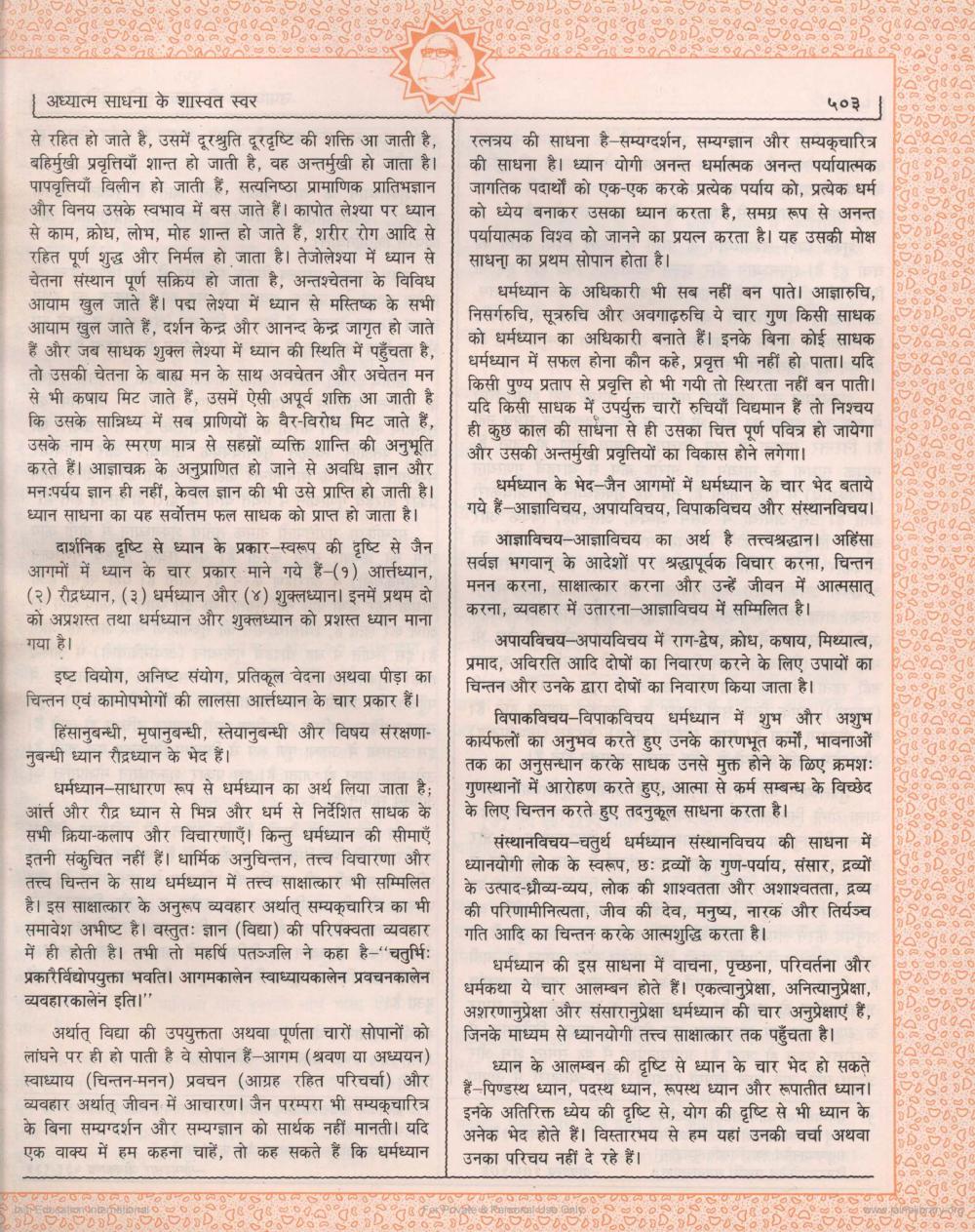________________
अध्यात्म साधना के शास्वत स्वर
से रहित हो जाते हैं, उसमें दूरश्रुति दूरदृष्टि की शक्ति आ जाती है, बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ शान्त हो जाती है, वह अन्तर्मुखी हो जाता है। पापवृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं, सत्यनिष्ठा प्रामाणिक प्रातिभज्ञान और विनय उसके स्वभाव में बस जाते हैं। कापोत लेश्या पर ध्यान से काम, क्रोध, लोभ, मोह शान्त हो जाते हैं, शरीर रोग आदि से रहित पूर्ण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तेजोलेश्या में ध्यान से चेतना संस्थान पूर्ण सक्रिय हो जाता है, अन्तश्चेतना के विविध आयाम खुल जाते हैं। पद्म लेश्या में ध्यान से मस्तिष्क के सभी आयाम खुल जाते हैं, दर्शन केन्द्र और आनन्द केन्द्र जागृत हो जाते हैं और जब साधक शुक्ल लेश्या में ध्यान की स्थिति में पहुँचता है, तो उसकी चेतना के बाह्य मन के साथ अवचेतन और अचेतन मन से भी कषाय मिट जाते हैं, उसमें ऐसी अपूर्व शक्ति आ जाती है। कि उसके सान्निध्य में सब प्राणियों के वैर-विरोध मिट जाते हैं, उसके नाम के स्मरण मात्र से सहस्रों व्यक्ति शान्ति की अनुभूति करते हैं। आज्ञाचक्र के अनुप्राणित हो जाने से अवधि ज्ञान और मन:पर्यय ज्ञान ही नहीं, केवल ज्ञान की भी उसे प्राप्ति हो जाती है। ध्यान साधना का यह सर्वोत्तम फल साधक को प्राप्त हो जाता है।
दार्शनिक दृष्टि से ध्यान के प्रकार-स्वरूप की दृष्टि से जैन आगमों में ध्यान के चार प्रकार माने गये हैं- (१) आर्त्तध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) शुक्लध्यान। इनमें प्रथम दो को अप्रशस्त तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान को प्रशस्त ध्यान माना गया है।
इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग प्रतिकूल वेदना अथवा पीड़ा का चिन्तन एवं कामोपभोगों की लालसा आर्त्तध्यान के चार प्रकार हैं।
हिंसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषय संरक्षणानुबन्धी ध्यान रौद्रध्यान के भेद है।
धर्मध्यान-साधारण रूप से धर्मध्यान का अर्थ लिया जाता है; आंत और रौद्र ध्यान से भिन्न और धर्म से निर्देशित साधक के सभी क्रिया-कलाप और विचारणाएँ । किन्तु धर्मध्यान की सीमाएँ इतनी संकुचित नहीं हैं। धार्मिक अनुचिन्तन, तत्त्व विचारणा और तत्त्व चिन्तन के साथ धर्मध्यान में तत्त्व साक्षात्कार भी सम्मिलित है। इस साक्षात्कार के अनुरूप व्यवहार अर्थात् सम्यक्चारित्र का भी समावेश अभीष्ट है। वस्तुतः ज्ञान (विद्या) की परिपक्वता व्यवहार में ही होती है। तभी तो महर्षि पतञ्जलि ने कहा है- “चतुर्भिः प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति । आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन इति । "
अर्थात् विद्या की उपयुक्तता अथवा पूर्णता चारों सोपानों को लांघने पर ही हो पाती है वे सोपान है-आगम (श्रवण या अध्ययन ) स्वाध्याय (चिन्तन-मनन) प्रवचन ( आग्रह रहित परिचर्चा) और व्यवहार अर्थात् जीवन में आचारण। जैन परम्परा भी सम्यक्चारित्र के बिना सम्प्रग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को सार्थक नहीं मानती। यदि एक वाक्य में हम कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि धर्मध्यान
80 tarpali
DOOD
५०३
रत्नत्रय की साधना है- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की साधना है। ध्यान योगी अनन्त धर्मात्मक अनन्त पर्यायात्मक जागतिक पदार्थों को एक-एक करके प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक धर्म को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करता है, समग्र रूप से अनन्त पर्यायात्मक विश्व को जानने का प्रयत्न करता है। यह उसकी मोक्ष साधना का प्रथम सोपान होता है।
धर्मध्यान के अधिकारी भी सब नहीं बन पाते। आज्ञारुचि, निसर्गरुचि, सूत्ररुचि और अवगाढ़रुचि ये चार गुण किसी साधक को धर्मध्यान का अधिकारी बनाते हैं। इनके बिना कोई साधक धर्मध्यान में सफल होना कौन कहे, प्रवृत्त भी नहीं हो पाता। यदि किसी पुण्य प्रताप से प्रवृत्ति हो भी गयी तो स्थिरता नहीं बन पाती। यदि किसी साधक में उपर्युक्त चारों रुचियाँ विद्यमान हैं तो निश्चय ही कुछ काल की साधना से ही उसका चित पूर्ण पवित्र हो जायेगा और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों का विकास होने लगेगा।
धर्मध्वान के भेद जैन आगमों में धर्मध्यान के चार भेद बताये गये हैं-आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ।
आज्ञाविचय- आज्ञाविचय का अर्थ है तत्त्वश्रद्धान। अहिंसा सर्वज्ञ भगवान् के आदेशों पर श्रद्धापूर्वक विचार करना, चिन्तन मनन करना, साक्षात्कार करना और उन्हें जीवन में आत्मसात् करना, व्यवहार में उतारना आज्ञाविचय में सम्मिलित है।
अपायविचय- अपायविचय में राग-द्वेष, क्रोध, कषाय, मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति आदि दोषों का निवारण करने के लिए उपायों का चिन्तन और उनके द्वारा दोषों का निवारण किया जाता है।
विपाकविचय-विपाकविचय धर्मध्यान में शुभ और अशुभ कार्यफलों का अनुभव करते हुए उनके कारणभूत कर्मों, भावनाओं तक का अनुसन्धान करके साधक उनसे मुक्त होने के लिए क्रमशः गुणस्थानों में आरोहण करते हुए, आत्मा से कर्म सम्बन्ध के विच्छेद के लिए चिन्तन करते हुए तदनुकूल साधना करता है।
संस्थानविचय- चतुर्थ धर्मध्यान संस्थानविचय की साधना में ध्यानयोगी लोक के स्वरूप, छः द्रव्यों के गुण-पर्याय, संसार, द्रव्यों के उत्पाद- ध्रौव्य-व्यय, लोक की शाश्वतता और अशाश्वतता, द्रव्य की परिणामी नित्यता, जीव की देव, मनुष्य, नारक और तिर्यञ्च गति आदि का चिन्तन करके आत्मशुद्धि करता है।
धर्मध्यान की इस साधना में वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और धर्मकथा ये चार आलम्बन होते हैं एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और संसारानुप्रेक्षा धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं हैं, जिनके माध्यम से ध्यानयोगी तत्त्व साक्षात्कार तक पहुँचता है।
ध्यान के आलम्बन की दृष्टि से ध्यान के चार भेद हो सकते हैं-पिण्डस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान । इनके अतिरिक्त ध्येय की दृष्टि से योग की दृष्टि से भी ध्यान के अनेक भेद होते हैं। विस्तारभय से हम यहां उनकी चर्चा अथवा उनका परिचय नहीं दे रहे हैं।
Co
simp