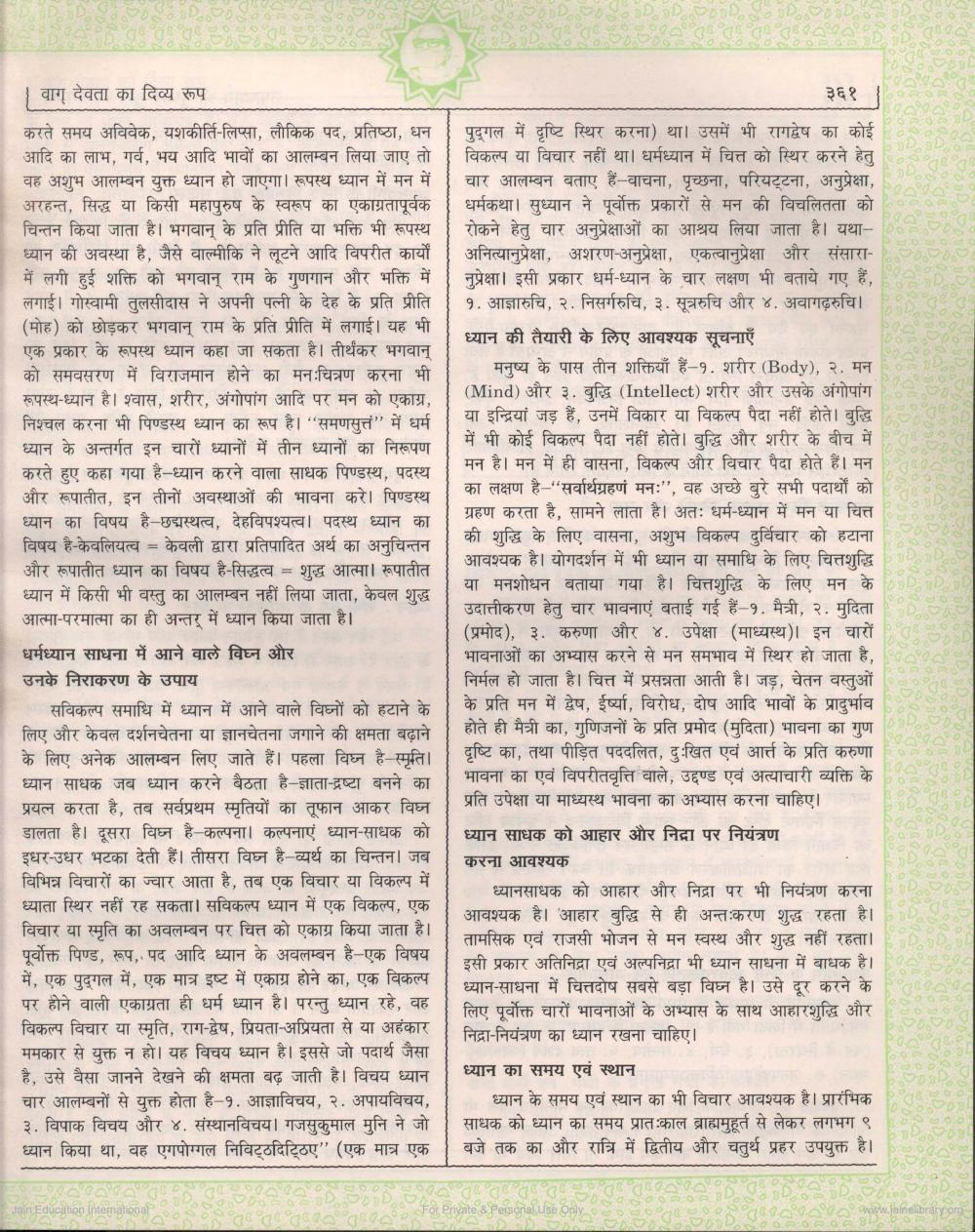________________
। वाग् देवता का दिव्य रूप
३६१ ।
करते समय अविवेक, यशकीर्ति-लिप्सा, लौकिक पद, प्रतिष्ठा, धन । पुद्गल में दृष्टि स्थिर करना) था। उसमें भी रागद्वेष का कोई आदि का लाभ, गर्व, भय आदि भावों का आलम्बन लिया जाए तो विकल्प या विचार नहीं था। धर्मध्यान में चित्त को स्थिर करने हेतु वह अशुभ आलम्बन युक्त ध्यान हो जाएगा। रूपस्थ ध्यान में मन में चार आलम्बन बताए हैं-वाचना, पृच्छना, परियट्टना, अनुप्रेक्षा, अरहन्त, सिद्ध या किसी महापुरुष के स्वरूप का एकाग्रतापूर्वक धर्मकथा। सुध्यान ने पूर्वोक्त प्रकारों से मन की विचलितता को चिन्तन किया जाता है। भगवान् के प्रति प्रीति या भक्ति भी रूपस्थ रोकने हेतु चार अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लिया जाता है। यथाध्यान की अवस्था है, जैसे वाल्मीकि ने लूटने आदि विपरीत कार्यों अनित्यानुप्रेक्षा, अशरण-अनुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा और संसारामें लगी हुई शक्ति को भगवान् राम के गुणगान और भक्ति में | नुप्रेक्षा। इसी प्रकार धर्म-ध्यान के चार लक्षण भी बताये गए हैं, लगाई। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी पत्नी के देह के प्रति प्रीति १. आज्ञारुचि, २. निसर्गरुचि, ३. सूत्ररुचि और ४. अवागढ़रुचि। (मोह) को छोड़कर भगवान् राम के प्रति प्रीति में लगाई। यह भी
ध्यान की तैयारी के लिए आवश्यक सूचनाएँ एक प्रकार के रूपस्थ ध्यान कहा जा सकता है। तीर्थंकर भगवान् को समवसरण में विराजमान होने का मनःचित्रण करना भी
मनुष्य के पास तीन शक्तियाँ हैं-१. शरीर (Body), २. मन रूपस्थ-ध्यान है। श्वास, शरीर, अंगोपांग आदि पर मन को एकाग्र,
(Mind) और ३. बुद्धि (Intellect) शरीर और उसके अंगोपांग निश्चल करना भी पिण्डस्थ ध्यान का रूप है। “समणसुत्तं" में धर्म
या इन्द्रियां जड़ हैं, उनमें विकार या विकल्प पैदा नहीं होते। बुद्धि ध्यान के अन्तर्गत इन चारों ध्यानों में तीन ध्यानों का निरूपण
में भी कोई विकल्प पैदा नहीं होते। बुद्धि और शरीर के बीच में करते हुए कहा गया है-ध्यान करने वाला साधक पिण्डस्थ, पदस्थ
मन है। मन में ही वासना, विकल्प और विचार पैदा होते हैं। मन और रूपातीत, इन तीनों अवस्थाओं की भावना करे। पिण्डस्थ
का लक्षण है-“सर्वार्थग्रहणं मनः", वह अच्छे बुरे सभी पदार्थों को ध्यान का विषय है-छद्मस्थत्व, देहविपश्यत्व। पदस्थ ध्यान का
ग्रहण करता है, सामने लाता है। अतः धर्म-ध्यान में मन या चित्त विषय है-केवलियत्व = केवली द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनुचिन्तन
की शुद्धि के लिए वासना, अशुभ विकल्प दुर्विचार को हटाना और रूपातीत ध्यान का विषय है-सिद्धत्व = शुद्ध आत्मा। रूपातीत
आवश्यक है। योगदर्शन में भी ध्यान या समाधि के लिए चित्तशुद्धि ध्यान में किसी भी वस्तु का आलम्बन नहीं लिया जाता, केवल शुद्ध
या मनशोधन बताया गया है। चित्तशुद्धि के लिए मन के आत्मा-परमात्मा का ही अन्तर में ध्यान किया जाता है।
उदात्तीकरण हेतु चार भावनाएं बताई गई हैं-१. मैत्री, २. मुदिता
(प्रमोद), ३. करुणा और ४. उपेक्षा (माध्यस्थ)। इन चारों धर्मध्यान साधना में आने वाले विघ्न और
भावनाओं का अभ्यास करने से मन समभाव में स्थिर हो जाता है, उनके निराकरण के उपाय
निर्मल हो जाता है। चित्त में प्रसन्नता आती है। जड़, चेतन वस्तुओं सविकल्प समाधि में ध्यान में आने वाले विघ्नों को हटाने के के प्रति मन में द्वेष, ईर्ष्या, विरोध, दोष आदि भावों के प्रादुर्भाव लिए और केवल दर्शनचेतना या ज्ञानचेतना जगाने की क्षमता बढ़ाने
होते ही मैत्री का, गुणिजनों के प्रति प्रमोद (मुदिता) भावना का गुण के लिए अनेक आलम्बन लिए जाते हैं। पहला विघ्न है-स्मृति।
दृष्टि का, तथा पीड़ित पददलित, दुःखित एवं आर्त्त के प्रति करुणा ध्यान साधक जब ध्यान करने बैठता है-ज्ञाता-द्रष्टा बनने का
भावना का एवं विपरीतवृत्ति वाले, उद्दण्ड एवं अत्याचारी व्यक्ति के प्रयत्न करता है, तब सर्वप्रथम स्मृतियों का तूफान आकर विघ्न
प्रति उपेक्षा या माध्यस्थ भावना का अभ्यास करना चाहिए। डालता है। दूसरा विघ्न है-कल्पना। कल्पनाएं ध्यान-साधक को ध्यान साधक को आहार और निद्रा पर नियंत्रण इधर-उधर भटका देती हैं। तीसरा विघ्न है-व्यर्थ का चिन्तन। जब
करना आवश्यक विभिन्न विचारों का ज्वार आता है, तब एक विचार या विकल्प में
ध्यानसाधक को आहार और निद्रा पर भी नियंत्रण करना ध्याता स्थिर नहीं रह सकता। सविकल्प ध्यान में एक विकल्प, एक
आवश्यक है। आहार बुद्धि से ही अन्तःकरण शुद्ध रहता है। विचार या स्मृति का अवलम्बन पर चित्त को एकाग्र किया जाता है।
तामसिक एवं राजसी भोजन से मन स्वस्थ और शुद्ध नहीं रहता। पूर्वोक्त पिण्ड, रूप, पद आदि ध्यान के अवलम्बन है-एक विषय
इसी प्रकार अतिनिद्रा एवं अल्पनिद्रा भी ध्यान साधना में बाधक है। में, एक पुद्गल में, एक मात्र इष्ट में एकाग्र होने का, एक विकल्प
ध्यान-साधना में चित्तदोष सबसे बड़ा विघ्न है। उसे दूर करने के पर होने वाली एकाग्रता ही धर्म ध्यान है। परन्तु ध्यान रहे, वह
लिए पूर्वोक्त चारों भावनाओं के अभ्यास के साथ आहारशुद्धि और विकल्प विचार या स्मृति, राग-द्वेष, प्रियता-अप्रियता से या अहंकार
निद्रा-नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। ममकार से युक्त न हो। यह विचय ध्यान है। इससे जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा जानने देखने की क्षमता बढ़ जाती है। विचय ध्यान
ध्यान का समय एवं स्थान चार आलम्बनों से युक्त होता है-१. आज्ञाविचय, २. अपायविचय, ध्यान के समय एवं स्थान का भी विचार आवश्यक है। प्रारंभिक ३. विपाक विचय और ४. संस्थानविचय। गजसुकुमाल मुनि ने जो साधक को ध्यान का समय प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त से लेकर लगभग ९ ध्यान किया था, वह एगपोग्गल निविट्ठदिट्ठिए" (एक मात्र एक बजे तक का और रात्रि में द्वितीय और चतुर्थ प्रहर उपयुक्त है।
56002050566
009
2
उ
EGGS696FI0
हरकताDJanpooo FREnate a personal usedyo20000 0 000 6 00CRICAN
D ONESISoon
JainEducation intematioga66569